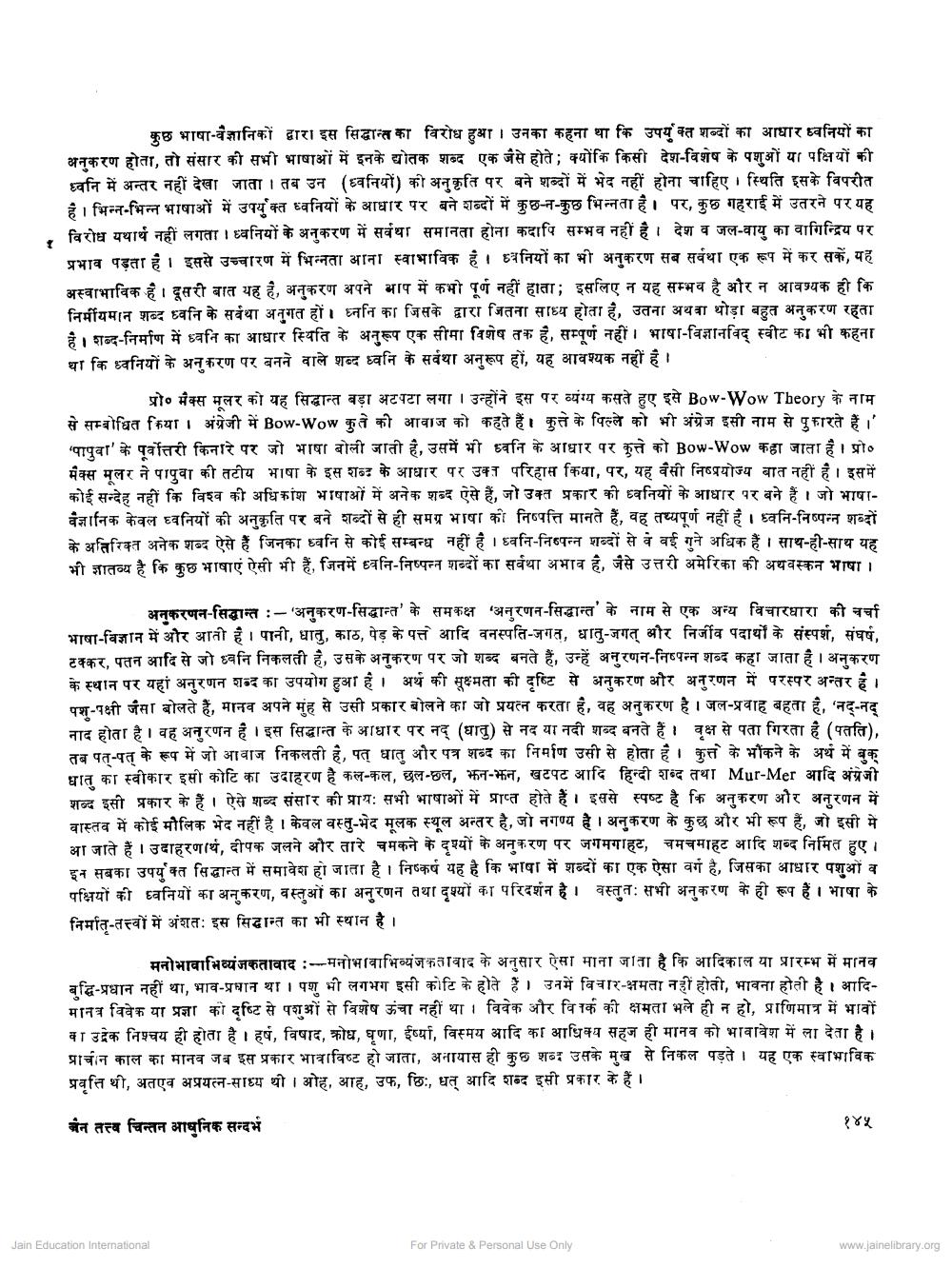________________
कुछ भाषा-वैज्ञानिकों द्वारा इस सिद्धान्त का विरोध हुआ। उनका कहना था कि उपर्युक्त शब्दों का आधार ध्वनियों का अनुकरण होता, तो संसार की सभी भाषाओं में इनके द्योतक शब्द एक जैसे होते; क्योंकि किसी देश-विशेष के पशुओं या पक्षियों की ध्वनि में अन्तर नहीं देखा जाता । तब उन (ध्वनियों) की अनुकृति पर बने शब्दों में भेद नहीं होना चाहिए। स्थिति इसके विपरीत है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपर्युक्त ध्वनियों के आधार पर बने शब्दों में कुछ-न-कुछ भिन्नता है। पर, कुछ गहराई में उतरने पर यह विरोध यथार्थ नहीं लगता। ध्वनियों के अनुकरण में सर्वथा समानता होना कदापि सम्भव नहीं है। देश व जल-वायु का वागिन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है। इससे उच्चारण में भिन्नता आना स्वाभाविक है। ध्वनियों का भी अनुकरण सब सर्वथा एक रूप में कर सकें, यह अस्वाभाविक है। दूसरी बात यह है, अनुकरण अपने भाप में कभी पूर्ण नहीं हाता; इसलिए न यह सम्भव है और न आवश्यक ही कि निर्मीयमान शब्द ध्वनि के सर्वथा अनुगत हों। ध्ननि का जिसके द्वारा जितना साध्य होता है, उतना अथवा थोड़ा बहुत अनुकरण रहता है। शब्द-निर्माण में ध्वनि का आधार स्थिति के अनुरूप एक सीमा विशेष तक है, सम्पूर्ण नहीं। भाषा-विज्ञानविद् स्वीट का भी कहना था कि ध्वनियों के अनुकरण पर बनने वाले शब्द ध्वनि के सर्वथा अनुरूप हों, यह आवश्यक नहीं है।
प्रो० मैक्स मूलर को यह सिद्धान्त बड़ा अटपटा लगा । उन्होंने इस पर व्यंग्य कसते हुए इसे Bow-Wow Theory के नाम से सम्बोधित किया। अंग्रेजी में Bow-Wow कुते की आवाज को कहते हैं। कुत्ते के पिल्ले को भी अंग्रेज इसी नाम से पुकारते हैं।' 'पापूवा' के पूर्वोत्तरी किनारे पर जो भाषा बोली जाती है, उसमें भी ध्वनि के आधार पर कुत्ते को Bow-Wow कहा जाता है। प्रो० मैक्स मूलर ने पापुवा की तटीय भाषा के इस शब्द के आधार पर उक्त परिहास किया, पर, यह वैसी निष्प्रयोज्य बात नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विश्व की अधिकांश भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो उक्त प्रकार की ध्वनियों के आधार पर बने हैं । जो भाषावैज्ञानिक केवल ध्वनियों की अनुकृति पर बने शब्दों से ही समग्र भाषा को निष्पत्ति मानते हैं, वह तथ्यपूर्ण नहीं है । ध्वनि-निष्पन्न शब्दों के अतिरिक्त अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्वनि-निष्पन्न शब्दों से वे वई गुने अधिक हैं। साथ-ही-साथ यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं, जिनमें ध्वनि-निष्पन्न शब्दों का सर्वथा अभाव है, जैसे उत्तरी अमेरिका की अथवस्कन भाषा ।
अनकरणन-सिद्धान्त :- 'अनुकरण-सिद्धान्त' के समकक्ष 'अनुरणन-सिद्धान्त' के नाम से एक अन्य विचारधारा की चर्चा भाषा-विज्ञान में और आती है। पानी, धातु, काठ, पेड़ के पत्ते आदि वनस्पति-जगत, धातु-जगत् और निर्जीव पदार्थों के संस्पर्श, संघर्ष, टक्कर, पतन आदि से जो ध्वनि निकलती है, उसके अनुकरण पर जो शब्द बनते हैं, उन्हें अनुरणन-निष्पन्न शब्द कहा जाता है । अनुकरण के स्थान पर यहां अनुरणन शब्द का उपयोग हुआ है। अर्थ की सूक्ष्मता की दृष्टि से अनुकरण और अनुरणन में परस्पर अन्तर है। पश-पक्षी जैसा बोलते हैं, मानव अपने मुंह से उसी प्रकार बोलने का जो प्रयत्न करता है, वह अनुकरण है । जल-प्रवाह बहता है, 'नद्-नद् नाद होता है। वह अनुरणन है । इस सिद्धान्त के आधार पर नद् (धातु) से नद या नदी शब्द बनते हैं। वृक्ष से पता गिरता है (पतति), तब पत-पत् के रूप में जो आवाज निकलती है, पत् धातु और पत्र शब्द का निर्माण उसी से होता है। कुत्ते के भौंकने के अर्थ में बक धात का स्वीकार इसी कोटि का उदाहरण है कल-कल, छल-छल, झन-झन, खटपट आदि हिन्दी शब्द तथा Mur-Mer आदि अंग्रेजी शब्द इसी प्रकार के हैं। ऐसे शब्द संसार की प्राय: सभी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुकरण और अनुरणन में वास्तव में कोई मौलिक भेद नहीं है । केवल वस्तु-भेद मूलक स्थूल अन्तर है, जो नगण्य है । अनुकरण के कुछ और भी रूप हैं, जो इसी में आ जाते हैं । उदाहरणार्थ, दीपक जलने और तारे चमकने के दृश्यों के अनुकरण पर जगमगाहट, चमचमाहट आदि शब्द निर्मित हए। इन सबका उपर्युक्त सिद्धान्त में समावेश हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि भाषा में शब्दों का एक ऐसा वर्ग है, जिसका आधार पशुओं व पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण, वस्तुओं का अनुरणन तथा दृश्यों का परिदर्शन है। वस्तुत: सभी अनुकरण के ही रूप हैं। भाषा के निर्मात-तत्त्वों में अंशतः इस सिद्धान्त का भी स्थान है।
मनोभावाभिव्यंजकतावाद :--मनोभावाभिव्यंजकतावाद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आदिकाल या प्रारम्भ में मानव बद्धि-प्रधान नहीं था, भाव-प्रधान था। पशु भी लगभग इसी कोटि के होते हैं। उनमें विचार-क्षमता नहीं होती, भावना होती है। आदिमानव विवेक या प्रज्ञा को दृष्टि से पशुओं से विशेष ऊंचा नहीं था। विवेक और वितर्क की क्षमता भले ही न हो, प्राणिमात्र में भावों का उद्रेक निश्चय ही होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय आदि का आधिक्य सहज ही मानव को भावावेश में ला देता है। प्राचीन काल का मानव जब इस प्रकार भावाविष्ट हो जाता, अनायास ही कुछ शब्द उसके मुख से निकल पड़ते। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतएव अप्रयत्न-साध्य थी । ओह, आह, उफ, छिः, धत् आदि शब्द इसी प्रकार के हैं ।
जन तत्त्व चिन्तन आधुनिक सन्दर्भ
१४५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org