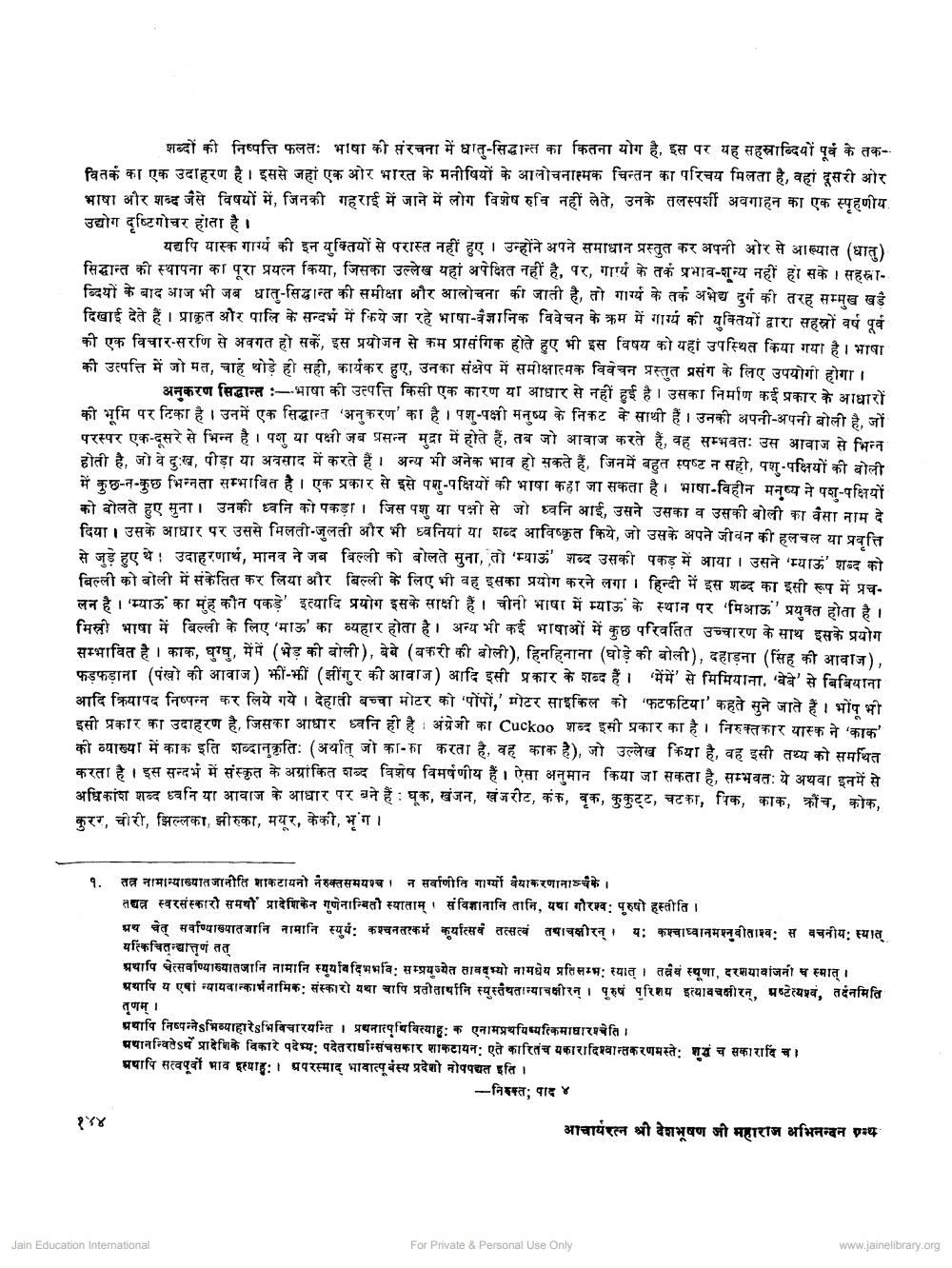________________
शब्दों की निष्पत्ति फलतः भाषा की संरचना में धातु-सिद्धान्त का कितना योग है, इस पर यह सहस्राब्दियों पूर्व के तकवितर्क का एक उदाहरण है। इससे जहां एक ओर भारत के मनीषियों के आलोचनात्मक चिन्तन का परिचय मिलता है, वहां दूसरी ओर भाषा और शब्द जैसे विषयों में, जिनकी गहराई में जाने में लोग विशेष रुचि नहीं लेते, उनके तलस्पर्शी अवगाहन का एक स्पृहणीय उद्योग दृष्टिगोचर होता है।
यद्यपि यास्क गार्य की इन युक्तियों से परास्त नहीं हुए। उन्होंने अपने समाधान प्रस्तुत कर अपनी ओर से आख्यात (धातु) सिद्धान्त की स्थापना का पूरा प्रयत्न किया, जिसका उल्लेख यहां अपेक्षित नहीं है, पर, गार्य के तर्क प्रभाव-शून्य नहीं हो सके । सहस्राब्दियों के बाद आज भी जब धात-सिद्धान्त की समीक्षा और आलोचना की जाती है, तो गाये के तर्क अभेद्य दुर्ग की तरह सम्मख खडे दिखाई देते हैं । प्राकृत और पालि के सन्दर्भ में किये जा रहे भाषा-वैज्ञानिक विवेचन के क्रम में गाय की युक्तियों द्वारा सहस्रों वर्ष पूर्व की एक विचार-सरणि से अवगत हो सकें, इस प्रयोजन से कम प्रासंगिक होते हुए भी इस विषय को यहां उपस्थित किया गया है। भाषा की उत्पत्ति में जो मत, चाह थोड़े ही सही, कार्यकर हुए, उनका संक्षेप में समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रसंग के लिए उपयोगी होगा।
अनुकरण सिद्धान्त :-भाषा की उत्पत्ति किसी एक कारण या आधार से नहीं हुई है। उसका निर्माण कई प्रकार के आधारों की भूमि पर टिका है । उनमें एक सिद्धान्त 'अनुकरण' का है । पशु-पक्षी मनुष्य के निकट के साथी हैं। उनकी अपनी-अपनी बोली है. जों परस्पर एक-दूसरे से भिन्न है । पशु या पक्षी जब प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तब जो आवाज करते हैं, वह सम्भवतः उस आवाज से भिन्न होती है, जो वे दुःख, पीड़ा या अवसाद में करते हैं। अन्य भी अनेक भाव हो सकते हैं, जिनमें बहुत स्पष्ट न सही, पशु-पक्षियों की बोली में कुछ-न-कुछ भिन्नता सम्भावित है। एक प्रकार से इसे पशु-पक्षियों की भाषा कहा जा सकता है। भाषा-विहीन मनुष्य ने पश-पक्षियों को बोलते हुए सुना। उनकी ध्वनि को पकड़ा। जिस पशु या पक्षो से जो ध्वनि आई, उसने उसका व उसकी बोली का वैसा नाम दे दिया। उसके आधार पर उससे मिलती-जुलती और भी ध्वनियां या शब्द आविष्कृत किये, जो उसके अपने जीवन की हलचल या प्रवत्ति से जड़े हुए थे। उदाहरणार्थ, मानव ने जब बिल्ली को बोलते सुना, तो 'म्याऊँ' शब्द उसकी पकड़ में आया। उसने 'म्याऊं' शब्द को नितीको बोली में संकेतित कर लिया और बिल्ली के लिए भी वह इसका प्रयोग करने लगा। हिन्दी में इस शब्द का इसी रूप में प्रचलन है । 'म्याऊ का मंह कौन पकड़े' इत्यादि प्रयोग इसके साक्षी हैं। चीनी भाषा में म्याऊ के स्थान पर मिआऊ' प्रयक्त होता है। मिस्री भाषा में बिल्ली के लिए 'माऊ' का व्यहार होता है। अन्य भी कई भाषाओं में कुछ परिवर्तित उच्चारण के साथ इसके प्रयोग सम्भावित है । काक, घुग्घु, में में (भेड़ की बोली), बेबे (बकरी की बोली), हिनहिनाना (घोड़े की बोली), दहाड़ना (सिंह की आवाज). फड़फड़ाना (पंखो की आवाज) झी-झी (झींगुर की आवाज) आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। मेंमें' से मिमियाना, 'बेबे' से बिबियाना आदि क्रियापद निष्पन्न कर लिये गये । देहाती बच्चा मोटर को 'पोपों,' मोटर साइकिल को 'फटफटिया' कहते सुने जाते हैं। भोप भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसका आधार ध्वनि ही है । अंग्रेजी का Cuckoo शब्द इसी प्रकार का है। निरुक्तकार यास्क ने 'काक' की व्याख्या में काक इति शब्दानुकृतिः (अर्थात् जो का-का करता है, वह काक है), जो उल्लेख किया है, वह इसी तथ्य को समर्थित करता है । इस सन्दर्भ में संस्कृत के अग्रांकित शब्द विशेष विमर्षणीय हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है, सम्भवतः ये अथवा इनमें से अधिकांश शब्द ध्वनि या आवाज के आधार पर बने हैं : घूक, खंजन, खंजरीट, कंक, बृक, कुकुट्ट, चटका, पिक, काक, क्रौंच, कोक, कुरर, चीरी, झिल्लका, झीरुका, मयूर, केकी, भृग।
१. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नरुक्तसमयश्च । न सर्वाणीति गार्यो वैयाकरणानाचके।
तधन स्वरसंस्कारी समथों प्रादेशिकेन गुणेनान्विती स्याताम् । संविज्ञानानि तानि, यथा गौरश्व: पुरुषो हस्तीति । प्रथ चेत् सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्यः कश्चनतत्कर्म कुर्यात्सर्व तत्सत्वं तथाचक्षीरन्। यः कश्चाघ्वानमश्न बीताश्वः स वचनीय: स्यात् यत्किचितन्द्यात्तुणं तत् प्रथापि चेत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्यावदिभविः सम्प्रयुज्येत तावद्भ्यो नामधेय प्रति सम्म: स्यात् । तवं स्थूणा, दरयावांजनी च स्मात् । प्रथापि य एषां न्यायवान्काभेनामिक: संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथतान्याचक्षीरन् । पुरुषं परिशय इत्यावचक्षीरन्, प्रष्टेत्यश्वं, तदनमिति तृणम् । प्रथापि निष्पन्न भिव्याहारेऽभिविचारयन्ति । प्रथनात्पपिवित्याहः क एनामप्रथयिष्यरिकमाघारपचेति। प्रथानन्वितेय प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धासंघसकार शाकटायन: एते कारितंच यकारादिश्वान्तकरणमस्ते: शुखं च सकारादि च। प्रथापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहुः। प्रपरस्माद् भावात्पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति ।
-निरुक्त; पाद४
आचार्यरत्न श्री वेशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रस्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org