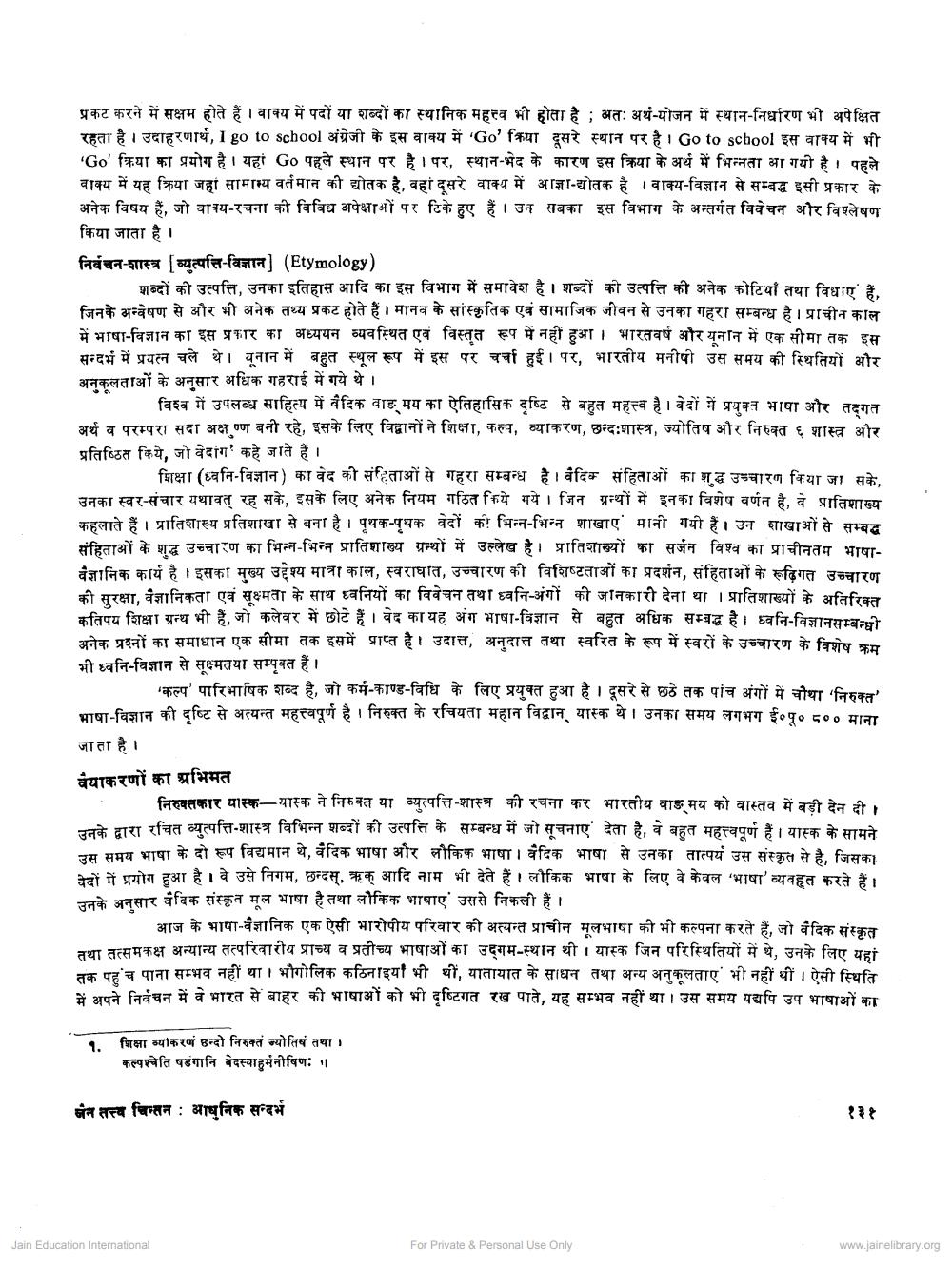________________
.
.
प्रकट करने में सक्षम होते हैं । वाक्य में पदों या शब्दों का स्थानिक महत्त्व भी होता है ; अतः अर्थ-योजन में स्थान-निर्धारण भी अपेक्षित रहता है। उदाहरणार्थ, I go to school अंग्रेजी के इस वाक्य में 'Go' क्रिया दूसरे स्थान पर है। Go to school इस वाक्य में भी 'Go' क्रिया का प्रयोग है। यहां Go पहले स्थान पर है। पर, स्थान-भेद के कारण इस क्रिया के अर्थ में भिन्नता आ गयी है। पहले वाक्य में यह क्रिया जहा सामान्य वर्तमान की द्योतक है, वहां दूसरे वाक्य में आज्ञा-द्योतक है । वाक्य-विज्ञान से सम्बद्ध इसी प्रकार के अनेक विषय हैं, जो वाक्य-रचना की विविध अपेक्षाओं पर टिके हुए हैं। उन सबका इस विभाग के अन्तर्गत विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। निर्वचन-शास्त्र [व्युत्पत्ति-विज्ञान] (Etymology)
शब्दों की उत्पत्ति, उनका इतिहास आदि का इस विभाग में समावेश है। शब्दों की उत्पत्ति की अनेक कोटियाँ तथा विधाए हैं, जिनके अन्वेषण से और भी अनेक तथ्य प्रकट होते हैं। मानव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है। प्राचीन काल में भाषा-विज्ञान का इस प्रकार का अध्ययन व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप में नहीं हुआ। भारतवर्ष और यूनान में एक सीमा तक इस सन्दर्भ में प्रयत्न चले थे। यूनान में बहुत स्थूल रूप में इस पर चर्चा हुई। पर, भारतीय मनीषी उस समय की स्थितियों और अनुकूलताओं के अनुसार अधिक गहराई में गये थे।
" विश्व में उपलब्ध साहित्य में वैदिक वाङ्मय का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है । वेदों में प्रयुक्त भाषा और तद्गत अर्थ व परम्परा सदा अक्षण्ण बनी रहे, इसके लिए विद्वानों ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दःशास्त्र, ज्योतिष और निरुक्त ६ शास्त्र और प्रतिष्ठित किये, जो वेदांग' कहे जाते हैं।
शिक्षा (ध्वनि-विज्ञान) का वेद की संहिताओं से गहरा सम्बन्ध है। वैदिक संहिताओं का शुद्ध उच्चारण किया जा सके, उनका स्वर-संचार यथावत् रह सके, इसके लिए अनेक नियम गठित किये गये। जिन ग्रन्थों में इनका विशेष वर्णन है, वे प्रातिशाख्य कहलाते हैं। प्रातिशाख्य प्रतिशाखा से बना है। पृथक-पृथक वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाएं मानी गयी हैं। उन शाखाओं से सम्बद्ध संहिताओं के शद्ध उच्चारण का भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उल्लेख है। प्रातिशाख्यों का सर्जन विश्व का प्राचीनतम भाषावैज्ञानिक कार्य है । इसका मुख्य उद्देश्य मात्रा काल, स्वराघात, उच्चारण की विशिष्टताओं का प्रदर्शन, संहिताओं के रूविगत उमार की सरक्षा. वैज्ञानिकता एवं सूक्ष्मता के साथ ध्वनियों का विवेचन तथा ध्वनि-अंगों की जानकारी देना था । प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त कतिपय शिक्षा ग्रन्थ भी हैं, जो कलेवर में छोटे हैं । वेद का यह अंग भाषा-विज्ञान से बहुत अधिक सम्बद्ध है। ध्वनि-विज्ञानसम्बन्धी अनेक प्रश्नों का समाधान एक सीमा तक इसमें प्राप्त है। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के रूप में स्वरों के उच्चारण के विशेष क्रम भी ध्वनि-विज्ञान से सूक्ष्मतया सम्पृक्त हैं।
'कल्प' पारिभाषिक शब्द है, जो कर्म-काण्ड-विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है । दूसरे से छठे तक पांच अंगों में चौथा निरुक्त' भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । निरुक्त के रचियता महान विद्वान यास्क थे। उनका समय लगभग ई०प०८०० माना जाता है। वैयाकरणों का अभिमत
निरुक्तकार यास्क-यास्क ने निरुक्त या व्युत्पत्ति-शास्त्र की रचना कर भारतीय वाङमय को वास्तव में बड़ी देन दी। उनके द्वारा रचित व्युत्पत्ति-शास्त्र विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सूचनाएं देता है, वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यास्क के सामने
म समय भाषा के दो रूप विद्यमान थे, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। वैदिक भाषा से उनका तात्पर्य उस संस्कृत से है, जिसका बेटों में प्रयोग हआ है। वे उसे निगम, छन्दस्, ऋक् आदि नाम भी देते हैं। लौकिक भाषा के लिए वे केवल 'भाषा' व्यवहृत करते हैं। उनके अनसार वैदिक संस्कृत मूल भाषा है तथा लौकिक भाषाएं उससे निकली हैं।
आज के भाषा-वैज्ञानिक एक ऐसी भारोपीय परिवार की अत्यन्त प्राचीन मूलभाषा की भी कल्पना करते हैं, जो वैदिक संस्कृत तथा तत्समकक्ष अन्यान्य तत्परिवारीय प्राच्य व प्रतीच्य भाषाओं का उद्गम-स्थान थी । यास्क जिन परिस्थितियों में थे, उनके लिए यहां तक पहच पाना सम्भव नहीं था। भौगोलिक कठिनाइयां भी थीं, यातायात के साधन तथा अन्य अनुकूलताएं भी नहीं थीं । ऐसी स्थिति से अपने निर्वचन में वे भारत से बाहर की भाषाओं को भी दृष्टिगत रख पाते, यह सम्भव नहीं था। उस समय यद्यपि उप भाषाओं का
१.
शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा । कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः ।।
जन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org