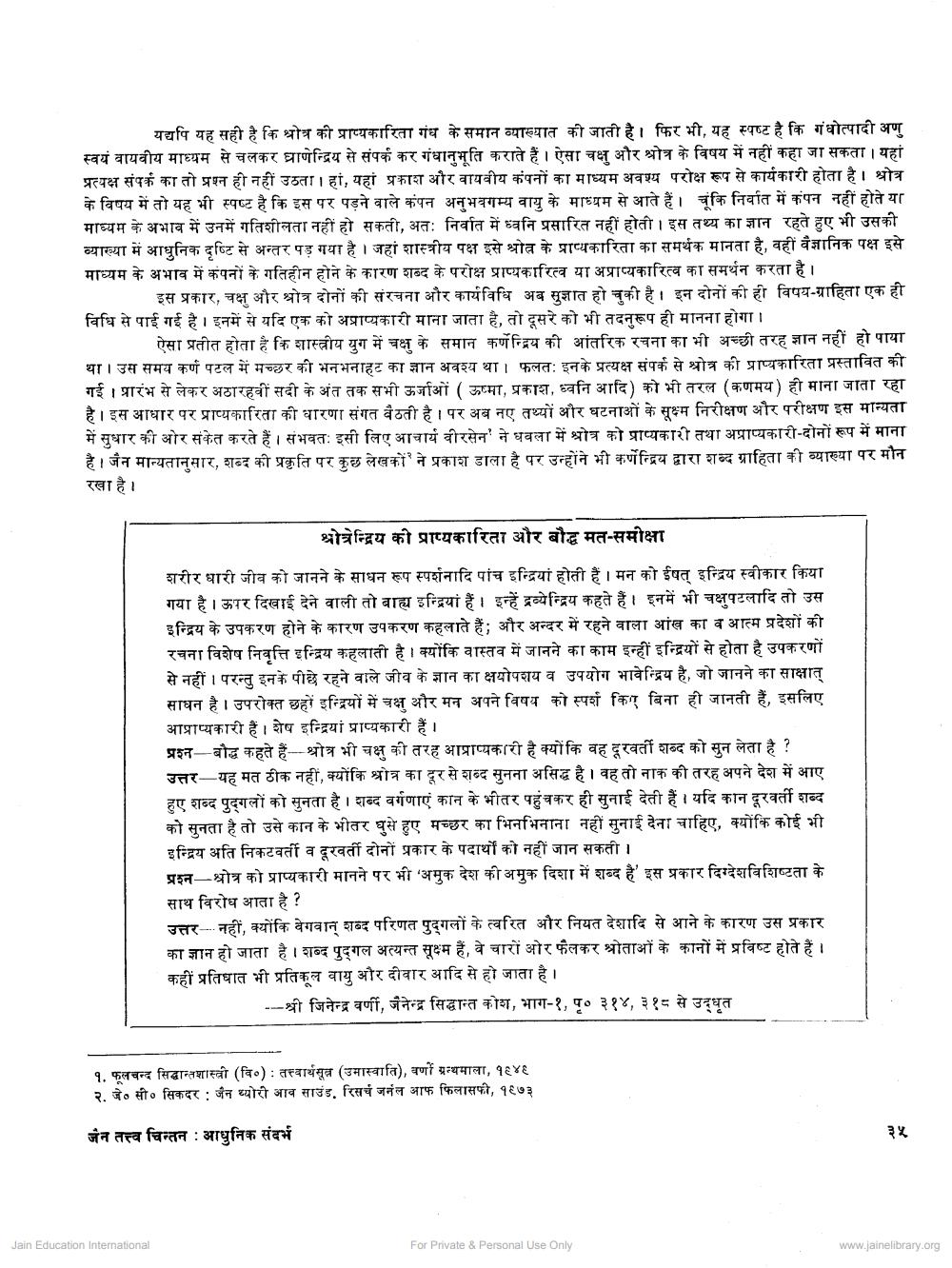________________
यद्यपि यह सही है कि श्रोत्र की प्राप्यकारिता गंध के समान व्याख्यात की जाती है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि गंधोत्पादी अणु स्वयं वायवीय माध्यम से चलकर घ्राणेन्द्रिय से संपर्क कर गंधानुभूति कराते हैं। ऐसा चक्षु और श्रोत्र के विषय में नहीं कहा जा सकता। यहां प्रत्यक्ष संपर्क का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हां, यहां प्रकाश और वायवीय कंपनों का माध्यम अवश्य परोक्ष रूप से कार्यकारी होता है। श्रोत्र के विषय में तो यह भी स्पष्ट है कि इस पर पड़ने वाले कंपन अनुभवगम्य वायु के माध्यम से आते हैं। चूंकि निर्वात में कंपन नहीं होते या माध्यम के अभाव में उनमें गतिशीलता नहीं हो सकती, अत: निर्वात में ध्वनि प्रसारित नहीं होती। इस तथ्य का ज्ञान रहते हुए भी उसकी व्याख्या में आधुनिक दृष्टि से अन्तर पड़ गया है। जहां शास्त्रीय पक्ष इसे श्रोत्र के प्राप्यकारिता का समर्थक मानता है, वहीं वैज्ञानिक पक्ष इसे माध्यम के अभाव में कंपनों के गतिहीन होने के कारण शब्द के परोक्ष प्राप्यकारित्व या अप्राप्यकारित्व का समर्थन करता है।
इस प्रकार, चक्ष और श्रोत्र दोनों की संरचना और कार्यविधि अब सुज्ञात हो चुकी है। इन दोनों की ही विषय-ग्राहिता एक ही विधि से पाई गई है। इनमें से यदि एक को अप्राप्यकारी माना जाता है, तो दूसरे को भी तदनुरूप ही मानना होगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रीय युग में चक्षु के समान कर्णेन्द्रिय की आंतरिक रचना का भी अच्छी तरह ज्ञान नहीं हो पाया था। उस समय कर्ण पटल में मच्छर की भनभनाहट का ज्ञान अवश्य था। फलत: इनके प्रत्यक्ष संपर्क से श्रोत्र की प्राप्यकारिता प्रस्तावित की गई। प्रारंभ से लेकर अठारहवीं सदी के अंत तक सभी ऊर्जाओं (ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि) को भी तरल (कणमय) ही माना जाता रहा है। इस आधार पर प्राप्यकारिता की धारणा संगत बैठती है। पर अब नए तथ्यों और घटनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण इस मान्यता में सुधार की ओर संकेत करते हैं। संभवतः इसी लिए आचार्य वीरसेन ने धवला में श्रोत्र को प्राप्यकारी तथा अप्राप्यकारी-दोनों रूप में माना है। जन मान्यतानुसार, शब्द की प्रकृति पर कुछ लेखकों ने प्रकाश डाला है पर उन्होंने भी कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द ग्राहिता की व्याख्या पर मौन रखा है।
श्रोत्रेन्द्रिय की प्राप्यकारिता और बौद्ध मत-समीक्षा
शरीर धारी जीव को जानने के साधन रूप स्पर्शनादि पांच इन्द्रियां होती हैं। मन को ईषत् इन्द्रिय स्वीकार किया गया है। ऊपर दिखाई देने वाली तो बाह्य इन्द्रियां हैं। इन्हें द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। इनमें भी चक्षुपटलादि तो उस इन्द्रिय के उपकरण होने के कारण उपकरण कहलाते हैं; और अन्दर में रहने वाला आंख का व आत्म प्रदेशों की रचना विशेष निवृत्ति इन्द्रिय कहलाती है। क्योंकि वास्तव में जानने का काम इन्हीं इन्द्रियों से होता है उपकरणों से नहीं । परन्तु इनके पीछे रहने वाले जीव के ज्ञान का क्षयोपशय व उपयोग भावेन्द्रिय है, जो जानने का साक्षात् साधन है। उपरोक्त छहों इन्द्रियों में चक्षु और मन अपने विषय को स्पर्श किए बिना ही जानती हैं, इसलिए आप्राप्यकारी हैं। शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। प्रश्न-बौद्ध कहते हैं-श्रोत्र भी चक्षु की तरह आप्राप्यकारी है क्योंकि वह दूरवर्ती शब्द को सुन लेता है ? उत्तर—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि श्रोत्र का दूर से शब्द सुनना असिद्ध है। वह तो नाक की तरह अपने देश में आए हुए शब्द पुद्गलों को सुनता है । शब्द वर्गणाएं कान के भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हैं। यदि कान दूरवर्ती शब्द को सुनता है तो उसे कान के भीतर घुसे हुए मच्छर का भिनभिनाना नहीं सुनाई देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती व दूरवर्ती दोनों प्रकार के पदार्थों को नहीं जान सकती। प्रश्न-श्रोत्र को प्राप्यकारी मानने पर भी 'अमुक देश की अमुक दिशा में शब्द है' इस प्रकार दिग्देशविशिष्टता के साथ विरोध आता है ? उत्तर--नहीं, क्योंकि वेगवान् शब्द परिणत पुद्गलों के त्वरित और नियत देशादि से आने के कारण उस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शब्द पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे चारों ओर फैलकर श्रोताओं के कानों में प्रविष्ट होते हैं। कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवार आदि से हो जाता है।
___---श्री जिनेन्द्र वर्णी, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग-१, पृ० ३१४, ३१८ से उद्धृत
१. फूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री (वि०) : तत्त्वार्थसूत्र (उमास्वाति), वर्णी ग्रन्थमाला, १९४६ २. जे० सी० सिकदर : जैन थ्योरी आव साउंड. रिसर्च जर्नल आफ फिलासफी, १६७३
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक संदर्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org