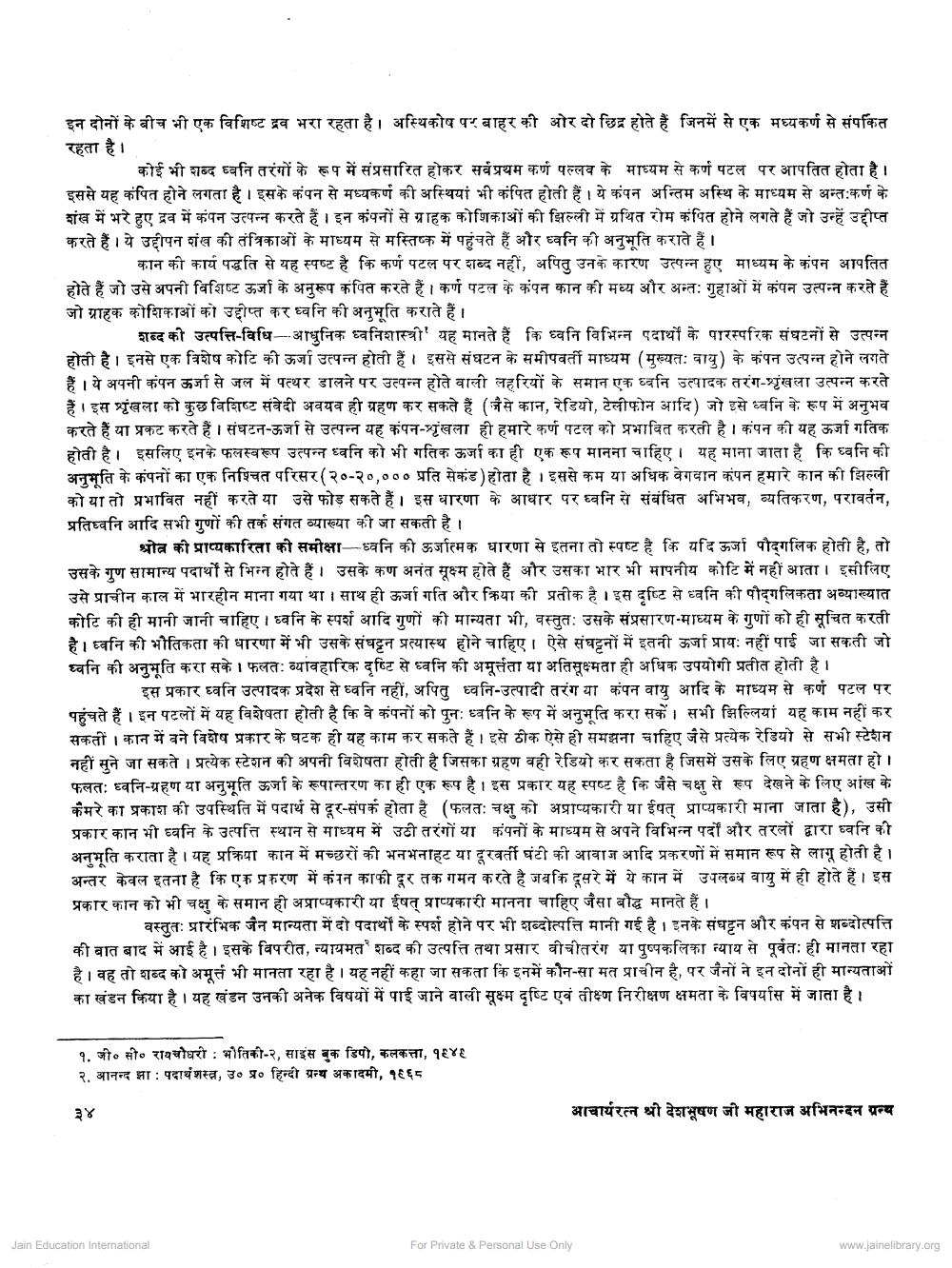________________
इन दोनों के बीच भी एक विशिष्ट द्रव भरा रहता है। अस्थिकोष पर बाहर की ओर दो छिद्र होते हैं जिनमें से एक मध्यकर्ण से संपकित रहता है।
कोई भी शब्द ध्वनि तरंगों के रूप में संप्रसारित होकर सर्वप्रथम कर्ण पल्लव के माध्यम से कर्ण पटल पर आपतित होता है। इससे यह कंपित होने लगता है। इसके कंपन से मध्यकर्ण की अस्थियां भी कंपित होती हैं । ये कंपन अन्तिम अस्थि के माध्यम से अन्त:कर्ण के शंख में भरे हुए द्रव में कंपन उत्पन्न करते हैं । इन कंपनों से ग्राहक कोशिकाओं की झिल्ली में ग्रथित रोम कंपित होने लगते हैं जो उन्हें उद्दीप्त करते हैं । ये उद्दीपन शंख की तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचते हैं और ध्वनि की अनुभूति कराते हैं।
कान की कार्य पद्धति से यह स्पष्ट है कि कर्ण पटल पर शब्द नहीं, अपितु उनके कारण उत्पन्न हुए माध्यम के कंपन आपतित होते हैं जो उसे अपनी विशिष्ट ऊर्जा के अनुरूप कपित करते हैं। कर्ण पटल के कंपन कान की मध्य और अन्त: गुहाओं में कंपन उत्पन्न करते हैं जो ग्राहक कोशिकाओं को उद्दीप्त कर ध्वनि की अनुभूति कराते हैं।
शब्द की उत्पत्ति-विधि-आधुनिक ध्वनिशास्त्री' यह मानते हैं कि ध्वनि विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संघटनों से उत्पन्न होती है। इनसे एक विशेष कोटि की ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। इससे संघटन के समीपवर्ती माध्यम (मुख्यतः वायु) के कंपन उत्पन्न होने लगते हैं । ये अपनी कंपन ऊर्जा से जल में पत्थर डालने पर उत्पन्न होते वाली लहरियों के समान एक ध्वनि उत्पादक तरंग-शृंखला उत्पन्न करते हैं । इस शृंखला को कुछ विशिष्ट संवेदी अवयव ही ग्रहण कर सकते हैं (जैसे कान, रेडियो, टेलीफोन आदि) जो इसे ध्वनि के रूप में अनुभव करते हैं या प्रकट करते हैं । संघटन-ऊर्जा से उत्पन्न यह कंपन-शृंखला ही हमारे कर्ण पटल को प्रभावित करती है। कंपन की यह ऊर्जा गतिक होती है। इसलिए इनके फलस्वरूप उत्पन्न ध्वनि को भी गतिक ऊर्जा का ही एक रूप मानना चाहिए। यह माना जाता है कि ध्वनि की अनुभूति के कंपनों का एक निश्चित परिसर (२०-२०,००० प्रति सेकंड) होता है । इससे कम या अधिक वेगवान कंपन हमारे कान की झिल्ली को या तो प्रभावित नहीं करते या उसे फोड़ सकते हैं। इस धारणा के आधार पर ध्वनि से संबंधित अभिभव, व्यतिकरण, परावर्तन, प्रतिध्वनि आदि सभी गुणों की तर्क संगत व्याख्या की जा सकती है।
श्रोत्र की प्राप्यकारिता की समीक्षा-ध्वनि की ऊर्जात्मक धारणा से इतना तो स्पष्ट है कि यदि ऊर्जा पौद्गलिक होती है, तो उसके गुण सामान्य पदार्थों से भिन्न होते हैं। उसके कण अनंत सूक्ष्म होते हैं और उसका भार भी मापनीय कोटि में नहीं आता। इसीलिए उसे प्राचीन काल में भारहीन माना गया था। साथ ही ऊर्जा गति और क्रिया की प्रतीक है । इस दृष्टि से ध्वनि की पौद्गलिकता अव्याख्यात कोटि की ही मानी जानी चाहिए। ध्वनि के स्पर्श आदि गुणों की मान्यता भी, वस्तुत: उसके संप्रसारण-माध्यम के गुणों को ही सूचित करती है। ध्वनि की भौतिकता की धारणा में भी उसके संघट्टन प्रत्यास्थ होने चाहिए। ऐसे संघटनों में इतनी ऊर्जा प्रायः नहीं पाई जा सकती जो ध्वनि की अनुभूति करा सके । फलतः व्यावहारिक दृष्टि से ध्वनि की अमूर्तता या अतिसूक्ष्मता ही अधिक उपयोगी प्रतीत होती है।
इस प्रकार ध्वनि उत्पादक प्रदेश से ध्वनि नहीं, अपितु ध्वनि-उत्पादी तरंग या कंपन वायु आदि के माध्यम से कर्ण पटल पर पहुंचते हैं। इन पटलों में यह विशेषता होती है कि वे कंपनों को पुन: ध्वनि के रूप में अनुभूति करा सकें। सभी झिल्लियां यह काम नहीं कर सकतीं। कान में बने विशेष प्रकार के घटक ही यह काम कर सकते हैं। इसे ठीक ऐसे ही समझना चाहिए जैसे प्रत्येक रेडियो से सभी स्टेशन नहीं सुने जा सकते । प्रत्येक स्टेशन को अपनी विशेषता होती है जिसका ग्रहण वही रेडियो कर सकता है जिसमें उसके लिए ग्रहण क्षमता हो। फलतः ध्वनि-ग्रहण या अनुभूति ऊर्जा के रूपान्तरण का ही एक रूप है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसे चक्षु से रूप देखने के लिए आंख के कैमरे का प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ से दूर-संपर्क होता है (फलतः चक्षु को अप्राप्यकारी या ईषत् प्राप्यकारी माना जाता है), उसी प्रकार कान भी ध्वनि के उत्पत्ति स्थान से माध्यम में उठी तरंगों या कंपनों के माध्यम से अपने विभिन्न पर्दो और तरलों द्वारा ध्वनि की अनुभूति कराता है। यह प्रक्रिया कान में मच्छरों की भनभनाहट या दूरवर्ती घंटी की आवाज आदि प्रकरणों में समान रूप से लागू होती है। अन्तर केवल इतना है कि एक प्रकरण में कंचन काफी दूर तक गमन करते है जबकि दूसरे में ये कान में उपलब्ध वायु में ही होते हैं। इस प्रकार कान को भी चक्षु के समान ही अप्राप्यकारी या ईषत् प्राप्यकारी मानना चाहिए जैसा बौद्ध मानते हैं।
वस्तुतः प्रारंभिक जैन मान्यता में दो पदार्थों के स्पर्श होने पर भी शब्दोत्पत्ति मानी गई है। इनके संघट्टन और कंपन से शब्दोत्पत्ति की बात बाद में आई है। इसके विपरीत, न्यायमत' शब्द की उत्पत्ति तथा प्रसार वीचीतरंग या पुष्पकलिका न्याय से पूर्वतः ही मानता रहा है। वह तो शब्द को अमूर्त भी मानता रहा है । यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन-सा मत प्राचीन है, पर जैनों ने इन दोनों ही मान्यताओं का खंडन किया है। यह खंडन उनकी अनेक विषयों में पाई जाने वाली सूक्ष्म दृष्टि एवं तीक्ष्ण निरीक्षण क्षमता के विपर्यास में जाता है।
१. जी० सी० रायचौधरी : भौतिकी-२, साइंस बुक डिपो, कलकत्ता, १९४६ २. आनन्द झा : पदार्थ शस्त्र, उ०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, १९६८
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org