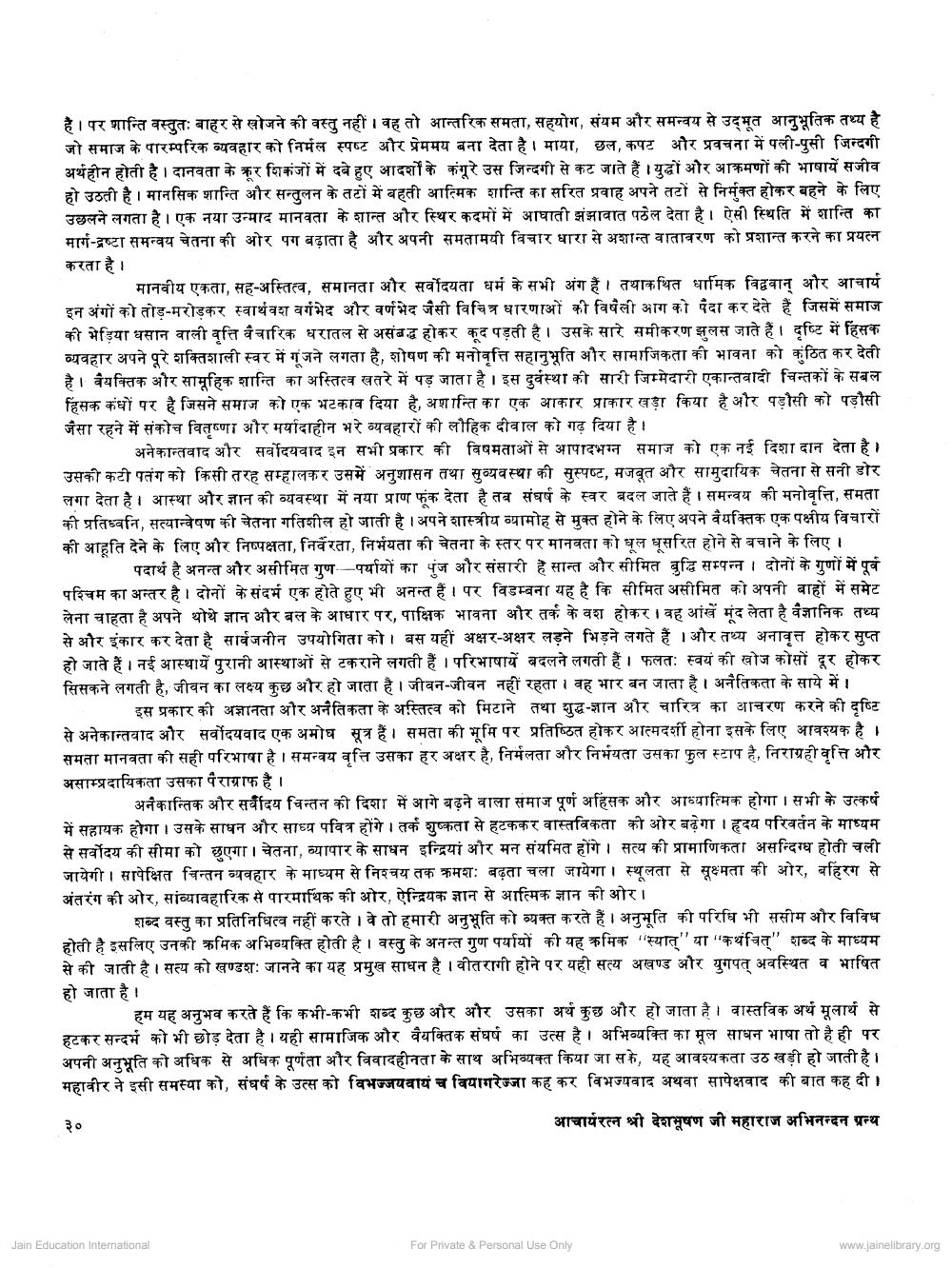________________
है। पर शान्ति वस्तुतः बाहर से खोजने की वस्तु नहीं। वह तो आन्तरिक समता, सहयोग, संयम और समन्वय से उद्भूत आनुभूतिक तथ्य है जो समाज के पारम्परिक व्यवहार को निर्मल स्पष्ट और प्रेममय बना देता है। माया, छल, कपट और प्रवचना में पली-पुसी जिन्दगी अर्थहीन होती है। दानवता के क्रूर शिकंजों में दबे हुए आदर्शों के कंगूरे उस जिन्दगी से कट जाते हैं । युद्धों और आक्रमणों की भाषायें सजीव हो उठती है। मानसिक शान्ति और सन्तुलन के तटों में बहती आत्मिक शान्ति का सरित प्रवाह अपने तटों से निर्मुक्त होकर बहने के लिए उछलने लगता है। एक नया उन्माद मानवता के शान्त और स्थिर कदमों में आघाती झंझावात पठेल देता है। ऐसी स्थिति में शान्ति का मार्ग-द्रष्टा समन्वय चेतना की ओर पग बढ़ाता है और अपनी समतामयी विचार धारा से अशान्त वातावरण को प्रशान्त करने का प्रयत्न करता है।
मानवीय एकता, सह-अस्तित्व, समानता और सर्वोदयता धर्म के सभी अंग हैं। तथाकथित धामिक विद्ववान् और आचार्य इन अंगों को तोड़-मरोड़कर स्वार्थवश वर्गभेद और वर्णभेद जैसी विचित्र धारणाओं की विषैली आग को पैदा कर देते हैं जिसमें समाज की भेड़िया धसान वाली वृत्ति वैचारिक धरातल से असंबद्ध होकर कूद पड़ती है। उसके सारे समीकरण झुलस जाते हैं। दृष्टि में हिंसक व्यवहार अपने पूरे शक्तिशाली स्वर में गूंजने लगता है, शोषण की मनोवृत्ति सहानुभूति और सामाजिकता की भावना को कुंठित कर देती है। वैयक्तिक और सामूहिक शान्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस दुर्वस्था की सारी जिम्मेदारी एकान्तवादी चिन्तकों के सबल हिंसक कंधों पर है जिसने समाज को एक भटकाव दिया है, अशान्ति का एक आकार प्राकार खड़ा किया है और पड़ोसी को पड़ोसी जैसा रहने में संकोच वितृष्णा और मर्यादाहीन भरे व्यवहारों की लौहिक दीवाल को गढ़ दिया है।
अनेकान्तवाद और सर्वोदयवाद इन सभी प्रकार की विषमताओं से आपादभग्न समाज को एक नई दिशा दान देता है। उसकी कटी पतंग को किसी तरह सम्हालकर उसमें अनुशासन तथा सुव्यवस्था की सुस्पष्ट, मजबूत और सामुदायिक चेतना से सनी डोर लगा देता है। आस्था और ज्ञान की व्यवस्था में नया प्राण फूंक देता है तब संघर्ष के स्वर बदल जाते हैं । समन्वय की मनोवृत्ति, समता की प्रतिध्वनि, सत्यान्वेषण की चेतना गतिशील हो जाती है । अपने शास्त्रीय व्यामोह से मुक्त होने के लिए अपने वैयक्तिक एक पक्षीय विचारों की आहूति देने के लिए और निष्पक्षता, निर्वैरता, निर्भयता की चेतना के स्तर पर मानवता को धूल धूसरित होने से बचाने के लिए।
पदार्थ है अनन्त और असीमित गुण–पर्यायों का पुंज और संसारी हे सान्त और सीमित बुद्धि सम्पन्न । दोनों के गुणों में पूर्व पश्चिम का अन्तर है। दोनों के संदर्भ एक होते हुए भी अनन्त हैं। पर विडम्बना यह है कि सीमित असीमित को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता है अपने थोथे ज्ञान और बल के आधार पर, पाक्षिक भावना और तर्क के वश होकर । वह आंखें मूंद लेता है वैज्ञानिक तथ्य से और इंकार कर देता है सार्वजनीन उपयोगिता को। बस यहीं अक्षर-अक्षर लड़ने भिड़ने लगते हैं । और तथ्य अनावृत्त होकर सुप्त हो जाते हैं। नई आस्थायें पुरानी आस्थाओं से टकराने लगती हैं । परिभाषायें बदलने लगती हैं। फलतः स्वयं की खोज कोसों दूर होकर सिसकने लगती है, जीवन का लक्ष्य कुछ और हो जाता है । जीवन-जीवन नहीं रहता । वह भार बन जाता है। अनैतिकता के साये में।
इस प्रकार की अज्ञानता और अनैतिकता के अस्तित्व को मिटाने तथा शुद्ध-ज्ञान और चारित्र का आचरण करने की दृष्टि से अनेकान्तवाद और सर्वोदयवाद एक अमोघ सूत्र हैं। समता की भूमि पर प्रतिष्ठित होकर आत्मदर्शी होना इसके लिए आवश्यक है । समता मानवता की सही परिभाषा है । समन्वय वृत्ति उसका हर अक्षर है, निर्मलता और निर्भयता उसका फुल स्टाप है, निराग्रही वृत्ति और असाम्प्रदायिकता उसका पैराग्राफ है ।
अनैकान्तिक और सर्वोदय चिन्तन की दिशा में आगे बढ़ने वाला समाज पूर्ण अहिंसक और आध्यात्मिक होगा। सभी के उत्कर्ष में सहायक होगा। उसके साधन और साध्य पवित्र होंगे। तर्क शुष्कता से हटककर वास्तविकता की ओर बढ़ेगा। हृदय परिवर्तन के माध्यम से सर्वोदय की सीमा को छुएगा। चेतना, व्यापार के साधन इन्द्रियां और मन संयमित होंगे। सत्य की प्रामाणिकता असन्दिग्ध होती चली जायेगी। सापेक्षित चिन्तन व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक क्रमशः बढ़ता चला जायेगा। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, बहिरग से अंतरंग की ओर, सांव्यावहारिक से पारमार्थिक की ओर, ऐन्द्रियक ज्ञान से आत्मिक ज्ञान की ओर।
__शब्द वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते । वे तो हमारी अनुभूति को व्यक्त करते हैं। अनुभूति की परिधि भी ससीम और विविध होती है इसलिए उनकी क्रमिक अभिव्यक्ति होती है । वस्तु के अनन्त गुण पर्यायों की यह क्रमिक "स्यात्" या "कथंचित्" शब्द के माध्यम से की जाती है । सत्य को खण्डशः जानने का यह प्रमुख साधन है । वीतरागी होने पर यही सत्य अखण्ड और युगपत् अवस्थित व भाषित हो जाता है।
हम यह अनुभव करते हैं कि कभी-कभी शब्द कुछ और और उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। वास्तविक अर्थ मूलार्थ से हटकर सन्दर्भ को भी छोड़ देता है। यही सामाजिक और वैयक्तिक संघर्ष का उत्स है। अभिव्यक्ति का मूल साधन भाषा तो है ही पर अपनी अनुभूति को अधिक से अधिक पूर्णता और विवादहीनता के साथ अभिव्यक्त किया जा सके, यह आवश्यकता उठ खड़ी हो जाती है। महावीर ने इसी समस्या को, संघर्ष के उत्स को विभज्जयवायं च वियागरेज्जा कह कर विभज्यवाद अथवा सापेक्षवाद की बात कह दी।
३०
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org