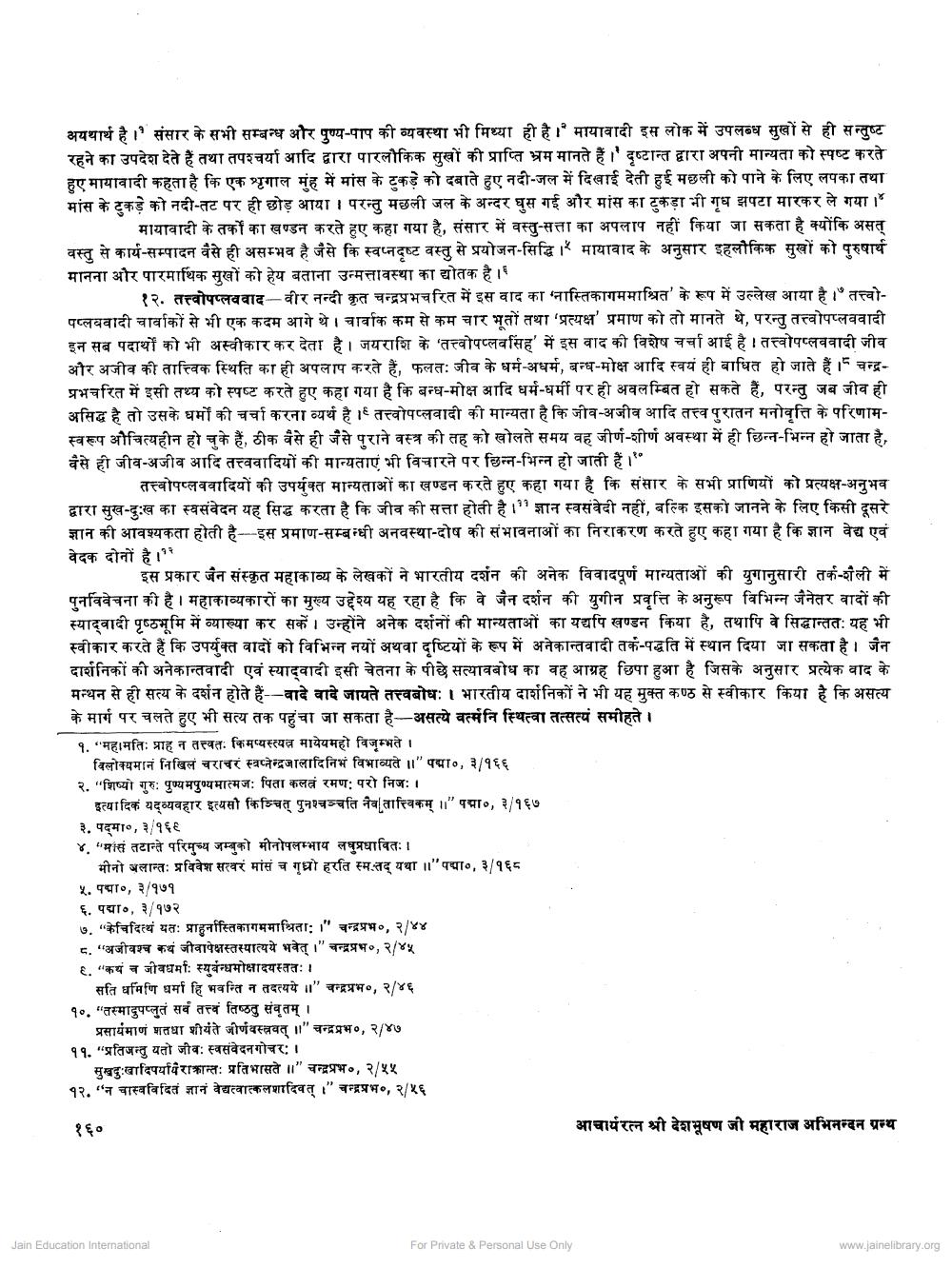________________
अयथार्थ है ।' संसार के सभी सम्बन्ध और पुण्य-पाप की व्यवस्था भी मिथ्या ही है। मायावादी इस लोक में उपलब्ध सुखों से ही सन्तुष्ट रहने का उपदेश देते हैं तथा तपश्चर्या आदि द्वारा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति भ्रम मानते हैं।' दृष्टान्त द्वारा अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए मायावादी कहता है कि एक श्रृंगाल मुंह में मांस के टुकड़े को दबाते हुए नदी जल में दिखाई देती हुई मछली को पाने के लिए लपका तथा मांस के टुकड़े को नदी तट पर ही छोड़ आया । परन्तु मछली जल के अन्दर घुस गई और मांस का टुकड़ा भी गृध झपटा मारकर ले गया । * मायावादी के तर्कों का खण्डन करते हुए कहा गया है, संसार में वस्तु-सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता है क्योंकि असत् वस्तु से कार्य सम्पादन पैसे ही असम्भव है जैसे कि स्वप्नदृष्ट वस्तु से प्रयोजन-सिद्धि। मायावाद के अनुसार इहलौकिक सुखों को पुरुषार्थ मानना और पारमार्थिक सुखों को हेय बताना उन्मत्तावस्था का द्योतक है।
१२. तत्त्वोपप्लववाद - वीर नन्दी कृत चन्द्रप्रभचरित में इस वाद का 'नास्तिकागममाश्रित' के रूप में उल्लेख आया है।" तत्त्वोपप्लववादी चार्वाकों से भी एक कदम आगे थे। चार्वाक कम से कम चार भूतों तथा 'प्रत्यक्ष' प्रमाण को तो मानते थे, परन्तु तत्त्वोपप्लववादी इन सब पदार्थों को भी अस्वीकार कर देता है । जयराशि के 'तत्त्वोपप्लवसिंह' में इस वाद की विशेष चर्चा आई है। तत्त्वोपप्लववादी जीव और अजीव की तात्त्विक स्थिति का ही अपलाप करते हैं, फलतः जीव के धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्ष आदि स्वयं ही बाधित हो जाते हैं । चन्द्रप्रभचरित में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि बन्ध-मोक्ष आदि धर्म-धर्मी पर ही अवलम्बित हो सकते हैं, परन्तु जब जीव ही असिद्ध है तो उसके धर्मों की चर्चा करना व्यर्थ है । तत्त्वोपप्लवादी की मान्यता है कि जीव अजीव आदि तत्त्व पुरातन मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप औचित्यहीन हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने वस्त्र की तह को खोलते समय वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में ही छिन्न-भिन्न हो जाता है, वैसे ही जीव अजीव आदि तत्त्ववादियों की मान्यताएं भी विचारने पर छिन्न-भिन्न हो जाती है।"
तत्त्वोपप्लववादियों की उपर्युक्त मान्यताओं का खण्डन करते हुए कहा गया है कि संसार के सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सुख-दुःख का स्वसंवेदन यह सिद्ध करता है कि जीव की सत्ता होती है।" ज्ञान स्वसंवेदी नहीं, बल्कि इसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है-इस प्रमाण-सम्बन्धी अनवस्था दोष की संभावनाओं का निराकरण करते हुए कहा गया है कि ज्ञान वेद्य एवं वेदक दोनों है।"
इस प्रकार जैन संस्कृत महाकाव्य के लेखकों ने भारतीय दर्शन की अनेक विवादपूर्ण मान्यताओं की युगानुसारी तर्क-धौली में पुनर्विवेचना की है। महाकाव्यकारों का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि वे जैन दर्शन की युगीन प्रवृत्ति के अनुरूप विभिन्न जैनेतर वादों की स्यादवादी पृष्ठभूमि में व्याख्या कर सकें। उन्होंने अनेक दर्शनों की मान्यताओं का यद्यपि खण्डन किया है, तथापि ने सिद्धान्ततः यह भी स्वीकार करते हैं कि उपर्युक्त वादों को विभिन्न नयों अथवा दृष्टियों के रूप में अनेकान्तवादी तर्क-पद्धति में स्थान दिया जा सकता है। जैन दार्शनिकों की अनेकान्तवादी एवं स्याद्वादी इसी चेतना के पीछे सत्यावबोध का वह आग्रह छिपा हुआ है जिसके अनुसार प्रत्येक वाद के मन्थन से ही सत्य के दर्शन होते हैं- वादे वादे जायते तत्त्वबोधः । भारतीय दार्शनिकों ने भी यह मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है कि असत्य के मार्ग पर चलते हुए भी सत्य तक पहुंचा जा सकता है-असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत्सत्यं समीहते ।
१. "महामतिः प्राह न तत्त्वतः किमप्यस्त्यत्न मायेयमहो विजृम्भते ।
विलोक्यमानं निखिलं चराचरं स्वप्नेन्द्रजालादिनिभं विभाव्यते ॥" पद्मा०, ३ / १६६
२. " शिष्यो गुरुः पुण्यमपुण्यमात्मजः पिता कलवं रमण: परो निजः ।
इत्यादिकं यद्व्यवहार इत्यसौ किञ्चित् पुनश्चञ्चति नैव [ तात्त्विकम् ।। " पद्मा०, ३/१६७ ३. पद्मा०, ३ / १६६
४. "मांसं तटान्ते परिमुच्य जम्बुको मीनोपलम्भाय लघुप्रधावितः ।
मनोजलान्तः प्रविवेश सत्वरं मांसं च गृध्रो हरति स्मः तद् यथा ।" पद्मा०, ३/१६८
५. पद्मा०, ३/१७१
६. पद्मा०, ३/१७२
७.
"केचिदित्यं यतः प्राहुर्नास्तिकागममाश्रिता: ।" चन्द्रप्रभ०, २/४४
८. "अजीवश्च कथं जीवापेक्षस्तस्यात्यये भवेत् । " चन्द्रप्रभ०, २/४५
६.
"कथं च जीवधर्माः स्युर्वन्धमोक्षादयस्ततः ।
सति धर्मिणि धर्मा हि भवन्ति न तदत्यये ॥" चन्द्रप्रभ०, २/४६ १०. "तस्मादुपप्लुतं सर्वं तत्त्वं तिष्ठतु संवृतम् ।
प्रसार्यमाणं शतधा शीयंते जीर्णवस्त्रवत् ॥" चन्द्रप्रभ०, २/४७ ११. "प्रतिजन्तु यतो जीवः स्वसंवेदनगोचरः ।
सुखदुःखादिपर्याय राक्रान्तः प्रतिभासते ।। " चन्द्रप्रभ०, २/५५ १२. " न चास्वविदितं ज्ञानं वेद्यत्वात्कलशादिवत् । " चन्द्रप्रभ०, २ / ५६
१६०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
www.jainelibrary.org