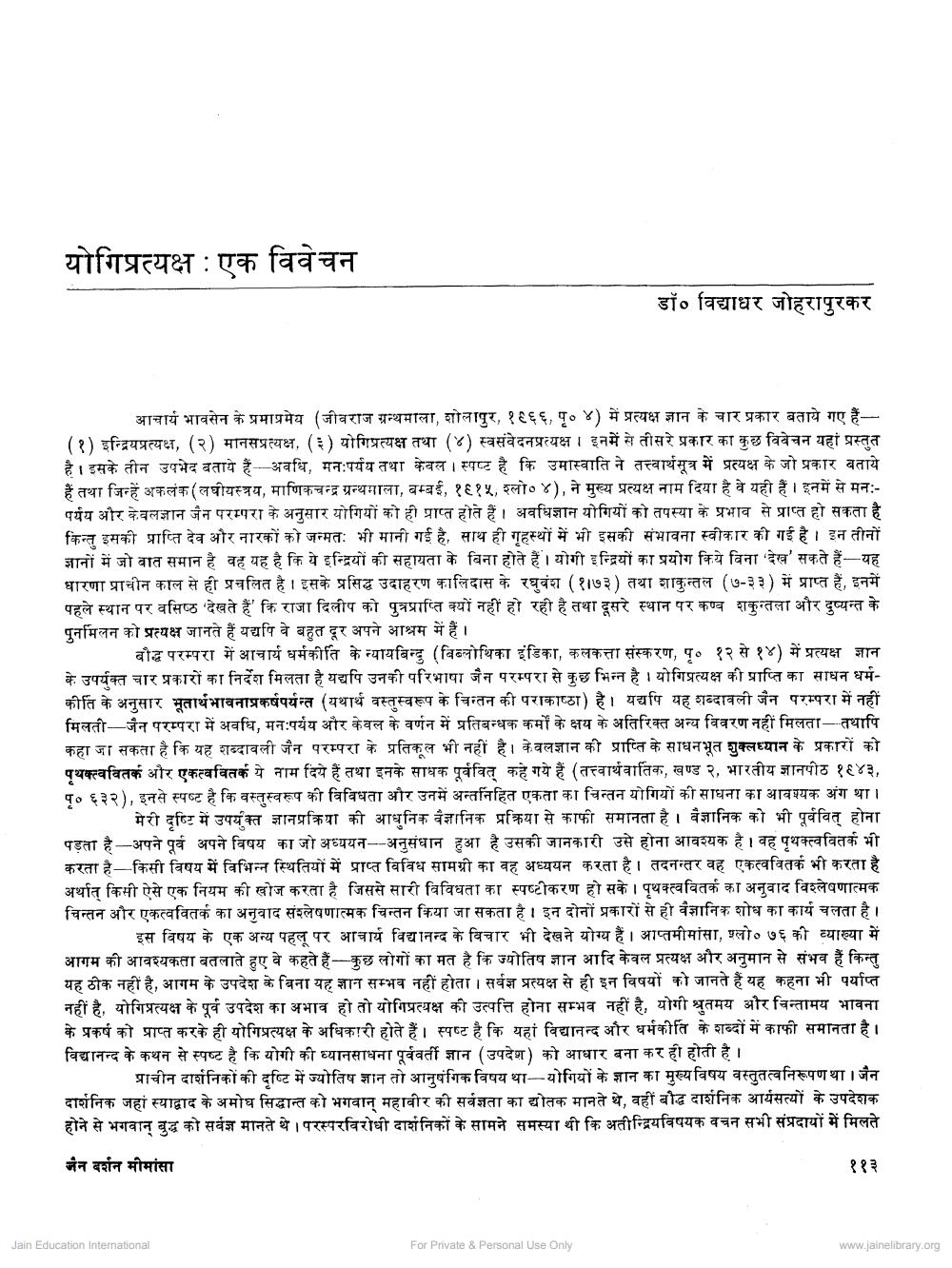________________
योगिप्रत्यक्ष : एक विवेचन
डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर
आचार्य भावसेन के प्रमाप्रमेय (जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर, १९६६, पृ० ४) में प्रत्यक्ष ज्ञान के चार प्रकार बताये गए हैं(१) इन्द्रियप्रत्यक्ष, (२) मानसप्रत्यक्ष, (३) योगिप्रत्यक्ष तथा (४) स्वसंवेदनप्रत्यक्ष । इनमें से तीसरे प्रकार का कुछ विवेचन यहां प्रस्तुत है। इसके तीन उपभेद बताये हैं—अवधि, मन:पर्यय तथा केवल । स्पष्ट है कि उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में प्रत्यक्ष के जो प्रकार बताये हैं तथा जिन्हें अकलंक (लघीयस्त्रय, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई, १९१५, श्लो०४), ने मुख्य प्रत्यक्ष नाम दिया है वे यही हैं। इनमें से मन:पर्यय और केवलज्ञान जैन परम्परा के अनुसार योगियों को ही प्राप्त होते हैं। अवधिज्ञान योगियों को तपस्या के प्रभाव से प्राप्त हो सकता है किन्तु इसकी प्राप्ति देव और नारकों को जन्मतः भी मानी गई है, साथ ही गृहस्थों में भी इसकी संभावना स्वीकार की गई है। इन तीनों ज्ञानों में जो बात समान है वह यह है कि ये इन्द्रियों की सहायता के बिना होते हैं। योगी इन्द्रियों का प्रयोग किये बिना 'देख' सकते हैं यह धारणा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इसके प्रसिद्ध उदाहरण कालिदास के रघुवंश (११७३) तथा शाकुन्तल (७-३३) में प्राप्त हैं, इनमें पहले स्थान पर वसिष्ठ 'देखते हैं कि राजा दिलीप को पुत्रप्राप्ति क्यों नहीं हो रही है तथा दूसरे स्थान पर कण्व शकुन्तला और दुष्यन्त के पुनर्मिलन को प्रत्यक्ष जानते हैं यद्यपि वे बहुत दूर अपने आश्रम में हैं।
बौद्ध परम्परा में आचार्य धर्मकीति के न्यायबिन्दु (बिब्लोथिका इंडिका, कलकत्ता संस्करण, पृ० १२ से १४) में प्रत्यक्ष ज्ञान के उपर्युक्त चार प्रकारों का निर्देश मिलता है यद्यपि उनकी परिभाषा जैन परम्परा से कुछ भिन्न है । योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति का साधन धर्मकीति के अनुसार भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्त (यथार्थ वस्तुस्वरूप के चिन्तन की पराकाष्ठा) है। यद्यपि यह शब्दावली जैन परम्परा में नहीं मिलती-जैन परम्परा में अवधि, मनःपर्यय और केवल के वर्णन में प्रतिबन्धक कर्मों के क्षय के अतिरिक्त अन्य विवरण नहीं मिलता-तथापि कहा जा सकता है कि यह शब्दावली जैन परम्परा के प्रतिकूल भी नहीं है। केवलज्ञान की प्राप्ति के साधनभूत शुक्लध्यान के प्रकारों को पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क ये नाम दिये हैं तथा इनके साधक पूर्ववित् कहे गये हैं (तत्त्वार्थवार्तिक, खण्ड २, भारतीय ज्ञानपीठ १६४३, पृ० ६३२), इनसे स्पष्ट है कि वस्तुस्वरूप की विविधता और उनमें अन्तर्निहित एकता का चिन्तन योगियों की साधना का आवश्यक अंग था।
मेरी दृष्टि में उपर्युक्त ज्ञानप्रक्रिया की आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया से काफी समानता है। वैज्ञानिक को भी पूर्ववित् होना पड़ता है-अपने पूर्व अपने विषय का जो अध्ययन--अनुसंधान हुआ है उसकी जानकारी उसे होना आवश्यक है। वह पृथक्त्ववितर्क भी करता है—किसी विषय में विभिन्न स्थितियों में प्राप्त विविध सामग्री का वह अध्ययन करता है। तदनन्तर वह एकत्ववितर्क भी करता है अर्थात् किसी ऐसे एक नियम की खोज करता है जिससे सारी विविधता का स्पष्टीकरण हो सके । पृथक्त्ववितर्क का अनुवाद विश्लेषणात्मक चिन्तन और एकत्ववितर्क का अनुवाद संश्लेषणात्मक चिन्तन किया जा सकता है। इन दोनों प्रकारों से ही वैज्ञानिक शोध का कार्य चलता है।
इस विषय के एक अन्य पहलू पर आचार्य विद्यानन्द के विचार भी देखने योग्य हैं। आप्तमीमांसा, श्लो०७६ की व्याख्या में आगम की आवश्यकता बतलाते हुए वे कहते हैं-कुछ लोगों का मत है कि ज्योतिष ज्ञान आदि केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से संभव हैं किन्तु यह ठीक नहीं है, आगम के उपदेश के बिना यह ज्ञान सम्भव नहीं होता। सर्वज्ञ प्रत्यक्ष से ही इन विषयों को जानते हैं यह कहना भी पर्याप्त नहीं है, योगिप्रत्यक्ष के पूर्व उपदेश का अभाव हो तो योगिप्रत्यक्ष की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है, योगी श्रुतमय और चिन्तामय भावना के प्रकर्ष को प्राप्त करके ही योगिप्रत्यक्ष के अधिकारी होते हैं। स्पष्ट है कि यहां विद्यानन्द और धर्मकीर्ति के शब्दों में काफी समानता है। विद्यानन्द के कथन से स्पष्ट है कि योगी की ध्यानसाधना पूर्ववर्ती ज्ञान (उपदेश) को आधार बना कर ही होती है।
प्राचीन दार्शनिकों की दृष्टि में ज्योतिष ज्ञान तो आनुषंगिक विषय था-योगियों के ज्ञान का मुख्य विषय वस्तुतत्वनिरूपण था। जैन दार्शनिक जहां स्याद्वाद के अमोघ सिद्धान्त को भगवान महावीर की सर्वज्ञता का द्योतक मानते थे, वहीं बौद्ध दार्शनिक आर्यसत्यों के उपदेशक होने से भगवान् बुद्ध को सर्वज्ञ मानते थे। परस्परविरोधी दार्शनिकों के सामने समस्या थी कि अतीन्द्रियविषयक वचन सभी संप्रदायों में मिलते
जैन दर्शन मीमांसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org