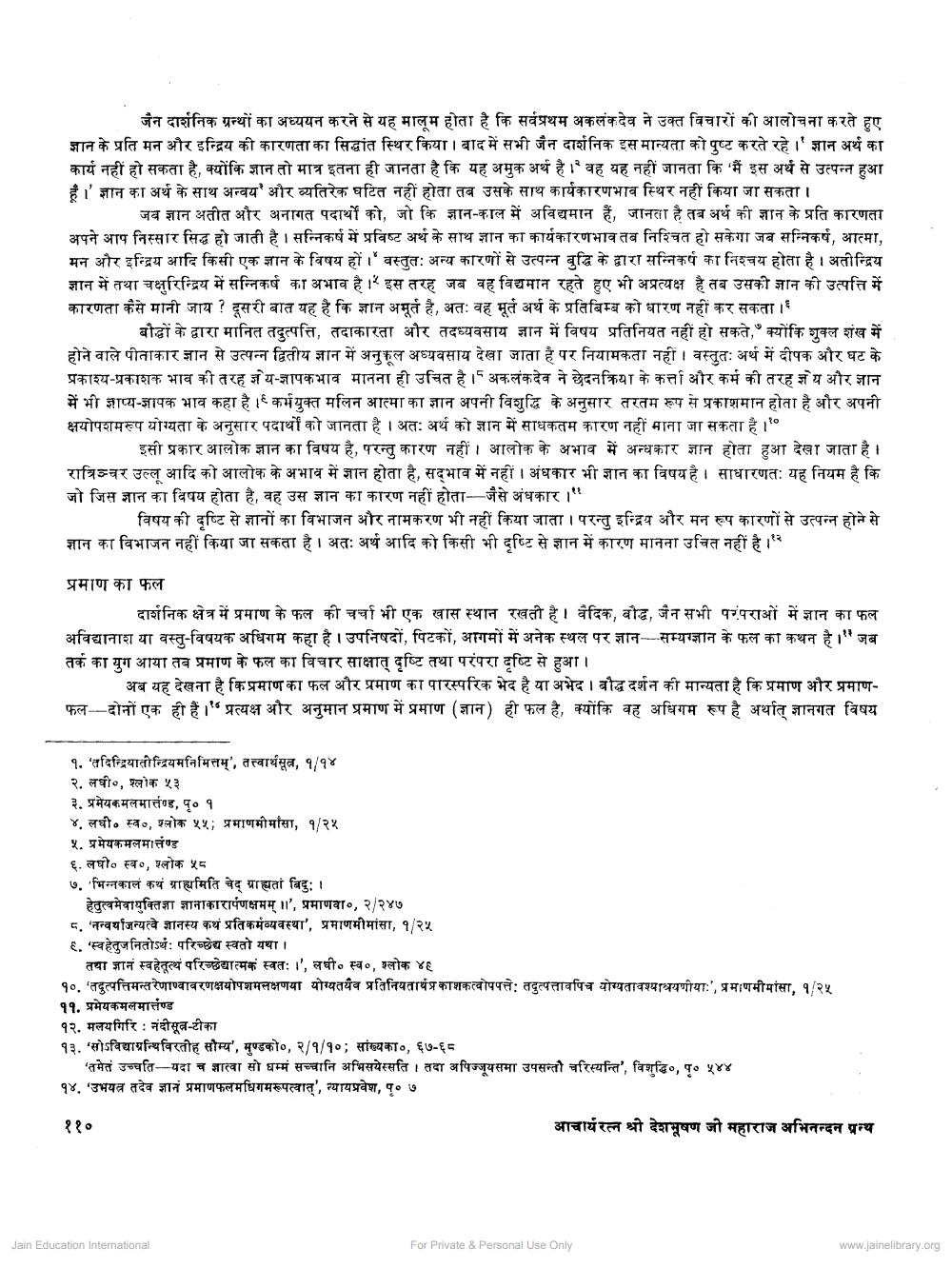________________
जैन दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि सर्वप्रथम अकलंकदेव ने उक्त विचारों की आलोचना करते हुए ज्ञान के प्रति मन और इन्द्रिय की कारणता का सिद्धांत स्थिर किया। बाद में सभी जैन दार्शनिक इस मान्यता को पुष्ट करते रहे ।' ज्ञान अर्थ का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो मात्र इतना ही जानता है कि यह अमुक अर्थ है । वह यह नहीं जानता कि 'मैं इस अर्थ से उत्पन्न हुआ हैं।' ज्ञान का अर्थ के साथ अन्वय और व्यतिरेक घटित नहीं होता तब उसके साथ कार्यकारणभाव स्थिर नहीं किया जा सकता।
जब ज्ञान अतीत और अनागत पदार्थों को, जो कि ज्ञान-काल में अविद्यमान हैं, जानता है तब अर्थ की ज्ञान के प्रति कारणता अपने आप निस्सार सिद्ध हो जाती है । सन्निकर्ष में प्रविष्ट अर्थ के साथ ज्ञान का कार्यकारणभाव तब निश्चित हो सकेगा जब सन्निकर्ष, आत्मा, मन और इन्द्रिय आदि किसी एक ज्ञान के विषय हों। वस्तुत: अन्य कारणों से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा सन्निकर्ष का निश्चय होता है । अतीन्द्रिय ज्ञान में तथा चक्षुरिन्द्रिय में सन्निकर्ष का अभाव है। इस तरह जब वह विद्यमान रहते हुए भी अप्रत्यक्ष है तब उसकी ज्ञान की उत्पत्ति में कारणता कैसे मानी जाय? दूसरी बात यह है कि ज्ञान अमूर्त है, अतः वह मूर्त अर्थ के प्रतिबिम्ब को धारण नहीं कर सकता।
बौद्धों के द्वारा मानित तदुत्पत्ति, तदाकारता और तदध्यवसाय ज्ञान में विषय प्रतिनियत नहीं हो सकते, क्योंकि शुक्ल शंख में होने वाले पीताकार ज्ञान से उत्पन्न द्वितीय ज्ञान में अनुकल अध्यवसाय देखा जाता है पर नियामकता नहीं। वस्तुतः अर्थ में दीपक और घट के प्रकाश्य-प्रकाशक भाव की तरह ज्ञ य-ज्ञापकभाव मानना ही उचित है। अकलंकदेव ने छेदनक्रिया के कर्ता और कर्म की तरह ज्ञय और ज्ञान में भी ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव कहा है। कर्म युक्त मलिन आत्मा का ज्ञान अपनी विशुद्धि के अनुसार तरतम रूप से प्रकाशमान होता है और अपनी क्षयोपशमरूप योग्यता के अनुसार पदार्थों को जानता है । अतः अर्थ को ज्ञान में साधकतम कारण नहीं माना जा सकता है।
इसी प्रकार आलोक ज्ञान का विषय है, परन्तु कारण नहीं। आलोक के अभाव में अन्धकार ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। रात्रिञ्चर उल्लू आदि को आलोक के अभाव में ज्ञान होता है, सद्भाव में नहीं । अंधकार भी ज्ञान का विषय है। साधारणत: यह नियम है कि जो जिस ज्ञान का विषय होता है, वह उस ज्ञान का कारण नहीं होता-जैसे अंधकार ।"
विषय की दृष्टि से ज्ञानों का विभाजन और नामकरण भी नहीं किया जाता । परन्तु इन्द्रिय और मन रूप कारणों से उत्पन्न होने से ज्ञान का विभाजन नहीं किया जा सकता है । अतः अर्थ आदि को किसी भी दृष्टि से ज्ञान में कारण मानना उचित नहीं है।१२
प्रमाण का फल
दार्शनिक क्षेत्र में प्रमाण के फल की चर्चा भी एक खास स्थान रखती है। वैदिक, बौद्ध, जैन सभी परंपराओं में ज्ञान का फल अविद्यानाश या वस्तु-विषयक अधिगम कहा है । उपनिषदों, पिटकों, आगमों में अनेक स्थल पर ज्ञान-सम्यग्ज्ञान के फल का कथन है। जब तर्क का युग आया तब प्रमाण के फल का विचार साक्षात् दृष्टि तथा परंपरा दृष्टि से हुआ।
अब यह देखना है कि प्रमाण का फल और प्रमाण का पारस्परिक भेद है या अभेद । बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि प्रमाण और प्रमाणफल-दोनों एक ही हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण में प्रमाण (ज्ञान) ही फल है, क्योंकि वह अधिगम रूप है अर्थात् ज्ञानगत विषय
१. 'तदिन्द्रियातीन्द्रियमनिमित्तम्', तत्त्वार्थसूत्र, १/१४ २. लघी०, श्लोक ५३ ३. प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ०१ ४. लघी. स्व०, श्लोक ५५; प्रमाणमीमांसा, १/२५ ५. प्रमेयकमलमार्तण्ड ६. लघी० स्व०, श्लोक ५८ ७. भिन्नकाल कथं ग्राह्यमिति चेद् ग्राह्यतां बिदुः ।
हेतुत्वमेवायुक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पणक्षमम् ॥', प्रमाणवा०, २/२४७ ८. 'नत्वर्थाजन्यत्वे ज्ञानस्य कथं प्रतिकर्मव्यवस्था', प्रमाणमीमांसा, १/२५ ६. 'स्वहेतुजनितोऽर्थः परिच्छेद्य स्वतो यथा । ___ तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेद्यात्मकं स्वतः ।', लघी० स्व०, श्लोक ४६ १०. 'तदुत्पत्तिमन्तरेणाण्वावरणक्षयोपशमलक्षणया योग्यतयैव प्रतिनियतार्थप्रकाशकत्वोपपत्ते: तदुत्पत्तावपिच योग्यतावश्याश्रयणीयाः', प्रमाणमीमांसा, १/२५ ११. प्रमेयकमलमार्तण्ड १२. मलयगिरि : नंदीसूत्र-टीका १३. 'सोऽविद्याग्रन्थिविरतीह सौम्य', मुण्डको०, २/१/१०; सांख्यका०, ६७-६८ __तमेत उपचति-यदा च ज्ञात्वा सो धम्म सच्चानि अभिसयेस्सति । तदा अपिज्जयसमा उपसन्तौ चरिस्यन्ति', विशुद्धि०, पृ०५४४ १४. 'उभयत्र तदेव ज्ञानं प्रमाणफलमधिगमरूपत्वात्', न्यायप्रवेश, पृ०७
११०
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org