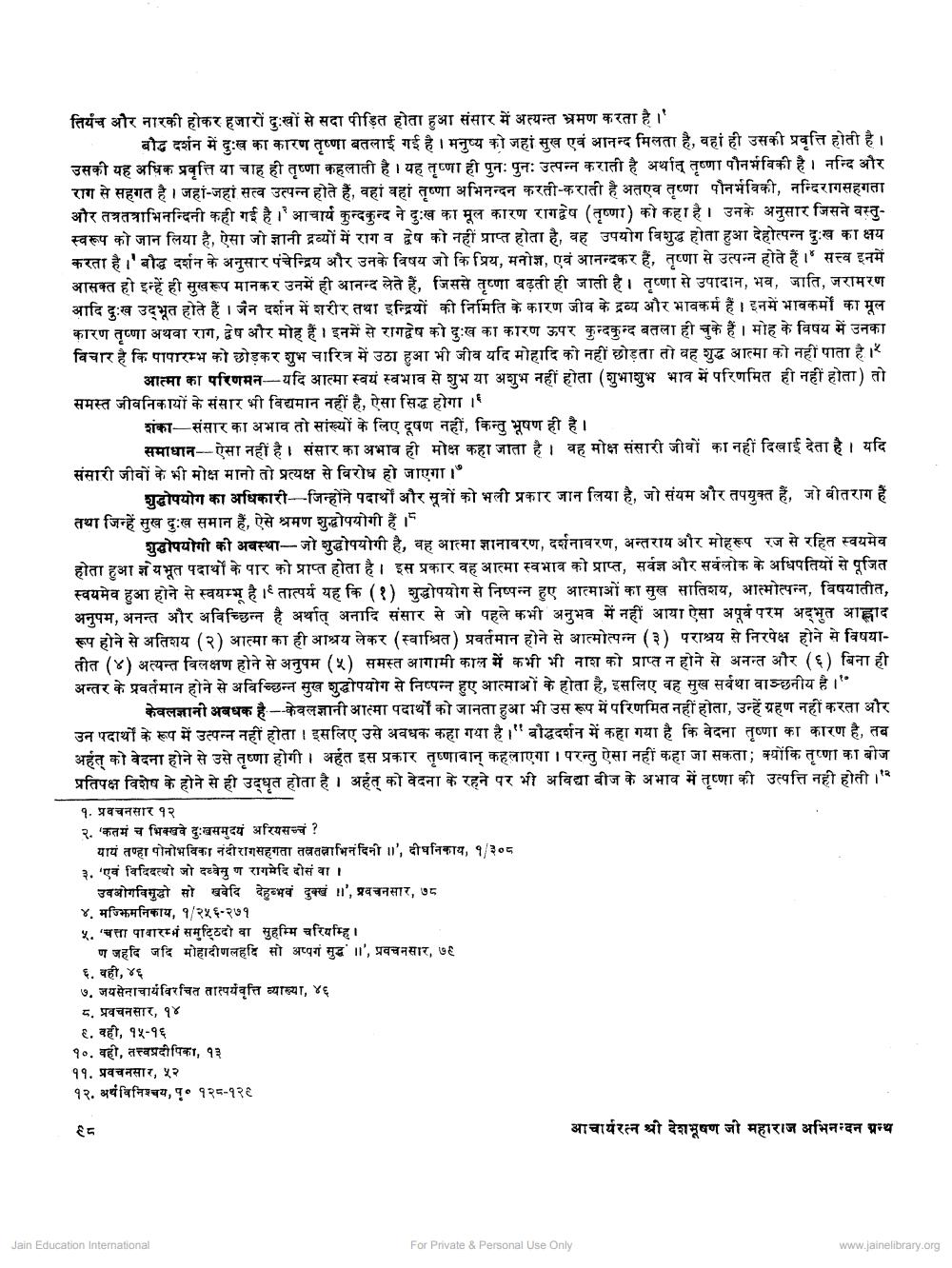________________
तिर्यच और नारकी होकर हजारों दुःखों से सदा पीड़ित होता हुआ संसार में अत्यन्त भ्रमण करता है।'
बौद्ध दर्शन में दुःख का कारण तृष्णा बतलाई गई है । मनुष्य को जहां सुख एवं आनन्द मिलता है, वहां ही उसकी प्रवृत्ति होती है। उसकी यह अधिक प्रवृत्ति या चाह ही तृष्णा कहलाती है। यह तृष्णा ही पुनः पुनः उत्पन्न कराती है अर्थात् तृष्णा पौनविकी है। नन्दि और राग से सहगत है। जहां-जहां सत्व उत्पन्न होते हैं, वहां वहां तृष्णा अभिनन्दन करती-कराती है अतएव तृष्णा पौनविकी, नन्दिरागसहगता और तत्रतत्राभिनन्दिनी कही गई है। आचार्य कुन्दकुन्द ने दुःख का मूल कारण रागद्वेष (तृष्णा) को कहा है। उनके अनुसार जिसने वस्तुस्वरूप को जान लिया है, ऐसा जो ज्ञानी द्रव्यों में राग व द्वेष को नहीं प्राप्त होता है, वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुःख का क्षय करता है।' बौद्ध दर्शन के अनुसार पंचेन्द्रिय और उनके विषय जो कि प्रिय, मनोज्ञ, एवं आनन्दकर हैं, तृष्णा से उत्पन्न होते हैं। सत्त्व इनमें आसक्त हो इन्हें ही सुखरूप मानकर उनमें ही आनन्द लेते हैं, जिससे तृष्णा बढ़ती ही जाती है। तृष्णा से उपादान, भव, जाति, जरामरण आदि दुःख उद्भूत होते हैं । जैन दर्शन में शरीर तथा इन्द्रियों की निमिति के कारण जीव के द्रव्य और भावकर्म हैं। इनमें भावकर्मों का मूल कारण तृष्णा अथवा राग, द्वेष और मोह हैं। इनमें से रागद्वेष को दुःख का कारण ऊपर कुन्दकुन्द बतला ही चुके हैं। मोह के विषय में उनका विचार है कि पापारम्भ को छोड़कर शुभ चारित्र में उठा हुआ भी जीव यदि मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्ध आत्मा को नहीं पाता है।
आत्मा का परिणमन-यदि आत्मा स्वयं स्वभाव से शुभ या अशुभ नहीं होता (शुभाशुभ भाव में परिणमित ही नहीं होता) तो समस्त जीवनिकायों के संसार भी विद्यमान नहीं है, ऐसा सिद्ध होगा।
शंका–संसार का अभाव तो सांख्यों के लिए दूषण नहीं, किन्तु भूषण ही है।
समाधान-ऐसा नहीं है। संसार का अभाव ही मोक्ष कहा जाता है। वह मोक्ष संसारी जीवों का नहीं दिखाई देता है। यदि संसारी जीवों के भी मोक्ष मानो तो प्रत्यक्ष से विरोध हो जाएगा।
शुद्धोपयोग का अधिकारी--जिन्होंने पदार्थों और सूत्रों को भली प्रकार जान लिया है, जो संयम और तपयुक्त हैं, जो वीतराग हैं तथा जिन्हें सुख दुःख समान हैं, ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी हैं।
शुद्धोपयोगी की अवस्था-जो शुद्धोपयोगी है, वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहरूप रज से रहित स्वयमेव होता हुआ शेयभूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त, सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयम्भू है। तात्पर्य यह कि (१) शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं का सुख सातिशय, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनन्त और अविच्छिन्न है अर्थात् अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया ऐसा अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय (२) आत्मा का ही आश्रय लेकर (स्वाश्रित) प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न (३) पराश्रय से निरपेक्ष होने से विषयातीत (४) अत्यन्त विलक्षण होने से अनुपम (५) समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनन्त और (६) बिना ही अन्तर के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के होता है, इसलिए वह सुख सर्वथा वाञ्छनीय है।"
केवलज्ञानी अवधक है-केवलज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी उस रूप में परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उसे अवधक कहा गया है।" बौद्धदर्शन में कहा गया है कि वेदना तृष्णा का कारण है, तब अर्हत् को वेदना होने से उसे तृष्णा होगी। अर्हत इस प्रकार तृष्णावान् कहलाएगा। परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि तृष्णा का बोज प्रतिपक्ष विशेष के होने से ही उद्धृत होता है। अर्हत् को वेदना के रहने पर भी अविद्या बीज के अभाव में तृष्णा की उत्पत्ति नहीं होती।१२ १. प्रवचनसार १२ २. 'कतमं च भिक्खवे दुःखसमुदयं अरियसच्चं?
यायं तण्हा पोनोभविका नंदीरागसहगता तवतन्नाभिनंदिनी ॥', दीघनिकाय, १/३०८ ३. 'एवं विदिदत्थो जो दब्वेमु ण रागमेदि दोसं वा ।
उवोगविमुद्धो सो खवेदि देहुब्भवं दुक्खं ॥', प्रवचनसार, ७८ ४. मज्झिमनिकाय, १/२५६-२७१ ५. 'चत्ता पाबारम्भ समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्हि ।
ण जहदि जदि मोहादीणलहदि सो अप्पगं सुद्ध' ॥', प्रवचनसार, ७६ ६. वही, ४६ ७. जयसेनाचार्यविरचित तात्पर्यवृत्ति व्याख्या, ४६ ८. प्रवचनसार, १४ ६. वही, १५-१६ १०. वही, तत्त्वप्रदीपिका, १३ ११. प्रवचनसार, ५२ १२. अयं विनिश्चय, पृ० १२८-१२६
१८
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org