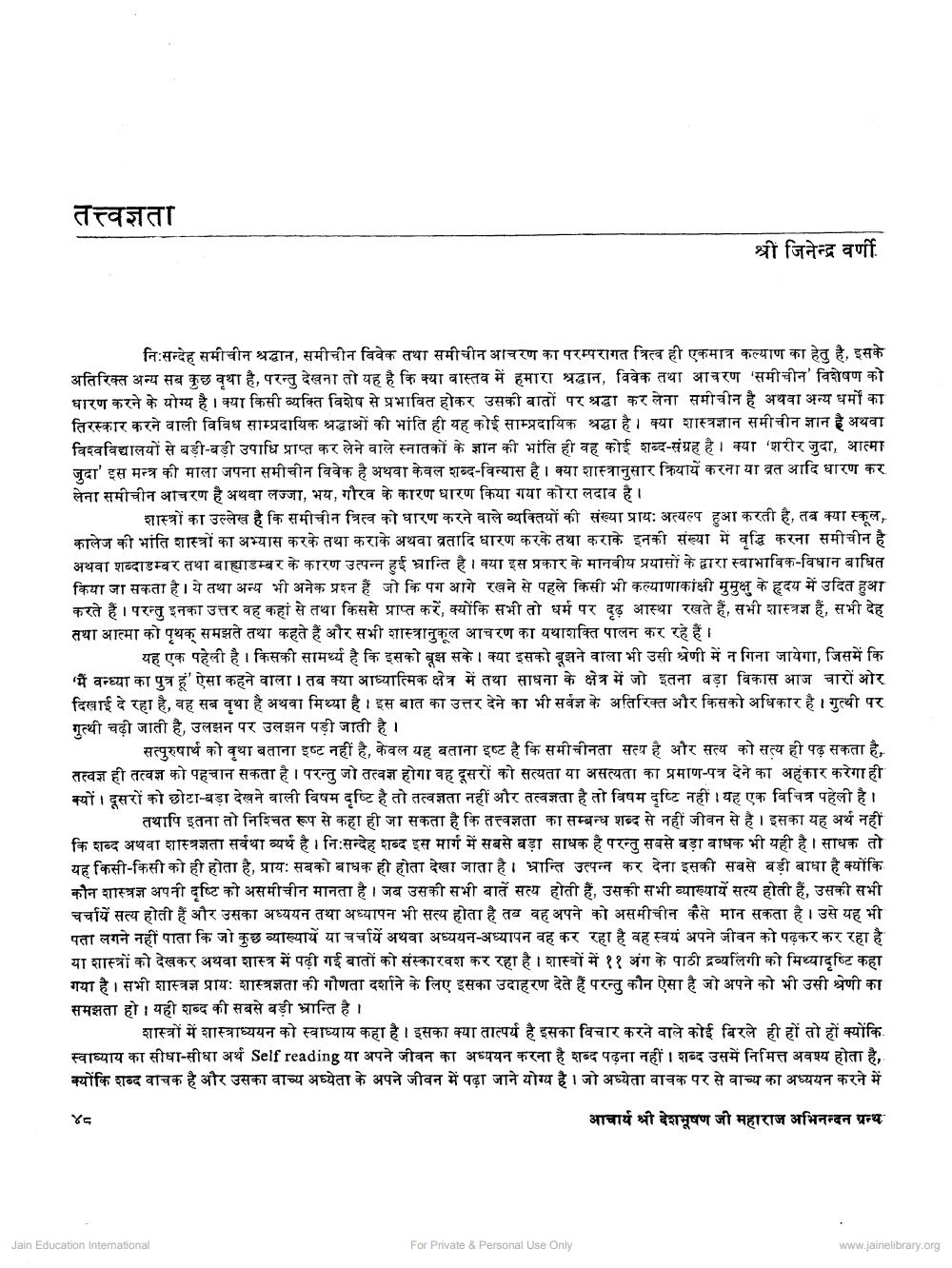________________
तत्त्वज्ञता
श्री जिनेन्द्र वर्णी.
निःसन्देह समीचीन श्रद्धान, समीचीन विवेक तथा समीचीन आचरण का परम्परागत त्रित्व ही एकमात्र कल्याण का हेतु है, इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ वृथा है, परन्तु देखना तो यह है कि क्या वास्तव में हमारा श्रद्धान, विवेक तथा आचरण 'समीचीन' विशेषण को धारण करने के योग्य है। क्या किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर उसकी बातों पर श्रद्धा कर लेना समीचीन है अथवा अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वाली विविध साम्प्रदायिक श्रद्धाओं की भांति ही यह कोई साम्प्रदायिक श्रद्धा है। क्या शास्त्रज्ञान समीचीन ज्ञान है अथवा विश्वविद्यालयों से बड़ी-बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेने वाले स्नातकों के ज्ञान की भांति ही वह कोई शब्द-संग्रह है। क्या 'शरीर जुदा, आत्मा जुदा' इस मन्त्र की माला जपना समीचीन विवेक है अथवा केवल शब्द-विन्यास है। क्या शास्त्रानुसार क्रियायें करना या व्रत आदि धारण कर लेना समीचीन आचरण है अथवा लज्जा, भय, गौरव के कारण धारण किया गया कोरा लदाव है।
शास्त्रों का उल्लेख है कि समीचीन त्रित्व को धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रायः अत्यल्प हुआ करती है, तब क्या स्कूल, कालेज की भांति शास्त्रों का अभ्यास करके तथा कराके अथवा व्रतादि धारण करके तथा कराके इनकी संख्या में वृद्धि करना समीचीन है अथवा शब्दाडम्बर तथा बाह्याडम्बर के कारण उत्पन्न हुई भ्रान्ति है। क्या इस प्रकार के मानवीय प्रयासों के द्वारा स्वाभाविक-विधान बाधित किया जा सकता है । ये तथा अन्य भी अनेक प्रश्न हैं जो कि पग आगे रखने से पहले किसी भी कल्याणाकांक्षी मुमुक्षु के हृदय में उदित हुआ करते हैं। परन्तु इनका उत्तर वह कहां से तथा किससे प्राप्त करें, क्योंकि सभी तो धर्म पर दृढ़ आस्था रखते हैं, सभी शास्त्रज्ञ हैं, सभी देह सथा आत्मा को पृथक् समझते तथा कहते हैं और सभी शास्त्रानुकूल आचरण का यथाशक्ति पालन कर रहे हैं।
यह एक पहेली है । किसकी सामर्थ्य है कि इसको बूझ सके। क्या इसको बूझने वाला भी उसी श्रेणी में न गिना जायेगा, जिसमें कि 'मैं वन्ध्या का पुत्र हूं' ऐसा कहने वाला । तब क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में तथा साधना के क्षेत्र में जो इतना बड़ा विकास आज चारों ओर दिखाई दे रहा है, वह सब वृथा है अथवा मिथ्या है। इस बात का उत्तर देने का भी सर्वज्ञ के अतिरिक्त और किसको अधिकार है। गुत्थी पर गुत्थी चढ़ी जाती है, उलझन पर उलझन पड़ी जाती है।
सत्पुरुषार्थ को वृथा बताना इष्ट नहीं है, केवल यह बताना इष्ट है कि समीचीनता सत्य है और सत्य को सत्य ही पढ़ सकता है, तत्वज्ञ ही तत्वज्ञ को पहचान सकता है । परन्तु जो तत्वज्ञ होगा वह दूसरों को सत्यता या असत्यता का प्रमाण-पत्र देने का अहंकार करेगा ही क्यों। दूसरों को छोटा-बड़ा देखने वाली विषम दृष्टि है तो तत्वज्ञता नहीं और तत्वज्ञता है तो विषम दृष्टि नहीं। यह एक विचित्र पहेली है।
तथापि इतना तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि तत्त्वज्ञता का सम्बन्ध शब्द से नहीं जीवन से है। इसका यह अर्थ नहीं कि शब्द अथवा शास्त्रज्ञता सर्वथा व्यर्थ है । निःसन्देह शब्द इस मार्ग में सबसे बड़ा साधक है परन्तु सबसे बड़ा बाधक भी यही है। साधक तो यह किसी-किसी को ही होता है, प्रायः सबको बाधक ही होता देखा जाता है। भ्रान्ति उत्पन्न कर देना इसकी सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि कौन शास्त्रज्ञ अपनी दृष्टि को असमीचीन मानता है। जब उसकी सभी बातें सत्य होती हैं, उसकी सभी व्याख्यायें सत्य होती हैं, उसकी सभी चर्चायें सत्य होती हैं और उसका अध्ययन तथा अध्यापन भी सत्य होता है तब वह अपने को असमीचीन कैसे मान सकता है । उसे यह भी पता लगने नहीं पाता कि जो कुछ व्याख्यायें या चर्चायें अथवा अध्ययन-अध्यापन वह कर रहा है वह स्वयं अपने जीवन को पढ़कर कर रहा है या शास्त्रों को देखकर अथवा शास्त्र में पढ़ी गई बातों को संस्कारवश कर रहा है । शास्त्रों में ११ अंग के पाठी द्रव्यलिंगी को मिथ्यादृष्टि कहा गया है। सभी शास्त्रज्ञ प्रायः शास्त्रज्ञता की गौणता दर्शाने के लिए इसका उदाहरण देते हैं परन्तु कौन ऐसा है जो अपने को भी उसी श्रेणी का समझता हो । यही शब्द की सबसे बड़ी भ्रान्ति है।
शास्त्रों में शास्त्राध्ययन को स्वाध्याय कहा है। इसका क्या तात्पर्य है इसका विचार करने वाले कोई बिरले ही हों तो हों क्योंकि स्वाध्याय का सीधा-सीधा अर्थ Self reading या अपने जीवन का अध्ययन करना है शब्द पढ़ना नहीं । शब्द उसमें निमित्त अवश्य होता है, क्योंकि शब्द वाचक है और उसका वाच्य अध्येता के अपने जीवन में पढ़ा जाने योग्य है । जो अध्येता वाचक पर से वाच्य का अध्ययन करने में
४८
आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org