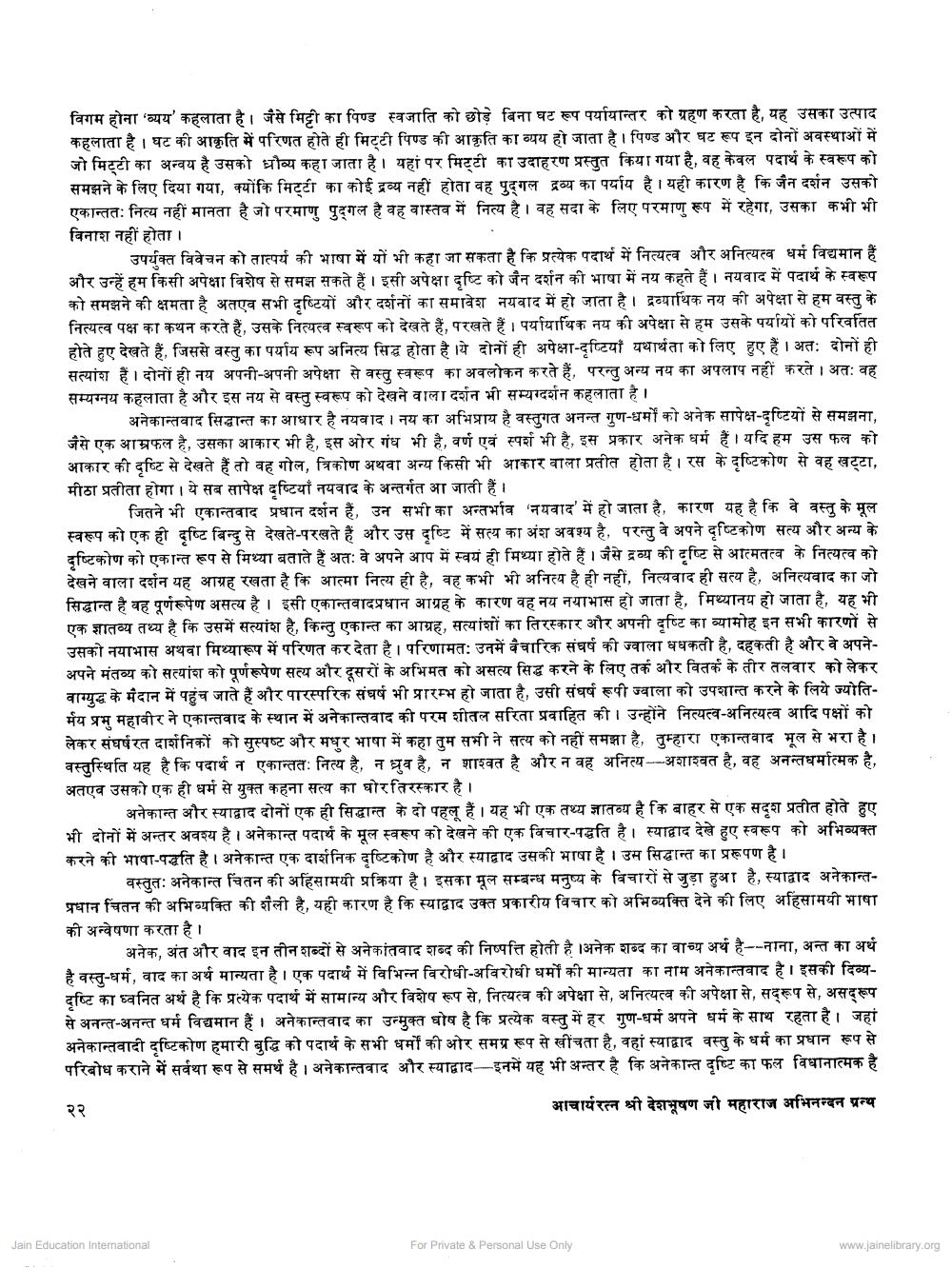________________
विगम होना 'व्यय' कहलाता है। जैसे मिट्टी का पिण्ड स्वजाति को छोड़े बिना घट रूप पर्यायान्तर को ग्रहण करता है, यह उसका उत्पाद कहलाता है । घट की आकृति में परिणत होते ही मिट्टी पिण्ड की आकृति का व्यय हो जाता है। पिण्ड और घट रूप इन दोनों अवस्थाओं में जो मिट्टी का अन्वय है उसको ध्रौव्य कहा जाता है। यहां पर मिट्टी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वह केवल पदार्थ के स्वरूप को समझने के लिए दिया गया, क्योंकि मिट्टी का कोई द्रव्य नहीं होता वह पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। यही कारण है कि जैन दर्शन उसको एकान्ततः नित्य नहीं मानता है जो परमाणु पुद्गल है वह वास्तव में नित्य है। वह सदा के लिए परमाणु रूप में रहेगा, उसका कभी भी विनाश नहीं होता।
उपर्युक्त विवेचन को तात्पर्य की भाषा में यों भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म विद्यमान हैं और उन्हें हम किसी अपेक्षा विशेष से समझ सकते हैं। इसी अपेक्षा दृष्टि को जैन दर्शन की भाषा में नय कहते हैं। नयवाद में पदार्थ के स्वरूप को समझने की क्षमता है अतएव सभी दृष्टियों और दर्शनों का समावेश नयवाद में हो जाता है। द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से हम वस्तु के नित्यत्व पक्ष का कथन करते हैं, उसके नित्यत्व स्वरूप को देखते हैं, परखते हैं। पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से हम उसके पर्यायों को परिवर्तित होते हुए देखते हैं, जिससे वस्तु का पर्याय रूप अनित्य सिद्ध होता है ।ये दोनों ही अपेक्षा-दृष्टियाँ यथार्थता को लिए हुए हैं । अत: दोनों ही सत्यांश हैं। दोनों ही नय अपनी-अपनी अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का अवलोकन करते हैं, परन्तु अन्य नय का अपलाप नहीं करते । अत: वह सम्यग्नय कहलाता है और इस नय से वस्तु स्वरूप को देखने वाला दर्शन भी सम्यग्दर्शन कहलाता है।
अनेकान्तवाद सिद्धान्त का आधार है नयवाद । नय का अभिप्राय है वस्तुगत अनन्त गुण-धर्मों को अनेक सापेक्ष-दृष्टियों से समझना, जैसे एक आम्रफल है, उसका आकार भी है, इस ओर गंध भी है, वर्ण एवं स्पर्श भी है, इस प्रकार अनेक धर्म हैं। यदि हम उस फल को आकार की दृष्टि से देखते हैं तो वह गोल, त्रिकोण अथवा अन्य किसी भी आकार वाला प्रतीत होता है। रस के दृष्टिकोण से वह खट्टा, मीठा प्रतीता होगा। ये सब सापेक्ष दृष्टियाँ नयवाद के अन्तर्गत आ जाती हैं।
जितने भी एकान्तवाद प्रधान दर्शन हैं, उन सभी का अन्तर्भाव 'नयवाद' में हो जाता है, कारण यह है कि वे वस्तु के मूल स्वरूप को एक ही दृष्टि बिन्दु से देखते-परखते हैं और उस दृष्टि में सत्य का अंश अवश्य है, परन्तु वे अपने दृष्टिकोण सत्य और अन्य के दृष्टिकोण को एकान्त रूप से मिथ्या बताते हैं अतः वे अपने आप में स्वयं ही मिथ्या होते हैं। जैसे द्रव्य की दृष्टि से आत्मतत्व के नित्यत्व को देखने वाला दर्शन यह आग्रह रखता है कि आत्मा नित्य ही है, वह कभी भी अनित्य है ही नहीं, नित्यवाद ही सत्य है, अनित्यवाद का जो सिद्धान्त है वह पूर्णरूपेण असत्य है। इसी एकान्तवादप्रधान आग्रह के कारण वह नय नयाभास हो जाता है, मिथ्यानय हो जाता है, यह भी एक ज्ञातव्य तथ्य है कि उसमें सत्यांश है, किन्तु एकान्त का आग्रह, सत्यांशों का तिरस्कार और अपनी दृष्टि का व्यामोह इन सभी कारणों से उसको नयाभास अथवा मिथ्यारूप में परिणत कर देता है। परिणामत: उनमें वैचारिक संघर्ष की ज्वाला धधकती है, दहकती है और वे अपनेअपने मंतव्य को सत्यांश को पूर्णरूपेण सत्य और दूसरों के अभिमत को असत्य सिद्ध करने के लिए तर्क और वितर्क के तीर तलवार को लेकर वाग्युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और पारस्परिक संघर्ष भी प्रारम्भ हो जाता है, उसी संघर्ष रूपी ज्वाला को उपशान्त करने के लिये ज्योतिर्मय प्रभु महावीर ने एकान्तवाद के स्थान में अनेकान्तवाद की परम शीतल सरिता प्रवाहित की। उन्होंने नित्यत्व-अनित्यत्व आदि पक्षों को लेकर संघर्षरत दार्शनिकों को सुस्पष्ट और मधुर भाषा में कहा तुम सभी ने सत्य को नहीं समझा है, तुम्हारा एकान्तवाद भूल से भरा है। वस्तुस्थिति यह है कि पदार्थ न एकान्ततः नित्य है, न ध्रुव है, न शाश्वत है और न वह अनित्य--अशाश्वत है, वह अनन्तधर्मात्मक है, अतएव उसको एक ही धर्म से युक्त कहना सत्य का घोर तिरस्कार है।
___ अनेकान्त और स्याद्वाद दोनों एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं। यह भी एक तथ्य ज्ञातव्य है कि बाहर से एक सदृश प्रतीत होते हुए भी दोनों में अन्तर अवश्य है । अनेकान्त पदार्थ के मूल स्वरूप को देखने की एक विचार-पद्धति है। स्याद्वाद देखे हुए स्वरूप को अभिव्यक्त करने की भाषा-पद्धति है। अनेकान्त एक दार्शनिक दृष्टिकोण है और स्याद्वाद उसकी भाषा है । उस सिद्धान्त का प्ररूपण है।
वस्तुतः अनेकान्त चिंतन की अहिंसामयी प्रक्रिया है। इसका मूल सम्बन्ध मनुष्य के विचारों से जुड़ा हुआ है, स्याद्वाद अनेकान्तप्रधान चिंतन की अभिव्यक्ति की शैली है, यही कारण है कि स्याद्वाद उक्त प्रकारीय विचार को अभिव्यक्ति देने की लिए अहिंसामयी भाषा की अन्वेषणा करता है।
अनेक, अंत और वाद इन तीन शब्दों से अनेकांतवाद शब्द की निष्पत्ति होती है ।अनेक शब्द का वाच्य अर्थ है--नाना, अन्त का अर्थ है वस्तु-धर्म, वाद का अर्थ मान्यता है। एक पदार्थ में विभिन्न विरोधी-अविरोधी धर्मों की मान्यता का नाम अनेकान्तवाद है। इसकी दिव्यदृष्टि का ध्वनित अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ में सामान्य और विशेष रूप से, नित्यत्व की अपेक्षा से, अनित्यत्व की अपेक्षा से, सद्प से, असद्रूप से अनन्त-अनन्त धर्म विद्यमान हैं। अनेकान्तवाद का उन्मुक्त घोष है कि प्रत्येक वस्तु में हर गुण-धर्म अपने धर्म के साथ रहता है। जहां अनेकान्तवादी दृष्टिकोण हमारी बुद्धि को पदार्थ के सभी धर्मों की ओर समग्र रूप से खींचता है, वहां स्याद्वाद वस्तु के धर्म का प्रधान रूप से परिबोध कराने में सर्वथा रूप से समर्थ है। अनेकान्तवाद और स्याद्वाद–इनमें यह भी अन्तर है कि अनेकान्त दृष्टि का फल विधानात्मक है
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org