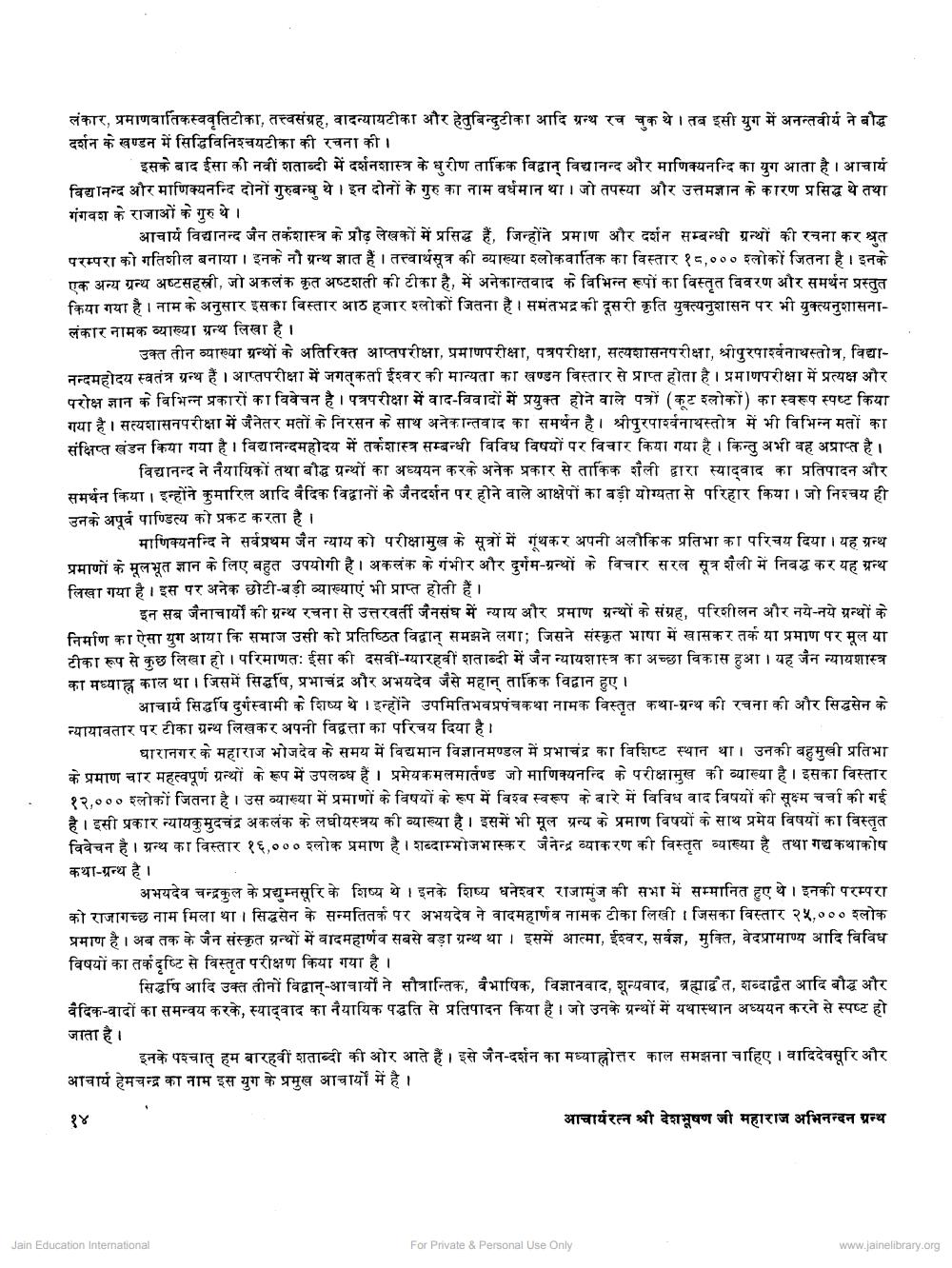________________
लंकार, प्रमाणवातिकस्ववृतिटोका, तत्त्वसंग्रह, वादन्यायटीका और हेतुबिन्दुटीका आदि ग्रन्थ रच चुक थे। तब इसी युग में अनन्तवीर्य ने बौद्ध दर्शन के खण्डन में सिद्धिविनिश्चयटीका की रचना की।
इसके बाद ईसा की नवीं शताब्दी में दर्शनशास्त्र के धुरीण तार्किक विद्वान् विद्यानन्द और माणिक्यनन्दि का युग आता है । आचार्य विद्यानन्द और माणिक्यनन्दि दोनों गुरुबन्धु थे। इन दोनों के गुरु का नाम वर्धमान था। जो तपस्या और उत्तमज्ञान के कारण प्रसिद्ध थे तथा गंगवश के राजाओं के गुरु थे।
आचार्य विद्यानन्द जैन तर्कशास्त्र के प्रौढ़ लेखकों में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने प्रमाण और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना कर श्रुत परम्परा को गतिशील बनाया। इनके नौ ग्रन्थ ज्ञात हैं । तत्त्वार्थसूत्र की व्याख्या श्लोकवातिक का विस्तार १८,००० श्लोकों जितना है। इनके एक अन्य ग्रन्थ अष्टसहस्री, जो अकलंक कृत अष्टशती की टीका है, में अनेकान्तवाद के विभिन्न रूपों का विस्तृत विवरण और समर्थन प्रस्तुत किया गया है । नाम के अनुसार इसका विस्तार आठ हजार श्लोकों जितना है । समंतभद्र की दूसरी कृति युक्त्यनुशासन पर भी युक्त्यनुशासनालंकार नामक व्याख्या ग्रन्थ लिखा है।
उक्त तीन व्याख्या ग्रन्थों के अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र, विद्यानन्दमहोदय स्वतंत्र ग्रन्थ हैं । आप्तपरीक्षा में जगत्कर्ता ईश्वर की मान्यता का खण्डन विस्तार से प्राप्त होता है । प्रमाणपरीक्षा में प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का विवेचन है । पत्रपरीक्षा में वाद-विवादों में प्रयुक्त होने वाले पत्रों (कूट श्लोकों) का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। सत्यशासनपरीक्षा में जैनेतर मतों के निरसन के साथ अनेकान्तवाद का समर्थन है। श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र में भी विभिन्न मतों का संक्षिप्त खंडन किया गया है। विद्यानन्दमहोदय में तर्कशास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर विचार किया गया है । किन्तु अभी वह अप्राप्त है।
विद्यानन्द ने नैयायिकों तथा बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन करके अनेक प्रकार से ताकिक शैली द्वारा स्याद्वाद का प्रतिपादन और समर्थन किया। इन्होंने कुमारिल आदि वैदिक विद्वानों के जैनदर्शन पर होने वाले आक्षेपों का बड़ी योग्यता से परिहार किया। जो निश्चय ही उनके अपूर्व पाण्डित्य को प्रकट करता है।
माणिक्यनन्दि ने सर्वप्रथम जैन न्याय को परीक्षामुख के सूत्रों में गूंथकर अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया। यह ग्रन्थ प्रमाणों के मूलभूत ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। अकलंक के गंभीर और दुर्गम-ग्रन्थों के विचार सरल सूत्र शैली में निबद्ध कर यह ग्रन्थ लिखा गया है। इस पर अनेक छोटी-बड़ी व्याख्याएं भी प्राप्त होती हैं।
इन सब जैनाचार्यों की ग्रन्थ रचना से उत्तरवर्ती जनसंघ में न्याय और प्रमाण ग्रन्थों के संग्रह, परिशीलन और नये-नये ग्रन्थों के निर्माण का ऐसा युग आया कि समाज उसी को प्रतिष्ठित विद्वान् समझने लगा; जिसने संस्कृत भाषा में खासकर तर्क या प्रमाण पर मूल या टीका रूप से कुछ लिखा हो । परिमाणतः ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में जैन न्यायशास्त्र का अच्छा विकास हुआ। यह जैन न्यायशास्त्र का मध्याह्न काल था। जिसमें सिषि, प्रभाचंद्र और अभयदेव जैसे महान तार्किक विद्वान हुए।
आचार्य सिद्धर्षि दुर्गस्वामी के शिष्य थे । इन्होंने उपमितिभवप्रपंचकथा नामक विस्तृत कथा-ग्रन्थ की रचना की और सिद्धसेन के न्यायावतार पर टीका ग्रन्थ लिखकर अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है।
धारानगर के महाराज भोजदेव के समय में विद्यमान विज्ञानमण्डल में प्रभाचंद्र का विशिष्ट स्थान था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के प्रमाण चार महत्वपूर्ण ग्रन्थों के रूप में उपलब्ध हैं। प्रमेयकमलमार्तण्ड जो माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख की व्याख्या है। इसका विस्तार १२,००० श्लोकों जितना है । उस व्याख्या में प्रमाणों के विषयों के रूप में विश्व स्वरूप के बारे में विविध वाद विषयों की सूक्ष्म चर्चा की गई है। इसी प्रकार न्यायकुमुदचंद्र अकलंक के लघीयस्त्रय की व्याख्या है। इसमें भी मूल ग्रन्य के प्रमाण विषयों के साथ प्रमेय विषयों का विस्तृत विवेचन है। ग्रन्थ का विस्तार १६,००० श्लोक प्रमाण है। शब्दाम्भोजभास्कर जैनेन्द्र व्याकरण की विस्तृत व्याख्या है तथा गद्य कथाकोष कथा-ग्रन्थ है।
अभयदेव चन्द्रकुल के प्रद्युम्नसूरि के शिष्य थे । इनके शिष्य धनेश्वर राजामुंज की सभा में सम्मानित हुए थे। इनकी परम्परा को राजागच्छ नाम मिला था। सिद्धसेन के सन्मतितर्क पर अभयदेव ने वादमहार्णव नामक टीका लिखी। जिसका विस्तार २५,००० श्लोक प्रमाण है। अब तक के जैन संस्कृत ग्रन्थों में वादमहार्णव सबसे बड़ा ग्रन्थ था। इसमें आत्मा, ईश्वर, सर्वज्ञ, मुक्ति, वेदप्रामाण्य आदि विविध विषयों का तर्क दृष्टि से विस्तृत परीक्षण किया गया है ।
सिद्धषि आदि उक्त तीनों विद्वान्-आचार्यों ने सौत्रान्तिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ब्रह्माद्वत, शब्दाद्वैत आदि बौद्ध और वैदिक-वादों का समन्वय करके, स्याद्वाद का नैयायिक पद्धति से प्रतिपादन किया है। जो उनके ग्रन्थों में यथास्थान अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है।
___ इनके पश्चात् हम बारहवीं शताब्दी की ओर आते हैं। इसे जैन-दर्शन का मध्याह्नोत्तर काल समझना चाहिए । वादिदेवसूरि और आचार्य हेमचन्द्र का नाम इस युग के प्रमुख आचार्यों में है।
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org