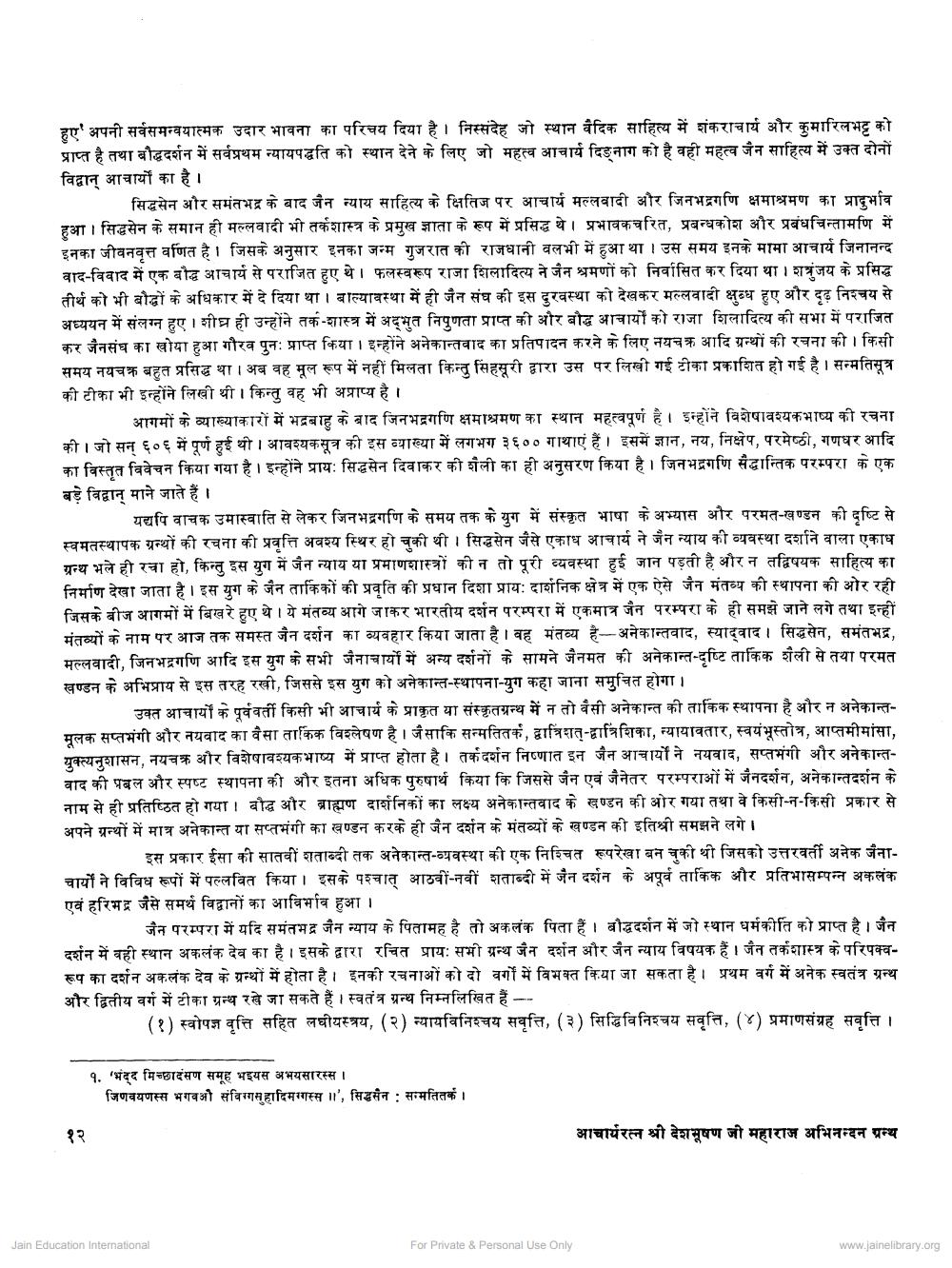________________
हुए अपनी सर्वसमन्वयात्मक उदार भावना का परिचय दिया है। निस्संदेह जो स्थान वैदिक साहित्य में शंकराचार्य और कुमारिलभट्ट को प्राप्त है तथा बौद्धदर्शन में सर्वप्रथम न्यायपद्धति को स्थान देने के लिए जो महत्व आचार्य दिङ्नाग को है वही महत्व जैन साहित्य में उक्त दोनों विद्वान् आचार्यों का है।
सिद्धसेन और समंतभद्र के बाद जैन न्याय साहित्य के क्षितिज पर आचार्य मल्लवादी और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का प्रादुर्भाव हुआ। सिद्धसेन के समान ही मल्लवादी भी तर्कशास्त्र के प्रमुख ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रभावकचरित, प्रबन्धकोश और प्रबंधचिन्तामणि में इनका जीवनवृत्त वणित है। जिसके अनुसार इनका जन्म गुजरात की राजधानी बलभी में हुआ था। उस समय इनके मामा आचार्य जिनानन्द वाद-विवाद में एक बौद्ध आचार्य से पराजित हुए थे। फलस्वरूप राजा शिलादित्य ने जैन श्रमणों को निर्वासित कर दिया था। शत्रुजय के प्रसिद्ध तीर्थ को भी बौद्धों के अधिकार में दे दिया था। बाल्यावस्था में ही जैन संघ की इस दुरवस्था को देखकर मल्लवादी क्षुब्ध हुए और दृढ़ निश्चय से अध्ययन में संलग्न हुए । शीघ्र ही उन्होंने तर्क-शास्त्र में अद्भुत निपुणता प्राप्त की और बौद्ध आचार्यों को राजा शिलादित्य की सभा में पराजित कर जैनसंघ का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त किया। इन्होंने अनेकान्तवाद का प्रतिपादन करने के लिए नयचक्र आदि ग्रन्थों की रचना की। किसी समय नयचक्र बहुत प्रसिद्ध था । अब वह मूल रूप में नहीं मिलता किन्तु सिंहसूरी द्वारा उस पर लिखी गई टीका प्रकाशित हो गई है। सन्मतिसूत्र की टीका भी इन्होंने लिखी थी। किन्तु वह भी अप्राप्य है।
आगमों के व्याख्याकारों में भद्रबाहु के बाद जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य की रचना की। जो सन् ६०६ में पूर्ण हुई थी। आवश्यक सूत्र की इस व्याख्या में लगभग ३६०० गाथाएं हैं। इसमें ज्ञान, नय, निक्षेप, परमेष्ठी, गणधर आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। इन्होंने प्रायः सिद्धसेन दिवाकर की शैली का ही अनुसरण किया है। जिनभद्रगणि सैद्धान्तिक परम्परा के एक बड़े विद्वान् माने जाते हैं।
यद्यपि वाचक उमास्वाति से लेकर जिनभद्रगणि के समय तक के युग में संस्कृत भाषा के अभ्यास और परमत-खण्डन की दृष्टि से स्वमतस्थापक ग्रन्थों की रचना की प्रवृत्ति अवश्य स्थिर हो चुकी थी। सिद्धसेन जैसे एकाध आचार्य ने जैन न्याय की व्यवस्था दर्शाने वाला एकाध ग्रन्थ भले ही रचा हो, किन्तु इस युग में जैन न्याय या प्रमाणशास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है और न तद्विषयक साहित्य का निर्माण देखा जाता है। इस युग के जैन तार्किकों की प्रवृति की प्रधान दिशा प्रायः दार्शनिक क्षेत्र में एक ऐसे जैन मंतव्य की स्थापना की ओर रही जिसके बीज आगमों में बिखरे हुए थे। ये मंतव्य आगे जाकर भारतीय दर्शन परम्परा में एकमात्र जैन परम्परा के ही समझे जाने लगे तथा इन्हीं मंतव्यों के नाम पर आज तक समस्त जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है। वह मंतव्य है-अनेकान्तवाद, स्याद्वाद। सिद्धसेन, समंतभद्र, मल्लवादी, जिनभद्रगणि आदि इस युग के सभी जैनाचार्यों में अन्य दर्शनों के सामने जैनमत की अनेकान्त-दृष्टि ताकिक शैली से तथा परमत खण्डन के अभिप्राय से इस तरह रखी, जिससे इस युग को अनेकान्त-स्थापना-युग कहा जाना समुचित होगा।
उक्त आचार्यों के पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य के प्राकृत या संस्कृतग्रन्थ में न तो वैसी अनेकान्त की ताकिक स्थापना है और न अनेकान्तमूलक सप्तभंगी और नयवाद का वैसा तार्किक विश्लेषण है । जैसाकि सन्मतितर्क, द्वात्रिंशत्-द्वात्रिशिका, न्यायावतार, स्वयंभूस्तोत्र, आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन, नयचक्र और विशेषावश्यकभाष्य में प्राप्त होता है। तर्कदर्शन निष्णात इन जैन आचार्यों ने नयवाद, सप्तभंगी और अनेकान्तवाद की प्रबल और स्पष्ट स्थापना की और इतना अधिक पुरुषार्थ किया कि जिससे जैन एवं जैनेतर परम्पराओं में जैनदर्शन, अनेकान्तदर्शन के नाम से ही प्रतिष्ठित हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण दार्शनिकों का लक्ष्य अनेकान्तवाद के खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने ग्रन्थों में मात्र अनेकान्त या सप्तभंगी का खण्डन करके ही जैन दर्शन के मंतव्यों के खण्डन की इतिश्री समझने लगे।
इस प्रकार ईसा की सातवीं शताब्दी तक अनेकान्त-व्यवस्था की एक निश्चित रूपरेखा बन चुकी थी जिसको उत्तरवर्ती अनेक जैनाचार्यों ने विविध रूपों में पल्लवित किया। इसके पश्चात् आठवीं-नवीं शताब्दी में जैन दर्शन के अपूर्व ताकिक और प्रतिभासम्पन्न अकलंक एवं हरिभद्र जैसे समर्थ विद्वानों का आविर्भाव हुआ।
जैन परम्परा में यदि समंतभद्र जैन न्याय के पितामह है तो अकलंक पिता हैं। बौद्धदर्शन में जो स्थान धर्मकीति को प्राप्त है। जैन दर्शन में वही स्थान अकलंक देव का है। इसके द्वारा रचित प्रायः सभी ग्रन्थ जैन दर्शन और जैन न्याय विषयक हैं । जैन तर्कशास्त्र के परिपक्वरूप का दर्शन अकलंक देव के ग्रन्थों में होता है। इनकी रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ और द्वितीय वर्ग में टीका ग्रन्थ रखे जा सकते हैं । स्वतंत्र ग्रन्थ निम्नलिखित हैं --
(१) स्वोपज्ञ वृत्ति सहित लघीयस्त्रय, (२) न्यायविनिश्चय सवृत्ति, (३) सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति, (४) प्रमाणसंग्रह सवृत्ति ।
१. 'भंद्द मिच्छादसण समूह भइयस अभयसारस्स । जिणवयणस्स भगवऔ संविग्गसुहादिमग्गस्स ॥', सिद्धसैन : सन्मतितर्क ।
आचार्यरत्न श्री देशमूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org