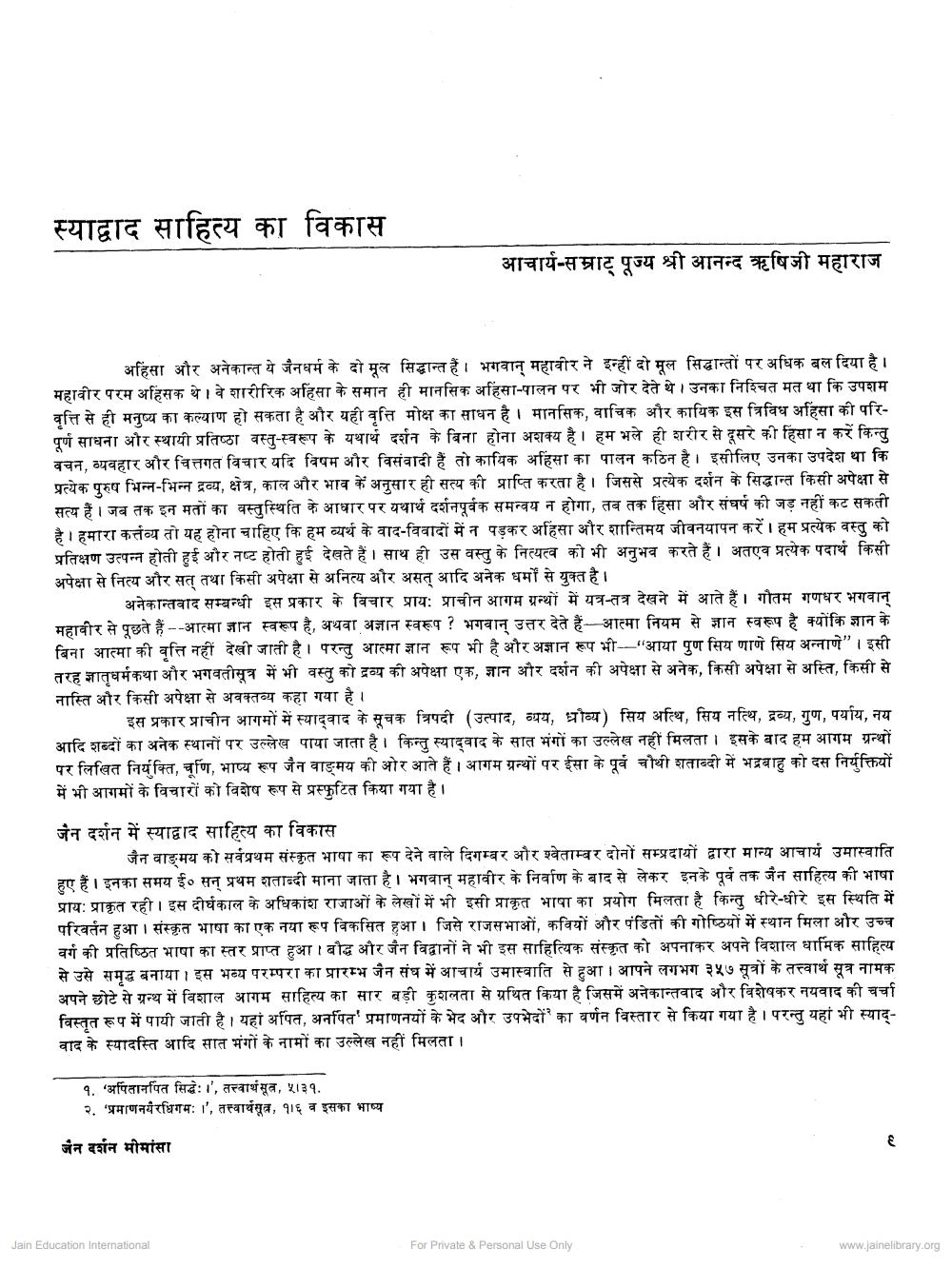________________
स्याद्वाद साहित्य का विकास
आचार्य-सम्राट् पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज
अहिंसा और अनेकान्त ये जैनधर्म के दो मूल सिद्धान्त हैं। भगवान् महावीर ने इन्हीं दो मूल सिद्धान्तों पर अधिक बल दिया है। महावीर परम अहिंसक थे। वे शारीरिक अहिंसा के समान ही मानसिक अहिंसा-पालन पर भी जोर देते थे। उनका निश्चित मत था कि उपशम वृत्ति से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है और यही वृत्ति मोक्ष का साधन है। मानसिक, वाचिक और कायिक इस त्रिविध अहिंसा की परिपूर्ण साधना और स्थायी प्रतिष्ठा वस्तु-स्वरूप के यथार्थ दर्शन के बिना होना अशक्य है। हम भले ही शरीर से दूसरे की हिंसा न करें किन्तु वचन, व्यवहार और चित्तगत विचार यदि विषम और विसंवादी हैं तो कायिक अहिंसा का पालन कठिन है। इसीलिए उनका उपदेश था कि प्रत्येक पुरुष भिन्न-भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही सत्य की प्राप्ति करता है। जिससे प्रत्येक दर्शन के सिद्धान्त किसी अपेक्षा से सत्य हैं । जब तक इन मतों का वस्तुस्थिति के आधार पर यथार्थ दर्शनपूर्वक समन्वय न होगा, तब तक हिंसा और संघर्ष की जड़ नहीं कट सकती है। हमारा कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि हम व्यर्थ के वाद-विवादों में न पड़कर अहिंसा और शान्तिमय जीवनयापन करें। हम प्रत्येक वस्तु को प्रतिक्षण उत्पन्न होती हुई और नष्ट होती हुई देखते हैं। साथ ही उस वस्तु के नित्यत्व को भी अनुभव करते हैं। अतएव प्रत्येक पदार्थ किसी अपेक्षा से नित्य और सत् तथा किसी अपेक्षा से अनित्य और असत् आदि अनेक धर्मों से युक्त है।
अनेकान्तवाद सम्बन्धी इस प्रकार के विचार प्राय: प्राचीन आगम ग्रन्थों में यत्र-तत्र देखने में आते हैं। गौतम गणधर भगवान् महावीर से पूछते हैं --आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अथवा अज्ञान स्वरूप ? भगवान् उत्तर देते हैं-आत्मा नियम से ज्ञान स्वरूप है क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा की वृत्ति नहीं देखी जाती है। परन्तु आत्मा ज्ञान रूप भी है और अज्ञान रूप भी_“आया पुण सिय णाणे सिय अन्नाणे"। इसी तरह ज्ञातृधर्मकथा और भगवतीसूत्र में भी वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा एक, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से अनेक, किसी अपेक्षा से अस्ति, किसी से नास्ति और किसी अपेक्षा से अवक्तव्य कहा गया है।
इस प्रकार प्राचीन आगमों में स्याद्वाद के सूचक त्रिपदी (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य) सिय अत्थि, सिय नत्थि, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय आदि शब्दों का अनेक स्थानों पर उल्लेख पाया जाता है। किन्तु स्याद्वाद के सात भंगों का उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद हम आगम ग्रन्थों पर लिखित नियुक्ति, चूणि, भाष्य रूप जैन वाङ्मय की ओर आते हैं। आगम ग्रन्थों पर ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में भद्रबाहु को दस नियुक्तियों में भी आगमों के विचारों को विशेष रूप से प्रस्फुटित किया गया है।
जैन दर्शन में स्याद्वाद साहित्य का विकास
जैन वाङ्मय को सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का रूप देने वाले दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों द्वारा मान्य आचार्य उमास्वाति हुए हैं। इनका समय ई० सन् प्रथम शताब्दी माना जाता है। भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद से लेकर इनके पूर्व तक जैन साहित्य की भाषा प्रायः प्राकृत रही। इस दीर्घकाल के अधिकांश राजाओं के लेखों में भी इसी प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है किन्तु धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन हुआ । संस्कृत भाषा का एक नया रूप विकसित हुआ। जिसे राजसभाओं, कवियों और पंडितों की गोष्ठियों में स्थान मिला और उच्च वर्ग की प्रतिष्ठित भाषा का स्तर प्राप्त हुआ। बौद्ध और जैन विद्वानों ने भी इस साहित्यिक संस्कृत को अपनाकर अपने विशाल धार्मिक साहित्य से उसे समृद्ध बनाया। इस भव्य परम्परा का प्रारम्भ जैन संघ में आचार्य उमास्वाति से हुआ। आपने लगभग ३५७ सूत्रों के तत्त्वार्थ सूत्र नामक अपने छोटे से ग्रन्थ में विशाल आगम साहित्य का सार बड़ी कुशलता से ग्रथित किया है जिसमें अनेकान्तवाद और विशेषकर नयवाद की चर्चा विस्तृत रूप में पायी जाती है। यहां अपित, अनर्पित प्रमाणनयों के भेद और उपभेदों का वर्णन विस्तार से किया गया है। परन्तु यहां भी स्याद्वाद के स्यादस्ति आदि सात भंगों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता।
१. 'अर्पितानपित सिद्धेः।', तत्त्वार्थ सूत्र, ५।३१. २. 'प्रमाणनयरधिगमः ।', तत्त्वार्थसूत्र, ११६ व इसका भाष्य
जैन दर्शन मीमांसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org