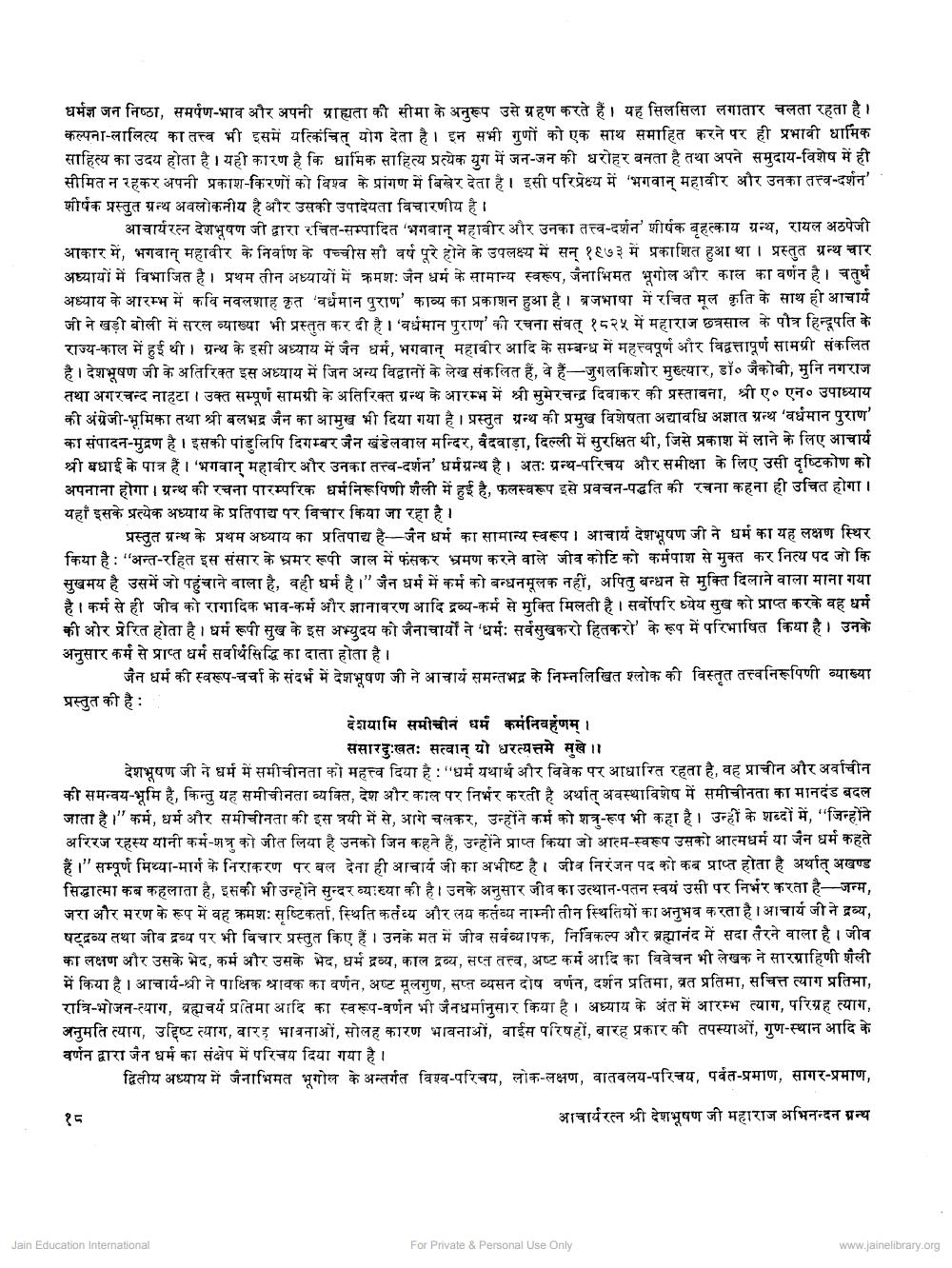________________
धर्मज्ञ जन निष्ठा, समर्पण-भाव और अपनी ग्राह्यता की सीमा के अनुरूप उसे ग्रहण करते हैं। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। कल्पना-लालित्य का तत्त्व भी इसमें यत्किंचित् योग देता है। इन सभी गुणों को एक साथ समाहित करने पर ही प्रभावी धार्मिक साहित्य का उदय होता है। यही कारण है कि धार्मिक साहित्य प्रत्येक युग में जन-जन की धरोहर बनता है तथा अपने समुदाय-विशेष में ही सीमित न रहकर अपनी प्रकाश-किरणों को विश्व के प्रांगण में बिखेर देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में "भगवान् महावीर और उनका तत्त्व-दर्शन' - शीर्षक प्रस्तुत ग्रन्थ अवलोकनीय है और उसकी उपादेयता विचारणीय है।
आचार्यरत्न देशभूषण जी द्वारा रचित-सम्पादित 'भगवान् महावीर और उनका तत्त्व-दर्शन' शीर्षक बृहत्काय ग्रन्थ, रायल अठपेजी आकार में, भगवान् महावीर के निर्वाण के पच्चीस सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सन् १९७३ में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत ग्रन्थ चार अध्यायों में विभाजित है। प्रथम तीन अध्यायों में क्रमशः जैन धर्म के सामान्य स्वरूप, जैनाभिमत भूगोल और काल का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में कवि नवलशाह कृत 'बर्धमान पुराण' काव्य का प्रकाशन हुआ है। ब्रजभाषा में रचित मूल कृति के साथ ही आचार्य जी ने खड़ी बोली में सरल व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है। 'वर्धमान पुराण' की रचना संवत् १८२५ में महाराज छत्रसाल के पौत्र हिन्दूपति के राज्य-काल में हुई थी। ग्रन्थ के इसी अध्याय में जैन धर्म, भगवान महावीर आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण और विद्वत्तापूर्ण सामग्री संकलित है। देशभूषण जी के अतिरिक्त इस अध्याय में जिन अन्य विद्वानों के लेख संकलित हैं, वे हैं-जुगलकिशोर मुख्त्यार, डॉ० जैकोबी, मुनि नगराज तथा अगरचन्द नाहटा । उक्त सम्पूर्ण सामग्री के अतिरिक्त ग्रन्थ के आरम्भ में श्री सुमेरचन्द्र दिवाकर की प्रस्तावना, श्री ए० एन० उपाध्याय की अंग्रेजी-भृमिका तथा श्री बलभद्र जैन का आमुख भी दिया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता अद्यावधि अज्ञात ग्रन्थ 'वर्धमान पुराण' का संपादन-मुद्रण है। इसकी पांडुलिपि दिगम्बर जैन खंडेलवाल मन्दिर, वैदवाड़ा, दिल्ली में सुरक्षित थी, जिसे प्रकाश में लाने के लिए आचार्य श्री बधाई के पात्र हैं । 'भगवान् महावीर और उनका तत्त्व-दर्शन' धर्मग्रन्थ है। अतः ग्रन्थ-परिचय और समीक्षा के लिए उसी दृष्टिकोण को अपनाना होगा । ग्रन्थ की रचना पारम्परिक धर्मनिरूपिणी शैली में हुई है, फलस्वरूप इसे प्रवचन-पद्धति की रचना कहना ही उचित होगा। यहाँ इसके प्रत्येक अध्याय के प्रतिपाद्य पर विचार किया जा रहा है।
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य है-जैन धर्म का सामान्य स्वरूप। आचार्य देशभूषण जी ने धर्म का यह लक्षण स्थिर किया है : “अन्त-रहित इस संसार के भ्रमर रूपी जाल में फंसकर भ्रमण करने वाले जीव कोटि को कर्मपाश से मुक्त कर नित्य पद जो कि सुखमय है उसमें जो पहुंचाने वाला है, वही धर्म है।" जैन धर्म में कर्म को बन्धनमूलक नहीं, अपितु बन्धन से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कर्म से ही जीव को रागादिक भाव-कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य-कर्म से मुक्ति मिलती है। सर्वोपरि ध्येय सुख को प्राप्त करके वह धर्म की ओर प्रेरित होता है। धर्म रूपी सुख के इस अभ्युदय को जैनाचार्यों ने 'धर्मः सर्वसुखकरो हितकरो' के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार कर्म से प्राप्त धर्म सर्वार्थसिद्धि का दाता होता है।
जैन धर्म की स्वरूप-चर्चा के संदर्भ में देशभूषण जी ने आचार्य समन्तभद्र के निम्नलिखित श्लोक की विस्तृत तत्त्वनिरूपिणी व्याख्या प्रस्तुत की है :
देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिवहणम्।
संसारदुःखतः सत्वान् यो धरत्यत्तमे मुखे। देशभूषण जी ने धर्म में समीचीनता को महत्त्व दिया है : "धर्म यथार्थ और विवेक पर आधारित रहता है, वह प्राचीन और अर्वाचीन की समन्वय-भूमि है, किन्तु यह समीचीनता व्यक्ति, देश और काल पर निर्भर करती है अर्थात् अवस्थाविशेष में समीचीनता का मानदंड बदल जाता है।" कर्म, धर्म और समीचीनता की इस त्रयी में से, आगे चलकर, उन्होंने कर्म को शत्र-रूप भी कहा है। उन्हीं के शब्दों में, "जिन्होंने अरिरज रहस्य यानी कर्म-शत्रु को जीत लिया है उनको जिन कहते हैं, उन्होंने प्राप्त किया जो आत्म-स्वरूप उसको आत्मधर्म या जैन धर्म कहते हैं।" सम्पूर्ण मिथ्या-मार्ग के निराकरण पर बल देना ही आचार्य जी का अभीष्ट है। जीव निरंजन पद को कब प्राप्त होता है अर्थात् अखण्ड सिद्धात्मा कब कहलाता है, इसकी भी उन्होंने सुन्दर व्याख्या की है। उनके अनुसार जीव का उत्थान-पतन स्वयं उसी पर निर्भर करता है—जन्म, जरा और मरण के रूप में वह क्रमशः सृष्टिकर्ता, स्थिति कर्तव्य और लय कर्तव्य नाम्नी तीन स्थितियों का अनुभव करता है । आचार्य जी ने द्रव्य, षद्रव्य तथा जीव द्रव्य पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके मत में जीव सर्वव्यापक, निर्विकल्प और ब्रह्मानंद में सदा तैरने वाला है । जीव का लक्षण और उसके भेद, कर्म और उसके भेद, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, सप्त तत्त्व, अष्ट कर्म आदि का विवेचन भी लेखक ने सारग्राहिणी शैली में किया है । आचार्य-श्री ने पाक्षिक श्रावक का वर्णन, अष्ट मूलगुण, सप्त व्यसन दोष वर्णन, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि-भोजन-त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा आदि का स्वरूप-वर्णन भी जैनधर्मानुसार किया है। अध्याय के अंत में आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, बारह भावनाओं, सोलह कारण भावनाओं, बाईस परिषहों, बारह प्रकार की तपस्याओं, गुण-स्थान आदि के वर्णन द्वारा जैन धर्म का संक्षेप में परिचय दिया गया है।
द्वितीय अध्याय में जैनाभिमत भूगोल के अन्तर्गत विश्व-परिचय, लोक-लक्षण, वातवलय-परिचय, पर्वत-प्रमाण, सागर-प्रमाण,
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org