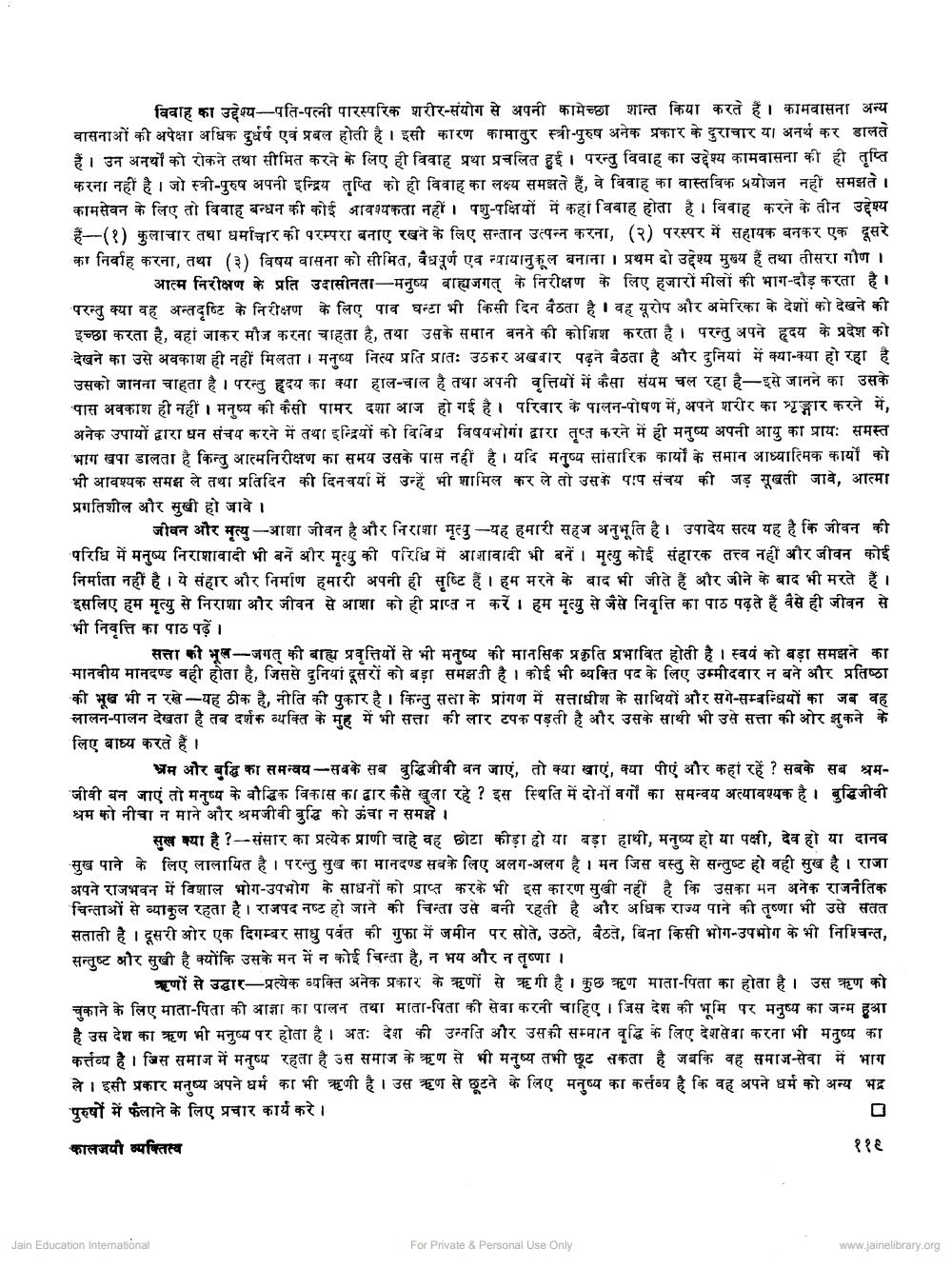________________
विवाह का उद्देश्य-पति-पत्नी पारस्परिक शरीर-संयोग से अपनी कामेच्छा शान्त किया करते हैं। कामवासना अन्य वासनाओं की अपेक्षा अधिक दुर्धर्ष एवं प्रबल होती है । इसी कारण कामातुर स्त्री-पुरुष अनेक प्रकार के दुराचार या अनर्थ कर डालते हैं। उन अनर्थों को रोकने तथा सीमित करने के लिए ही विवाह प्रथा प्रचलित हुई। परन्तु विवाह का उद्देश्य कामवासना की ही तृप्ति करना नहीं है । जो स्त्री-पुरुष अपनी इन्द्रिय तृप्ति को ही विवाह का लक्ष्य समझते हैं, वे विवाह का वास्तविक प्रयोजन नहीं समझते। कामसेवन के लिए तो विवाह बन्धन की कोई आवश्यकता नहीं। पशु-पक्षियों में कहां विवाह होता है । विवाह करने के तीन उद्देश्य हैं-(१) कुलाचार तथा धर्माचार की परम्परा बनाए रखने के लिए सन्तान उत्पन्न करना, (२) परस्पर में सहायक बनकर एक दूसरे का निर्वाह करना, तथा (३) विषय वासना को सीमित, वैधपूर्ण एव न्यायानुकूल बनाना । प्रथम दो उद्देश्य मुख्य हैं तथा तीसरा गौण ।
आत्म निरीक्षण के प्रति उदासीनता-मनुष्य बाह्यजगत् के निरीक्षण के लिए हजारों मीलों की भाग-दौड़ करता है। परन्तु क्या वह अन्तदृष्टि के निरीक्षण के लिए पाव घन्टा भी किसी दिन बैठता है । वह यूरोप और अमेरिका के देशों को देखने की इच्छा करता है, वहां जाकर मौज करना चाहता है, तथा उसके समान बनने की कोशिश करता है। परन्तु अपने हृदय के प्रदेश को देखने का उसे अवकाश ही नहीं मिलता। मनुष्य नित्य प्रति प्रातः उठकर अखबार पढ़ने बैठता है और दुनियां में क्या-क्या हो रहा है उसको जानना चाहता है। परन्तु हृदय का क्या हाल-चाल है तथा अपनी वृत्तियों में कैसा संयम चल रहा है-इसे जानने का उसके पास अवकाश ही नहीं। मनुष्य की कैसी पामर दशा आज हो गई है। परिवार के पालन-पोषण में, अपने शरीर का शृङ्गार करने में, अनेक उपायों द्वारा धन संचय करने में तथा इन्द्रियों को विविध विषयभोगी द्वारा तृप्त करने में ही मनुष्य अपनी आयु का प्रायः समस्त भाग खपा डालता है किन्तु आत्मनिरीक्षण का समय उसके पास नहीं है। यदि मनुष्य सांसारिक कार्यों के समान आध्यात्मिक कार्यों को भी आवश्यक समझ ले तथा प्रतिदिन की दिनचर्या में उन्हें भी शामिल कर ले तो उसके पाप संचय की जड़ सूखती जावे, आत्मा प्रगतिशील और सुखी हो जावे।
जीवन और मृत्यु-आशा जीवन है और निराशा मृत्यु-यह हमारी सहज अनुभूति है। उपादेय सत्य यह है कि जीवन की परिधि में मनुष्य निराशावादी भी बनें और मृत्यु की परिधि में आशावादी भी बनें। मृत्यु कोई संहारक तत्त्व नहीं और जीवन कोई निर्माता नहीं है । ये संहार और निर्माण हमारी अपनी ही सृष्टि हैं । हम मरने के बाद भी जीते हैं और जीने के बाद भी मरते हैं। इसलिए हम मृत्यु से निराशा और जीवन से आशा को ही प्राप्त न करें। हम मृत्यु से जैसे निवृत्ति का पाठ पढ़ते हैं वैसे ही जीवन से भी निवृत्ति का पाठ पढ़ें।
सत्ता की भूख-जगत् की बाह्य प्रवृत्तियों से भी मनुष्य की मानसिक प्रकृति प्रभावित होती है। स्वयं को बड़ा समझने का मानवीय मानदण्ड वही होता है, जिससे दुनियां दूसरों को बड़ा समझती है। कोई भी व्यक्ति पद के लिए उम्मीदवार न बने और प्रतिष्ठा की भूख भी न रखे-यह ठीक है, नीति की पुकार है। किन्तु सत्ता के प्रांगण में सत्ताधीश के साथियों और सगे-सम्बन्धियों का जब वह लालन-पालन देखता है तब दर्शक व्यक्ति के मुह में भी सत्ता की लार टपक पड़ती है और उसके साथी भी उसे सत्ता की ओर झुकने के लिए बाध्य करते हैं।
भ्रम और बुद्धि का समन्वय-सबके सब बुद्धिजीवी बन जाएं, तो क्या खाएं, क्या पीएं और कहां रहें ? सबके सब श्रमजीवी बन जाएं तो मनुष्य के बौद्धिक विकास का द्वार कैसे खुला रहे ? इस स्थिति में दोनों वगों का समन्वय अत्यावश्यक है। बुद्धिजीवी श्रम को नीचा न माने और श्रमजीवी बुद्धि को ऊंचा न समझे।
सुख क्या है ?--संसार का प्रत्येक प्राणी चाहे वह छोटा कीड़ा हो या बड़ा हाथी, मनुष्य हो या पक्षी, देव हो या दानव सुख पाने के लिए लालायित है । परन्तु सुख का मानदण्ड सबके लिए अलग-अलग है । मन जिस वस्तु से सन्तुष्ट हो वही सुख है । राजा अपने राजभवन में विशाल भोग-उपभोग के साधनों को प्राप्त करके भी इस कारण सुखी नहीं है कि उसका मन अनेक राजनैतिक चिन्ताओं से व्याकुल रहता है। राजपद नष्ट हो जाने की चिन्ता उसे बनी रहती है और अधिक राज्य पाने की तृष्णा भी उसे सतत सताती है । दूसरी ओर एक दिगम्बर साधु पर्वत की गुफा में जमीन पर सोते, उठते, बैठते, बिना किसी भोग-उपभोग के भी निश्चिन्त, सन्तुष्ट और सुखी है क्योंकि उसके मन में न कोई चिन्ता है, न भय और न तृष्णा ।
ऋणों से उद्धार–प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के ऋणों से ऋगी है । कुछ ऋण माता-पिता का होता है। उस ऋण को चुकाने के लिए माता-पिता की आज्ञा का पालन तथा माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। जिस देश की भूमि पर मनुष्य का जन्म हुआ है उस देश का ऋण भी मनुष्य पर होता है। अतः देश की उन्नति और उसकी सम्मान वृद्धि के लिए देशसेवा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है । जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के ऋण से भी मनुष्य तभी छूट सकता है जबकि वह समाज-सेवा में भाग ले। इसी प्रकार मनुष्य अपने धर्म का भी ऋणी है । उस ऋण से छूटने के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म को अन्य भद्र पुरुषों में फैलाने के लिए प्रचार कार्य करे। कालजयी व्यक्तित्व
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org