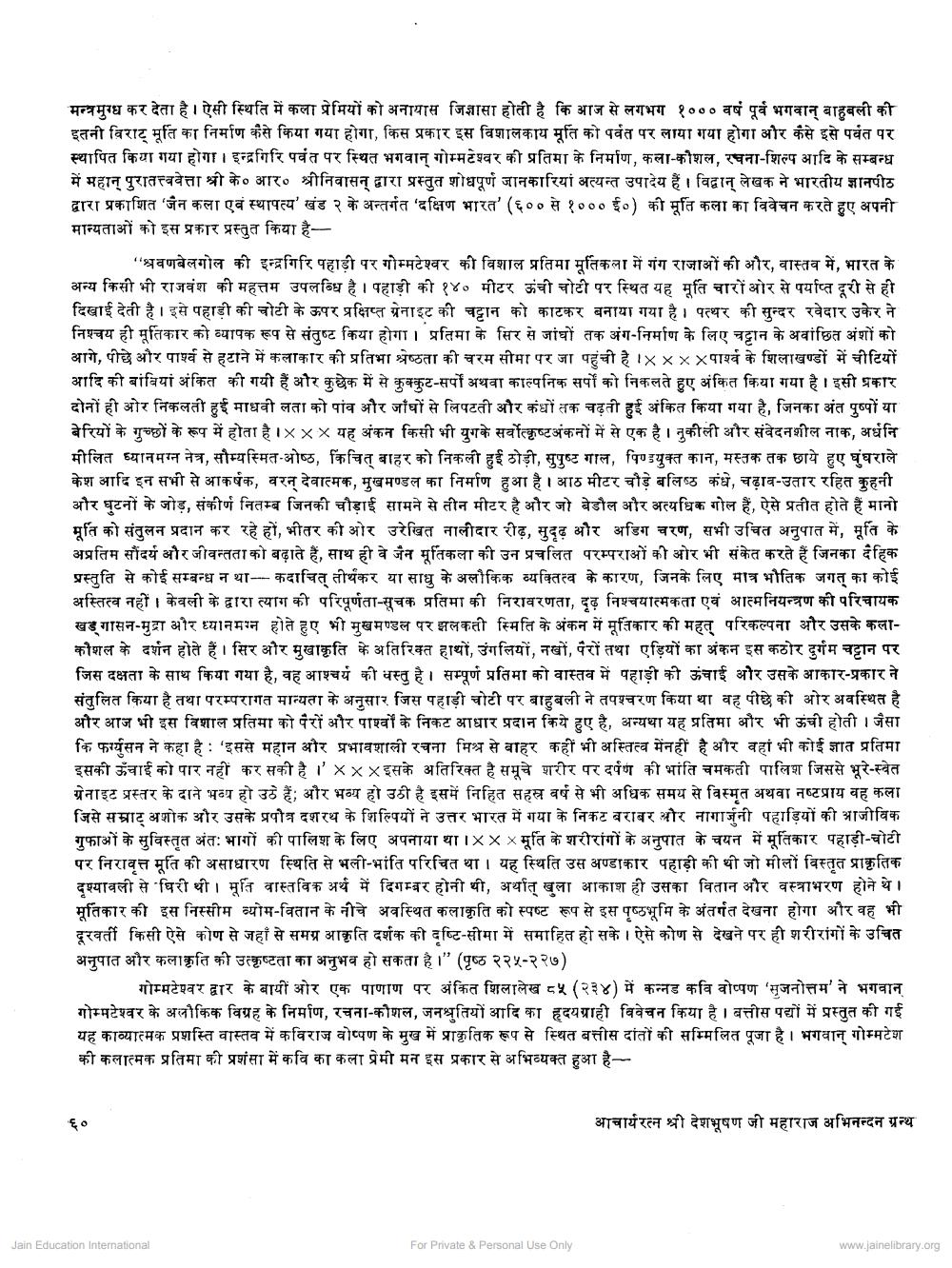________________
मन्त्रमुग्ध कर देता है । ऐसी स्थिति में कला प्रेमियों को अनायास जिज्ञासा होती है कि आज से लगभग १००० वर्ष पूर्व भगवान् बाहुबली की इतनी विराट् मूर्ति का निर्माण कैसे किया गया होगा, किस प्रकार इस विशालकाय मूर्ति को पर्वत पर लाया गया होगा और कैसे इसे पर्वत पर स्थापित किया गया होगा । इन्द्रगिरि पर्वत पर स्थित भगवान् गोम्मटेश्वर की प्रतिमा के निर्माण, कला-कौशल, रचना - शिल्प आदि के सम्बन्ध में महान पुरातत्ववेत्ता श्री के० आर० श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत शोधपूर्ण जानकारियां अत्यन्त उपादेय हैं। विद्वान् लेखक ने भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'जैन कला एवं स्थापत्य' खंड २ के अन्तर्गत 'दक्षिण भारत' (६०० से १००० ई०) की मूर्ति कला का विवेचन करते मान्यताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया है
हुए
अपनी
3
"श्रवणबेलगोल की इन्द्रगिरि पहाड़ी पर गोम्मटेश्वर की विशाल प्रतिमा मूर्तिकला में गंग राजाओं की और वास्तव में, भारत के अन्य किसी भी राजवंश की महत्तम उपलब्धि है। पहाड़ी की १४० मीटर ऊंची चोटी पर स्थित यह मूर्ति चारों ओर से पर्याप्त दूरी से ही दिखाई देती है । इसे पहाड़ी की चोटी के ऊपर प्रक्षिप्त ग्रेनाइट की चट्टान को काटकर बनाया गया है। पत्थर की सुन्दर रवेदार उकेर ने निश्चय ही मूर्तिकार को व्यापक रूप से संतुष्ट किया होगा प्रतिमा के सिर से जांघों तक अंग निर्माण के लिए चट्टान के अवांछित अंशों को आगे, पीछे और पार्श्व से हटाने में कलाकार की प्रतिभा श्रेष्ठता की चरम सीमा पर जा पहुंची है । XXX X पार्श्व के शिलाखण्डों में चीटियों आदि की बबियां अंकित की गयी हैं और कुछेक में से कुक्कुट सर्पो अथवा काल्पनिक सर्पों को निकलते हुए अंकित किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही ओर निकलती हुई माधवी लता को पांव और जांघों से लिपटती और कंधों तक चढ़ती हुई अंकित किया गया है, जिनका अंत पुष्पों वा बेरियों के गुच्छों के रूप में होता है। XXX यह अंकन किसी भी युगके सर्वोत्कृष्ट अंकनों में से एक है। नुकीली और संवेदनशील नाक, अर्धनि मीलित ध्यानमग्न नेत्र, सौम्यस्मित-ओष्ठ, किंचित् बाहर को निकली हुई ठोड़ी, सुपुष्ट गाल, पिण्डयुक्त कान, मस्तक तक छाये हुए घुंघराले केश आदि इन सभी से आकर्षक, वरन् देवात्मक, मुखमण्डल का निर्माण हुआ है। आठ मीटर चौड़े बलिष्ठ कंधे चढ़ाव उतार रहित कुहनी और घुटनों के जोड़, संकीर्ण नितम्ब जिनकी चौड़ाई सामने से तीन मीटर है और जो बेडौल और अत्यधिक गोल हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मूर्ति को संतुलन प्रदान कर रहे हों, भीतर की ओर उरेखित नालीदार रोड़, मुदृद्द और अगि चरण, सभी उचित अनुपात में मूर्ति के अप्रतिम सौंदर्य और जीवन्तता को बढ़ाते हैं, साथ ही वे जैन मूर्तिकला की उन प्रचलित परम्पराओं की ओर भी संकेत करते हैं जिनका दैहिक प्रस्तुति से कोई सम्बन्ध न था कदाचित् तीर्थंकर या साधु के अलौकिक व्यक्तित्व के कारण, जिनके लिए मात्र भौतिक जगत् का कोई अस्तित्व नहीं । केवली के द्वारा त्याग की परिपूर्णता सूचक प्रतिमा की निरावरणता, दृढ़ निश्चयात्मकता एवं आत्मनियन्त्रण की परिचायक खड्गासन मुद्रा और ध्यानमग्न होते हुए भी मुखमण्डल पर झलकती स्मिति के अंकन में मूर्तिकार की महत् परिकल्पना और उसके कलाकौशल के दर्शन होते हैं। सिर और मुखाकृति के अतिरिक्त हाथों, उंगलियों, नखों, पैरों तथा एड़ियों का अंकन इस कठोर दुर्गम चट्टान पर जिस दक्षता के साथ किया गया है, वह आश्चर्य की वस्तु है । सम्पूर्ण प्रतिमा को वास्तव में पहाड़ी की ऊंचाई और उसके आकार-प्रकार ने संतुलित किया है तथा परम्परागत मान्यता के अनुसार जिस पहाड़ी चोटी पर बाहुबली ने तपश्चरण किया था वह पीछे की ओर अवस्थित है और आज भी इस विशाल प्रतिमा को पैरों और पाश्र्वों के निकट आधार प्रदान किये हुए है, अन्यथा यह प्रतिमा और भी ऊंची होती । जैसा कि फर्ग्युसन ने कहा है : 'इससे महान और प्रभावशाली रचना मिश्र से बाहर कहीं भी अस्तित्व मेंनहीं है और वहां भी कोई ज्ञात प्रतिमा इसकी ऊँचाई को पार नहीं कर सकी है ।' x x x इसके अतिरिक्त है समूचे शरीर पर दर्पण की भांति चमकती पालिश जिससे भूरे-स्वेत ग्रेनाइट प्रस्तर के दाने भव्य हो उठे हैं; और भव्य हो उठी है इसमें निहित सहस्र वर्ष से भी अधिक समय से विस्मृत अथवा नष्टप्राय वह कला जिसे सम्राट् अशोक और उसके प्रपौत्र दशरथ के शिल्पियों ने उत्तर भारत में गया के निकट बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की आजीविक गुफाओं के सुविस्तृत अंतः भागों की पालिश के लिए अपनाया था। XXX मूर्ति के शरीरांगों के अनुपात के चयन में मूर्तिकार पहाड़ी-चोटी पर निरावृत्त मूर्ति की असाधारण स्थिति से भली-भांति परिचित था । यह स्थिति उस अण्डाकार पहाड़ी की थी जो मीलों विस्तृत प्राकृतिक दृश्यावली से घिरी थी । मूर्ति वास्तविक अर्थ में दिगम्बर होनी थी, अर्थात् खुला आकाश ही उसका वितान और वस्त्राभरण होने थे । मूर्तिकार की इस निस्सीम स्पोष वितान के नीचे अवस्थित कलाकृति को स्पष्ट रूप से इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखना होगा और वह भी दूरवर्ती किसी ऐसे कोण से जहाँ से समग्र आकृति दर्शक की दृष्टि-सीमा में समाहित हो सके। ऐसे कोण से देखने पर ही शरीरांगों के उचित अनुपात और कलाकृति की उत्कृष्टता का अनुभव हो सकता है।” (पृष्ठ २२५-२२७ )
गोम्मटेश्वर द्वार के बायीं ओर एक पाणाण पर अंकित शिलालेख ८५ (२३४) में कन्नड़ कवि वोप्पण 'सुजनोत्तम' ने भगवान् गोम्मटेश्वर के अलौकिक विग्रह के निर्माण, रचना कौशल, जनधुतियों आदि का हृदयग्राही विवेचन किया है। बत्तीस पद्यों में प्रस्तुत की गई यह काव्यात्मक प्रशस्ति वास्तव में कविराज वोप्पण के मुख में प्राकृतिक रूप से स्थित बत्तीस दांतों की सम्मिलित पूजा है । भगवान् गोम्मटेश की कलात्मक प्रतिमा की प्रशंसा में कवि का कला प्रेमी मन इस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है
६०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
www.jainelibrary.org