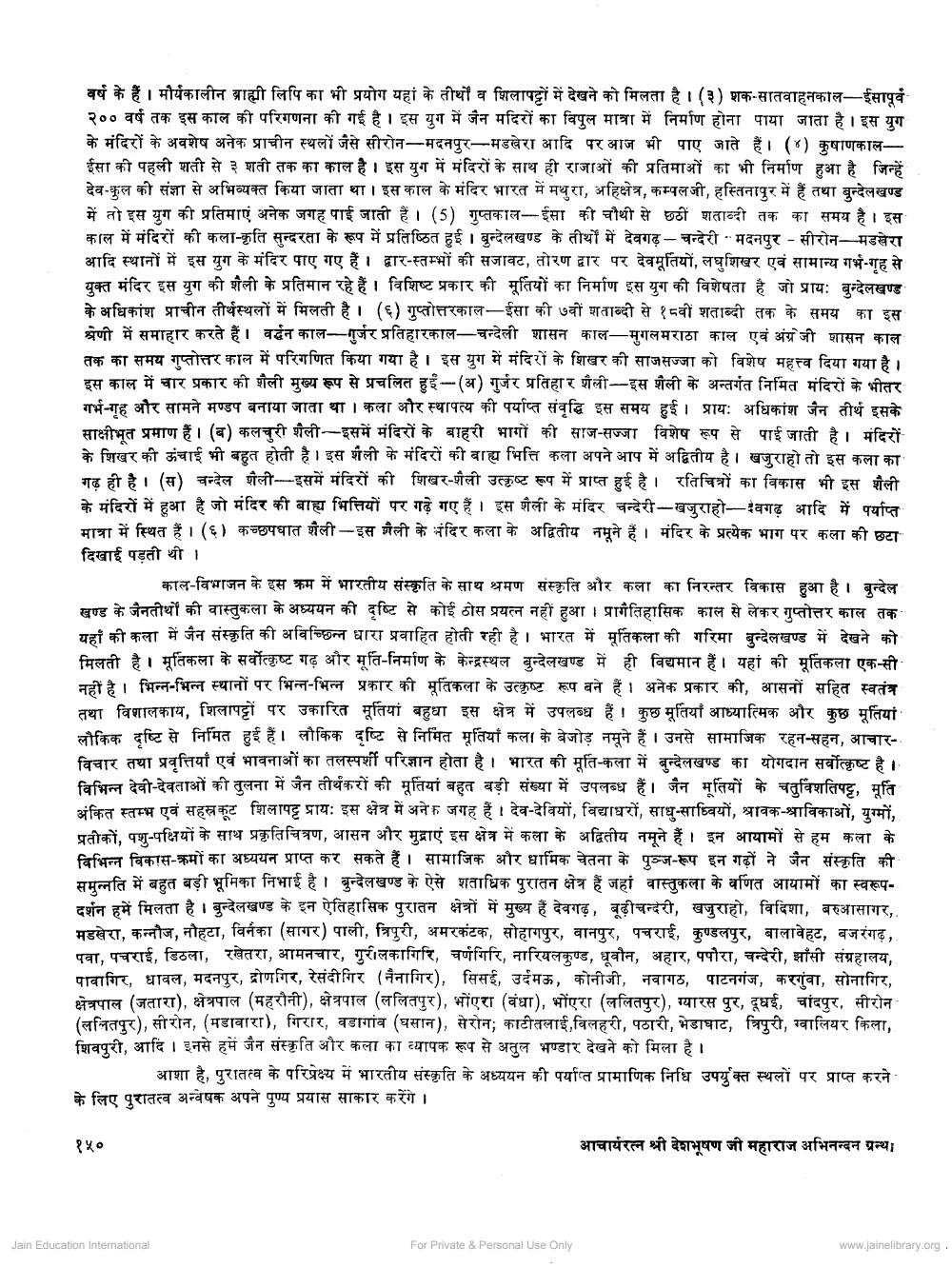________________
वर्ष के हैं । मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग यहां के तीर्थों व शिलापट्टों में देखने को मिलता है। (३) शक-सातवाहनकाल–ईसापूर्व २०० वर्ष तक इस काल की परिगणना की गई है । इस युग में जैन मदिरों का विपुल मात्रा में निर्माण होना पाया जाता है । इस युग के मंदिरों के अवशेष अनेक प्राचीन स्थलों जैसे सीरोन-मदनपुर-मडखेरा आदि पर आज भी पाए जाते हैं। (४) कुषाणकालईसा की पहली शती से ३ शती तक का काल है। इस युग में मंदिरों के साथ ही राजाओं की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है जिन्हें देव-कुल की संज्ञा से अभिव्यक्त किया जाता था। इस काल के मंदिर भारत में मथुरा, अहिक्षेत्र, कम्पलजी, हस्तिनापुर में हैं तथा बुन्देलखण्ड में तो इस युग की प्रतिमाएं अनेक जगह पाई जाती हैं। (5) गुप्तकाल-ईसा की चौथी से छठी शताब्दी तक का समय है। इस काल में मंदिरों की कला-कृति सुन्दरता के रूप में प्रतिष्ठित हुई । बुन्देलखण्ड के तीर्थों में देवगढ़- चन्देरी मदनपुर - सीरोन-मडखेरा आदि स्थानों में इस युग के मंदिर पाए गए हैं। द्वार-स्तम्भों की सजावट, तोरण द्वार पर देवमूर्तियों, लघुशिखर एवं सामान्य गर्भ-गृह से युक्त मंदिर इस युग की शैली के प्रतिमान रहे हैं। विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों का निर्माण इस युग की विशेषता है जो प्रायः बुन्देलखण्ड के अधिकांश प्राचीन तीर्थस्थलों में मिलती है। (६) गुप्तोत्तरकाल-ईसा की ७वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक के समय का इस श्रेणी में समाहार करते हैं। वर्द्धन काल-गुर्जर प्रतिहारकाल-चन्देली शासन काल-मुगलमराठा काल एवं अंग्रेजी शासन काल तक का समय गुप्तोत्तर काल में परिगणित किया गया है। इस युग में मंदिरों के शिखर की साजसज्जा को विशेष महत्त्व दिया गया है। इस काल में चार प्रकार की शैली मुख्य रूप से प्रचलित हुई-(अ) गुर्जर प्रतिहार शैली-इस शैली के अन्तर्गत निर्मित मंदिरों के भीतर गर्भ-गह और सामने मण्डप बनाया जाता था। कला और स्थापत्य की पर्याप्त संवृद्धि इस समय हुई। प्रायः अधिकांश जैन तीर्थ इसके साक्षीभूत प्रमाण हैं। (ब) कलचुरी शैली-इसमें मंदिरों के बाहरी भागों की साज-सज्जा विशेष रूप से पाई जाती है। मंदिरों के शिखर की ऊंचाई भी बहत होती है। इस शैली के मंदिरों की बाह्य भित्ति कला अपने आप में अद्वितीय है। खजुराहो तो इस कला का गढ ही है। (स) चन्देल शैली-इसमें मंदिरों की शिखर-शैली उत्कृष्ट रूप में प्राप्त हुई है। रतिचित्रों का विकास भी इस शैली के मंदिरों में हुआ है जो मंदिर की बाह्य भित्तियों पर गढ़े गए हैं। इस शैली के मंदिर चन्देरी-खजुराहो-देवगढ़ आदि में पर्याप्त मात्रा में स्थित हैं। (६) कच्छपघात शैली-इस शैली के नंदिर कला के अद्वितीय नमूने हैं। मंदिर के प्रत्येक भाग पर कला की छटा दिखाई पड़ती थी।
काल-विभाजन के इस क्रम में भारतीय संस्कृति के साथ श्रमण संस्कृति और कला का निरन्तर विकास हुआ है। बुन्देल खण्ड के जैनतीर्थों की वास्तुकला के अध्ययन की दृष्टि से कोई ठोस प्रयत्न नहीं हुआ। प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक यहाँ की कला में जैन संस्कृति की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रही है। भारत में मूर्तिकला की गरिमा बुन्देलखण्ड में देखने को मिलती है। मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट गढ़ और मूर्ति-निर्माण के केन्द्रस्थल बुन्देलखण्ड में ही विद्यमान हैं। यहां की मूर्तिकला एक-सी नहीं है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मूर्तिकला के उत्कृष्ट रूप बने हैं। अनेक प्रकार की, आसनों सहित स्वतंत्र तथा विशालकाय, शिलापट्टों पर उकारित मूर्तियां बहुधा इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। कुछ मूर्तियाँ आध्यात्मिक और कुछ मूर्तियां लौकिक दष्टि से निर्मित हुई हैं। लौकिक दृष्टि से निर्मित मूर्तियाँ कला के बेजोड़ नमूने हैं । उनसे सामाजिक रहन-सहन, आचारविचार तथा प्रवृत्तियाँ एवं भावनाओं का तलस्पर्शी परिज्ञान होता है। भारत की मूर्ति-कला में बुन्देलखण्ड का योगदान सर्वोत्कृष्ट है। विभिन्न देवी-देवताओं की तुलना में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। जैन मूर्तियों के चतुर्विंशतिपट्ट, मूर्ति अंकित स्तम्भ एवं सहस्रकूट शिलापट्ट प्रायः इस क्षेत्र में अनेक जगह हैं । देव-देवियों, विद्याधरों, साधु-साध्वियों, श्रावक-श्राविकाओं, युग्मों, प्रतीकों, पशु-पक्षियों के साथ प्रकृतिचित्रण, आसन और मुद्राएं इस क्षेत्र में कला के अद्वितीय नमूने हैं। इन आयामों से हम कला के विभिन्न विकास-क्रमों का अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक चेतना के पुज-रूप इन गढ़ों ने जैन संस्कृति की समन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बुन्देलखण्ड के ऐसे शताधिक पुरातन क्षेत्र हैं जहां वास्तुकला के वणित आयामों का स्वरूपदर्शन हमें मिलता है । बुन्देलखण्ड के इन ऐतिहासिक पुरातन क्षेत्रों में मुख्य हैं देवगढ़, बूढ़ीचन्देरी, खजुराहो, विदिशा, बरुआसागर, मडखेरा, कन्नौज, नौहटा, विनका (सागर) पाली, त्रिपुरी, अमरकंटक, सोहागपुर, वानपुर, पचराई, कुण्डलपुर, बालावेहट, बजरंगढ़, पवा, पचराई, डिठला, रखेतरा, आमनचार, गुरीलकागिरि, चर्णगिरि, नारियलकुण्ड, धूवौन, अहार, पपौरा, चन्देरी, झाँसी संग्रहालय, पावागिर, धावल, मदनपुर, द्रोणगिर, रेसंदीगिर (नैनागिर), सिसई, उर्दमऊ, कोनीजी, नवागठ, पाटनगंज, करगुंवा, सोनागिर, क्षेत्रपाल (जतारा), क्षेत्रपाल (महरौनी), क्षेत्रपाल (ललितपुर), भोंएरा (वंधा), भोंएरा (ललितपुर), ग्यारस पुर, दूधई, चांदपुर, सीरोन (ललितपुर), सीरोन, (मडावारा), गिरार, वडागांव (घसान), सेरोन; काटीतलाई,विलहरी, पठारी, भेडाघाट, त्रिपुरी, ग्वालियर किला, शिवपुरी, आदि । इनसे हमें जैन संस्कृति और कला का व्यापक रूप से अतुल भण्डार देखने को मिला है।
आशा है, पुरातत्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति के अध्ययन की पर्याप्त प्रामाणिक निधि उपयुक्त स्थलों पर प्राप्त करने के लिए पुरातत्व अन्वेषक अपने पुण्य प्रयास साकार करेंगे।
१५०
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्था
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.