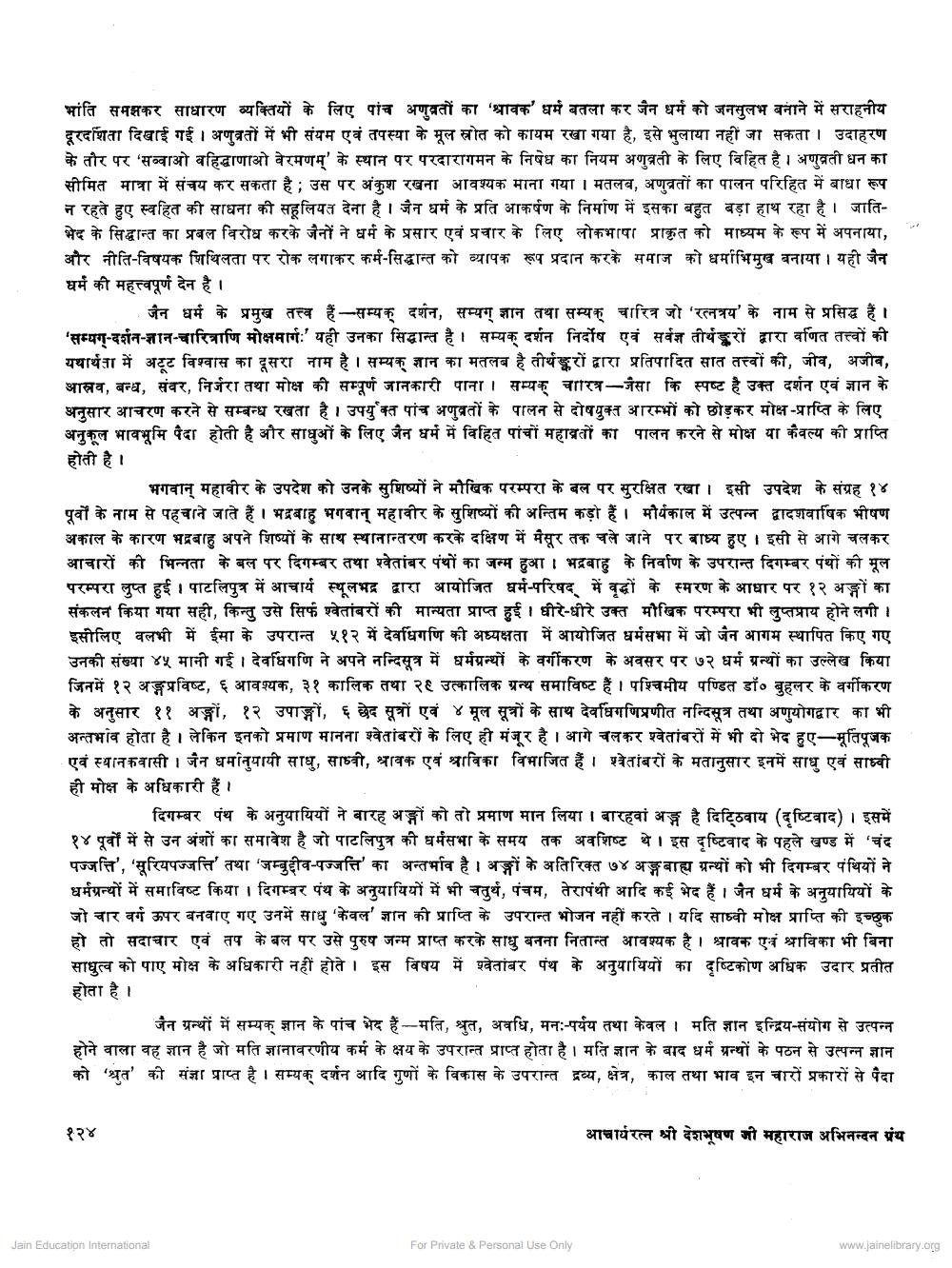________________
भांति समझकर साधारण व्यक्तियों के लिए पांच अणुव्रतों का 'श्रावक' धर्म बतला कर जैन धर्म को जनसुलभ बनाने में सराहनीय दूरदर्शिता दिखाई गई । अणुव्रतों में भी संयम एवं तपस्या के मूल स्रोत को कायम रखा गया है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर 'सवाओ वहिद्धाणाओ वेरमणम्' के स्थान पर परदारागमन के निषेध का नियम अणुव्रती के लिए विहित है । अणुव्रती धन का सीमित मात्रा में संचय कर सकता है ; उस पर अंकुश रखना आवश्यक माना गया । मतलब, अणुव्रतों का पालन परिहित में बाधा रूप न रहते हुए स्वहित की साधना की सहूलियत देना है । जैन धर्म के प्रति आकर्षण के निर्माण में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जातिभेद के सिद्धान्त का प्रबल विरोध करके जैनों ने धर्म के प्रसार एवं प्रचार के लिए लोकभाषा प्राकृत को माध्यम के रूप में अपनाया, और नीति-विषयक शिथिलता पर रोक लगाकर कर्म-सिद्धान्त को व्यापक रूप प्रदान करके समाज को धर्माभिमुख बनाया। यही जैन धर्म की महत्त्वपूर्ण देन है।
जैन धर्म के प्रमुख तत्त्व हैं-सम्यक् दर्शन, सम्यग् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र जो 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'सम्यग-दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः' यही उनका सिद्धान्त है। सम्यक् दर्शन निर्दोष एवं सर्वज्ञ तीर्थङ्करों द्वारा वणित तत्त्वों की यथार्थता में अटूट विश्वास का दूसरा नाम है । सम्यक् ज्ञान का मतलब है तीर्थङ्करों द्वारा प्रतिपादित सात तत्त्वों की, जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष की सम्पूर्ण जानकारी पाना । सम्यक् चारित्र-जैसा कि स्पष्ट है उक्त दर्शन एवं ज्ञान के अनुसार आचरण करने से सम्बन्ध रखता है। उपयुक्त पांच अणुव्रतों के पालन से दोषयुक्त आरम्भों को छोड़कर मोक्ष-प्राप्ति के लिए अनुकूल भावभूमि पैदा होती है और साधुओं के लिए जैन धर्म में विहित पांचों महाव्रतों का पालन करने से मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति होती है।
भगवान महावीर के उपदेश को उनके सुशिष्यों ने मौखिक परम्परा के बल पर सुरक्षित रखा। इसी उपदेश के संग्रह १४ पूर्वो के नाम से पहचाने जाते हैं । भद्रबाहु भगवान् महावीर के सुशिष्यों की अन्तिम कड़ो हैं। मौर्यकाल में उत्पन्न द्वादशवार्षिक भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ स्थानान्तरण करके दक्षिण में मैसूर तक चले जाने पर बाध्य हुए। इसी से आगे चलकर आचारों की भिन्नता के बल पर दिगम्बर तथा श्वेतांबर पंथों का जन्म हुआ। भद्रबाहु के निर्वाण के उपरान्त दिगम्बर पंथों की मूल परम्परा लुप्त हुई । पाटलिपुत्र में आचार्य स्थूलभद्र द्वारा आयोजित धर्म-परिषद में वृद्धों के स्मरण के आधार पर १२ अङ्गों का संकलन किया गया सही, किन्तु उसे सिर्फ श्वेतांबरों की मान्यता प्राप्त हुई। धीरे-धीरे उक्त मौखिक परम्परा भी लुप्तप्राय होने लगी। इसीलिए वलभी में ईमा के उपरान्त ५१२ में देवधिगणि की अध्यक्षता में आयोजित धर्मसभा में जो जैन आगम स्थापित किए गए उनकी संख्या ४५ मानी गई । देवधिगणि ने अपने नन्दिसूत्र में धर्मग्रन्थों के वर्गीकरण के अवसर पर ७२ धर्म ग्रन्थों का उल्लेख किया जिनमें १२ अङ्गप्रविष्ट, ६ आवश्यक, ३१ कालिक तथा २६ उत्कालिक ग्रन्थ समाविष्ट हैं । पश्चिमीय पण्डित डॉ. बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार ११ अङ्गों, १२ उपाङ्गों, ६ छेद सूत्रों एवं ४ मूल सूत्रों के साथ देवधिगणिप्रणीत नन्दिसूत्र तथा अणुयोगद्वार का भी अन्तभाव होता है। लेकिन इनको प्रमाण मानना श्वेतांबरों के लिए ही मंजूर है। आगे चलकर श्वेतांबरों में भी दो भेद हुए-मूर्तिपूजक एवं स्थानकवासी । जैन धर्मानुयायी साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका विभाजित हैं। श्वेतांबरों के मतानुसार इनमें साधु एवं साध्वी ही मोक्ष के अधिकारी हैं।
दिगम्बर पंथ के अनुयायियों ने बारह अङ्गों को तो प्रमाण मान लिया । बारहवां अङ्ग है दिठिवाय (दृष्टिवाद)। इसमें १४ पूर्वो में से उन अंशों का समावेश है जो पाटलिपुत्र की धर्मसभा के समय तक अवशिष्ट थे। इस दृष्टिवाद के पहले खण्ड में 'चंद पज्जत्ति', 'सूरियपज्जत्ति' तथा 'जम्बुद्दीव-पज्जत्ति' का अन्तर्भाव है । अङ्गों के अतिरिक्त ७४ अङ्गबाह्य ग्रन्थों को भी दिगम्बर पंथियों ने धर्मग्रन्थों में समाविष्ट किया । दिगम्बर पंथ के अनुयायियों में भी चतुर्थ, पंचम, तेरापंथी आदि कई भेद हैं । जैन धर्म के अनुयायियों के जो चार वर्ग ऊपर बनवाए गए उनमें साधु 'केवल' ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त भोजन नहीं करते । यदि साध्वी मोक्ष प्राप्ति की इच्छुक हो तो सदाचार एवं तप के बल पर उसे पुरुष जन्म प्राप्त करके साधु बनना नितान्त आवश्यक है। श्रावक एवं श्राविका भी बिना साधुत्व को पाए मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। इस विषय में श्वेतांबर पंथ के अनुयायियों का दृष्टिकोण अधिक उदार प्रतीत होता है।
जैन ग्रन्थों में सम्यक् ज्ञान के पांच भेद हैं --मति, श्रुत, अवधि, मनः-पर्यय तथा केवल । मति ज्ञान इन्द्रिय-संयोग से उत्पन्न होने वाला वह ज्ञान है जो मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के उपरान्त प्राप्त होता है। मति ज्ञान के बाद धर्म ग्रन्थों के पठन से उत्पन्न ज्ञान को 'श्रुत' की संज्ञा प्राप्त है । सम्यक् दर्शन आदि गुणों के विकास के उपरान्त द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव इन चारों प्रकारों से पैदा
१२४
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रंथ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org