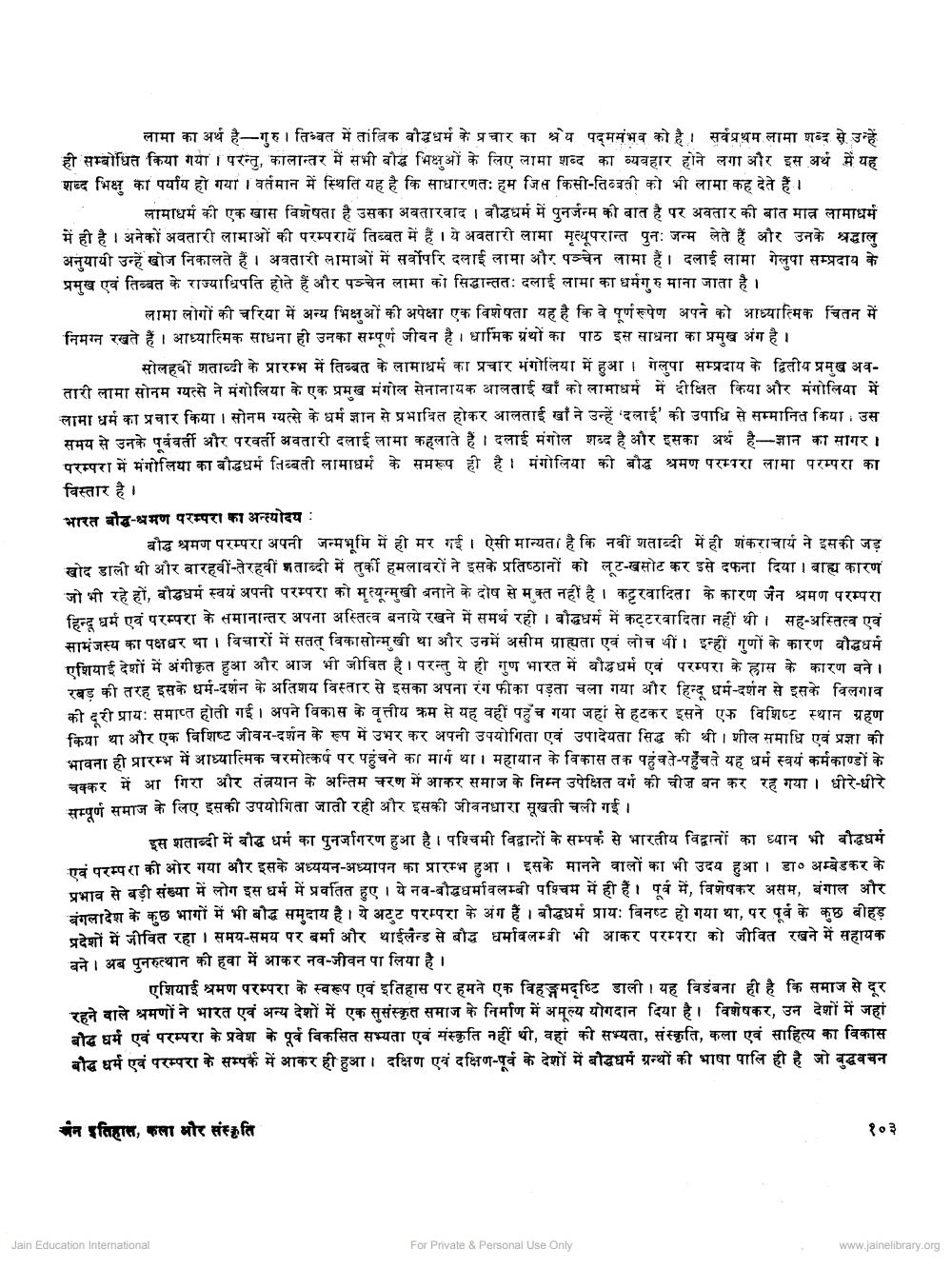________________
लामा का अर्थ है – गुरु । तिब्बत में तांत्रिक बौद्धधर्म के प्रचार का श्रेय पद्मसंभव को है । सर्वप्रथम लामा शब्द से उन्हें ही सम्बोधित किया गया । परन्तु कालान्तर में सभी बौद्ध भिक्षुओं के लिए लामा शब्द का व्यवहार होने लगा और इस अर्थ में यह शब्द भिक्षु का पर्याय हो गया । वर्तमान में स्थिति यह है कि साधारणतः हम जिस किसी-तिब्बती को भी लामा कह देते हैं ।
लामाधर्म की एक खास विशेषता है उसका अवतारवाद । बौद्धधर्म में पुनर्जन्म की बात है पर अवतार की बात मात्र लामाधर्मं में ही है । अनेकों अवतारी लामाओं की परम्परायें तिब्बत में हैं ये अवतारी लामा मृत्यूपरान्त पुनः जन्म लेते हैं और उनके श्रद्धालु अनुयायी उन्हें खोज निकालते हैं । अवतारी लामाओं में सर्वोपरि दलाई लामा और पञ्चेन लामा हैं। दलाई लामा गेलुपा सम्प्रदाय के प्रमुख एवं तिब्बत के राज्याधिपति होते हैं और पञ्चेन लामा को सिद्धान्ततः दलाई लामा का धर्मगुरु माना जाता है ।
लामा लोगों की चरिया में अन्य भिक्षुओं की अपेक्षा एक विशेषता यह है कि वे पूर्णरूपेण अपने को आध्यात्मिक चिंतन में निमग्न रखते हैं । आध्यात्मिक साधना ही उनका सम्पूर्ण जीवन है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस साधना का प्रमुख अंग है ।
सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तिब्बत के लामाधर्म का प्रचार मंगोलिया में हुआ । गेलुपा सम्प्रदाय के द्वितीय प्रमुख अवतारी लामा सोनम ग्यत्से ने मंगोलिया के एक प्रमुख मंगोल सेनानायक आलताई खाँ को लामाधर्म में दीक्षित किया और मंगोलिया में लामा धर्म का प्रचार किया। सोनम ग्यत्से के धर्म ज्ञान से प्रभावित होकर आलताई खाँ ने उन्हें 'दलाई' की उपाधि से सम्मानित किया। उस समय से उनके पूर्ववर्ती और परवर्ती अवतारी दलाई लामा कहलाते हैं। दलाई मंगोल शब्द है और इसका अर्थ है- ज्ञान का सागर । परम्परा में मंगोलिया का बौद्धधर्म तिब्बती लामाधर्म के समरूप ही है । मंगोलिया की बौद्ध श्रमण परम्परा लामा परम्परा का विस्तार है।
भारत बौद्ध-श्रमण परम्परा का अन्त्योदय :
बौद्ध श्रमण परम्परा अपनी जन्मभूमि में ही मर गई। ऐसी मान्यता है कि नवीं शताब्दी में ही शंकराचार्य ने इसकी जड़ खोद डाली थी और बारहवीं - तेरहवीं शताब्दी में तुर्की हमलावरों ने इसके प्रतिष्ठानों को लूट-खसोट कर इसे दफना दिया । बाह्य कारण जो भी रहे हों, बौद्धधर्म स्वयं अपनी परम्परा को मृत्यूमुखी बनाने के दोष से मुक्त नहीं है कट्टरवादिता के कारण जैन भ्रमण परम्परा हिन्दू धर्म एवं परम्परा के समानान्तर अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ रही । बौद्धधर्म में कट्टरवादिता नहीं थी । सह-अस्तित्व एवं सामंजस्य का पक्षधर या विचारों में सतत् विकासोन्मुखी था और उनमें असीम ग्राह्यता एवं सोच थी। इन्हीं गुणों के कारण बौद्धधर्म एशियाई देशों में अंगीकृत हुआ और आज भी जीवित है । परन्तु ये ही गुण भारत में बौद्धधर्म एवं परम्परा के ह्रास के कारण बने । रबड़ की तरह इसके धर्म-दर्शन के अतिशय विस्तार से इसका अपना रंग फीका पड़ता चला गया और हिन्दू धर्म-दर्शन से इसके विलगाव की दूरी प्रायः समाप्त होती गई । अपने विकास के वृत्तीय क्रम से यह वहीं पहुँच गया जहां से हटकर इसने एक विशिष्ट स्थान ग्रहण किया था और एक विशिष्ट जीवन-दर्शन के रूप में उभर कर अपनी उपयोगिता एवं उपादेयता सिद्ध की थी। शील समाधि एवं प्रज्ञा की भावना ही प्रारम्भ में आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग था । महायान के विकास तक पहुंचते-पहुँचते यह धर्म स्वयं कर्मकाण्डों के चक्कर में आ गिरा और तंत्रयान के अन्तिम चरण में आकर समाज के निम्न उपेक्षित वर्ग की चीज़ बन कर रह गया । धीरे-धीरे सम्पूर्ण समाज के लिए इसकी उपयोगिता जाती रही और इसकी जीवनधारा युती चली गई।
इस शताब्दी में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ है। पश्चिमी विद्वानों के सम्पर्क से भारतीय विद्वानों का ध्यान भी बौद्धधर्म एवं परम्परा की ओर गया और इसके अध्ययन-अध्यापन का प्रारम्भ हुआ । इसके मानने वालों का भी उदय हुआ । डा० अम्बेडकर के प्रभाव से बड़ी संख्या में लोग इस धर्म में प्रवर्तित हुए। ये नव-बौद्धधर्मावलम्बी पश्चिम में ही हैं। पूर्व में, विशेषकर असम, बंगाल और बंगलादेश के कुछ भागों में भी बौद्ध समुदाय है। ये अटुट परम्परा के अंग हैं । बौद्धधर्म प्रायः विनष्ट हो गया था, पर पूर्व के कुछ बीहड़ प्रदेशों में जीवित रहा । समय-समय पर बर्मा और थाईलैन्ड से बौद्ध धर्मावलम्बी भी आकर परम्परा को जीवित रखने में सहायक बने । अब पुनरुत्थान की हवा में आकर नव-जीवन पा लिया है।
एशियाई श्रमण परम्परा के स्वरूप एवं इतिहास पर हमने एक विहङ्गमदृष्टि डाली । यह विडंबना ही है कि समाज से दूर रहने वाले भ्रमणों ने भारत एवं अन्य देशों में एक सुसंस्कृत समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। विशेषकर उन देशों में जहां बौद्ध धर्म एवं परम्परा के प्रवेश के पूर्व विकसित सभ्यता एवं संस्कृति नहीं थी, वहां की सभ्यता, संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास बौद्ध धर्म एवं परम्परा के सम्पर्क में आकर ही हुआ । दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व के देशों में बौद्धधर्म ग्रन्थों की भाषा पालि ही है जो बुद्धवचन
संग इतिहास, कला और संस्कृति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१०३
www.jainelibrary.org