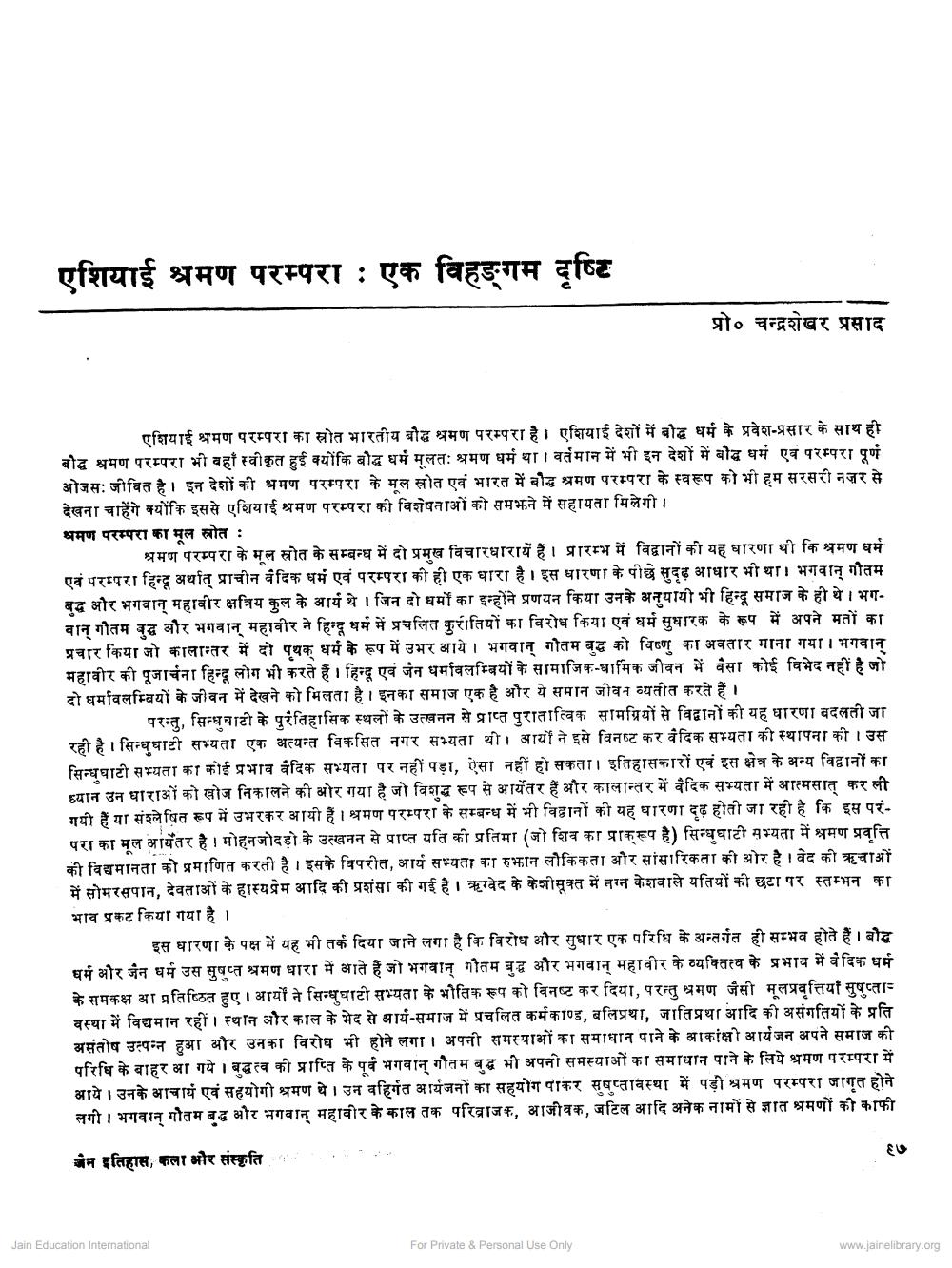________________
एशियाई श्रमण परम्परा एक विहङ्गम दृष्टि
एशियाई श्रमण परम्परा का स्रोत भारतीय बौद्ध श्रमण परम्परा है। एशियाई देशों में बौद्ध धर्म के प्रवेश-प्रसार के साथ ही बौद्ध श्रमण परम्परा भी वहाँ स्वीकृत हुई क्योंकि बौद्ध धर्म मूलतः श्रमण धर्म था। वर्तमान में भी इन देशों में बौद्ध धर्म एवं परम्परा पूर्ण ओजसः जीवित है । इन देशों की श्रमण परम्परा के मूल स्रोत एवं भारत में बौद्ध श्रमण परम्परा के स्वरूप को भी हम सरसरी नज़र से देखना चाहेंगे क्योंकि इससे एशियाई श्रमण परम्परा की विशेषताओं को समझने में सहायता मिलेगी. 1
प्रो० चन्द्रशेखर प्रसाद
श्रमण परम्परा का मूल स्रोत :
श्रमण परम्परा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में दो प्रमुख विचारधारायें हैं। प्रारम्भ में विद्वानों की यह धारणा थी कि श्रमण धर्म एवं परम्परा हिन्दू अर्थात् प्राचीन वैदिक धर्म एवं परम्परा की ही एक धारा है। इस धारणा के पीछे सुदृढ़ आधार भी था। भगवान् गौतम बुद्ध • और भगवान् महावीर क्षत्रिय कुल के आर्य थे। जिन दो धर्मों का इन्होंने प्रणयन किया उनके अनुयायी भी हिन्दू समाज के ही थे। भगवान् गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर ने हिन्दू धर्म में प्रचलित कुरीतियों का विरोध किया एवं धर्म सुधारक के रूप में अपने मतों का प्रचार किया जो कालान्तर में दो पृथक् धर्म के रूप में उभर आये । भगवान् गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया । भगवान् महावीर की पूजार्चना हिन्दू लोग भी करते हैं हिन्दू एवं जैन धर्मावलम्बियों के सामाजिक-धार्मिक जीवन में वैसा कोई विभेद नहीं है जो दो धर्मावलम्बियों के जीवन में देखने को मिलता है। इनका समाज एक है और ये समान जीवन व्यतीत करते हैं ।
परन्तु सम्माटी के पुरंतिहासिक स्थलों के
प्राप्त पुरातात्विक सामदियों से विद्वानों की यह पारणा बदलती जा रही है । सिन्धुघाटी सभ्यता एक अत्यन्त विकसित नगर सभ्यता थी। आर्यों ने इसे विनष्ट कर वैदिक सभ्यता की स्थापना की। उस सिन्धुघाटी सभ्यता का कोई प्रभाव वैदिक सभ्यता पर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहासकारों एवं इस क्षेत्र के अन्य विद्वानों का ध्यान उन धाराओं को खोज निकालने की ओर गया है जो विशुद्ध रूप से आर्येतर हैं और कालान्तर में वैदिक सभ्यता में आत्मसात् कर ली गयी हैं या संश्लेषित रूप में उभरकर आयी हैं। श्रमण परम्परा के सम्बन्ध में भी विद्वानों की यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि इस परंपरा का मूल आर्येतर है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त यति की प्रतिमा (जो शिव का प्रारूप है) सिन्धुघाटी सभ्यता में श्रमण प्रवृत्ति की विद्यमानता को प्रमाणित करती है। इसके विपरीत, आर्य सभ्यता का रुझान लौकिकता और सांसारिकता की ओर है। वेद की ऋचाओं में सोमरसपान, देवताओं के हास्यप्रेम आदि की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के केशीसूक्त में नग्न केशवाले यतियों की छटा पर स्तम्भन का भाव प्रकट किया गया है ।
इस धारणा के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाने लगा है कि विरोध और सुधार एक परिधि के अन्तर्गत ही सम्भव होते हैं । बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस सुषुप्त श्रमण धारा में आते हैं जो भगवान् गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर के व्यक्तित्व के प्रभाव में वैदिक धर्म के समकक्ष आ प्रतिष्ठित हुए। आर्यों ने सिन्धुघाटी सभ्यता के भौतिक रूप को विनष्ट कर दिया, परन्तु श्रमण जैसी मूलप्रवृत्तियाँ सुषुप्ता वस्था में विद्यमान रहीं स्थान और काल के भेद से आर्य समाज में प्रचलित कर्मकाण्ड, बलिप्रथा, जातिप्रथा आदि की असंगतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और उनका विरोध भी होने लगा। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के आकांक्षी आर्यजन अपने समाज की परिधि के बाहर आ गये । बुद्धत्व की प्राप्ति के पूर्व भगवान् गौतम बुद्ध भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिये श्रमण परम्परा में आये । उनके आचार्य एवं सहयोगी श्रमण थे। उन वहिर्गत आर्यजनों का सहयोग पाकर सुषुप्तावस्था में पड़ी श्रमण परम्परा जागृत होने लगी। भगवान् गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर के काल तक परिव्राजक, आजीवक, जटिल आदि अनेक नामों से ज्ञात श्रमणों की काफी
जैन इतिहास, कला और संस्कृति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
६७
www.jainelibrary.org