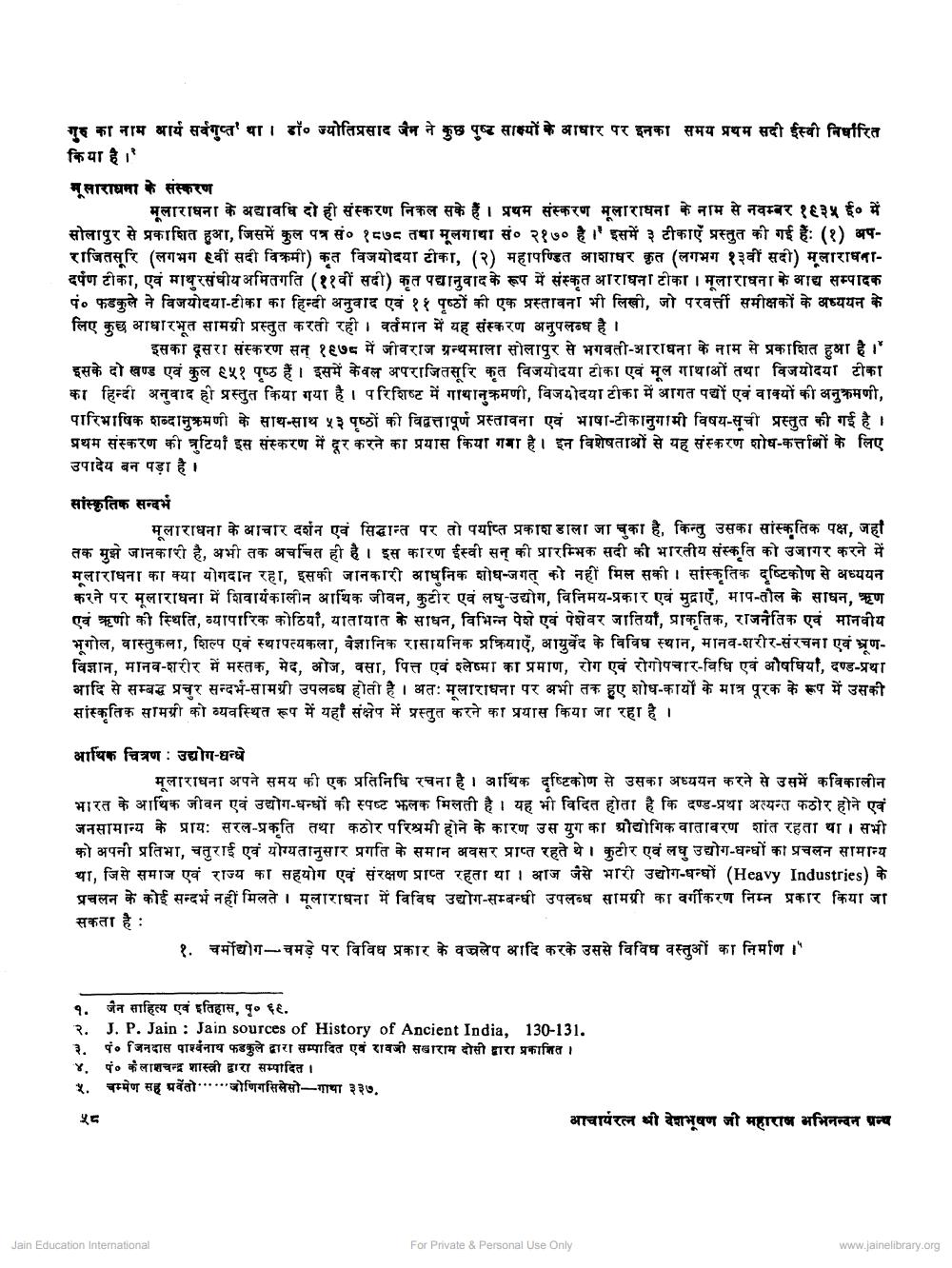________________
गुरु का नाम आर्य सर्वगुप्त' था। डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन ने कुछ पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर इनका समय प्रथम सदी ईस्वी निर्धारित किया है।' मूलाराधना के संस्करण
मूलाराधना के अद्यावधि दो ही संस्करण निकल सके हैं। प्रथम संस्करण मूलाराधना के नाम से नवम्बर १९३५ ई० में सोलापुर से प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल पत्र सं० १८७८ तथा मूलगाथा सं० २१७० है। इसमें ३ टीकाएँ प्रस्तुत की गई हैं: (१) अपराजितसूरि (लगभग 6वीं सदी विक्रमी) कृत विजयोदया टीका, (२) महापण्डित आशाधर कृत (लगभग १३वीं सदी) मलाराधनादर्पण टीका, एवं माथुरसंघीय अमितगति (११वीं सदी) कृत पद्यानुवाद के रूप में संस्कृत आराधना टीका । मूलाराधना के आद्य सम्पादक पं० फडकुले ने विजयोदया-टीका का हिन्दी अनुवाद एवं ११ पृष्ठों की एक प्रस्तावना भी लिखी, जो परवर्ती समीक्षकों के अध्ययन के लिए कुछ आधारभूत सामग्री प्रस्तुत करती रही। वर्तमान में यह संस्करण अनुपलब्ध है।
इसका दूसरा संस्करण सन् १९७८ में जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर से भगवती-आराधना के नाम से प्रकाशित हुआ है।' इसके दो खण्ड एवं कुल ६५१ पृष्ठ हैं। इसमें केवल अपराजितसूरि कृत विजयोदया टोका एवं मूल गाथाओं तथा विजयोदया टीका का हिन्दी अनुवाद ही प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट में गाथानुक्रमणी, विजयोदया टीका में आगत पद्यों एवं वाक्यों की अनुक्रमणी, पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी के साथ-साथ ५३ पृष्ठों की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना एवं भाषा-टीकानुगामी विषय-सूची प्रस्तुत की गई है। प्रथम संस्करण की त्रुटियाँ इस संस्करण में दूर करने का प्रयास किया गया है। इन विशेषताओं से यह संस्करण शोध-कर्ताओं के लिए उपादेय बन पड़ा है। सांस्कृतिक सन्दर्भ
मूलाराधना के आचार दर्शन एवं सिद्धान्त पर तो पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, किन्तु उसका सांस्कृतिक पक्ष, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तक अचचित ही है। इस कारण ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदी की भारतीय संस्कृति को उजागर करने में मलाराधना का क्या योगदान रहा, इसकी जानकारी आधुनिक शोध-जगत् को नहीं मिल सकी। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर मूलाराधना में शिवार्यकालीन आर्थिक जीवन, कुटीर एवं लघु-उद्योग, विनिमय-प्रकार एवं मुद्राएँ, माप-तौल के साधन, ऋण एवं ऋणी की स्थिति, व्यापारिक कोठियां, यातायात के साधन, विभिन्न पेशे एवं पेशेवर जातियाँ, प्राकृतिक, राजनैतिक एवं मानवीय भूगोल, वास्तुकला, शिल्प एवं स्थापत्यकला, वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रियाएँ, आयुर्वेद के विविध स्थान, मानव-शरीर-संरचना एवं भ्रूणविज्ञान, मानव-शरीर में मस्तक, मेद, ओज, वसा, पित्त एवं श्लेष्मा का प्रमाण, रोग एवं रोगोपचार-विधि एवं औषधियां, दण्ड-प्रथा आदि से सम्बद्ध प्रचुर सन्दर्भ-सामग्री उपलब्ध होती है । अतः मूलाराधना पर अभी तक हुए शोध-कार्यों के मात्र पूरक के रूप में उसकी सांस्कृतिक सामग्री को व्यवस्थित रूप में यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है ।
आर्थिक चित्रण : उद्योग-धन्धे
__ मूलाराधना अपने समय की एक प्रतिनिधि रचना है । आर्थिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करने से उसमें कविकालीन भारत के आर्थिक जीवन एवं उद्योग-धन्धों की स्पष्ट झलक मिलती है। यह भी विदित होता है कि दण्ड-प्रथा अत्यन्त कठोर होने एवं जनसामान्य के प्राय: सरल-प्रकृति तथा कठोर परिश्रमी होने के कारण उस युग का औद्योगिक वातावरण शांत रहता था। सभी को अपनी प्रतिभा, चतुराई एवं योग्यतानुसार प्रगति के समान अवसर प्राप्त रहते थे। कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों का प्रचलन सामान्य था, जिसे समाज एवं राज्य का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त रहता था । आज जैसे भारी उद्योग-धन्धों (Heavy Industries) के प्रचलन के कोई सन्दर्भ नहीं मिलते । मूलाराधना में विविध उद्योग-सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है:
१. चर्मोद्योग-चमड़े पर विविध प्रकार के वज्रलेप आदि करके उससे विविध वस्तुओं का निर्माण ।
१. जैन साहित्य एवं इतिहास, पु. ६६. २. J. P. Jain : Jain sources of History of Ancient India, 130-131. ३. पं.जिनदास पाश्वनाथ फडकुले द्वारा सम्पादित एवं रावजी सखाराम दोसी द्वारा प्रकाशित । ४. पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा सम्पादित । ५. चम्मेण सह पावेतो...."जोणिगसिलेसो-गाथा ३३७.
आचार्यरत्न श्री वेशभूषण जी महाराज भभिनन्दन अन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org