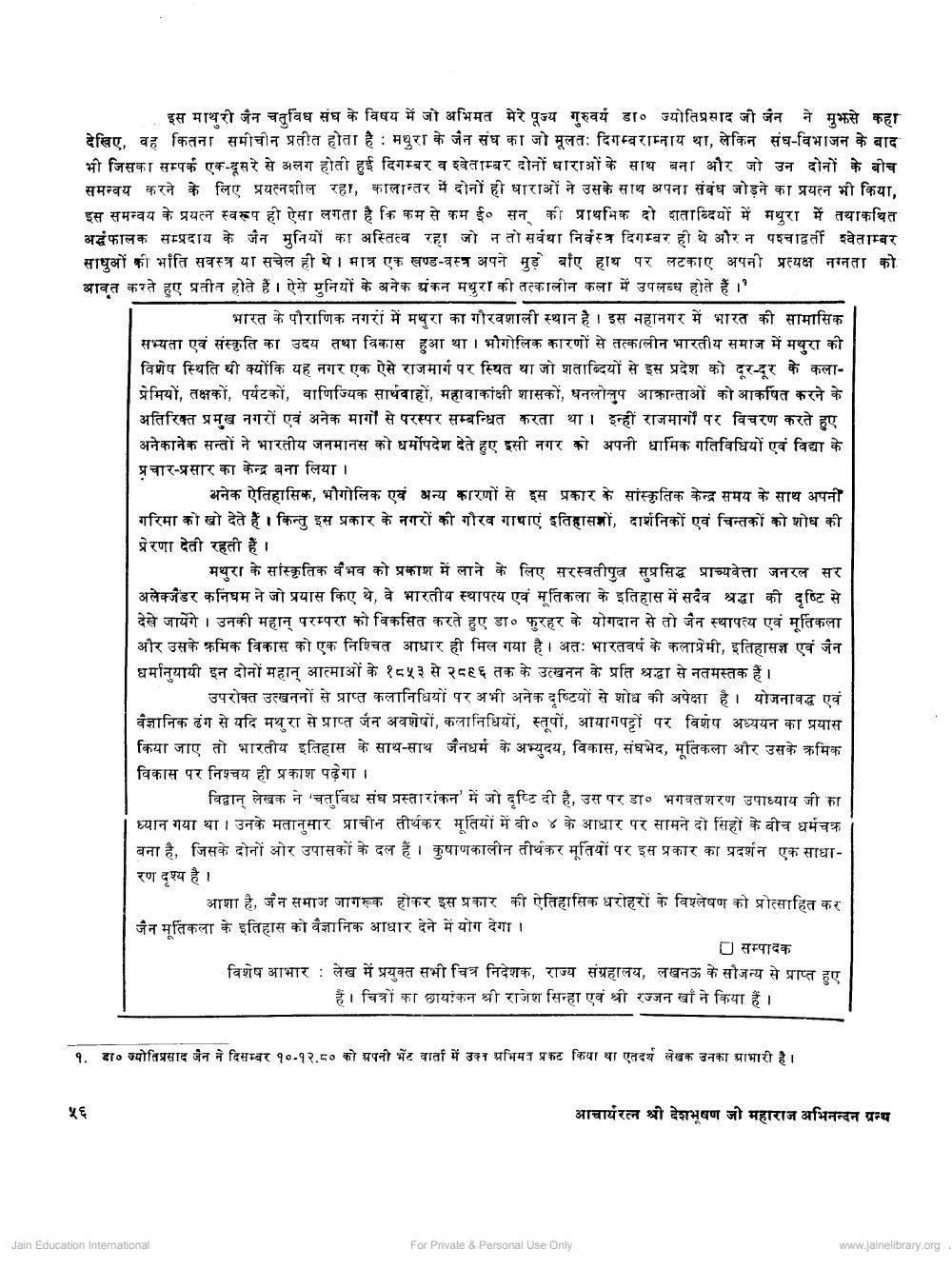________________
इस माथरी जैन चविध संघ के विषय में जो अभिमत मेरे पूज्य गुरुवर्य डा० ज्योतिप्रसाद जी जैन ने मुझसे कहा देखिए, वह कितना समीचीन प्रतीत होता है : मथुरा के जैन संघ का जो मूलतः दिगम्बराम्नाय था, लेकिन संघ-विभाजन के बाद भी जिसका सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होती हुई दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों धाराओं के साथ बना और जो उन दोनों के बीच समन्वय करने के लिए प्रयत्नशील रहा, कालान्तर में दोनों ही धाराओं ने उसके साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयत्न भी किया, इस समन्वय के प्रयत्न स्वरूप ही ऐसा लगता है कि कम से कम ई० सन की प्राथमिक दो शताब्दियों में मथुरा में तथाकथित अर्द्धफालक सम्प्रदाय के जैन मुनियों का अस्तित्व रहा जो न तो सर्वथा निर्वस्त्र दिगम्बर ही थे और न पश्चाद्वर्ती श्वेताम्बर साधुओं की भाँति सवस्त्र या सचेल ही थे। मात्र एक खण्ड-वस्त्र अपने मुड़े बाँए हाथ पर लटकाए अपनी प्रत्यक्ष नग्नता को आवत करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे मुनियों के अनेक अंकन मथुरा की तत्कालीन कला में उपलब्ध होते हैं।"
भारत के पौराणिक नगरों में मथुरा का गौरवशाली स्थान है। इस महानगर में भारत की सामासिक सभ्यता एवं संस्कृति का उदय तथा विकास हुआ था । भौगोलिक कारणों से तत्कालीन भारतीय समाज में मथुरा की विशेष स्थिति थी क्योंकि यह नगर एक ऐसे राजमार्ग पर स्थित था जो शताब्दियों से इस प्रदेश को दूर-दूर के कलाप्रेमियों, तक्षकों, पर्यटकों, वाणिज्यिक सार्थवाहों, महावाकांक्षी शासकों, धनलोलुप आक्रान्ताओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त प्रमुख नगरों एवं अनेक मागों से परस्पर सम्बन्धित करता था। इन्हीं राजमार्गों पर विचरण करते हुए अनेकानेक सन्तों ने भारतीय जनमानस को धर्मोपदेश देते हुए इसी नगर को अपनी धार्मिक गतिविधियों एवं विद्या के प्रचार-प्रसार का केन्द्र बना लिया।
अनेक ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य कारणों से इस प्रकार के सांस्कृतिक केन्द्र समय के साथ अपनी गरिमा को खो देते हैं । किन्तु इस प्रकार के नगरों की गौरव गाथाएं इतिहासज्ञों, दार्शनिकों एवं चिन्तकों को शोध की प्रेरणा देती रहती हैं।
मथुरा के सांस्कृतिक वैभव को प्रकाश में लाने के लिए सरस्वतीपुत्र सुप्रसिद्ध प्राच्यवेत्ता जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो प्रयास किए थे, वे भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला के इतिहास में सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखे जायेंगे। उनकी महान् परम्परा को विकसित करते हुए डा० फुरहर के योगदान से तो जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला और उसके क्रमिक विकास को एक निश्चित आधार ही मिल गया है। अतः भारतवर्ष के कलाप्रेमी, इतिहासज्ञ एवं जैन धर्मानुयायी इन दोनों महान् आत्माओं के १८५३ से २८६६ तक के उत्खनन के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हैं।
उपरोक्त उत्खननों से प्राप्त कलानिधियों पर अभी अनेक दृष्टियों से शोध की अपेक्षा है। योजनावद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से यदि मथुरा से प्राप्त जन अवशेषों, कलानिधियों, स्तूपों, आयागपट्टों पर विशेष अध्ययन का प्रयास किया जाए तो भारतीय इतिहास के साथ-साथ जैनधर्म के अभ्युदय, विकास, संघभेद, मूर्तिकला और उसके क्रमिक विकास पर निश्चय ही प्रकाश पढ़ेगा।
विद्वान् लेखक ने 'चतुविध संघ प्रस्तारांकन' में जो दृष्टि दी है, उस पर डा० भगवतशरण उपाध्याय जी का ध्यान गया था। उनके मतानुसार प्राचीन तीर्थकर मूर्तियों में बी० ४ के आधार पर सामने दो सिंहों के बीच धर्मचक्र बना है, जिसके दोनों ओर उपासकों के दल हैं। कुषाणकालीन तीर्थकर मूर्तियों पर इस प्रकार का प्रदर्शन एक साधारण दृश्य है।
आशा है, जैन समाज जागरूक होकर इस प्रकार की ऐतिहासिक धरोहरों के विश्लेषण को प्रोत्साहित कर जैन मूर्तिकला के इतिहास को वैज्ञानिक आधार देने में योग देगा।
सम्पादक विशेष आभार : लेख में प्रयुक्त सभी चित्र निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त हुए
हैं। चित्रों का छायांकन श्री राजेश सिन्हा एवं श्री रज्जन खाँ ने किया हैं।
१. डा. ज्योतिप्रसाद जैन ने दिसम्बर १०.१२.८० को अपनी भेंट वार्ता में उक्त अभिमत प्रकट किया था एतदर्थ लेखक उनका आभारी है।
५६
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org