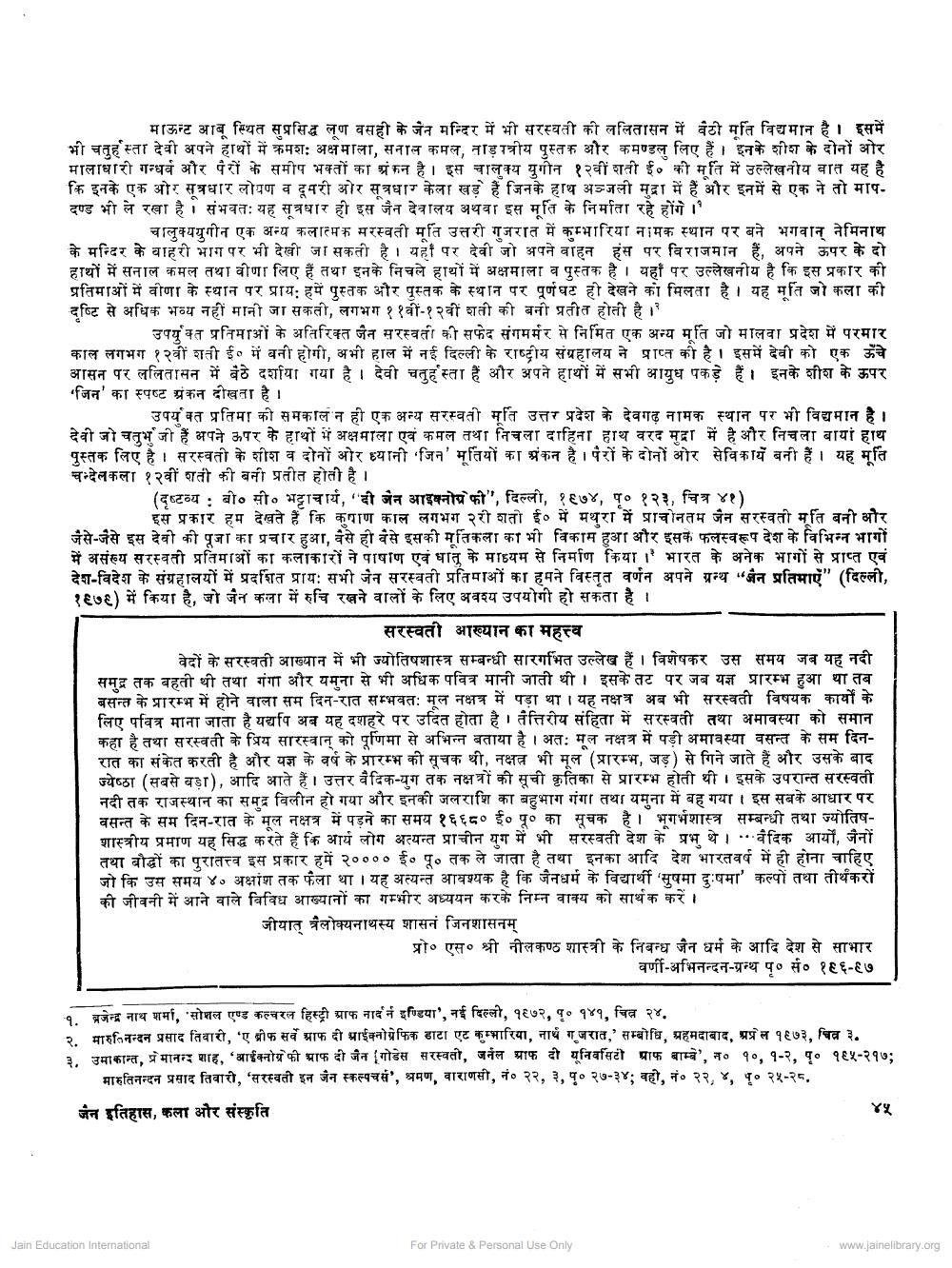________________
माऊन्ट आबू स्थित सुप्रसिद्ध लण वसही के जैन मन्दिर में भी सरस्वती की ललितासन में बैठी मति विद्यमान है। इसमें भी चतुर्हस्ता देवी अपने हाथों में क्रमश: अक्षमाला, सनाल कमल, ताडपत्रीय पुस्तक और कमण्डल लिए हैं। इनके शीश के दोनों ओर मालाधारी गन्धर्व और पैरों के समीप भक्तों का अंकन है। इस चालुक्य युगीन १२वीं शती ई. की मति में उल्लेखनीय बात यह है कि इनके एक ओर सूत्रधार लोयण व दूसरी ओर सूत्रधार केला खड़े हैं जिनके हाथ अञ्जली मुद्रा में हैं और इनमें से एक ने तो मापदण्ड भी ले रखा है। संभवतः यह सूत्रधार ही इस जैन देवालय अथवा इस मूर्ति के निर्माता रहे होंगे।
चालुक्ययुगीन एक अन्य कलात्मक सरस्वती मूर्ति उत्तरी गुजरात में कुम्भारिया नामक स्थान पर बने भगवान् नेमिनाथ के मन्दिर के बाहरी भाग पर भी देखी जा सकती है। यहाँ पर देवी जो अपने वाहन हंस पर विराजमान हैं, अपने ऊपर के दो हाथों में सनाल कमल तथा वीणा लिए हैं तथा इनके निचले हाथों में अक्षमाला व पुस्तक है । यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रतिमाओं में वीणा के स्थान पर प्राय: हमें पुस्तक और पुस्तक के स्थान पर पूर्ण घट ही देखने को मिलता है। यह मूर्ति जो कला की दृष्टि से अधिक भव्य नहीं मानी जा सकती, लगभग ११वीं-१२वीं शती की बनी प्रतीत होती है।'
उपयुक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैन सरस्वती की सफेद संगमर्मर से निर्मित एक अन्य मति जो मालवा प्रदेश में परमार काल लगभग १२वीं शती ई० में बनी होगी, अभी हाल में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्राप्त की है। इसमें देवी को एक ऊँचे आसन पर ललितासन में बैठे दर्शाया गया है। देवी चतुर्हस्ता हैं और अपने हाथों में सभी आयुध पकड़े हैं। इनके शीश के ऊपर 'जिन' का स्पष्ट अंकन दीखता है।
उपर्य क्त प्रतिमा की समकाल न ही एक अन्य सरस्वती मूर्ति उत्तर प्रदेश के देवगढ़ नामक स्थान पर भी विद्यमान है। देवी जो चतुर्भजी हैं अपने ऊपर के हाथों में अक्षमाला एवं कमल तथा निचला दाहिना हाथ वरद मद्रा में है और निचला बायां हाथ पुस्तक लिए है। सरस्वती के शीश व दोनों ओर ध्यानी 'जिन' मूर्तियों का अंकन है। पैरों के दोनों ओर सेविकायें बनी हैं। यह मूर्ति चन्देलकला १२वीं शती की बनी प्रतीत होती है ।
(दृष्टव्य : बी०सी० भट्टाचार्य, "दी जैन आइक्नोग्रेको", दिल्ली, १६७४, पृ० १२३, चित्र ४१)
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण काल लगभग २री शती ई० में मथुरा में प्राचीनतम जैन सरस्वती मति बनी और जैसे-जैसे इस देवी की पूजा का प्रचार हुआ, वैसे ही वैसे इसकी मूर्तिकला का भी विकास हुआ और इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में असंख्य सरस्वती प्रतिमाओं का कलाकारों ने पाषाण एवं धातु के माध्यम से निर्माण किया। भारत के अनेक भागों से प्राप्त एवं देश-विदेश के संग्रहालयों में प्रदर्शित प्राय: सभी जैन सरस्वती प्रतिमाओं का हमने विस्तृत वर्णन अपने ग्रन्थ “जैन प्रतिमाएँ" (दिल्ली, १९७६) में किया है, जो जैन कला में रुचि रखने वालों के लिए अवश्य उपयोगी हो सकता है।
सरस्वती आख्यान का महत्त्व वेदों के सरस्वती आख्यान में भी ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी सारगभित उल्लेख हैं। विशेषकर उस समय जब यह नदी समुद्र तक बहती थी तथा गंगा और यमुना से भी अधिक पवित्र मानी जाती थी। इसके तट पर जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ था तब बसन्त के प्रारम्भ में होने वाला सम दिन-रात सम्भवत: मूल नक्षत्र में पड़ा था । यह नक्षत्र अब भी सरस्वती विषयक कार्यों के लिए पवित्र माना जाता है यद्यपि अब यह दशहरे पर उदित होता है। तैत्तिरीय संहिता में सरस्वती तथा अमावस्या को समान कहा है तथा सरस्वती के प्रिय सारस्वान् को पूर्णिमा से अभिन्न बताया है । अत: मूल नक्षत्र में पड़ी अमावस्या वसन्त के सम दिनरात का संकेत करती है और यज्ञ के वर्ष के प्रारम्भ की सूचक थी, नक्षत्र भी मूल (प्रारम्भ, जड़) से गिने जाते हैं और उसके बाद ज्येष्ठा (सबसे बड़ा), आदि आते हैं। उत्तर वैदिक-युग तक नक्षत्रों की सूची कृतिका से प्रारम्भ होती थी। इसके उपरान्त सरस्वती नदी तक राजस्थान का समुद्र विलीन हो गया और इनकी जलराशि का बहुभाग गंगा तथा यमुना में बह गया। इस सबके आधार पर वसन्त के सम दिन-रात के मूल नक्षत्र में पड़ने का समय १६६८० ई०पू० का सूचक है। भूगर्भशास्त्र सम्बन्धी तथा ज्योतिषशास्त्रीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग अत्यन्त प्राचीन युग में भी सरस्वती देश के प्रभ थे। .. वैदिक आर्यों, जैनों तथा बौद्धों का पुरातत्त्व इस प्रकार हमें २०००० ई०पू० तक ले जाता है तथा इनका आदि देश भारतवर्ष में ही होना चाहिए जो कि उस समय ४० अक्षांश तक फैला था। यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैनधर्म के विद्यार्थी 'सुषमा दुःषमा' कल्पों तथा तीर्थंकरों की जीवनी में आने वाले विविध आख्यानों का गम्भीर अध्ययन करके निम्न वाक्य को सार्थक करें। जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् प्रो० एस० श्री नीलकण्ठ शास्त्री के निबन्ध जैन धर्म के आदि देश से साभार
वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ प० सं०१६६-६७
१. ब्रजेन्द्र नाथ शर्मा, 'सोशल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री आफ नार्दर्न इण्डिया', नई दिल्ली, १९७२, पृ० १४१, चित्र २४, २. मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी, 'ए ब्रीफ सर्वे आफ दी माईक्नोग्रेफिक डाटा एट कुम्भारिया, नार्थ गजरात,' सम्बोधि, अहमदाबाद, अप्रेल १९७३, चित्र ३. ३. उमाकान्त, प्रेमानन्द शाह, 'आईक्नोग्रफी माफ दी जैन गोडेस सरस्वती, जर्नल आफ दी यूनिवर्सिटी प्राफ बाम्बे',न० १०, १-२, पृ० १९५-२१७;
मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी, 'सरस्वती इन जैन स्कल्पचर्स', श्रमण, वाराणसी, नं०२२, ३, पृ० २७-३४; वही, नं० २२, ४, पृ० २५-२८. जैन इतिहास, कला और संस्कृति
४५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org