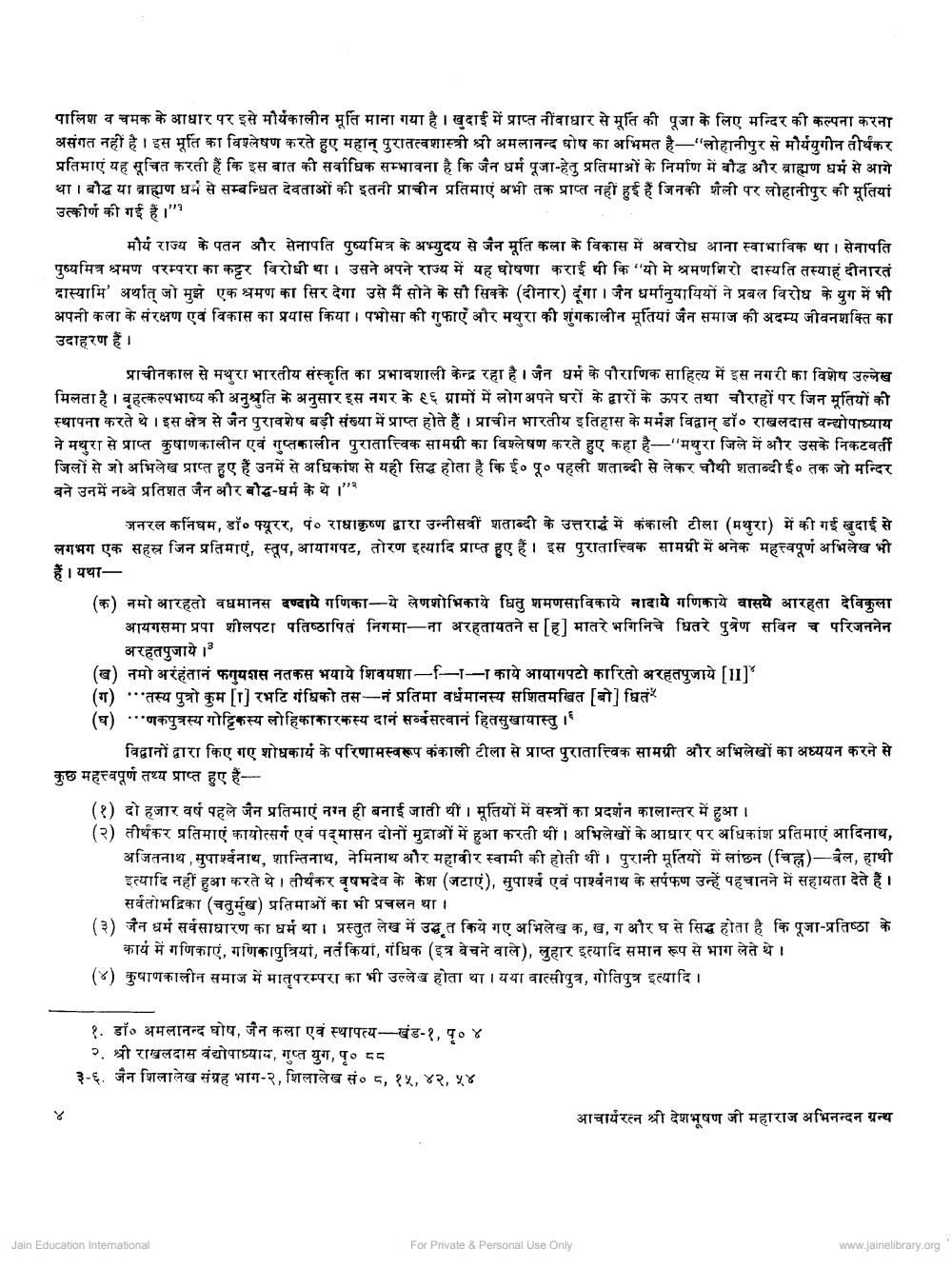________________
पालिश व चमक के आधार पर इसे मौर्यकालीन मूर्ति माना गया है । खुदाई में प्राप्त नींवाधार से मूर्ति की पूजा के लिए मन्दिर की कल्पना करना असंगत नहीं है । इस भूर्ति का विश्लेषण करते हुए महान् पुरातत्वशास्त्री श्री अमलानन्द घोष का अभिमत है—"लोहानीपुर से मौर्ययुगीन तीर्थंकर प्रतिमाएं यह सूचित करती हैं कि इस बात की सर्वाधिक सम्भावना है कि जैन धर्म पूजा-हेतु प्रतिमाओं के निर्माण में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से आगे था । बौद्ध या ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित देवताओं की इतनी प्राचीन प्रतिमाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं जिनकी शैली पर लोहानीपुर की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं।"
मौर्य राज्य के पतन और सेनापति पुष्यमित्र के अभ्युदय से जैन मूर्ति कला के विकास में अवरोध आना स्वाभाविक था। सेनापति पुष्यमित्र श्रमण परम्परा का कट्टर विरोधी था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कराई थी कि “यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारतं दास्यामि' अर्थात् जो मुझे एक श्रमण का सिर देगा उसे मैं सोने के सौ सिक्के (दीनार) दूंगा। जैन धर्मानुयायियों ने प्रबल विरोध के युग में भी अपनी कला के संरक्षण एवं विकास का प्रयास किया। पभोसा की गुफाएं और मथुरा की शुंगकालीन मूर्तियां जैन समाज की अदम्य जीवनशक्ति का उदाहरण हैं।
प्राचीनकाल से मथुरा भारतीय संस्कृति का प्रभावशाली केन्द्र रहा है। जैन धर्म के पौराणिक साहित्य में इस नगरी का विशेष उल्लेख मिलता है । बृहत्कल्पभाष्य की अनुश्रुति के अनुसार इस नगर के ६६ ग्रामों में लोग अपने घरों के द्वारों के ऊपर तथा चौराहों पर जिन मूर्तियों की स्थापना करते थे । इस क्षेत्र से जैन पुरावशेष बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० राखलदास वन्द्योपाध्याय ने मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन पुरातात्त्विक सामग्री का विश्लेषण करते हुए कहा है-"मथुरा जिले में और उसके निकटवर्ती जिलों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकांश से यही सिद्ध होता है कि ई० पू० पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ई० तक जो मन्दिर बने उनमें नब्बे प्रतिशत जैन और बौद्ध-धर्म के थे ।"
जनरल कनिंघम, डॉ० फ्यूरर, पं० राधाकृष्ण द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कंकाली टीला (मथुरा) में की गई खुदाई से लगभग एक सहस्र जिन प्रतिमाएं, स्तूप, आयागपट, तोरण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इस पुरातात्त्विक सामग्री में अनेक महत्त्वपूर्ण अभिलेख भी हैं । यथा(क) नमो आरहतो वधमानस दण्दाये गणिका-ये लेणशोभिकाये धितु शमणसाविकाये नादाये गणिकाये वासये आरहता देविकुला
आयगसमा प्रपा शीलपटा पतिष्ठापितं निगमा–ना अरहतायतने स [ह] मातरे भगिनिचे धितरे पुत्रेण सविन च परिजननेन
अरहतपुजाये। (ख) नमो अरहतानं फगुयशस नतकस भयाये शिवयशा--- काये आयागपटो कारितो अरहतपुजाये [II]' (ग) .."तस्य पुत्रो कुम [1] रभटि गंधिको तस-नं प्रतिमा वर्धमानस्य सशितमखित [बो धित (घ) .''णकपुत्रस्य गोट्टिकस्य लोहिकाकारकस्य दानं सर्वसत्वानं हितसुखायास्तु ।
विद्वानों द्वारा किए गए शोधकार्य के परिणामस्वरूप कंकाली टीला से प्राप्त पुरातात्त्विक सामग्री और अभिलेखों का अध्ययन करने से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं
(१) दो हजार वर्ष पहले जैन प्रतिमाएं नग्न ही बनाई जाती थी। मूर्तियों में वस्त्रों का प्रदर्शन कालान्तर में हुआ। (२) तीर्थकर प्रतिमाएं कायोत्सर्ग एवं पद्मासन दोनों मुद्राओं में हुआ करती थीं। अभिलेखों के आधार पर अधिकांश प्रतिमाएं आदिनाथ,
अजितनाथ , सुपार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी की होती थीं। पुरानी मूर्तियों में लांछन (चिह्न)-बैल, हाथी इत्यादि नहीं हुआ करते थे। तीर्थकर वृषभदेव के केश (जटाएं), सुपार्श्व एवं पार्श्वनाथ के सर्पफण उन्हें पहचानने में सहायता देते हैं ।
सर्वतोभद्रिका (चतुर्मख) प्रतिमाओं का भी प्रचलन था। (३) जैन धर्म सर्वसाधारण का धर्म था। प्रस्तुत लेख में उद्ध त किये गए अभिलेख क, ख, ग और घ से सिद्ध होता है कि पूजा-प्रतिष्ठा के
कार्य में गणिकाएं, गणिकापुत्रियां, नर्तकियां, गंधिक (इत्र बेचने वाले), लुहार इत्यादि समान रूप से भाग लेते थे। (४) कुषाणकालीन समाज में मातृपरम्परा का भी उल्लेख होता था । यया वात्सीपुत्र, गोतिपुत्र इत्यादि ।
१. डॉ० अमलानन्द घोष, जैन कला एवं स्थापत्य-खंड-१, पृ०४ २. श्री राखलदास वंद्योपाध्याय, गुप्त युग, पृ० ८८ ३-६, जैन शिलालेख संग्रह भाग-२, शिलालेख सं०८, १५, ४२, ५४
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org"