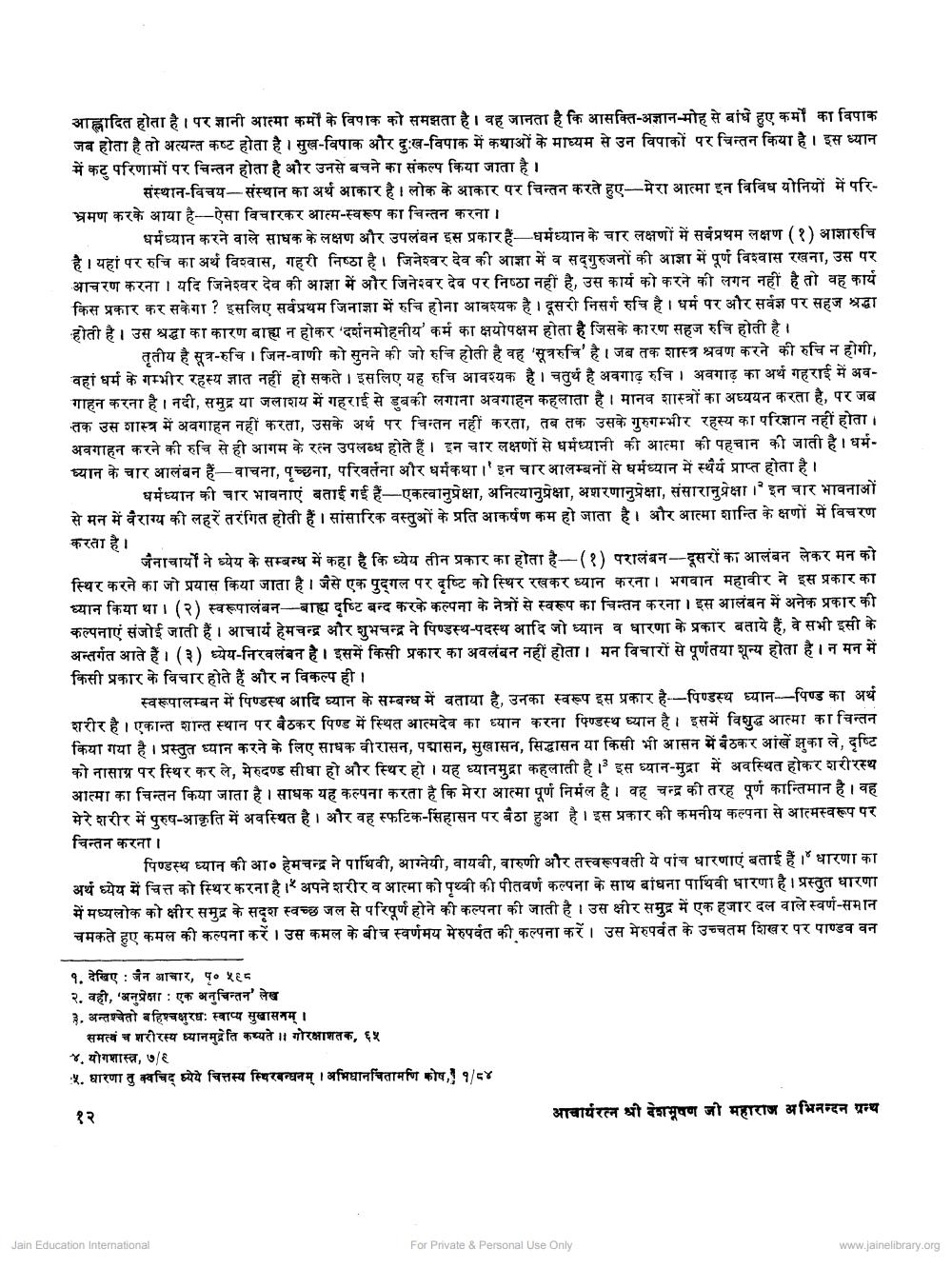________________
आह्लादित होता है। पर ज्ञानी आत्मा कर्मों के विपाक को समझता है। वह जानता है कि आसक्ति-अज्ञान-मोह से बांधे हुए कर्मों का विपाक जब होता है तो अत्यन्त कष्ट होता है । सुख-विपाक और दुःख-विपाक में कथाओं के माध्यम से उन विपाकों पर चिन्तन किया है। इस ध्यान में कटु परिणामों पर चिन्तन होता है और उनसे बचने का संकल्प किया जाता है।
संस्थान-विचय-संस्थान का अर्थ आकार है। लोक के आकार पर चिन्तन करते हुए मेरा आत्मा इन विविध योनियों में परिभ्रमण करके आया है-ऐसा विचारकर आत्म-स्वरूप का चिन्तन करना।
धर्मध्यान करने वाले साधक के लक्षण और उपलंबन इस प्रकार हैं-धर्मध्यान के चार लक्षणों में सर्वप्रथम लक्षण (१) आज्ञारुचि है। यहां पर रुचि का अर्थ विश्वास, गहरी निष्ठा है। जिनेश्वर देव की आज्ञा में व सद्गुरुजनों की आज्ञा में पूर्ण विश्वास रखना, उस पर आचरण करना । यदि जिनेश्वर देव की आज्ञा में और जिनेश्वर देव पर निष्ठा नहीं है, उस कार्य को करने की लगन नहीं है तो वह कार्य किस प्रकार कर सकेगा? इसलिए सर्वप्रथम जिनाज्ञा में रुचि होना आवश्यक है। दूसरी निसर्ग रुचि है। धर्म पर और सर्वज्ञ पर सहज श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा का कारण बाह्य न होकर 'दर्शनमोहनीय' कर्म का क्षयोपक्षम होता है जिसके कारण सहज रुचि होती है।
तृतीय है सूत्र-रुचि । जिन-वाणी को सुनने की जो रुचि होती है वह 'सूत्ररुचि' है। जब तक शास्त्र श्रवण करने की रुचि न होगी, वहां धर्म के गम्भीर रहस्य ज्ञात नहीं हो सकते। इसलिए यह रुचि आवश्यक है। चतुर्थ है अवगाढ़ रुचि । अवगाढ़ का अर्थ गहराई में अवगाहन करना है। नदी, समुद्र या जलाशय में गहराई से डुबकी लगाना अवगाहन कहलाता है। मानव शास्त्रों का अध्ययन करता है, पर जब तक उस शास्त्र में अवगाहन नहीं करता, उसके अर्थ पर चिन्तन नहीं करता, तब तक उसके गुरुगम्भीर रहस्य का परिज्ञान नहीं होता। अवगाहन करने की रुचि से ही आगम के रत्न उपलब्ध होते हैं। इन चार लक्षणों से धर्मध्यानी की आत्मा की पहचान की जाती है। धर्मध्यान के चार आलंबन हैं-वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और धर्मकथा।' इन चार आलम्बनों से धर्मध्यान में स्थैर्य प्राप्त होता है।
धर्मध्यान की चार भावनाएं बताई गई हैं—एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा। इन चार भावनाओं से मन में वैराग्य की लहरें तरंगित होती हैं । सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। और आत्मा शान्ति के क्षणों में विचरण करता है।
जैनाचार्यों ने ध्येय के सम्बन्ध में कहा है कि ध्येय तीन प्रकार का होता है-(१) परालंबन-दूसरों का आलंबन लेकर मन को स्थिर करने का जो प्रयास किया जाता है। जैसे एक पुद्गल पर दृष्टि को स्थिर रखकर ध्यान करना। भगवान महावीर ने इस प्रकार का ध्यान किया था। (२) स्वरूपालंबन-बाह्य दृष्टि बन्द करके कल्पना के नेत्रों से स्वरूप का चिन्तन करना। इस आलंबन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं संजोई जाती हैं । आचार्य हेमचन्द्र और शुभचन्द्र ने पिण्डस्थ-पदस्थ आदि जो ध्यान व धारणा के प्रकार बताये हैं, वे सभी इसी के अन्तर्गत आते हैं। (३) ध्येय-निरवलंबन है। इसमें किसी प्रकार का अवलंबन नहीं होता। मन विचारों से पूर्णतया शून्य होता है। न मन में किसी प्रकार के विचार होते हैं और न विकल्प ही।
स्वरूपालम्बन में पिण्डस्थ आदि ध्यान के सम्बन्ध में बताया है, उनका स्वरूप इस प्रकार है--पिण्डस्थ ध्यान-पिण्ड का अर्थ शरीर है। एकान्त शान्त स्थान पर बैठकर पिण्ड में स्थित आत्मदेव का ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान है। इसमें विशुद्ध आत्मा का चिन्तन किया गया है । प्रस्तुत ध्यान करने के लिए साधक वीरासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या किसी भी आसन में बैठकर आंखें झुका ले, दृष्टि को नासान पर स्थिर कर ले, मेरुदण्ड सीधा हो और स्थिर हो । यह ध्यानमुद्रा कहलाती है। इस ध्यान-मुद्रा में अवस्थित होकर शरीरस्थ आत्मा का चिन्तन किया जाता है । साधक यह कल्पना करता है कि मेरा आत्मा पूर्ण निर्मल है। वह चन्द्र की तरह पूर्ण कान्तिमान है। वह मेरे शरीर में पुरुष-आकृति में अवस्थित है। और वह स्फटिक-सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस प्रकार की कमनीय कल्पना से आत्मस्वरूप पर चिन्तन करना।
पिण्डस्थ ध्यान की आ० हेमचन्द्र ने पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी, वारुणी और तत्त्वरूपवती ये पांच धारणाएं बताई हैं। धारणा का अर्थ ध्येय में चित्त को स्थिर करना है। अपने शरीर व आत्मा को पृथ्वी की पीतवर्ण कल्पना के साथ बांधना पार्थिवी धारणा है । प्रस्तुत धारणा में मध्यलोक को क्षीर समुद्र के सदृश स्वच्छ जल से परिपूर्ण होने की कल्पना की जाती है । उस क्षीर समुद्र में एक हजार दल वाले स्वर्ण-समान चमकते हुए कमल की कल्पना करें। उस कमल के बीच स्वर्णमय मेरुपर्वत की कल्पना करें। उस मेरुपर्वत के उच्चतम शिखर पर पाण्डव वन
१. देखिए : जैन आचार, पृ० ५६८ २. वही, 'अनुप्रेक्षा : एक अनुचिन्तन' लेख ३. अन्तश्चेतो बहिश्चक्षुरधः स्वाप्य सुखासनम् ।
समत्वं च शरीरस्य ध्यानमुद्रेति कथ्यते ।। गोरक्षाशतक, ६५ ४. योगशास्त्र, ७/६ ५. धारणा तु क्वचिद् ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम् । अभिधानचिंतामणि कोष,! १/८४
१२
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org