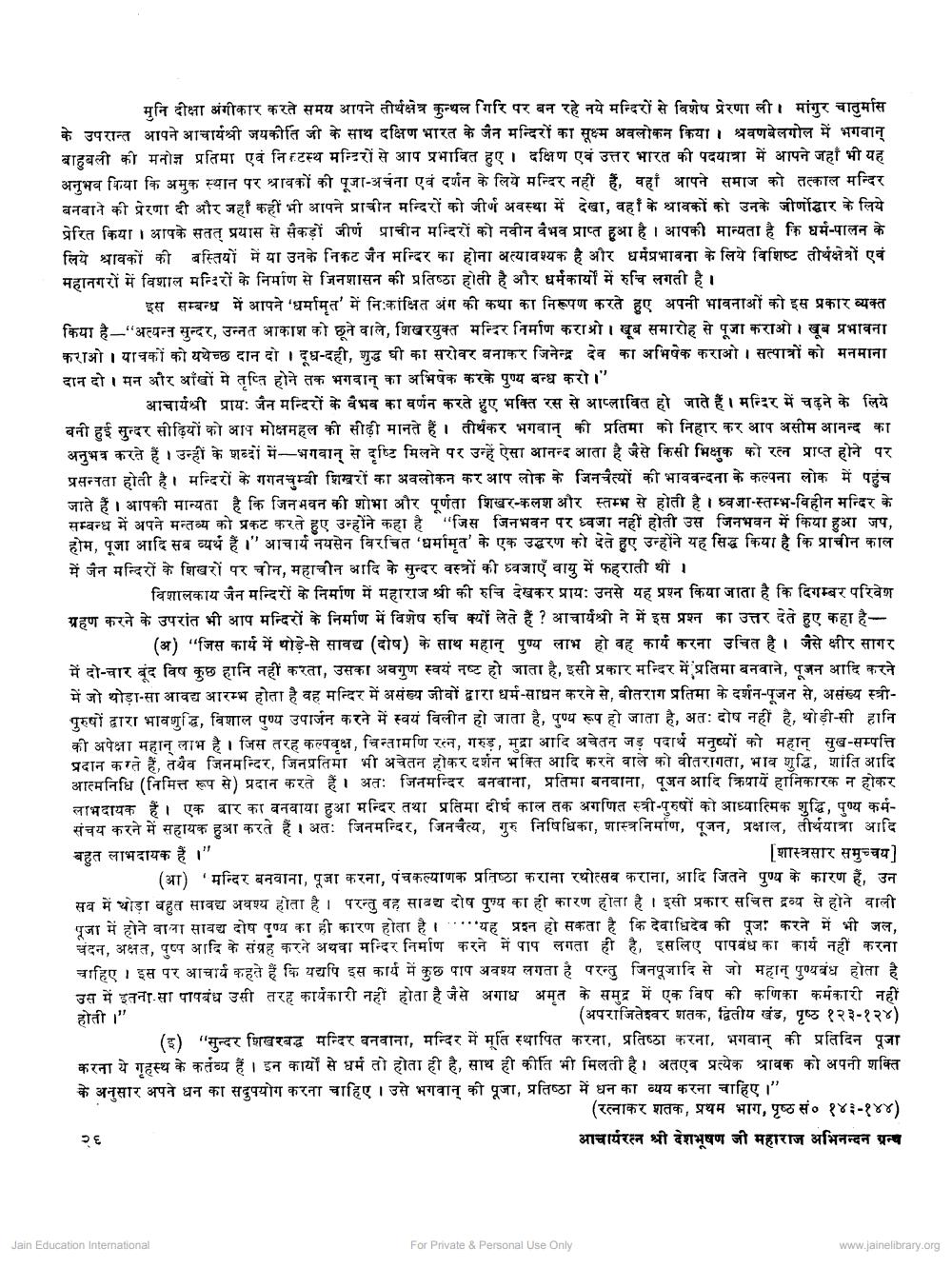________________
मुनि दीक्षा अंगीकार करते समय आपने तीर्थक्षेत्र कुन्थल गिरि पर बन रहे नये मन्दिरों से विशेष प्रेरणा ली। मांगुर चातुर्मा के उपरान्त आपने आचार्यश्री जयकीति जी के साथ दक्षिण भारत के जैन मन्दिरों का सूक्ष्म अवलोकन किया । श्रवणबेलगोल में भगवान् बाहुबली की मनोज्ञ प्रतिमा एवं निकटस्थ मन्दिरों से आप प्रभावित हुए। दक्षिण एवं उत्तर भारत की पदयात्रा में आपने जहाँ भी यह अनुभव किया कि अमुक स्थान पर श्रावकों की पूजा-अर्चना एवं दर्शन के लिये मन्दिर नहीं हैं, वहाँ आपने समाज को तत्काल मन्दिर बनवाने की प्रेरणा दी और नहीं कहीं भी आपने प्राचीन मन्दिरों को जीर्ण अवस्था में देखा, वहाँ के धावकों को उनके जीर्णोद्वार के लिये प्रेरित किया। आपके सतत् प्रयास से सैकड़ों जीर्ण प्राचीन मन्दिरों को नवीन वैभव प्राप्त हुआ है । आपकी मान्यता है कि धर्म-पालन के लिये श्रावकों की बस्तियों में या उनके निकट जैन मन्दिर का होना अत्यावश्यक है और धर्मप्रभावना के लिये विशिष्ट तीर्थक्षेत्रों एवं महानगरों में विशाल मन्दिरों के निर्माण से जिनशासन की प्रतिष्ठा होती है और धर्मकार्यों में रुचि लगती है।
66
इस सम्बन्ध में आपने 'धर्मामृत' में निःकांक्षित अंग की कथा का निरूपण करते हुए अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है "अत्यन्त सुन्दर, उन्नत आकाश को छूने वाले शिखरयुक्त मन्दिर निर्माण कराओ खूब समारोह से पूजा कराओ। खूब प्रभावना कराओ । याचकों को यथेच्छ दान दो । दूध-दही, शुद्ध घी का सरोवर बनाकर जिनेन्द्र देव का अभिषेक कराओ । सत्पात्रों को मनमाना दान दो । मन और आँखों में तृप्ति होने तक भगवान् का अभिषेक करके पुण्य बन्ध करो।"
आचार्यश्री प्रायः जैन मन्दिरों के वैभव का वर्णन करते हुए भक्ति रस से आप्लावित हो जाते हैं। मन्दिर में चढ़ने के लिये बनी हुई सुन्दर सीढ़ियों को आप मोक्षमहल की सीढ़ी मानते हैं । तीर्थंकर भगवान् की प्रतिमा को निहार कर आप असीम आनन्द का अनुभव करते हैं। उन्हीं के शब्दों में- भगवान् से दृष्टि मिलने पर उन्हें ऐसा आनन्द आता है जैसे किसी भिक्षुक को रत्न प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है । मन्दिरों के गगनचुम्बी शिखरों का अवलोकन कर आप लोक के जिनचैत्यों की भाववन्दना के कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं। आपकी मान्यता है कि जिनमवन की शोभा और पूर्णता शिखर कलश और स्तम्भ से होती है। वास्तम्भ विहीन मन्दिर के सम्बन्ध में अपने मन्तव्य को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है "जिस जिनभवन पर ध्वजा नहीं होती उस जिनभवन में किया हुआ जप, होम, पूजा आदि सब व्यर्थ हैं ।" आचार्य नयसेन विरचित 'धर्मामृत' के एक उद्धरण को देते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्राचीन काल
में जैन मन्दिरों के शिखरों पर चौन, महाचीन आदि के सुन्दर वस्त्रों की ध्वजाऍ वायु में फहराती थीं ।
विशालकाय जैन मन्दिरों के निर्माण में महाराज श्री की रुचि देखकर प्रायः उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि दिगम्बर परिवेश ग्रहण करने के उपरांत भी आप मन्दिरों के निर्माण में विशेष रुचि क्यों लेते हैं ? आचार्यश्री ने में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है( अ ) "जिस कार्य में थोड़े-से सावद्य (दोष) के साथ महान् पुण्य लाभ हो वह कार्य करना उचित है । जैसे क्षीर सागर
,
में दो-चार बूंद विष कुछ हानि नहीं करता, उसका अवगुण स्वयं नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मन्दिर में प्रतिमा बनवाने, पूजन आदि करने में जो थोड़ा-सा आव आरम्भ होता है वह मन्दिर में असंख्य जीवों द्वारा धर्म-साधन करने से वीतराग प्रतिमा के दर्शन-पूजन से असंख्य स्त्रीपुरुषों द्वारा भावशुद्धि, विशाल पुण्य उपार्जन करने में स्वयं विलीन हो जाता है, पुण्य रूप हो जाता है, अतः दोष नहीं है, थोड़ी-सी हानि की अपेक्षा महान् लाभ है। जिस तरह कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न, गरुड़, मुद्रा आदि अचेतन जड़ पदार्थ मनुष्यों को महान् सुख-सम्पत्ति प्रदान करते हैं, तथैव जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा भी अचेतन होकर दर्शन भक्ति आदि करने वाले को वीतरागता, भाव शुद्धि, शांति आदि आत्मनिधि (निमित्त रूप से) प्रदान करते हैं । अतः जिनमन्दिर बनवाना, प्रतिमा बनवाना, पूजन आदि क्रियायें हानिकारक न होकर लाभदायक हैं। एक बार का बनवाया हुआ मन्दिर तथा प्रतिमा दीर्घ काल तक अगणित स्त्री-पुरुषों को आध्यात्मिक शुद्धि, पुण्य कर्मसंचय करने में सहायक हुआ करते हैं । अतः जिनमन्दिर, जिनचैत्य, गुरु निषिधिका शास्त्रनिर्माण, पूजन, प्रक्षाल, तीर्थयात्रा आदि बहुत लाभदायक हैं ।" [सारसार समुच्चय ]
(आ) 'मन्दिर बनवाना, पूजा करना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराना रथोत्सव कराना, आदि जितने पुण्य के कारण हैं, उन सब में थोड़ा बहुत सावध अवश्य होता है । परन्तु वह सावध दोष पुण्य का ही कारण होता है । इसी प्रकार सचित्त द्रव्य से होने वाली पूजा में होने वाला सावद्य दोष पुण्य का ही कारण होता है । यह प्रश्न हो सकता है कि देवाधिदेव की पूजा करने में भी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के संग्रह करने अथवा मन्दिर निर्माण करने में पाप लगता ही है, इसलिए पापबंध का कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर आचार्य कहते है कि यद्यपि इस कार्य में कुछ पाप अवश्य लगता है परन्तु जिनपूजादि से जो महान् पुष्पबंध होता है उस में इतना सा पापबंध उसी तरह कार्यकारी नहीं होता है जैसे अगाध अमृत के समुद्र में एक विष की कणिका कर्मकारी नहीं होती ।" (अपराजितेश्वर शतक द्वितीय बंब, पृष्ठ १२३-१२४) (द) "सुन्दर विश्व मन्दिर बनवाना, मन्दिर में मूर्ति स्थापित करना, प्रतिष्ठा करना भगवान् की प्रतिदिन पूजा करना ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं। इन कार्यों से धर्म तो होता ही है, साथ ही कीर्ति भी मिलती है । अतएव प्रत्येक श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। उसे भगवान् की पूजा, प्रतिष्ठा में धन का व्यय करना चाहिए ।"
"
(रत्नाकर शतक प्रथम भाग, पृष्ठ सं० १४३-१४४)
1
आचार्यरश्न भी देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
२६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org