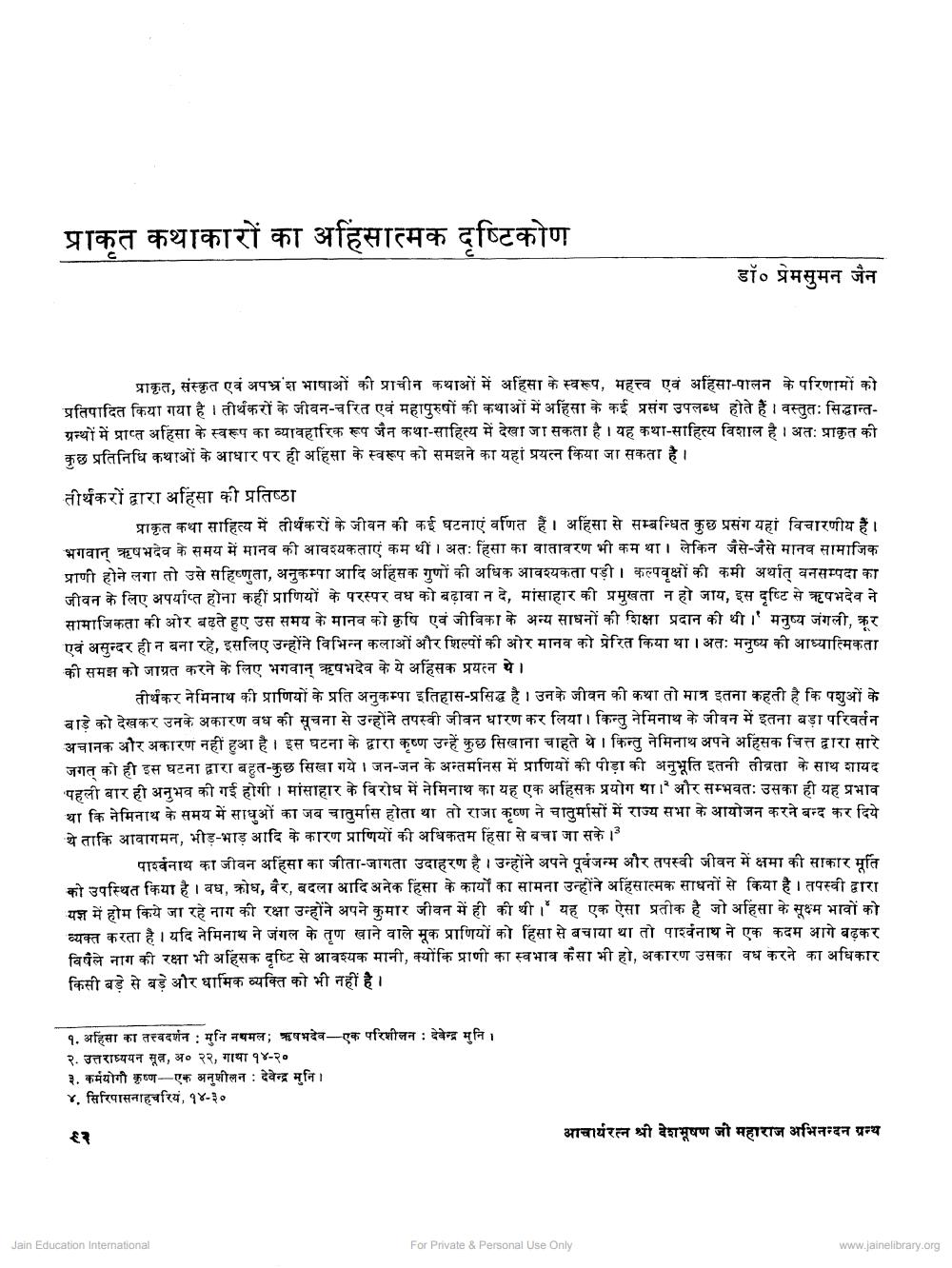________________
प्राकृत कथाकारों का अहिंसात्मक दृष्टिकोण
डॉ० प्रेमसुमन जैन
प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश भाषाओं की प्राचीन कथाओं में अहिंसा के स्वरूप, महत्त्व एवं अहिंसा-पालन के परिणामों को प्रतिपादित किया गया है। तीर्थंकरों के जीवन-चरित एवं महापुरुषों की कथाओं में अहिंसा के कई प्रसंग उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः सिद्धान्तग्रन्थों में प्राप्त अहिंसा के स्वरूप का व्यावहारिक रूप जैन कथा-साहित्य में देखा जा सकता है। यह कथा-साहित्य विशाल है। अत: प्राकृत की कछ प्रतिनिधि कथाओं के आधार पर ही अहिंसा के स्वरूप को समझने का यहां प्रयत्न किया जा सकता है।
तीर्थकरों द्वारा अहिंसा की प्रतिष्ठा
प्राकृत कथा साहित्य में तीर्थंकरों के जीवन की कई घटनाएं वर्णित हैं। अहिंसा से सम्बन्धित कुछ प्रसंग यहां विचारणीय है। भगवान ऋषभदेव के समय में मानव की आवश्यकताएं कम थीं। अतः हिंसा का वातावरण भी कम था। लेकिन जैसे-जैसे मानव सामाजिक प्राणी होने लगा तो उसे सहिष्णुता, अनुकम्पा आदि अहिंसक गुणों की अधिक आवश्यकता पड़ी। कल्पवृक्षों की कमी अर्थात् वनसम्पदा का जीवन के लिए अपर्याप्त होना कहीं प्राणियों के परस्पर वध को बढ़ावा न दे, मांसाहार की प्रमुखता न हो जाय, इस दृष्टि से ऋषभदेव ने सामाजिकता की ओर बढ़ते हुए उस समय के मानव को कृषि एवं जीविका के अन्य साधनों की शिक्षा प्रदान की थी। मनुष्य जंगली, कर एवं असन्दर हीन बना रहे, इसलिए उन्होंने विभिन्न कलाओं और शिल्पों की ओर मानव को प्रेरित किया था । अतः मनुष्य की आध्यात्मिकता की समझ को जाग्रत करने के लिए भगवान् ऋषभदेव के ये अहिंसक प्रयत्न थे।
तीर्थकर नेमिनाथ की प्राणियों के प्रति अनुकम्पा इतिहास-प्रसिद्ध है। उनके जीवन की कथा तो मात्र इतना कहती है कि पशुओं के बाडे को देखकर उनके अकारण वध की सूचना से उन्होंने तपस्वी जीवन धारण कर लिया। किन्तु नेमिनाथ के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन अचानक और अकारण नहीं हुआ है। इस घटना के द्वारा कृष्ण उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे। किन्तु नेमिनाथ अपने अहिंसक चित्त द्वारा सारे जगत को ही इस घटना द्वारा बहुत-कुछ सिखा गये । जन-जन के अन्तर्मानस में प्राणियों की पीड़ा की अनुभूति इतनी तीव्रता के साथ शायद पहली बार ही अनुभव की गई होगी। मांसाहार के विरोध में नेमिनाथ का यह एक अहिंसक प्रयोग था। और सम्भवतः उसका ही यह प्रभाव था कि नेमिनाथ के समय में साधुओं का जब चातुर्मास होता था तो राजा कृष्ण ने चातुर्मासों में राज्य सभा के आयोजन करने बन्द कर दिये थे ताकि आवागमन, भीड़-भाड़ आदि के कारण प्राणियों की अधिकतम हिंसा से बचा जा सके।
पार्श्वनाथ का जीवन अहिंसा का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने पूर्वजन्म और तपस्वी जीवन में क्षमा की साकार मूर्ति को उपस्थित किया है । वध, क्रोध, वैर, बदला आदि अनेक हिंसा के कार्यों का सामना उन्होंने अहिंसात्मक साधनों से किया है । तपस्वी द्वारा यज्ञ में होम किये जा रहे नाग की रक्षा उन्होंने अपने कुमार जीवन में ही की थी। यह एक ऐसा प्रतीक है जो अहिंसा के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करता है । यदि नेमिनाथ ने जंगल के तृण खाने वाले मूक प्राणियों को हिंसा से बचाया था तो पाश्र्वनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर विषैले नाग की रक्षा भी अहिंसक दृष्टि से आवश्यक मानी, क्योंकि प्राणी का स्वभाव कैसा भी हो, अकारण उसका वध करने का अधिकार किसी बड़े से बड़े और धार्मिक व्यक्ति को भी नहीं है।
१. अहिंसा का तत्त्वदर्शन : मुनि नथमल; ऋषभदेव-एक परिशीलन : देवेन्द्र मुनि । २. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २२, गाथा १४-२० ३. कर्मयोगी कृष्ण-एक अनुशीलन : देवेन्द्र मुनि। ४. सिरिपासनाहचरियं, १४-३०
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org