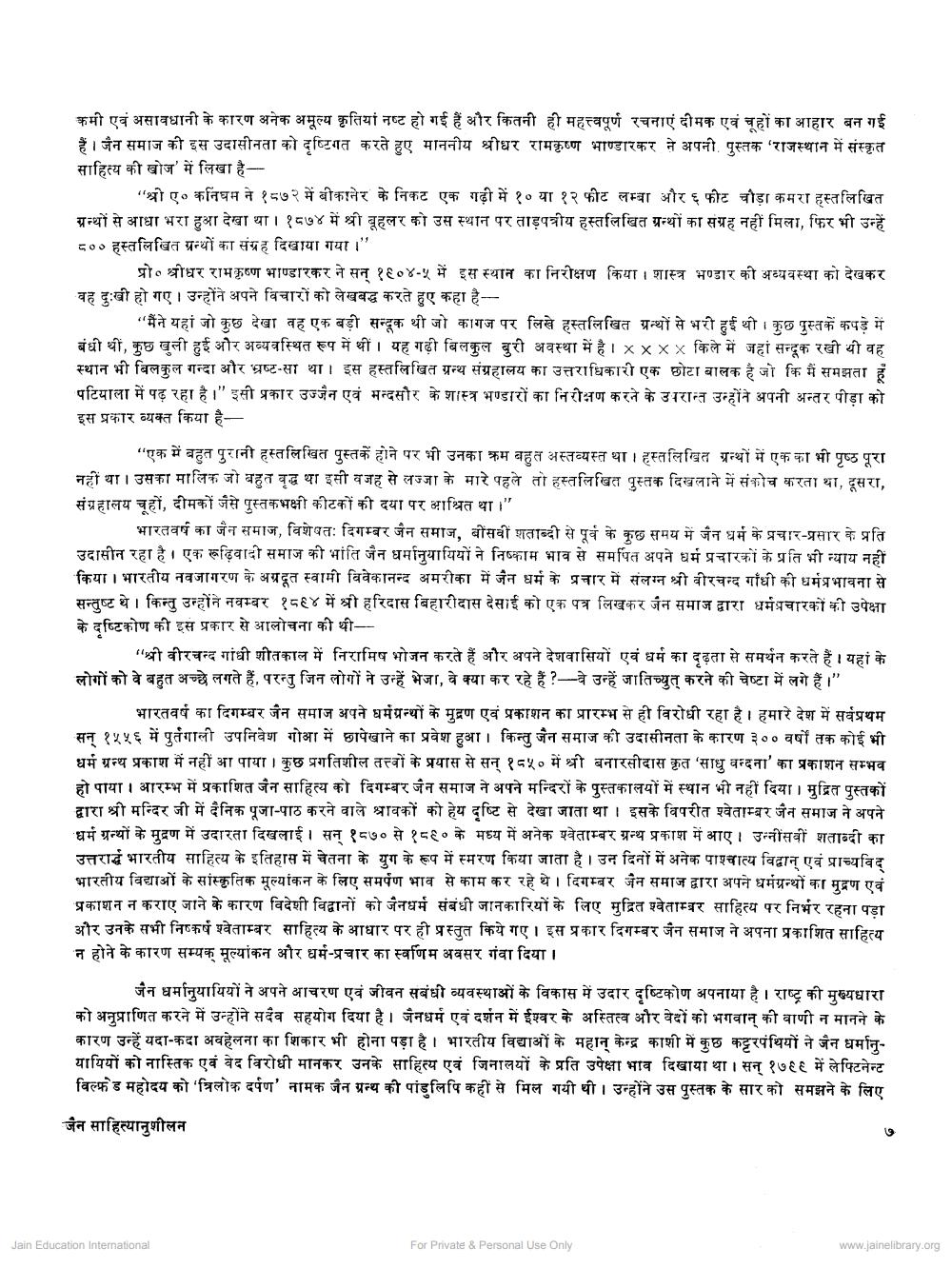________________
कमी एवं असावधानी के कारण अनेक अमूल्य कृतियां नष्ट हो गई हैं और कितनी ही महत्त्वपूर्ण रचनाएं दीमक एवं चूहों का आहार बन गई हैं। जैन समाज की इस उदासीनता को दृष्टिगत करते हुए माननीय श्रीधर रामकृष्ण भाण्डारकर ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज' में लिखा है
"श्री ए. कनिंघम ने १८७२ में बीकानेर के निकट एक गढ़ी में १० या १२ फीट लम्बा और ६ फीट चौड़ा कमरा हस्तलिखित ग्रन्थों से आधा भरा हुआ देखा था। १८७४ में श्री बूहलर को उस स्थान पर ताडपत्रीय हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह नहीं मिला, फिर भी उन्हें ८०० हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह दिखाया गया।"
प्रो० श्रीधर रामकृष्ण भाण्डारकर ने सन् १९०४-५ में इस स्थान का निरीक्षण किया। शास्त्र भण्डार की अव्यवस्था को देखकर वह दुःखी हो गए। उन्होंने अपने विचारों को लेखबद्ध करते हुए कहा है
“मैंने यहां जो कुछ देखा वह एक बड़ी सन्दूक थी जो कागज पर लिखे हस्तलिखित ग्रन्थों से भरी हुई थी। कुछ पुस्तके कपड़े में बंधी थीं, कुछ खुली हुई और अव्यवस्थित रूप में थीं। यह गढ़ी बिलकुल बुरी अवस्था में है। xxxx किले में जहां सन्दूक रखी थी वह स्थान भी बिलकुल गन्दा और भ्रष्ट-सा था। इस हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहालय का उत्तराधिकारी एक छोटा बालक है जो कि मैं समझता हूँ पटियाला में पढ़ रहा है।" इसी प्रकार उज्जैन एवं मन्दसौर के शास्त्र भण्डारों का निरीक्षण करने के उपरान्त उन्होंने अपनी अन्तर पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया है
"एक में बहुत पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें होने पर भी उनका क्रम बहुत अस्तव्यस्त था। हस्तलिखित ग्रन्थों में एक का भी पृष्ठ पूरा नहीं था। उसका मालिक जो बहुत वृद्ध था इसी वजह से लज्जा के मारे पहले तो हस्तलिखित पुस्तक दिखलाने में संकोच करता था, दूसरा, संग्रहालय चूहों, दीमकों जैसे पुस्तकभक्षी कीटकों की दया पर आश्रित था।"
भारतवर्ष का जैन समाज, विशेषतः दिगम्बर जैन समाज, बीसवीं शताब्दी से पूर्व के कुछ समय में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के प्रति उदासीन रहा है। एक रूढ़िवादी समाज की भांति जैन धर्मानुयायियों ने निष्काम भाव से समर्पित अपने धर्म प्रचारकों के प्रति भी न्याय नहीं किया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानन्द अमरीका में जैन धर्म के प्रनार में संलग्न श्री बीरचन्द गाँधी की धर्मप्रभावना से सन्तुष्ट थे। किन्तु उन्होंने नवम्बर १८६४ में श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को एक पत्र लिखकर जैन समाज द्वारा धर्मप्रचारकों की उपेक्षा के दष्टिकोण की इस प्रकार से आलोचना की थी--
"श्री वीरचन्द गांधी शीतकाल में निरामिष भोजन करते हैं और अपने देशवासियों एवं धर्म का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। यहां के लोगों को वे बहुत अच्छे लगते हैं, परन्तु जिन लोगों ने उन्हें भेजा, वे क्या कर रहे हैं ?-वे उन्हें जातिच्युत् करने की चेष्टा में लगे हैं।"
भारतवर्ष का दिगम्बर जैन समाज अपने धर्मग्रन्थों के मुद्रण एवं प्रकाशन का प्रारम्भ से ही विरोधी रहा है। हमारे देश में सर्वप्रथम सन् १५५६ में पुर्तगाली उपनिवेश गोआ में छापेखाने का प्रवेश हुआ। किन्तु जैन समाज की उदासीनता के कारण ३०० वर्षों तक कोई भी धर्म ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आ पाया। कुछ प्रगतिशील तत्त्वों के प्रयास से सन् १८५० में श्री बनारसीदास कृत 'साधु बन्दना' का प्रकाशन सम्भव हो पाया। आरम्भ में प्रकाशित जैन साहित्य को दिगम्बर जैन समाज ने अपने मन्दिरों के पुस्तकालयों में स्थान भी नहीं दिया। मुद्रित पुस्तकों द्वारा श्री मन्दिर जी में दैनिक पूजा-पाठ करने वाले श्रावकों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसके विपरीत श्वेताम्बर जैन समाज ने अपने धर्म ग्रन्थों के मुद्रण में उदारता दिखलाई। सन १८७० से १८९० के मध्य में अनेक श्वेताम्बर ग्रन्थ प्रकाश में आए। उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारतीय साहित्य के इतिहास में चेतना के युग के रूप में स्मरण किया जाता है। उन दिनों में अनेक पाश्चात्य विद्वान एवं प्राच्यविद भारतीय विद्याओं के सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे थे। दिगम्बर जैन समाज द्वारा अपने धर्मग्रन्थों का मुद्रण एवं प्रकाशन न कराए जाने के कारण विदेशी विद्वानों को जैनधर्म संबंधी जानकारियों के लिए मुद्रित श्वेताम्बर साहित्य पर निर्भर रहना पड़ा और उनके सभी निष्कर्ष श्वेताम्बर साहित्य के आधार पर ही प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार दिगम्बर जैन समाज ने अपना प्रकाशित साहित्य न होने के कारण सम्यक् मूल्यांकन और धर्म-प्रचार का स्वर्णिम अवसर गंवा दिया।
जैन धर्मानुयायियों ने अपने आचरण एवं जीवन सबंधी व्यवस्थाओं के विकास में उदार दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्र की मुख्यधारा को अनुप्राणित करने में उन्होंने सदैव सहयोग दिया है। जैनधर्म एवं दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व और वेदों को भगवान् की वाणी न मानने के कारण उन्हें यदा-कदा अवहेलना का शिकार भी होना पड़ा है। भारतीय विद्याओं के महान केन्द्र काशी में कुछ कट्टरपंथियों ने जैन धर्मानुयायियों को नास्तिक एवं वेद विरोधी मानकर उनके साहित्य एवं जिनालयों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाया था। सन् १७६६ में लेफ्टिनेन्ट विल्फ्रेड महोदय को 'त्रिलोक दर्पण' नामक जैन ग्रन्थ की पांडुलिपि कहीं से मिल गयी थी। उन्होंने उस पुस्तक के सार को समझने के लिए
जैन साहित्यानुशीलन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org