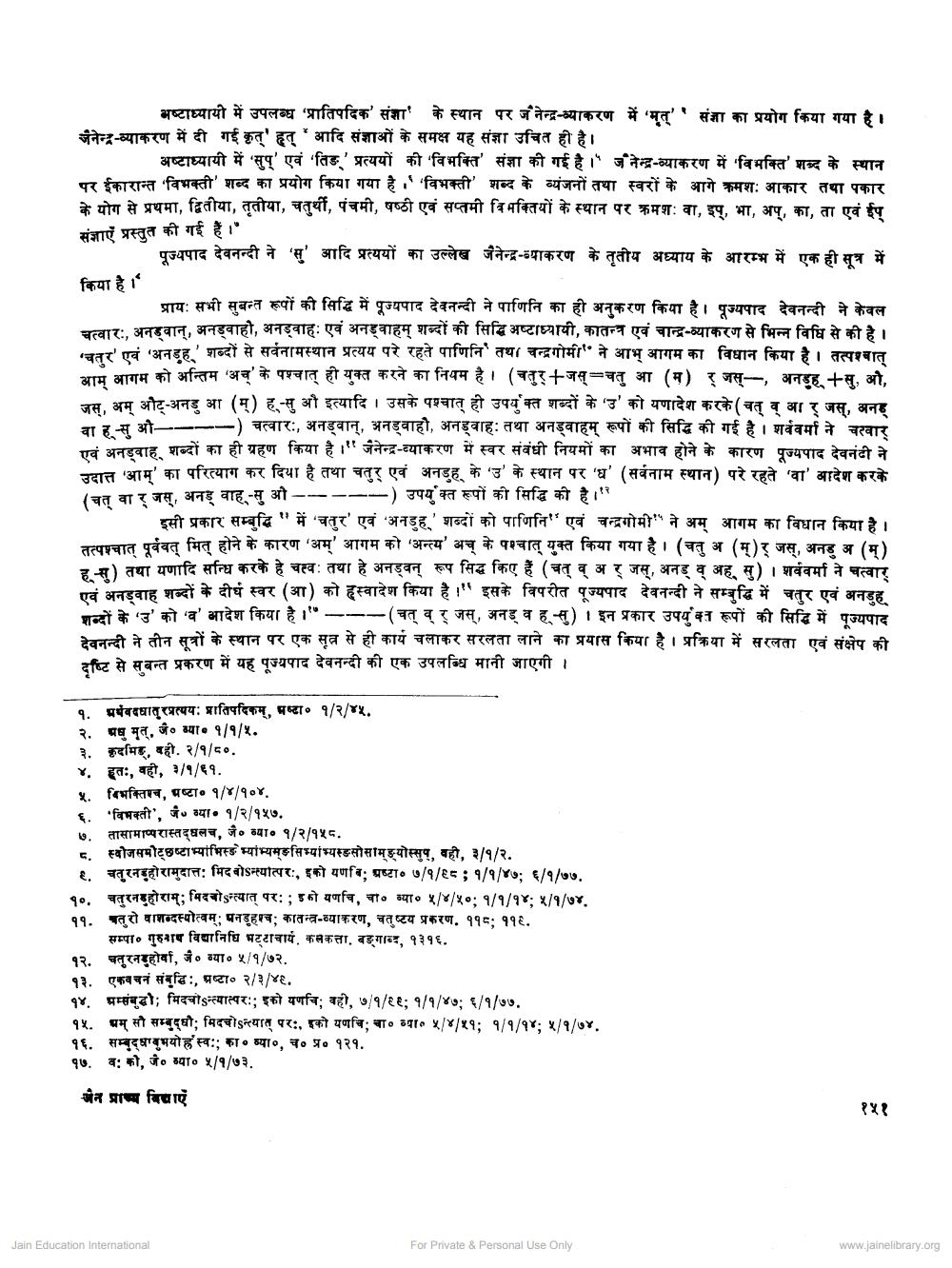________________
अष्टाध्यायी में उपलब्ध 'प्रातिपदिक' संज्ञा' के स्थान पर जैनेन्द्र-व्याकरण में 'मृत्' ' संज्ञा का प्रयोग किया गया है। जैनेन्द्र-व्याकरण में दी गई कृत्' हृत् ' आदि संज्ञाओं के समक्ष यह संज्ञा उचित ही है।
अष्टाध्यायी में ‘सुप्' एवं 'तिङ' प्रत्ययों की विभक्ति' संज्ञा की गई है।' जनेन्द्र-व्याकरण में विभक्ति' शब्द के स्थान पर ईकारान्त 'विभक्ती' शब्द का प्रयोग किया गया है। विभक्ती' शब्द के व्यंजनों तथा स्वरों के आगे क्रमशः आकार तथा पकार के योग से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियों के स्थान पर क्रमशः वा, इप्, भा, अप्, का, ता एवं ईप संज्ञाएँ प्रस्तुत की गई हैं।'
पूज्यपाद देवनन्दी ने 'सु' आदि प्रत्ययों का उल्लेख जैनेन्द्र-व्याकरण के तृतीय अध्याय के आरम्भ में एक ही सूत्र में किया है।
प्रायः सभी सुबन्त रूपों की सिद्धि में पूज्यपाद देवनन्दी ने पाणिनि का ही अनुकरण किया है। पूज्यपाद देवनन्दी ने केवल पर अनडवान, अनड़वाहो, अनड्वाहः एवं अनड्वाहम् शब्दों की सिद्धि अष्टाध्यायी, कातन्त्र एवं चान्द्र-व्याकरण से भिन्न विधि से की है।
एवं अनडह' शब्दों से सर्वनामस्थान प्रत्यय परे रहते पाणिनि' तथा चन्द्रगोमी" ने आभ् आगम का विधान किया है। तत्पश्चात् आगम को अन्तिम 'अच्' के पश्चात् ही युक्त करने का नियम है। (चतुर+जस्च तु आ (म) र जस्-, अनडुह, +सु, ओ,
अस औट-अनड आ (म) ह.-सु औ इत्यादि । उसके पश्चात् ही उपयुक्त शब्दों के 'उ' को यणादेश करके (चत व आर जस. अनह वारस औ----) चत्वारः, अनड्वान्, अनड्वाही, अनड्वाहः तथा अनड्वाहम् रूपों की सिद्धि की गई है । शर्ववर्मा ने चत्वार
अनडवाह शब्दों का ही ग्रहण किया है।" जैनेन्द्र-व्याकरण में स्वर संबंधी नियमों का अभाव होने के कारण पूज्यपाद देवनंदी ने उटात 'आम' का परित्याग कर दिया है तथा चतुर् एवं अनडुह के 'उ' के स्थान पर 'ध' (सर्वनाम स्थान) परे रहते 'वा' आदेश करके (चत् वा र् जस्, अनड वाह-सु ओ-----) उपर्युक्त रूपों की सिद्धि की है।
इसी प्रकार सम्बुद्धि " में 'चतुर' एवं 'अनडुह,' शब्दों को पाणिनि" एवं चन्द्रगोमी ने अम् आगम का विधान किया है। पर्ववत मित होने के कारण 'अम्' आगम को 'अन्त्य' अच् के पश्चात् युक्त किया गया है। (चतु अ (म्) र जस्, अनड़ अ (म) तथा यणादि सन्धि करके हे चस्वः तथा हे अनड्वन् रूप सिद्ध किए हैं (चत् व् अ र् जस्, अनड् व् अह, सु) । शर्ववर्मा ने चत्वार अनडवाह शब्दों के दीर्घ स्वर (आ) को हस्वादेश किया है। इसके विपरीत पूज्यपाद देवनन्दी ने सम्बुद्धि में चतर एवं अनडह शब्दों के 'उ' को 'व' आदेश किया है।"---(चत् व र् जस्, अनड् व ह-सु) । इन प्रकार उपर्युक्त रूपों की सिद्धि में पज्यपाद देवनन्दी ने तीन सत्रों के स्थान पर एक सूत्र से ही कार्य चलाकर सरलता लाने का प्रयास किया है। प्रक्रिया में सरलता एवं संक्षेप की दष्टि से सबन्त प्रकरण में यह पूज्यपाद देवनन्दी की एक उपलब्धि मानी जाएगी।
१. प्रवदधातप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, मष्टा० १/२/४५. २. मधु मृत्, जै० व्या.१/१/५. ३. कृदमिह, वही. २/१/८०. ४. हतः, वही, ३/१/६१.
विभक्तिश्च, अष्टा० १/४/१०४. ६. 'विभक्ती',. व्या• १/२/१५७.
तासामाप्परास्तद्धलच, जै० व्या० १/२/१५८. ६. स्वौजसमौट्छष्टाभ्यांभिस्ङ भ्यांभ्यम्कसिभ्यांभ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप, वही, ३/१/२. १. चतुरनहोरामुदात्त: मिद वोऽन्त्यत्पिरः, इको यणबि; अष्टा०७/१/१८% १/१/४७; ६/१/७७. १०. चतरनबहोराम: मिदमोऽन्त्यात पर: इको यणचि, चा० व्या०५/४/५०: १/१/१४:५/१/७४.
चतुरो वाशब्दस्योत्वम् पनडुहरच; कातन्त्र-व्याकरण, चतुष्टय प्रकरण. ११८; ११६. सम्पा. गुरुनाव विद्यानिधि भट्टाचार्य, कलकत्ता, बङ्गाब्द, १३१६.
चतुरनबुहोर्वा, जै० व्या०५/१/७२. १३. एकवचनं संवृद्धि:, प्रष्टा० २/३/४६. १४. मम्संबुद्धी; मिदचोऽन्त्यात्परः; इको याच; वही, ७/१/९६; १/१/४७; ६/१/७७. १५. अम् सौ सम्बुद्धौ; मिदचोऽन्त्यात् पर:, इको यणचि; चा० व्या० ५/४/११; १/१/१४; ५/१/७४. १६. सम्बुद्धाबुभयोह्रस्व:; का. व्या०, च०प्र० १२१. १७. व:को,जै० व्या० ५/१/७३.
१२.
जैन प्राच्य विद्याएं
१५१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org