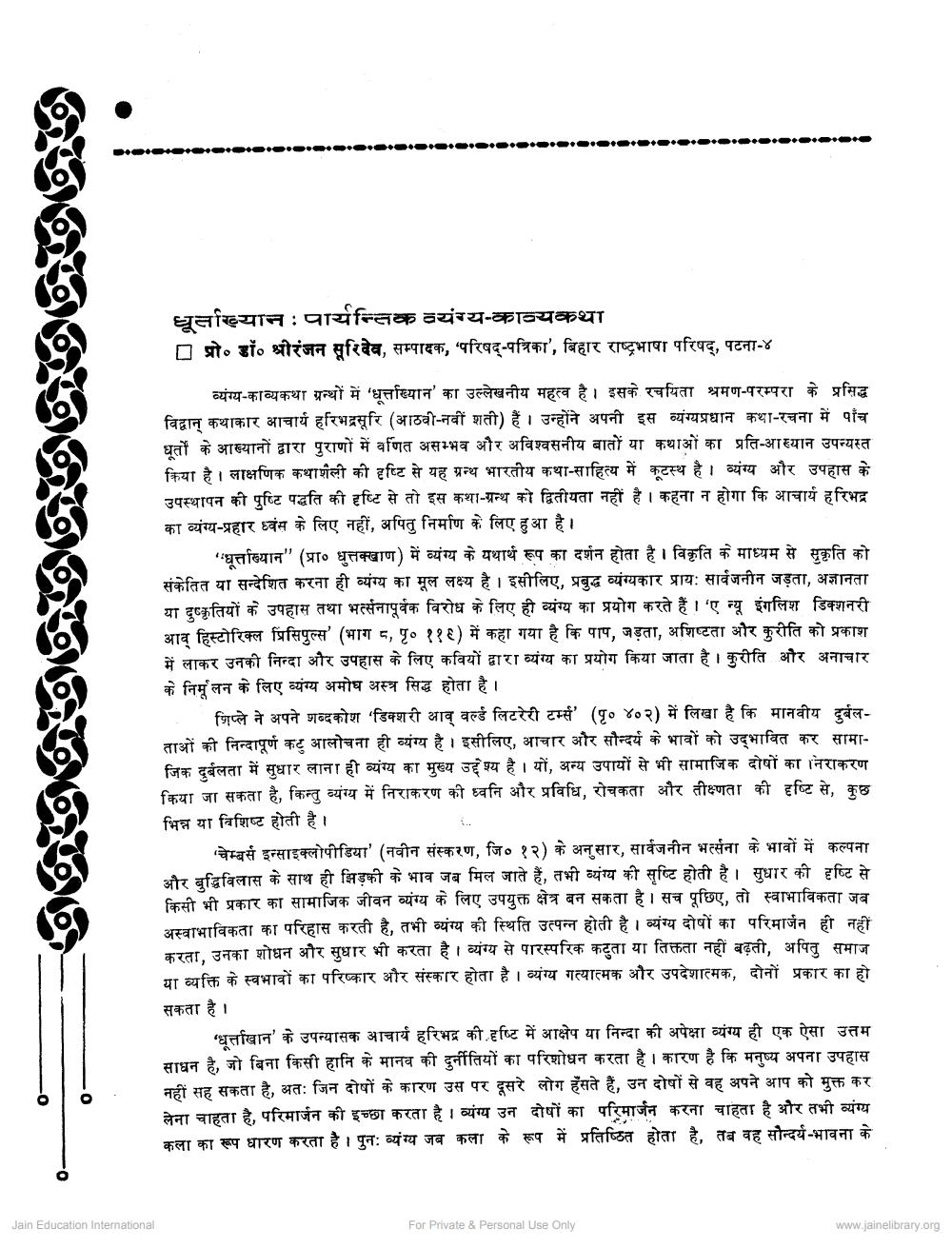________________
-.
-.
-
.
-.
-.
-.
-.
-
.
-
.
-.
-
.
-.
-.
-
.
-
.
-
.
-
.
-.
-.
-.
-.
-.
-
.
-.
-
.
-
.
-.
-
.
-.
-.
-.
-.
धूर्ताख्यान : पार्यन्तिक व्यंग्य-काव्यकथा
प्रो० डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव, सम्पादक, 'परिषद्-पत्रिका', बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना-४
व्यंग्य-काव्यकथा ग्रन्थों में 'धूर्ताख्यान' का उल्लेखनीय महत्व है। इसके रचयिता श्रमण-परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान् कथाकार आचार्य हरिभद्रसूरि (आठवी-नवीं शती) हैं। उन्होंने अपनी इस व्यंग्यप्रधान कथा-रचना में पाँच धुर्तों के आख्यानों द्वारा पुराणों में बणित असम्भव और अविश्वसनीय बातों या कथाओं का प्रति-आख्यान उपन्यस्त किया है । लाक्षणिक कथाशैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ भारतीय कथा-साहित्य में कूटस्थ है। व्यंग्य और उपहास के उपस्थापन की पुष्टि पद्धति की दृष्टि से तो इस कथा-ग्रन्थ को द्वितीयता नहीं है । कहना न होगा कि आचार्य हरिभद्र का व्यंग्य-प्रहार ध्वंस के लिए नहीं, अपितु निर्माण के लिए हुआ है।
धूर्ताख्यान" (प्रा० धुत्तक्खाण) में व्यंग्य के यथार्थ रूप का दर्शन होता है । विकृति के माध्यम से सूकृति को संकेतित या सन्देशित करना ही व्यंग्य का मूल लक्ष्य है। इसीलिए, प्रबुद्ध व्यंग्यकार प्रायः सार्वजनीन जड़ता, अज्ञानता या दुष्कृतियों के उपहास तथा भर्त्सनापूर्वक विरोध के लिए ही व्यंग्य का प्रयोग करते हैं । 'ए न्यू इंगलिश डिक्शनरी आव हिस्टोरिक्ल प्रिंसिपुल्स' (भाग ८, पृ० ११६) में कहा गया है कि पाप, जड़ता, अशिष्टता और कुरीति को प्रकाश में लाकर उनकी निन्दा और उपहास के लिए कवियों द्वारा व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है। कुरीति और अनाचार के निर्मूलन के लिए व्यंग्य अमोघ अस्त्र सिद्ध होता है।
शिप्ले ने अपने शब्दकोश 'डिक्शरी आव् वर्ल्ड लिटरेरी टर्न्स' (पृ० ४०२) में लिखा है कि मानवीय दुर्बलताओं की निन्दापूर्ण कटु आलोचना ही व्यंग्य है। इसीलिए, आचार और सौन्दर्य के भावों को उद्भावित कर सामाजिक दुर्बलता में सुधार लाना ही व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य है । यों, अन्य उपायों से भी सामाजिक दोषों का निराकरण किया जा सकता है, किन्तु व्यंग्य में निराकरण की ध्वनि और प्रविधि, रोचकता और तीक्ष्णता की दृष्टि से, कुछ भिन्न या विशिष्ट होती है।
___ 'चेम्बर्स इन्साइक्लोपीडिया' (नवीन संस्करण, जि० १२) के अनुसार, सार्वजनीन भर्त्सना के भावों में कल्पना और बुद्धिविलास के साथ ही झिड़की के भाव जब मिल जाते हैं, तभी व्यंग्य की सृष्टि होती है। सुधार की दृष्टि से किसी भी प्रकार का सामाजिक जीवन व्यंग्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र बन सकता है। सच पूछिए, तो स्वाभाविकता जब अस्वाभाविकता का परिहास करती है, तभी व्यंग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यंग्य दोषों का परिमार्जन ही नहीं करता, उनका शोधन और सुधार भी करता है । व्यंग्य से पारस्परिक कटुता या तिक्तता नहीं बढ़ती, अपितु समाज या व्यक्ति के स्वभावों का परिष्कार और संस्कार होता है। व्यंग्य गत्यात्मक और उपदेशात्मक, दोनों प्रकार का हो सकता है।
'धुर्ताखान' के उपन्यासक आचार्य हरिभद्र की दृष्टि में आक्षेप या निन्दा की अपेक्षा व्यंग्य ही एक ऐसा उत्तम साधन है, जो बिना किसी हानि के मानव की दुर्नीतियों का परिशोधन करता है। कारण है कि मनुष्य अपना उपहास नहीं सह सकता है, अत: जिन दोषों के कारण उस पर दूसरे लोग हँसते हैं, उन दोषों से वह अपने आप को मुक्त कर लेना चाहता है, परिमार्जन की इच्छा करता है । व्यंग्य उन दोषों का परिमार्जन करना चाहता है और तभी व्यंग्य कला का रूप धारण करता है। पुन: व्यंग्य जब कला के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तब वह सौन्दर्य-भावना के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org