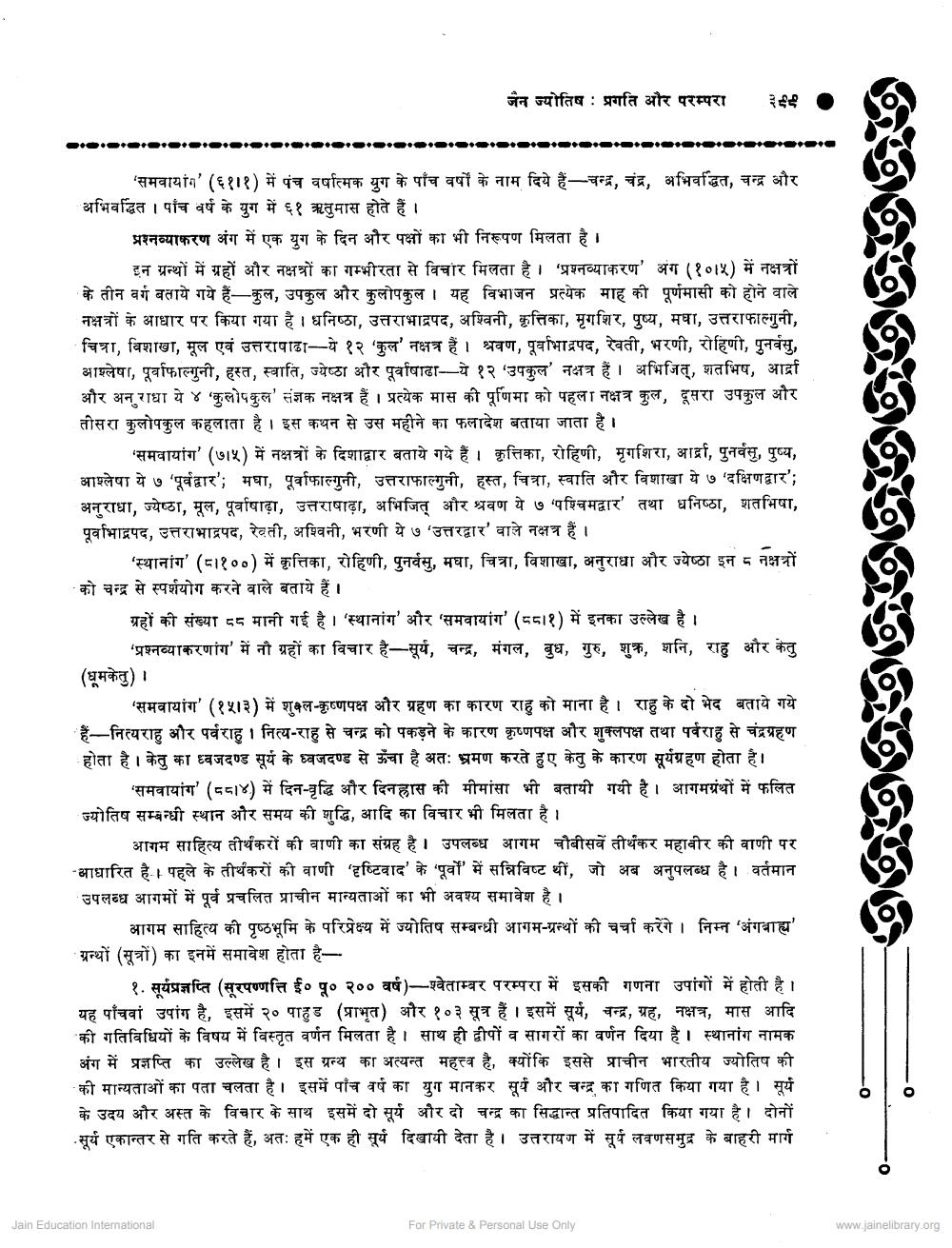________________
जैन ज्योतिष : प्रगति और परम्परा
३६५
-.-.-.-.--.-.-.-...
'समवायांग' (६१११) में पंच वर्षात्मक युग के पाँच वर्षों के नाम दिये हैं-चन्द्र, चंद्र, अभिवद्धित, चन्द्र और अभिवद्धित । पाँच वर्ष के युग में ६१ ऋतुमास होते हैं ।
प्रश्नव्याकरण अंग में एक युग के दिन और पक्षों का भी निरूपण मिलता है।
इन ग्रन्थों में ग्रहों और नक्षत्रों का गम्भीरता से विचार मिलता है। 'प्रश्नव्याकरण' अग (१०१५) में नक्षत्रों के तीन वर्ग बताये गये हैं—कुल, उपकुल और कुलोपकुल। यह विभाजन प्रत्येक माह की पूर्णमासी को होने वाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है । धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल एवं उत्तराषाढा-ये १२ 'कुल' नक्षत्र हैं। श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा और पूर्वाषाढा-ये १२ 'उपकुल' नक्षत्र हैं। अभिजित्, शतभिष, आर्द्रा और अनु राधा ये ४ 'कुलोपकुल' संज्ञक नक्षत्र हैं । प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पहला नक्षत्र कुल, दूसरा उपकुल और तीसरा कुलोपकुल कहलाता है। इस कथन से उस महीने का फलादेश बताया जाता है।
'समवायांग' (७५) में नक्षत्रों के दिशाद्वार बताये गये हैं। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा ये ७ 'पूर्वद्वार'; मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा ये ७ 'दक्षिणद्वार'; अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित् और श्रवण ये ७ 'पश्चिमद्वार' तथा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी ये ७ 'उत्तरद्वार' वाले नक्षत्र हैं।
'स्थानांग' (८।१००) में कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन ८ नक्षत्रों को चन्द्र से स्पर्शयोग करने वाले बताये हैं।
ग्रहों की संख्या ८८ मानी गई है। 'स्थानांग' और 'समवायांग' (८८१) में इनका उल्लेख है।
'प्रश्नव्याकरणांग' में नौ ग्रहों का विचार है-सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु (धूमकेतु)।
'समवायांग' (१॥३) में शुक्ल-कृष्णपक्ष और ग्रहण का कारण राहु को माना है। राहु के दो भेद बताये गये हैं-नित्यराहु और पर्वराहु । नित्य-राहु से चन्द्र को पकड़ने के कारण कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष तथा पर्वराहु से चंद्रग्रहण होता है। केतु का ध्वजदण्ड सूर्य के ध्वजदण्ड से ऊँचा है अतः भ्रमण करते हुए केतु के कारण सूर्यग्रहण होता है।
'समवायांग' (८८४) में दिन-वृद्धि और दिनह्रास की मीमांसा भी बतायी गयी है। आगमग्रंथों में फलित ज्योतिष सम्बन्धी स्थान और समय की शुद्धि, आदि का विचार भी मिलता है।
आगम साहित्य तीर्थंकरों की वाणी का संग्रह है। उपलब्ध आगम चौबीसवें तीर्थंकर महावीर की वाणी पर -आधारित है। पहले के तीर्थंकरों की वाणी 'दृष्टिवाद' के 'पूर्वो' में सन्निविष्ट थीं, जो अब अनुपलब्ध है। वर्तमान उपलब्ध आगमों में पूर्व प्रचलित प्राचीन मान्यताओं का भी अवश्य समावेश है।
आगम साहित्य की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष सम्बन्धी आगम-ग्रन्थों की चर्चा करेंगे। निम्न 'अंगबाह्य' ग्रन्थों (सूत्रों) का इनमें समावेश होता है
१. सूर्यप्रज्ञप्ति (सूरपण्णत्ति ई० पू० २०० वर्ष)-श्वेताम्बर परम्परा में इसकी गणना उपांगों में होती है। यह पाँचवां उपांग है, इसमें २० पाहुड (प्राभृत) और १०३ सूत्र हैं । इसमें सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, मास आदि की गतिविधियों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही द्वीपों व सागरों का वर्णन दिया है। स्थानांग नामक अंग में प्रज्ञप्ति का उल्लेख है। इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्त्व है, क्योंकि इससे प्राचीन भारतीय ज्योतिष की की मान्यताओं का पता चलता है। इसमें पाँच वर्ष का युग मानकर सूर्य और चन्द्र का गणित किया गया है। सूर्य के उदय और अस्त के विचार के साथ इसमें दो सूर्य और दो चन्द्र का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। दोनों सूर्य एकान्तर से गति करते हैं, अतः हमें एक ही सूर्य दिखायी देता है। उत्तरायग में सूर्य लवणसमुद्र के बाहरी मार्ग
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org