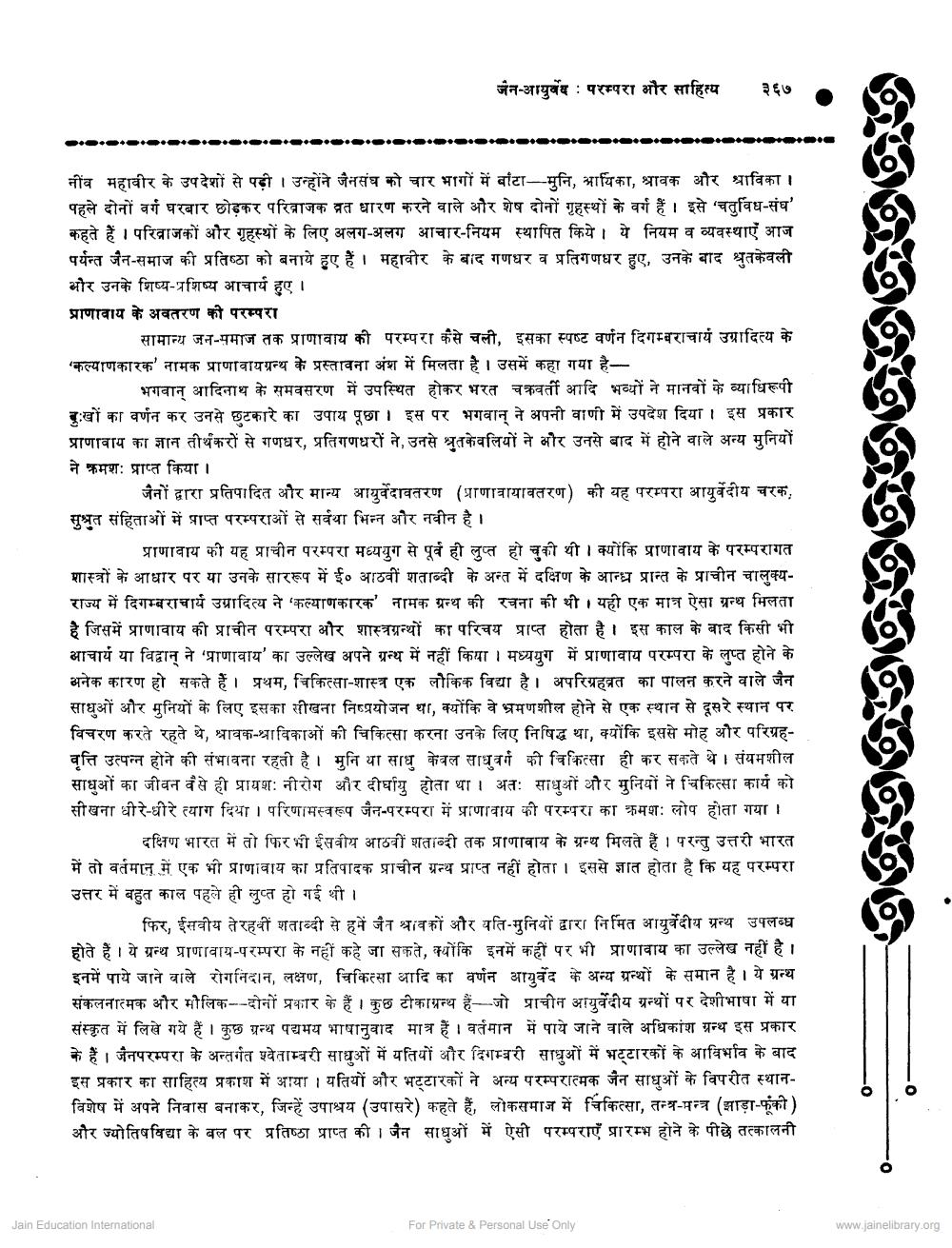________________
जैन-आयुर्वेद : परम्परा और साहित्य
३६७
नींव महावीर के उपदेशों से पड़ी । उन्होंने जनसंघ को चार भागों में बाँटा-मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविका । पहले दोनों वर्ग घरबार छोड़कर परिव्राजक व्रत धारण करने वाले और शेष दोनों गृहस्थों के वर्ग हैं। इसे 'चतुर्विध-संघ' कहते हैं । परिव्राजकों और गृहस्थों के लिए अलग-अलग आचार-नियम स्थापित किये। ये नियम व व्यवस्थाएँ आज पर्यन्त जैन-समाज की प्रतिष्ठा को बनाये हुए हैं। महावीर के बाद गणधर व प्रतिगणधर हुए, उनके बाद श्रुतकेवली भौर उनके शिष्य-प्रशिष्य आचार्य हुए। प्राणावाय के अवतरण को परम्परा
__ सामान्य जन-समाज तक प्राणावाय की परम्परा कैसे चली, इसका स्पष्ट वर्णन दिगम्बराचार्य उग्रादित्य के 'कल्याणकारक' नामक प्राणावायग्रन्थ के प्रस्तावना अंश में मिलता है । उसमें कहा गया है
भगवान् आदिनाथ के समवसरण में उपस्थित होकर भरत चक्रवर्ती आदि भव्यों ने मानवों के व्याधिरूपी दुःखों का वर्णन कर उनसे छुटकारे का उपाय पूछा। इस पर भगवान् ने अपनी वाणी में उपदेश दिया। इस प्रकार प्राणावाय का ज्ञान तीर्थंकरों से गणधर, प्रतिगणधरों ने, उनसे श्रुतकेवलियों ने और उनसे बाद में होने वाले अन्य मुनियों ने क्रमश: प्राप्त किया।
जैनों द्वारा प्रतिपादित और मान्य आयुर्वेदावतरण (प्राणाबायावतरण) की यह परम्परा आयुर्वेदीय चरक, सुश्रुत संहिताओं में प्राप्त परम्पराओं से सर्वथा भिन्न और नवीन है।
प्राणावाय की यह प्राचीन परम्परा मध्ययुग से पूर्व ही लुप्त हो चुकी थी। क्योंकि प्राणावाय के परम्परागत शास्त्रों के आधार पर या उनके साररूप में ई० आठवीं शताब्दी के अन्त में दक्षिण के आन्ध्र प्रान्त के प्राचीन चालुक्यराज्य में दिगम्बराचार्य उग्रादित्य ने 'कल्याणकारक' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यही एक मात्र ऐसा ग्रन्थ मिलता है जिसमें प्राणावाय की प्राचीन परम्परा और शास्त्रग्रन्थों का परिचय प्राप्त होता है। इस काल के बाद किसी भी आचार्य या विद्वान् ने 'प्राणावाय' का उल्लेख अपने ग्रन्थ में नहीं किया। मध्ययुग में प्राणावाय परम्परा के लुप्त होने के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रथम, चिकित्सा-शास्त्र एक लौकिक विद्या है। अपरिग्रहव्रत का पालन करने वाले जैन साधुओं और मुनियों के लिए इसका सीखना निष्प्रयोजन था, क्योंकि वे भ्रमणशील होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, श्रावक-श्राविकाओं की चिकित्सा करना उनके लिए निषिद्ध था, क्योंकि इससे मोह और परिग्रहवृत्ति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मुनि या साधु केवल साधुवर्ग की चिकित्सा ही कर सकते थे। संयमशील साधुओं का जीवन वैसे ही प्रायश: नीरोग और दीर्घायु होता था। अतः साधुओं और मुनियों ने चिकित्सा कार्य को सीखना धीरे-धीरे त्याग दिया। परिणामस्वरूप जैन-परम्परा में प्राणावाय की परम्परा का क्रमशः लोप होता गया ।
दक्षिण भारत में तो फिर भी ईसवीय आठवीं शताब्दी तक प्राणावाय के ग्रन्थ मिलते हैं । परन्तु उत्तरी भारत में तो वर्तमान में एक भी प्राणावाय का प्रतिपादक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि यह परम्परा उत्तर में बहुत काल पहले ही लुप्त हो गई थी।
फिर, ईसवीय तेरहवीं शताब्दी से हमें जैन श्रावकों और यति-मुनियों द्वारा निर्मित आयुर्वेदीय ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । ये ग्रन्थ प्राणावाय-परम्परा के नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें कहीं पर भी प्राणावाय का उल्लेख नहीं है। इनमें पाये जाने वाले रोगनिदान, लक्षण, चिकित्सा आदि का वर्णन आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों के समान है। ये ग्रन्थ संकलनात्मक और मौलिक--दोनों प्रकार के हैं। कुछ टीकाग्रन्थ हैं--जो प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों पर देशीभाषा में या संस्कृत में लिखे गये हैं। कुछ ग्रन्थ पद्यमय भाषानुवाद मात्र हैं । वर्तमान में पाये जाने वाले अधिकांश ग्रन्थ इस प्रकार के हैं। जैनपरम्परा के अन्तर्गत श्वेताम्बरी साधुओं में यतियों और दिगम्बरी साधुओं में भट्टारकों के आविर्भाव के बाद इस प्रकार का साहित्य प्रकाश में आया । यतियों और भट्टारकों ने अन्य परम्परात्मक जैन साधुओं के विपरीत स्थानविशेष में अपने निवास बनाकर, जिन्हें उपाश्रय (उपासरे) कहते हैं, लोकसमाज में चिकित्सा, तन्त्र-मन्त्र (झाड़ा-फूंकी) और ज्योतिष विद्या के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त की। जैन साधुओं में ऐसी परम्पराएँ प्रारम्भ होने के पीछे तत्कालनी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org