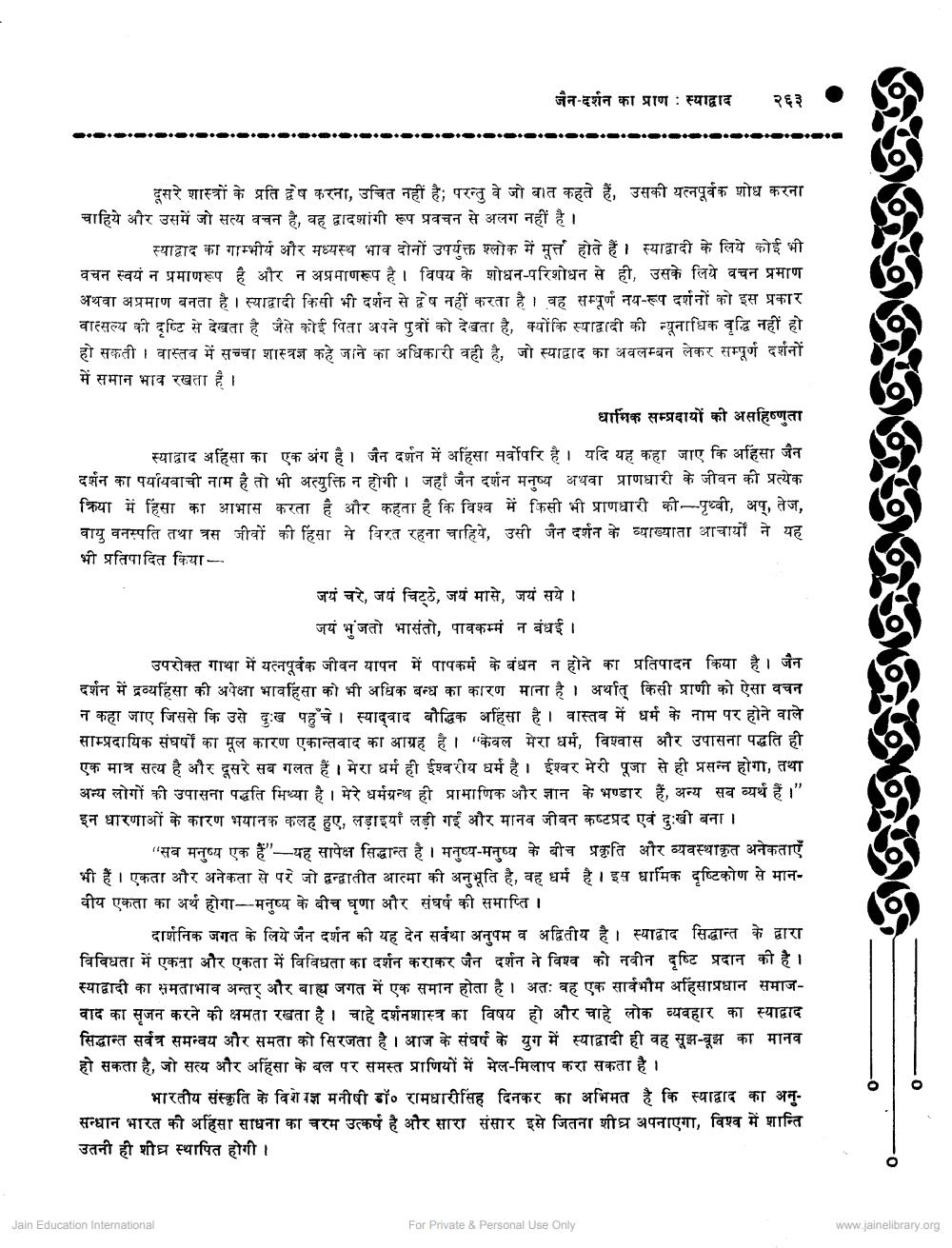________________
जैन-दर्शन का प्राण : स्याद्वाद
२६३
.
...........................................................................
दूसरे शास्त्रों के प्रति द्वेष करना, उचित नहीं है; परन्तु वे जो बात कहते हैं, उसकी यत्नपूर्वक शोध करना चाहिये और उसमें जो सत्य वचन है, वह द्वादशांगी रूप प्रवचन से अलग नहीं है।
स्याद्वाद का गाम्भीर्य और मध्यस्थ भाव दोनों उपर्युक्त श्लोक में मुर्त होते हैं। स्याद्वादी के लिये कोई भी वचन स्वयं न प्रमाणरूप है और न अप्रमाणरूप है। विषय के शोधन-परिशोधन से ही, उसके लिये वचन प्रमाण अथवा अप्रमाण बनता है। स्याद्वादी किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता है। वह सम्पूर्ण नय-रूप दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है, क्योंकि स्याद्वादी की न्यूनाधिक वृद्धि नहीं हो हो सकती। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है, जो स्याद्वाद का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है।
धार्मिक सम्प्रदायों को असहिष्णुता स्याद्वाद अहिंसा का एक अंग है। जैन दर्शन में अहिंसा सर्वोपरि है। यदि यह कहा जाए कि अहिंसा जैन दर्शन का पर्यायवाची नाम है तो भी अत्युक्ति न होगी। जहाँ जैन दर्शन मनुष्य अथवा प्राणधारी के जीवन की प्रत्येक क्रिया में हिंसा का आभास करता है और कहता है कि विश्व में किसी भी प्राणधारी की--पृथ्वी, अप, तेज, वायु वनस्पति तथा त्रस जीवों की हिंसा से विरत रहना चाहिये, उसी जैन दर्शन के व्याख्याता आचार्यों ने यह भी प्रतिपादित किया
जयं चरे, जयं चिट्टे, जयं मासे, जयं सये ।
जयं भुजतो भासंतो, पावकम्मं न बंधई। उपरोक्त गाथा में यत्नपूर्वक जीवन यापन में पापकर्म के बंधन न होने का प्रतिपादन किया है। जैन दर्शन में द्रव्यहिंसा की अपेक्षा भावहिंसा को भी अधिक बन्ध का कारण माना है। अर्थात् किसी प्राणी को ऐसा वचन न कहा जाए जिससे कि उसे दुःख पहुचे। स्याद्वाद बौद्धिक अहिंसा है। वास्तव में धर्म के नाम पर होने वाले साम्प्रदायिक संघर्षों का मूल कारण एकान्तवाद का आग्रह है। "केवल मेरा धर्म, विश्वास और उपासना पद्धति ही एक मात्र सत्य है और दूसरे सब गलत हैं। मेरा धर्म ही ईश्वरीय धर्म है। ईश्वर मेरी पूजा से ही प्रसन्न होगा, तथा अन्य लोगों की उपासना पद्धति मिथ्या है। मेरे धर्मग्रन्थ ही प्रामाणिक और ज्ञान के भण्डार हैं, अन्य सब व्यर्थ हैं।" इन धारणाओं के कारण भयानक कलह हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई और मानव जीवन कष्टप्रद एवं दुःखी बना।
“सब मनुष्य एक हैं"-यह सापेक्ष सिद्धान्त है। मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रकृति और व्यवस्थाकृत अनेकताएँ भी हैं । एकता और अनेकता से परे जो द्वन्द्वातीत आत्मा की अनुभूति है, वह धर्म है। इस धार्मिक दृष्टिकोण से मानवीय एकता का अर्थ होगा---मनुष्य के बीच घृणा और संघर्ष की समाप्ति ।
दार्शनिक जगत के लिये जैन दर्शन की यह देन सर्वथा अनुपम व अद्वितीय है। स्याद्वाद सिद्धान्त के द्वारा विविधता में एकता और एकता में विविधता का दर्शन कराकर जैन दर्शन ने विश्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है। स्याद्वादी का समताभाव अन्तर् और बाह्य जगत में एक समान होता है। अतः वह एक सार्वभौम अहिंसाप्रधान समाजवाद का सृजन करने की क्षमता रखता है। चाहे दर्शनशास्त्र का विषय हो और चाहे लोक व्यवहार का स्याद्वाद सिद्धान्त सर्वत्र समन्वय और समता को सिरजता है। आज के संघर्ष के युग में स्याद्वादी ही वह सूझ-बूझ का मानव हो सकता है, जो सत्य और अहिंसा के बल पर समस्त प्राणियों में मेल-मिलाप करा सकता है ।
भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ मनीषी डॉ. रामधारी सिंह दिनकर का अभिमत है कि स्याद्वाद का अनुसन्धान भारत की अहिंसा साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे जितना शीघ्र अपनाएगा, विश्व में शान्ति उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org