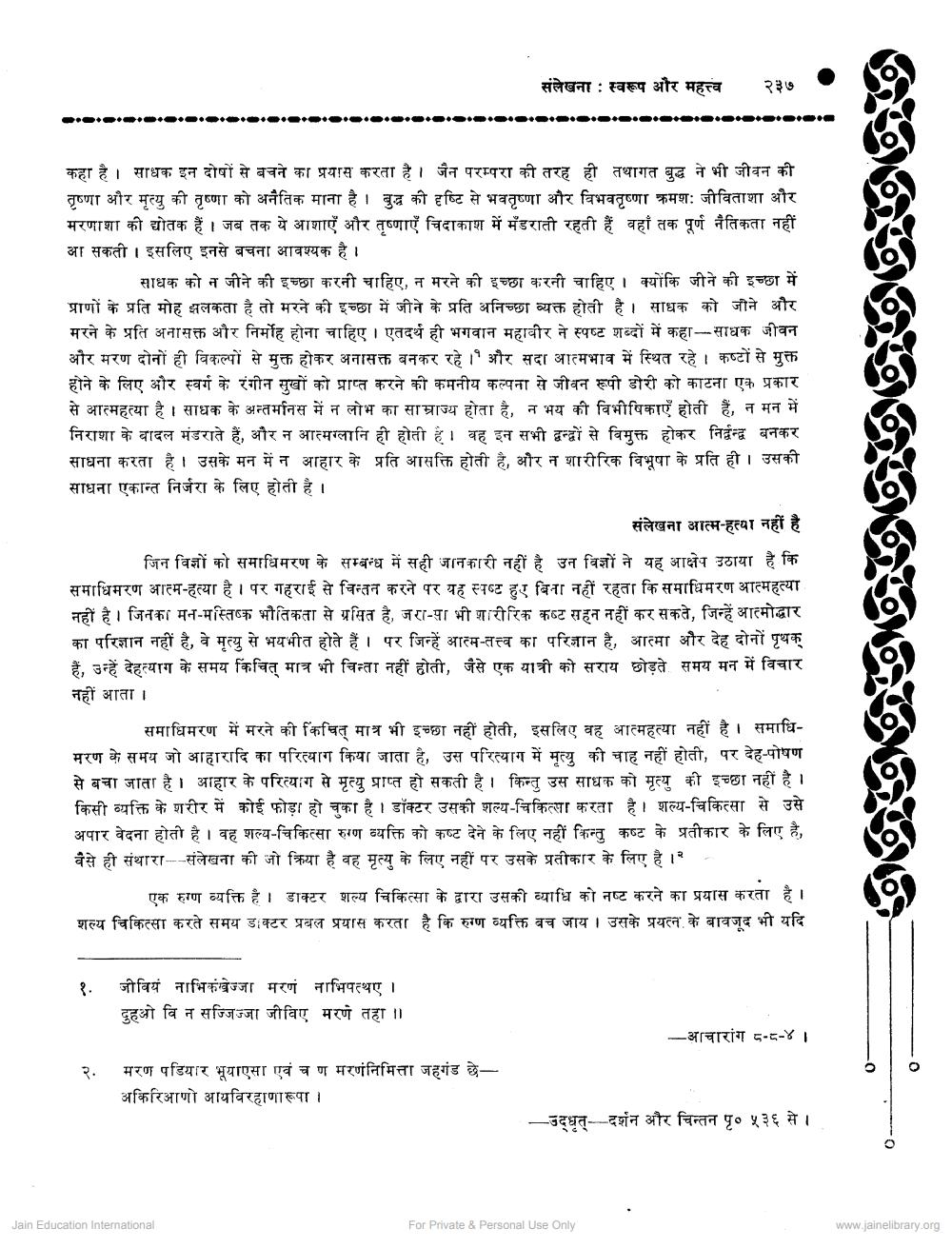________________
संलेखना : स्वरूप और महत्त्व २३७ ..........................................................................
कहा है। साधक इन दोषों से बचने का प्रयास करता है। जैन परम्परा की तरह ही तथागत बुद्ध ने भी जीवन की तृष्णा और मृत्यु की तृष्णा को अनैतिक माना है। बुद्ध की दृष्टि से भवतृष्णा और विभवतृष्णा क्रमश: जीविताशा और मरणाशा की द्योतक हैं । जब तक ये आशाएँ और तृष्णाएँ चिदाकाश में मँडराती रहती हैं बहाँ तक पूर्ण नैतिकता नहीं आ सकती। इसलिए इनसे बचना आवश्यक है।
साधक को न जीने की इच्छा करनी चाहिए, न मरने की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि जीने की इच्छा में प्राणों के प्रति मोह झलकता है तो मरने की इच्छा में जीने के प्रति अनिच्छा व्यक्त होती है। साधक को जीने और मरने के प्रति अनासक्त और निर्मोह होना चाहिए । एतदर्थ ही भगवान महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा-साधक जीवन और मरण दोनों ही विकल्पों से मुक्त होकर अनासक्त बनकर रहे ।' और सदा आत्मभाव में स्थित रहे। कष्टों से मुक्त होने के लिए और स्वर्ग के रंगीन सुखों को प्राप्त करने की कमनीय कल्पना से जीवन रूपी डोरी को काटना एक प्रकार से आत्महत्या है। साधक के अन्तर्मानस में न लोभ का साम्राज्य होता है, न भय की विभीषिकाएं होती हैं, न मन में निराशा के बादल मंडराते हैं, और न आत्मग्लानि ही होती है। वह इन सभी द्वन्द्वों से विमुक्त होकर निर्द्वन्द्व बनकर साधना करता है। उसके मन में न आहार के प्रति आसक्ति होती है, और न शारीरिक विभूषा के प्रति ही। उसकी साधना एकान्त निर्जरा के लिए होती है।
संलेखना आत्म-हत्या नहीं है जिन विज्ञों को समाधिमरण के सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं है उन विज्ञों ने यह आक्षेप उठाया है कि समाधिमरण आत्म-हत्या है। पर गहराई से चिन्तन करने पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि समाधिमर नहीं है। जिनका मन-मस्तिष्क भौतिकता से ग्रसित है, जरा-सा भी शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकते, जिन्हें आत्मोद्धार का परिज्ञान नहीं है, वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। पर जिन्हें आत्म-तत्त्व का परिज्ञान है, आत्मा और देह दोनों पृथक हैं, उन्हें देहत्याग के समय किंचित् मात्र भी चिन्ता नहीं होती, जैसे एक यात्री को सराय छोड़ते समय मन में विचार नहीं आता।
समाधिमरण में मरने की किचित् मात्र भी इच्छा नहीं होती, इसलिए वह आत्महत्या नहीं है। समाधिमरण के समय जो आहारादि का परित्याग किया जाता है, उस परित्याग में मृत्यु की चाह नहीं होती, पर देह-पोषण से बचा जाता है। आहार के परित्याग से मृत्यु प्राप्त हो सकती है। किन्तु उस साधक को मृत्यु की इच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति के शरीर में कोई फोड़ा हो चुका है। डॉक्टर उसकी शल्य-चिकित्सा करता है। शल्य-चिकित्सा से उसे अपार वेदना होती है। वह शल्य-चिकित्सा रुग्ण व्यक्ति को कष्ट देने के लिए नहीं किन्तु कष्ट के प्रतीकार के लिए है, वैसे ही संथारा--संलेखना की जो क्रिया है वह मृत्यु के लिए नहीं पर उसके प्रतीकार के लिए है ।
एक रुग्ण व्यक्ति है। डाक्टर शल्य चिकित्सा के द्वारा उसकी व्याधि को नष्ट करने का प्रयास करता है। शल्य चिकित्सा करते समय डाक्टर प्रबल प्रयास करता है कि रुग्ण व्यक्ति बच जाय । उसके प्रयत्न के बावजूद भी यदि
१. जीवियं नाभिकंखेज्जा मरणं नाभिपत्थए ।
दुहओ विन सज्जिज्जा जीविए मरण तहा।।
-आचारांग ८-८-४ ।
-
मरण पडियार भूयाएसा एवं च ण मरणंनिमित्ता जहगंड छअकिरिआणो आयविरहाणारूपा।
-उद्धत्-दर्शन और चिन्तन पृ० ५३६ से।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org