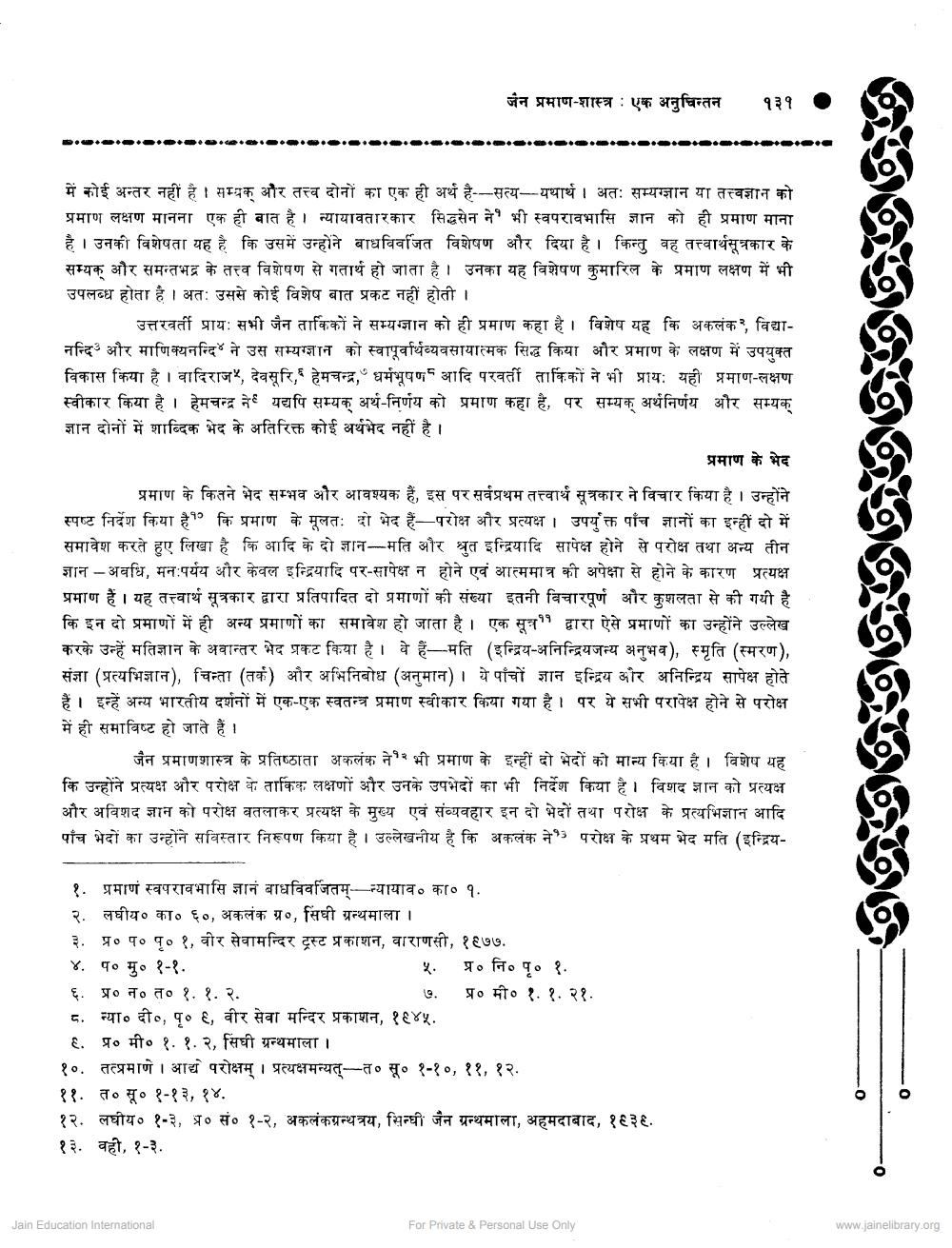________________
जैन प्रमाण-शास्त्र : एक अनुचिन्तन
१३१ .
में कोई अन्तर नहीं है । सम्यक् और तत्त्व दोनों का एक ही अर्थ है--सत्य-यथार्थ । अत: सम्यग्ज्ञान या तत्त्वज्ञान को प्रमाण लक्षण मानना एक ही बात है। न्यायावतारकार सिद्धसेन ने भी स्वपरावभासि ज्ञान को ही प्रमाण माना है । उनकी विशेषता यह है कि उसमें उन्होंने बाधविजित विशेषण और दिया है। किन्तु वह तत्त्वार्थसूत्रकार के सम्यक् और समन्तभद्र के तत्त्व विशेषण से गतार्थ हो जाता है। उनका यह विशेषण कुमारिल के प्रमाण लक्षण में भी उपलब्ध होता है । अत: उससे कोई विशेष बात प्रकट नहीं होती।
उत्तरवर्ती प्रायः सभी जैन ताकिकों ने सम्यग्ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। विशेष यह कि अकलंक, विद्यानन्दि और माणिक्यनन्दि ने उस सम्यग्ज्ञान को स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया और प्रमाण के लक्षण में उपयुक्त विकास किया है । वादिराज, देवसूरि,६ हेमचन्द्र, धर्मभूषण आदि परवर्ती ताकिकों ने भी प्राय: यही प्रमाण-लक्षण स्वीकार किया है । हेमचन्द्र ने यद्यपि सम्यक् अर्थ-निर्णय को प्रमाण कहा है, पर सम्यक् अर्थनिर्णय और सम्यक् ज्ञान दोनों में शाब्दिक भेद के अतिरिक्त कोई अर्थभेद नहीं है।
प्रमाण के भेद प्रमाण के कितने भेद सम्भव और आवश्यक हैं, इस पर सर्वप्रथम तत्त्वार्थ सूत्रकार ने विचार किया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि प्रमाण के मूलत: दो भेद हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष। उपर्युक्त पाँच ज्ञानों का इन्हीं दो में समावेश करते हुए लिखा है कि आदि के दो ज्ञान-मति और श्रुत इन्द्रियादि सापेक्ष होने से परोक्ष तथा अन्य तीन ज्ञान – अवधि, मनःपर्यय और केवल इन्द्रियादि पर-सापेक्ष न होने एवं आत्ममात्र की अपेक्षा से होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह तत्त्वार्थ सूत्रकार द्वारा प्रतिपादित दो प्रमाणों की संख्या इतनी विचारपूर्ण और कुशलता से की गयी है कि इन दो प्रमाणों में ही अन्य प्रमाणों का समावेश हो जाता है। एक सूत्र' द्वारा ऐसे प्रमाणों का उन्होंने उल्लेख करके उन्हें मतिज्ञान के अवान्तर भेद प्रकट किया है। वे हैं- मति (इन्द्रिय-अनिन्द्रियजन्य अनुभव), स्मृति (स्मरण), संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिबोध (अनुमान)। ये पांचों ज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय सापेक्ष होते हैं। इन्हें अन्य भारतीय दर्शनों में एक-एक स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया गया है। पर ये सभी परापेक्ष होने से परोक्ष में ही समाविष्ट हो जाते हैं।
जैन प्रमाणशास्त्र के प्रतिष्ठाता अकलंक ने१२ भी प्रमाण के इन्हीं दो भेदों को मान्य किया है। विशेष यह कि उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष के तार्किक लक्षणों और उनके उपभेदों का भी निर्देश किया है। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष और अविशद ज्ञान को परोक्ष बतलाकर प्रत्यक्ष के मुख्य एवं संव्यवहार इन दो भेदों तथा परोक्ष के प्रत्यभिज्ञान आदि पाँच भेदों का उन्होंने सविस्तार निरूपण किया है । उल्लेखनीय है कि अकलंक ने परोक्ष के प्रथम भेद मति (इन्द्रिय
१. प्रमाणं स्वपरावभासि ज्ञानं बाधविवजितम्-न्यायाव० का० १. २. लघीय० का० ६०, अकलंक ग्र०, सिंघी ग्रन्थमाला । ३. प्र० प० पृ० १, वीर सेवामन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, वाराणसी, १९७७. ४. प० मु० १-१. ६. प्र० न० त० १. १. २.
७. प्र० मी० १. १. २१. ८. न्या० दी०, पृ० ६, वीर सेवा मन्दिर प्रकाशन, १९४५. ६. प्र० मी० १. १.२, सिंघी ग्रन्थमाला। १०. तत्प्रमाणे । आद्य परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत्-त० सू० १-१०, ११, १२. ११. त० सू०१-१३, १४. १२. लघीय० १-३, ४० सं० १-२, अकलंकग्रन्थ त्रय, सिन्धी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, १९३६. १३. वही, १-३.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org