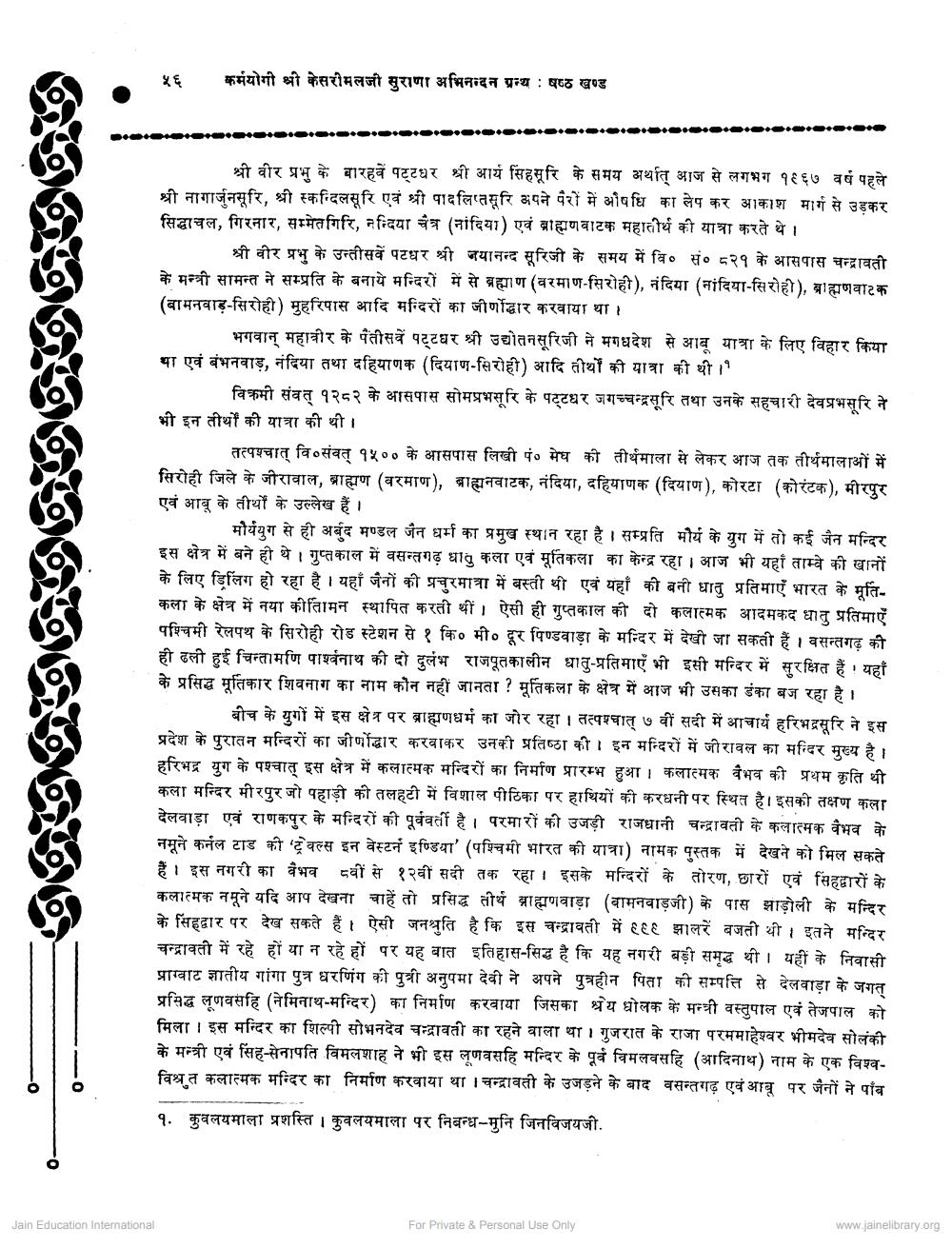________________
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठ खण्ड
श्री वीर प्रभु के बारहवें पट्टधर श्री आर्य सिंहसूरि के समय अर्थात् आज से लगभग १९६७ वर्ष पहले श्री नागार्जुनसूरि, श्री स्कन्दिलसूरि एवं श्री पादलिप्तसूरि अपने पैरों में औषधि का लेप कर आकाश मार्ग से उडकर सिद्धाचल, गिरनार, सम्मेत गिरि, नन्दिया चैत्र (नांदिया) एवं ब्राह्मणवाटक महातीर्थ की यात्रा करते थे।
श्री वीर प्रभु के उन्तीसवें पटधर श्री जयानन्द सूरिजी के समय में वि० सं० ८२१ के आसपास चन्द्रावती के मन्त्री सामन्त ने सम्प्रति के बनाये मन्दिरों में से ब्रह्माण (वरमाण-सिरोही), नंदिया (नांदिया-सिरोही), ब्राह्मणवाटक (बामनवाड़-सिरोही) मुहरिपास आदि मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया था।
भगवान महावीर के पैतीसवें पट्टधर श्री उद्योतनरिजी ने मगधदेश से आबू यात्रा के लिए विहार किया था एवं बंभनवाड़, नंदिया तथा दहियाणक (दियाण-सिरोही) आदि तीर्थों की यात्रा की थी।
विक्रमी संवत् १२८२ के आसपास सोमप्रभसूरि के पट्टधर जगच्चन्द्रसूरि तथा उनके सहचारी देवप्रभसूरि ने भी इन तीर्थों की यात्रा की थी।
तत्पश्चात् वि०संवत् १५०० के आसपास लिखी पं० मेघ की तीर्थमाला से लेकर आज तक तीर्थमालाओं में सिरोही जिले के जीरावाल, ब्राह्मण (वरमाण), ब्राह्मनवाटक, नंदिया, दहियाणक (दियाण), कोरटा (कोरंटक), मीरपुर एवं आबू के तीर्थों के उल्लेख हैं।
मौर्ययुग से ही अर्बुद मण्डल जैन धर्म का प्रमुख स्थान रहा है । सम्प्रति मौर्य के युग में तो कई जैन मन्दिर इस क्षेत्र में बने ही थे। गुप्तकाल में वसन्तगढ़ धातु कला एवं मूर्तिकला का केन्द्र रहा। आज भी यहाँ ताम्बे की खानों के लिए डिलिंग हो रहा है । यहाँ जैनों की प्रचुरमात्रा में बस्ती थी एवं यहाँ की बनी धातु प्रतिमाएं भारत के मूर्तिकला के क्षेत्र में नया कीतिगमन स्थापित करती थीं। ऐसी ही गुप्तकाल की दो कलात्मक आदमकद धातु प्रतिमाएँ पश्चिमी रेलपथ के सिरोही रोड स्टेशन से १ कि० मी० दूर पिण्डवाड़ा के मन्दिर में देखी जा सकती हैं । वसन्तगढ़ की ही ढली हुई चिन्तामणि पार्श्वनाथ की दो दुर्लभ राजपूतकालीन धातु-प्रतिमाएँ भी इसी मन्दिर में सुरक्षित हैं । यहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार शिवनाग का नाम कौन नहीं जानता? मूर्तिकला के क्षेत्र में आज भी उसका डंका बज रहा है।
बीच के युगों में इस क्षेत्र पर ब्राह्मणधर्म का जोर रहा । तत्पश्चात् ७ वीं सदी में आचार्य हरिभद्रसूरि ने इस प्रदेश के पुरातन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाकर उनकी प्रतिष्ठा की। इन मन्दिरों में जी रावल का मन्दिर मुख्य है। हरिभद्र युग के पश्चात् इस क्षेत्र में कलात्मक मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। कलात्मक वैभव की प्रथम कृति थी कला मन्दिर मीरपुर जो पहाड़ी की तलहटी में विशाल पीठिका पर हाथियों की करधनी पर स्थित है। इसकी तक्षण कला देलवाड़ा एवं राणकपुर के मन्दिरों की पूर्ववर्ती है। परमारों की उजड़ी राजधानी चन्द्रावती के कलात्मक वैभव के नमूने कर्नल टाड की 'ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इण्डिया' (पश्चिमी भारत की यात्रा) नामक पुस्तक में देखने को मिल सकते हैं। इस नगरी का वैभव ८वीं से १२वीं सदी तक रहा। इसके मन्दिरों के तोरण, छारों एवं सिंहद्वारों के कलात्मक नमूने यदि आप देखना चाहें तो प्रसिद्ध तीर्थ ब्राह्मणवाड़ा (बामनवाड़जी) के पास झाड़ोली के मन्दिर के सिंहद्वार पर देख सकते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि इस चन्द्रावती में 888 झालरें बजती थी। इतने मन्दिर चन्द्रावती में रहे हों या न रहे हों पर यह बात इतिहास-सिद्ध है कि यह नगरी बड़ी समृद्ध थी। यहीं के निवासी प्राग्वाट ज्ञातीय गांगा पुत्र धरणिंग की पुत्री अनुपमा देवी ने अपने पुत्रहीन पिता की सम्पत्ति से देलवाड़ा के जगत प्रसिद्ध लणवसहि (नेमिनाथ-मन्दिर) का निर्माण करवाया जिसका श्रेय धोलक के मन्त्री वस्तुपाल एवं तेजपाल को मिला। इस मन्दिर का शिल्पी सोभनदेव चन्द्रावती का रहने वाला था। गुजरात के राजा परममाहेश्वर भीमदेव सोलंकी के मन्त्री एवं सिंह-सेनापति विमलशाह ने भी इस लुणवसहि मन्दिर के पूर्व विमलवसहि (आदिनाथ) नाम के एक विश्वविश्रुत कलात्मक मन्दिर का निर्माण करवाया था । चन्द्रावती के उजड़ने के बाद वसन्तगढ़ एवं आबू पर जैनों ने पाँव
-०
१. कुवलयमाला प्रशस्ति । कुवलयमाला पर निबन्ध-मुनि जिनविजयजी.
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International