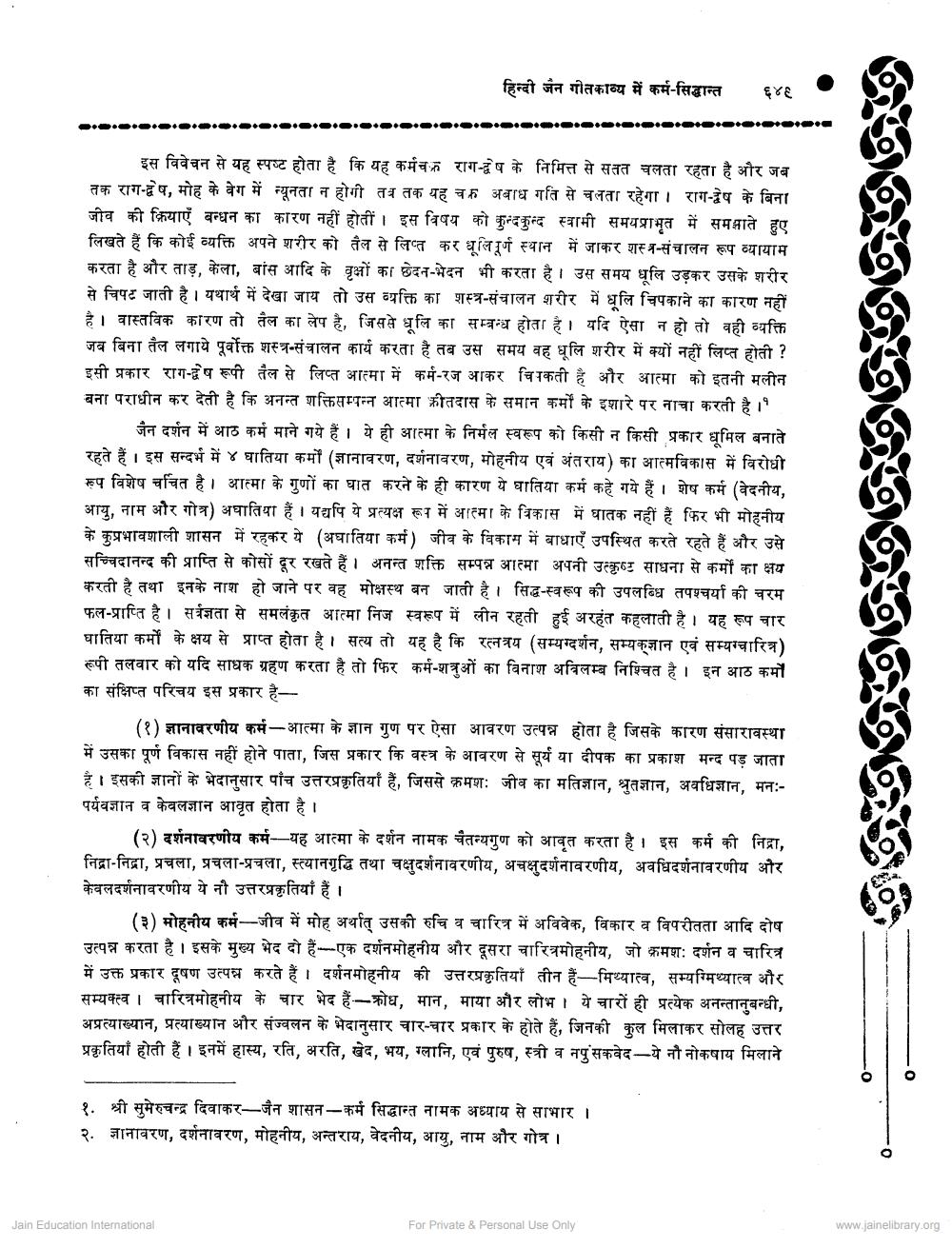________________
हिन्दी जैन गीतकाव्य में कर्म-सिद्धान्त
इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह कर्मचक्र राग-द्वेष के निमित्त से सतत चलता रहता है और जब तक राग-द्वेष, मोह के वेग में न्यूनता न होगी तब तक यह चक्र अबाध गति से चलता रहेगा। राग-द्वेष के बिना जीव की क्रियाएँ बन्धन का कारण नहीं होतीं। इस विषय को कुन्दकुन्द स्वामी समयप्राभृत में समझाते हुए लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को तैल से लिप्त कर धूलिपूर्ण स्थान में जाकर शस्त्र-संचालन रूप व्यायाम करता है और ताड़, केला, बांस आदि के वृक्षों का छेदन-भेदन भी करता है। उस समय धूलि उड़कर उसके शरीर से चिपट जाती है । यथार्थ में देखा जाय तो उस व्यक्ति का शस्त्र-संचालन शरीर में धूलि चिपकाने का कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो तैल का लेप है, जिससे धूलि का सम्बन्ध होता है। यदि ऐसा न हो तो वही व्यक्ति जब बिना तैल लगाये पूर्वोक्त शस्त्र-संचालन कार्य करता है तब उस समय वह धूलि शरीर में क्यों नहीं लिप्त होती? इसी प्रकार राग-द्वेष रूपी तैल से लिप्त आत्मा में कर्म-रज आकर चिपकती है और आत्मा को इतनी मलीन बना पराधीन कर देती है कि अनन्त शक्तिसम्पन्न आत्मा क्रीतदास के समान कर्मों के इशारे पर नाचा करती है।'
जैन दर्शन में आठ कर्म माने गये हैं। ये ही आत्मा के निर्मल स्वरूप को किसी न किसी प्रकार धूमिल बनाते रहते हैं । इस सन्दर्भ में ४ घातिया कर्मों (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय एवं अंतराय) का आत्मविकास में विरोधी रूप विशेष चर्चित है। आत्मा के गुणों का घात करने के ही कारण ये घातिया कर्म कहे गये हैं। शेष कर्म (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) अघातिया हैं । यद्यपि ये प्रत्यक्ष रूप में आत्मा के विकास में घातक नहीं हैं फिर भी मोहनीय के कुप्रभावशाली शासन में रहकर ये (अघातिया कर्म) जीव के विकास में बाधाएँ उपस्थित करते रहते हैं और उसे सच्चिदानन्द की प्राप्ति से कोसों दूर रखते हैं। अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा अपनी उत्कृष्ट साधना से कर्मों का क्षय करती है तथा इनके नाश हो जाने पर वह मोक्षस्थ बन जाती है। सिद्ध-स्वरूप की उपलब्धि तपश्चर्या की चरम फल-प्राप्ति है। सर्वज्ञता से समलंकृत आत्मा निज स्वरूप में लीन रहती हुई अरहंत कहलाती है। यह रूप चार घातिया कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है। सत्य तो यह है कि रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान एवं सम्यग्चारित्र) रूपी तलवार को यदि साधक ग्रहण करता है तो फिर कर्म-शत्रुओं का विनाश अविलम्ब निश्चित है। इन आठ कर्मों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है
(१) ज्ञानावरणीय कर्म-आत्मा के ज्ञान गुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न होता है जिसके कारण संसारावस्था में उसका पूर्ण विकास नहीं होने पाता, जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण से सूर्य या दीपक का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। इसकी ज्ञानों के भेदानुसार पाँच उत्तरप्रकृतियाँ हैं, जिससे क्रमश: जीव का मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्यवज्ञान व केवलज्ञान आवृत होता है।
(२) दर्शनावरणीय कर्म-यह आत्मा के दर्शन नामक चैतन्यगुण को आवृत करता है। इस कर्म की निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय ये नौ उत्तरप्रकृतियां हैं।
(३) मोहनीय कर्म-जीव में मोह अर्थात् उसकी रुचि व चारित्र में अविवेक, विकार व विपरीतता आदि दोष उत्पन्न करता है । इसके मुख्य भेद दो हैं---एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय, जो क्रमश: दर्शन व चारित्र में उक्त प्रकार दूषण उत्पन्न करते हैं। दर्शनमोहनीय की उत्तरप्रकृतियाँ तीन हैं-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व । चारित्रमोहनीय के चार भेद हैं-क्रोध, मान, माया और लोभ । ये चारों ही प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेदानुसार चार-चार प्रकार के होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर सोलह उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। इनमें हास्य, रति, अरति, खेद, भय, ग्लानि, एवं पुरुष, स्त्री व नपुंसकवेद-ये नौ नोकषाय मिलाने
१. श्री सुमेरुचन्द्र दिवाकर-जैन शासन-कर्म सिद्धान्त नामक अध्याय से साभार । २. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org