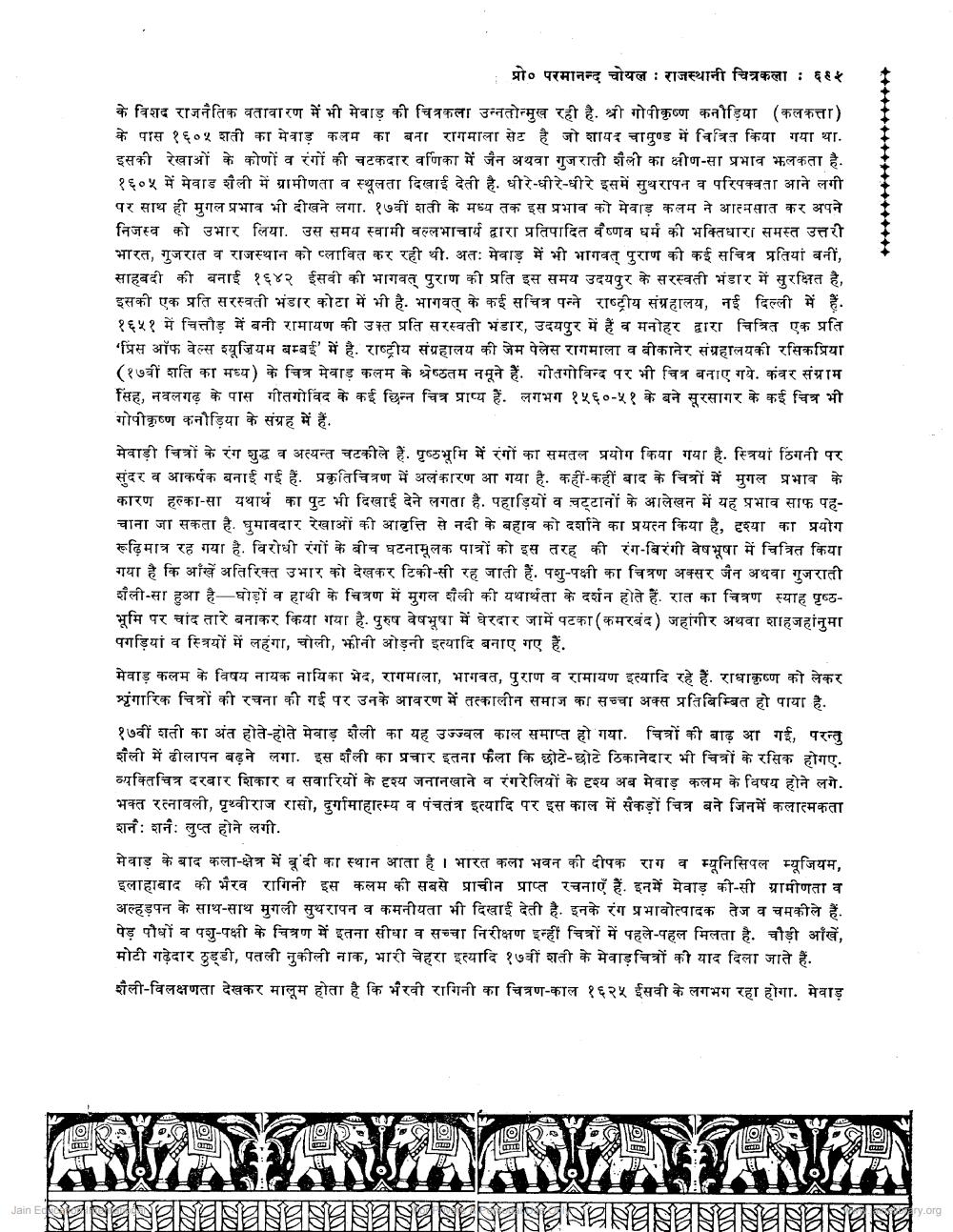________________
। प्रो० परमानन्द चोयल : राजस्थानी चित्रकला : ६६५
के विशद राजनैतिक वतावारण में भी मेवाड़ की चित्रकला उन्नतोन्मुख रही है. श्री गोपीकृष्ण कनौड़िया (कलकत्ता) के पास १६०५ शती का मेवाड़ कलम का बना रागमाला सेट है जो शायद चामुण्ड में चित्रित किया गया था. इसकी रेखाओं के कोणों व रंगों की चटकदार वणिका में जैन अथवा गुजराती शैली का क्षीण-सा प्रभाव झलकता है. १६०५ में मेवाड शैली में ग्रामीणता व स्थूलता दिखाई देती है. धीरे-धीरे-धीरे इसमें सुथरापन व परिपक्वता आने लगी पर साथ ही मुगल प्रभाव भी दीखने लगा. १७वीं शती के मध्य तक इस प्रभाव को मेवाड़ कलम ने आत्मसात कर अपने निजस्व को उभार लिया. उस समय स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म की भक्तिधारा समस्त उत्तरी भारत, गुजरात व राजस्थान को प्लावित कर रही थी. अतः मेवाड़ में भी भागवत् पुराण की कई सचित्र प्रतियां बनीं, साहबदी की बनाई १६४२ ईसवी की भागवत पुराण की प्रति इस समय उदयपुर के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है, इसकी एक प्रति सरस्वती भंडार कोटा में भी है. भागवत् के कई सचित्र पन्ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में हैं. १६५१ में चित्तौड़ में बनी रामायण की उक्त प्रति सरस्वती भंडार, उदयपुर में हैं व मनोहर द्वारा चित्रित एक प्रति 'प्रिंस ऑफ वेल्स श्यूजियम बम्बई' में है. राष्ट्रीय संग्रहालय की जेम पेलेस रागमाला व बीकानेर संग्रहालयकी रसिकप्रिया (१७वीं शति का मध्य) के चित्र मेवाड़ कलम के श्रेष्ठतम नमूने हैं. गीतगोविन्द पर भी चित्र बनाए गये. कंवर संग्राम सिंह, नवलगढ़ के पास गीतगोविंद के कई छिन्न चित्र प्राप्य हैं. लगभग १५६०-५१ के बने सूरसागर के कई चित्र भी गोपीकृष्ण कनौड़िया के संग्रह में हैं. मेवाड़ी चित्रों के रंग शुद्ध व अत्यन्त चटकीले हैं. पृष्ठभूमि में रंगों का समतल प्रयोग किया गया है. स्त्रियां ठिंगनी पर सुंदर व आकर्षक बनाई गई हैं. प्रकृतिचित्रण में अलंकारण आ गया है. कहीं-कहीं बाद के चित्रों में मुगल प्रभाव के कारण हल्का-सा यथार्थ का पुट भी दिखाई देने लगता है. पहाड़ियों व चट्टानों के आलेखन में यह प्रभाव साफ पहचाना जा सकता है. घुमावदार रेखाओं की आवृत्ति से नदी के बहाव को दर्शाने का प्रयत्न किया है, दृश्या का प्रयोग रूढ़ि मात्र रह गया है. विरोधी रंगों के बीच घटनामूलक पात्रों को इस तरह की रंग-बिरंगी वेषभूषा में चित्रित किया गया है कि आँखें अतिरिक्त उभार को देखकर टिकी-सी रह जाती हैं. पशु-पक्षी का चित्रण अक्सर जैन अथवा गुजराती शैली-सा हुआ है—घोड़ों व हाथी के चित्रण में मुगल शैली की यथार्थता के दर्शन होते हैं. रात का चित्रण स्याह पृष्ठभूमि पर चांद तारे बनाकर किया गया है. पुरुष वेषभूषा में घेरदार जामें पटका (कमरबंद) जहांगीर अथवा शाहजहांनुमा पगड़ियां व स्त्रियों में लहंगा, चोली, झीनी ओड़नी इत्यादि बनाए गए हैं. मेवाड़ कलम के विषय नायक नायिका भेद, रागमाला, भागवत, पुराण व रामायण इत्यादि रहे हैं. राधाकृष्ण को लेकर शृंगारिक चित्रों की रचना की गई पर उनके आवरण में तत्कालीन समाज का सच्चा अक्स प्रतिबिम्बित हो पाया है. १७वीं शती का अंत होते-होते मेवाड़ शैली का यह उज्ज्वल काल समाप्त हो गया. चित्रों की बाढ़ आ गई, परन्तु शैली में ढीलापन बढ़ने लगा. इस शैली का प्रचार इतना फैला कि छोटे-छोटे ठिकानेदार भी चित्रों के रसिक होगए. व्यक्तिचित्र दरबार शिकार व सवारियों के दृश्य जनानखाने व रंगरेलियों के दृश्य अब मेवाड़ कलम के विषय होने लगे. भक्त रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, दुर्गामाहात्म्य व पंचतंत्र इत्यादि पर इस काल में सैकड़ों चित्र बने जिनमें कलात्मकता शनैः शनैः लुप्त होने लगी. मेवाड़ के बाद कला-क्षेत्र में बूदी का स्थान आता है । भारत कला भवन की दीपक राग व म्यूनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद की भैरव रागिनी इस कलम की सबसे प्राचीन प्राप्त रचनाएँ हैं. इनमें मेवाड़ की-सी ग्रामीणता व अल्हड़पन के साथ-साथ मुगली सुथरापन व कमनीयता भी दिखाई देती है. इनके रंग प्रभावोत्पादक तेज व चमकीले हैं. पेड़ पौधों व पशु-पक्षी के चित्रण में इतना सीधा व सच्चा निरीक्षण इन्हीं चित्रों में पहले-पहल मिलता है. चौड़ी आँखें, मोटी गढ़ेदार ठुड्डी, पतली नुकीली नाक, भारी चेहरा इत्यादि १७वीं शती के मेवाड़चित्रों की याद दिला जाते हैं. शैली-विलक्षणता देखकर मालूम होता है कि भैरवी रागिनी का चित्रण-काल १६२५ ईसवी के लगभग रहा होगा. मेवाड़
-
REA
ALERS
FOR
PASEKA
danNINबनवानावाचवावाबाबवावाNININRNaray