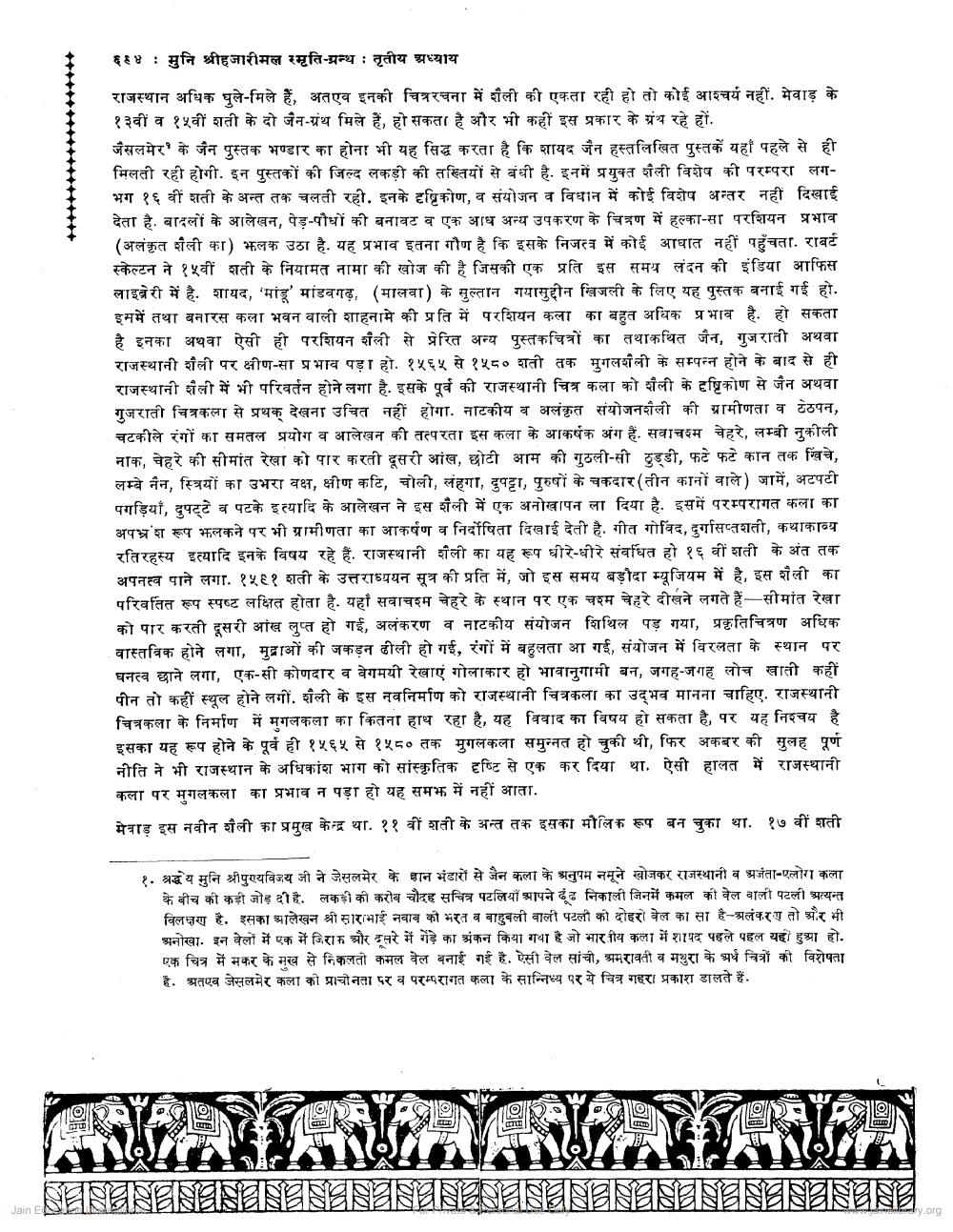________________
६६४ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : तृतीय अध्याय
राजस्थान अधिक घुले-मिले हैं, अतएव इनकी चित्ररचना में शैली की एकता रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं. मेवाड़ के १३वीं व १५वीं शती के दो जैन-ग्रंथ मिले हैं, हो सकता है और भी कहीं इस प्रकार के ग्रंथ रहे हों. जैसलमेर के जैन पुस्तक भण्डार का होना भी यह सिद्ध करता है कि शायद जैन हस्तलिखित पुस्तकें यहाँ पहले से ही मिलती रही होगी. इन पुस्तकों की जिल्द लकड़ी की तख्तियों से बंधी है. इनमें प्रयुक्त शैली विशेष की परम्परा लगभग १६ वीं शती के अन्त तक चलती रही. इनके दृष्टिकोण, व संयोजन व विधान में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता है. बादलों के आलेखन, पेड़-पौधों की बनावट व एक आध अन्य उपकरण के चित्रण में हल्का-सा परशियन प्रभाव (अलंकृत शैली का) झलक उठा है. यह प्रभाव इतना गौण है कि इसके निजत्व में कोई आघात नहीं पहुँचता. राबर्ट स्केल्टन ने १५वीं शती के नियामत नामा की खोज की है जिसकी एक प्रति इस समय लंदन की इंडिया आफिस लाइब्रेरी में है. शायद, 'मांडू' मांडवगढ़, (मालवा) के सुल्तान गयासुद्दीन खिजली के लिए यह पुस्तक बनाई गई हो. इममें तथा बनारस कला भवन वाली शाहनामे की प्रति में परशियन कला का बहुत अधिक प्रभाव है. हो सकता है इनका अथवा ऐसी ही परशियन शैली से प्रेरित अन्य पुस्तकचित्रों का तथाकथित जैन, गुजराती अथवा राजस्थानी शैली पर क्षीण-सा प्रभाव पड़ा हो. १५६५ से १५८० शती तक मुगलशैली के सम्पन्न होने के बाद से ही राजस्थानी शैली में भी परिवर्तन होने लगा है. इसके पूर्व की राजस्थानी चित्र कला को शैली के दृष्टिकोण से जैन अथवा गुजराती चित्रकला से प्रथक् देखना उचित नहीं होगा. नाटकीय व अलंकृत संयोजनशैली की ग्रामीणता व ठेठपन, चटकीले रंगों का समतल प्रयोग व आलेखन की तत्परता इस कला के आकर्षक अंग हैं. सवाचश्म चेहरे, लम्बी नुकीली नाक, चेहरे की सीमांत रेखा को पार करती दूसरी आंख, छोटी आम की गुठली-सी ठुड्डी, फटे फटे कान तक खिचे, लम्बे नैन, स्त्रियों का उभरा वक्ष, क्षीण कटि, चोली, लंहगा, दुपट्टा, पुरुषों के चकदार (तीन कानों वाले) जामें, अटपटी पगड़ियाँ, दुपट्टे व पटके इत्यादि के आलेखन ने इस शैली में एक अनोखापन ला दिया है. इसमें परम्परागत कला का अपभ्रंश रूप झलकने पर भी ग्रामीणता का आकर्षण व निर्दोषिता दिखाई देती है. गीत गोविंद, दुर्गासप्तशती, कथाकाव्य रतिरहस्य इत्यादि इनके विषय रहे हैं. राजस्थानी शैली का यह रूप धीरे-धीरे संवर्धित हो १६ वीं शती के अंत तक अपनत्व पाने लगा. १५९१ शती के उत्तराध्ययन सूत्र की प्रति में, जो इस समय बड़ौदा म्यूजियम में है, इस शैली का परिवर्तित रूप स्पष्ट लक्षित होता है. यहाँ सवाचश्म चेहरे के स्थान पर एक चश्म चेहरे दीखने लगते हैं.–सीमांत रेखा को पार करती दूसरी आंख लुप्त हो गई, अलंकरण व नाटकीय संयोजन शिथिल पड़ गया, प्रकृतिचित्रण अधिक वास्तविक होने लगा, मुद्राओं की जकड़न ढीली हो गई, रंगों में बहुलता आ गई, संयोजन में विरलता के स्थान पर घनत्व छाने लगा, एक-सी कोणदार व वेगमयी रेखाएं गोलाकार हो भावानुगामी बन, जगह-जगह लोच खाती कहीं पीन तो कहीं स्थूल होने लगी. शैली के इस नवनिर्माण को राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानना चाहिए. राजस्थानी चित्रकला के निर्माण में मुगलकला का कितना हाथ रहा है, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर यह निश्चय है इसका यह रूप होने के पूर्व ही १५६५ से १५८० तक मुगलकला समुन्नत हो चुकी थी, फिर अकबर की सुलह पूर्ण नीति ने भी राजस्थान के अधिकांश भाग को सांस्कृतिक दृष्टि से एक कर दिया था. ऐसी हालत में राजस्थानी कला पर मुगलकला का प्रभाव न पड़ा हो यह समझ में नहीं आता. मेवाड़ इस नवीन शैली का प्रमुख केन्द्र था. ११ वीं शती के अन्त तक इसका मौलिक रूप बन चुका था. १७ वीं शती
१. श्रद्धय मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने जेसलमेर के ज्ञान भंडारों से जैन कला के अनुपम नमूने खोजकर राजस्थानी व अजंता-एलोग कला
के बीच की कड़ी जोड़ दी है. लकड़ी की करीब चौदह सचित्र पटलियाँ आपने ढूंढ निकाली जिनमें कमल की वेल वाली पटली अत्यन्त विलक्षण है, इसका आलेखन श्री साराभाई नवाब की भरत व बाहुबली वाली पटली की दोहरो वेल का सा है-अलंकरण तो और भी अनोखा. इन वेलों में एक में जिराक और दूसरे में गेंड़े का अंकन किया गया है जो भारतीय कला में शायद पहले पहल यही हुआ हो. एक चित्र में मकर के मुख से निकलतो कमल वेल बनाई गई है. ऐसी वेल सांची, अमरावती व मथुरा के अर्ध चित्रों की विशेषता है. अतएव जेसलमेर कला को प्राचीनता पर व परम्परागत कला के सान्निध्य पर ये चित्र गहरा प्रकाश डालते हैं.
DU
AMPANDHAN MANARDANA
SHSANANINIRANASININEVASINERININISANOSOSE
Jain EN
Morely.org