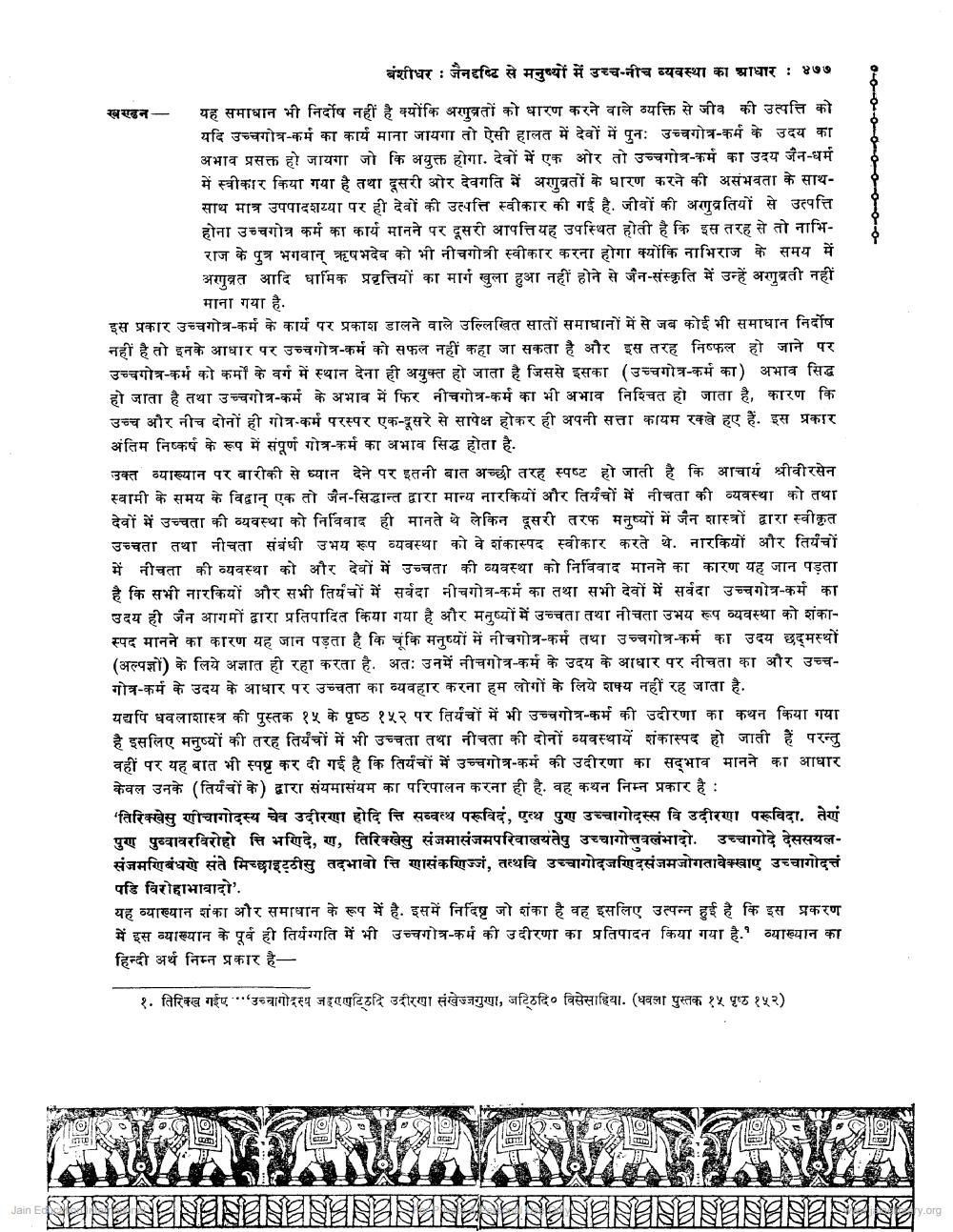________________
बंशीधर : जैनदृष्टि से मनुष्यों में उच्च-नीच व्यवस्था का प्राधार : ४७७
खरहन
0-0--0--0-0-0-0--0--0--0
यह समाधान भी निर्दोष नहीं है क्योंकि अणुव्रतों को धारण करने वाले व्यक्ति से जीव की उत्पत्ति को यदि उच्चगोत्र-कर्म का कार्य माना जायगा तो ऐसी हालत में देवों में पुन: उच्चगोत्र-कर्म के उदय का अभाव प्रसक्त हो जायगा जो कि अयुक्त होगा. देवों में एक ओर तो उच्चगोत्र-कर्म का उदय जैन-धर्म में स्वीकार किया गया है तथा दूसरी ओर देवगति में अणुव्रतों के धारण करने की असंभवता के साथसाथ मात्र उपपादशय्या पर ही देवों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है. जीवों की अणुव्रतियों से उत्पत्ति होना उच्चगोत्र कर्म का कार्य मानने पर दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि इस तरह से तो नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव को भी नीचगोत्री स्वीकार करना होगा क्योंकि नाभिराज के समय में अणुव्रत आदि धार्मिक प्रवृत्तियों का मार्ग खुला हुआ नहीं होने से जैन-संस्कृति में उन्हें अणुव्रती नहीं
माना गया है. इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्म के कार्य पर प्रकाश डालने वाले उल्लिखित सातों समाधानों में से जब कोई भी समाधान निर्दोष नहीं है तो इनके आधार पर उच्चगोत्र-कर्म को सफल नहीं कहा जा सकता है और इस तरह निष्फल हो जाने पर उच्चगोत्र-कर्म को कर्मों के वर्ग में स्थान देना ही अयुक्त हो जाता है जिससे इसका (उच्चगोत्र-कर्म का) अभाव सिद्ध हो जाता है तथा उच्चगोत्र-कर्म के अभाव में फिर नीचगोत्र-कर्म का भी अभाव निश्चित हो जाता है, कारण कि उच्च और नीच दोनों ही गोत्र-कर्म परस्पर एक-दूसरे से सापेक्ष होकर ही अपनी सत्ता कायम रक्खे हए हैं. इस प्रकार अंतिम निष्कर्ष के रूप में संपूर्ण गोत्र-कर्म का अभाव सिद्ध होता है. उक्त व्याख्यान पर बारीकी से ध्यान देने पर इतनी बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के समय के विद्वान् एक तो जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य नारकियों और तिर्यंचों में नीचता की व्यवस्था को तथा देवों में उच्चता की व्यवस्था को निर्विवाद ही मानते थे लेकिन दूसरी तरफ मनुष्यों में जैन शास्त्रों द्वारा स्वीकृत उच्चता तथा नीचता संबंधी उभय रूप व्यवस्था को वे शंकास्पद स्वीकार करते थे. नारकियों और तिर्यंचों में नीचता की व्यवस्था को और देवों में उच्चता की व्यवस्था को निर्विवाद मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सभी नारकियों और सभी तिर्य चों में सर्वदा नीचगोत्र-कर्म का तथा सभी देवों में सर्वदा उच्चगोत्र-कर्म का उदय ही जैन आगमों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और मनुष्यों में उच्चता तथा नीचता उभय रूप व्यवस्था को शंकास्पद मानने का कारण यह जान पड़ता है कि चूंकि मनुष्यों में नीचगोत्र-कर्म तथा उच्चगोत्र-कर्म का उदय छद्मस्थों (अल्पज्ञों) के लिये अज्ञात ही रहा करता है. अतः उनमें नीचगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीचता का और उच्चगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर उच्चता का व्यवहार करना हम लोगों के लिये शक्य नहीं रह जाता है. यद्यपि धवलाशास्त्र की पुस्तक १५ के पृष्ठ १५२ पर तिर्यचों में भी उच्चगोत्र-कर्म की उदीरणा का कथन किया गया है इसलिए मनुष्यों की तरह तिर्यंचों में भी उच्चता तथा नीचता की दोनों व्यवस्थायें शंकास्पद हो जाती हैं परन्तु वहीं पर यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि तिर्यंचों में उच्चगोत्र-कर्म की उदीरणा का सद्भाव मानने का आधार केवल उनके (तियंचों के) द्वारा संयमासंयम का परिपालन करना ही है. वह कथन निम्न प्रकार है : 'तिरिक्खेसु णीचागोदस्य चेव उदीरणा होदि त्ति सव्वस्थ परूविदं, एत्थ पुण उच्चागोदस्स वि उदीरणा परूविदा. तेणं पुण पुब्वावरविरोहो ति भणिदे, ण, तिरिक्खेसु संजमासंजमपरिवालयतेषु उच्चागोत्तवलंभादो. उच्चागोदे देससयलसंजमणिबंधणे संते मिच्छाइट्ठीसु तदभावो त्ति णासंकणिज्जं, तत्थवि उच्चागोदजणिदसंजमजोगतावेक्खाए उच्चागोदत्तं पडि विरोहाभावादो'. यह व्याख्यान शंका और समाधान के रूप में है. इसमें निर्दिष्ट जो शंका है वह इसलिए उत्पन्न हुई है कि इस प्रकरण में इस व्याख्यान के पूर्व ही तिर्यग्गति में भी उच्चगोत्र-कर्म की उदीरणा का प्रतिपादन किया गया है.' व्याख्यान का हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है
१. तिरिक्ख गईए "उच्चागोदस्थ जइएपढिदि उदीरणा संखेज्जगुणा, जििद० विसेसाहिया. (धवला पुस्तक १५ पृष्ठ १५२)
WER SPATI
Jan INDINANINNAININENENINEANININNINorg