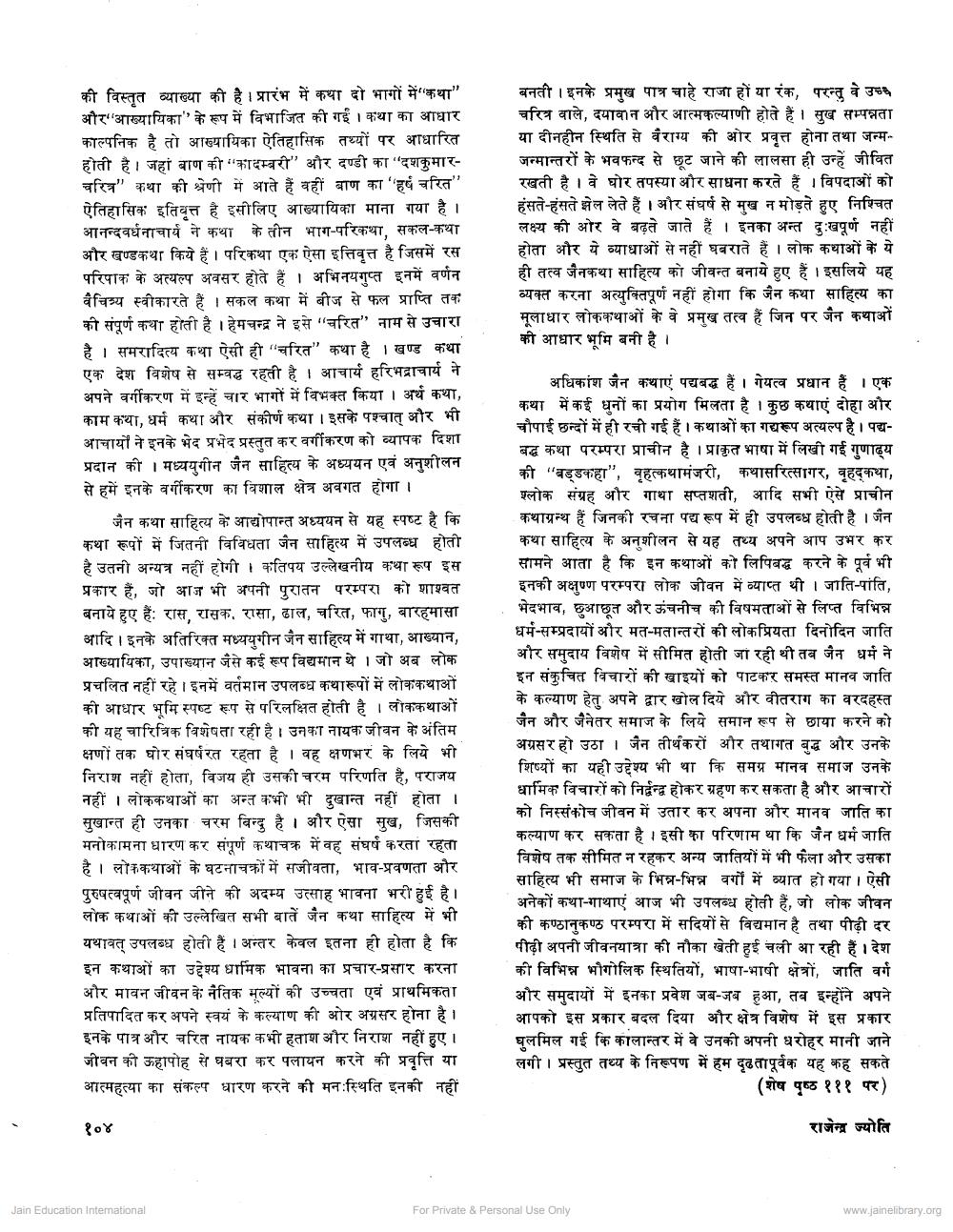________________
बनती । इनके प्रमुख पात्र चाहे राजा हों या रंक, परन्तु वे उच्च चरित्र वाले, दयावान और आत्मकल्याणी होते हैं। सुख सम्पन्नता या दीनहीन स्थिति से वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना तथा जन्मजन्मान्तरों के भवफन्द से छूट जाने की लालसा ही उन्हें जीवित रखती है । वे घोर तपस्या और साधना करते हैं । विपदाओं को हंसते-हंसते झेल लेते हैं । और संघर्ष से मुख न मोड़ते हुए निश्चित लक्ष्य की ओर वे बढ़ते जाते हैं । इनका अन्त दु:खपूर्ण नहीं होता और ये व्याधाओं से नहीं घबराते हैं । लोक कथाओं के ये ही तत्व जैनकथा साहित्य को जीवन्त बनाये हुए हैं । इसलिये यह व्यक्त करना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जैन कथा साहित्य का मूलाधार लोककथाओं के वे प्रमुख तत्व हैं जिन पर जैन कथाओं की आधार भूमि बनी है।
की विस्तृत व्याख्या की है। प्रारंभ में कथा दो भागों में 'कथा" और 'आख्यायिका' के रूप में विभाजित की गई। कथा का आधार काल्पनिक है तो आख्यायिका ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। जहां बाण की "कादम्बरी' और दण्डी का "दशकुमारचरित्र" कथा की श्रेणी में आते हैं वहीं बाण का 'हर्ष चरित' ऐतिहासिक इतिवृत्त है इसीलिए आख्यायिका माना गया है । आनन्दवर्धनाचार्य ने कथा के तीन भाग-परिकथा, सकल-कथा और खण्डकथा किये हैं। परिकथा एक ऐसा इत्तिवृत्त है जिसमें रस परिपाक के अत्यल्प अवसर होते हैं । अभिनयगुप्त इनमें वर्णन वैचित्र्य स्वीकारते हैं । सकल कथा में बीज से फल प्राप्ति तक की संपूर्ण कथा होती है । हेमचन्द्र ने इसे "चरित" नाम से उचारा है । समरादित्य कथा ऐसी ही "चरित" कथा है । खण्ड कथा एक देश विशेष से सम्बद्ध रहती है । आचार्य हरिभद्राचार्य ने अपने वर्गीकरण में इन्हें चार भागों में विभक्त किया । अर्थ कथा, काम कथा, धर्म कथा और संकीर्ण कथा । इसके पश्चात् और भी आचार्यों ने इनके भेद प्रभेद प्रस्तुत कर वर्गीकरण को व्यापक दिशा प्रदान की । मध्ययुगीन जैन साहित्य के अध्ययन एवं अनुशीलन से हमें इनके वर्गीकरण का विशाल क्षेत्र अवगत होगा। ___ जैन कथा साहित्य के आद्योपान्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कथा रूपों में जितनी विविधता जैन साहित्य में उपलब्ध होती है उतनी अन्यत्र नहीं होगी । कतिपय उल्लेखनीय कथा रूप इस प्रकार हैं, जो आज भी अपनी पुरातन परम्परा को शाश्वत बनाये हुए हैं: रास, रासक. रासा, ढाल, चरित, फागु, बारहमासा आदि । इनके अतिरिक्त मध्ययुगीन जैन साहित्य में गाथा, आख्यान, आख्यायिका, उपाख्यान जैसे कई रूप विद्यमान थे । जो अब लोक प्रचलित नहीं रहे। इनमें वर्तमान उपलब्ध कथारूपों में लोककथाओं की आधार भूमि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । लोककथाओं की यह चारित्रिक विशेषता रही है। उनका नायक जीवन के अंतिम क्षणों तक घोर संघर्षरत रहता है । वह क्षणभर के लिये भी निराश नहीं होता, विजय ही उसकी चरम परिणति है, पराजय नहीं । लोककथाओं का अन्त कभी भी दुखान्त नहीं होता । सुखान्त ही उनका चरम बिन्दु है । और ऐसा सुख, जिसकी मनोकामना धारण कर संपूर्ण कथाचक्र में वह संघर्ष करता रहता है। लोककथाओं के घटनाचक्रों में सजीवता, भाव-प्रवणता और पुरुषत्वपूर्ण जीवन जीने की अदम्य उत्साह भावना भरी हुई है। लोक कथाओं की उल्लेखित सभी बातें जैन कथा साहित्य में भी यथावत् उपलब्ध होती हैं । अन्तर केवल इतना ही होता है कि इन कथाओं का उद्देश्य धार्मिक भावना का प्रचार-प्रसार करना और मावन जीवन के नैतिक मूल्यों की उच्चता एवं प्राथमिकता प्रतिपादित कर अपने स्वयं के कल्याण की ओर अग्रसर होना है। इनके पात्र और चरित नायक कभी हताश और निराश नहीं हुए। जीवन की ऊहापोह से घबरा कर पलायन करने की प्रवृत्ति या आत्महत्या का संकल्प धारण करने की मन:स्थिति इनकी नहीं
___ अधिकांश जैन कथाएं पद्यबद्ध हैं। गेयत्व प्रधान हैं । एक कथा में कई धुनों का प्रयोग मिलता है । कुछ कथाएं दोहा और चौपाई छन्दों में ही रची गई हैं । कथाओं का गद्यरूप अत्यल्प है। पद्यबद्ध कथा परम्परा प्राचीन है । प्राकृत भाषा में लिखी गई गुणाढ्य की "बड्डकहा", वृहत्कथामंजरी, कथासरित्सागर, वृहद्कथा, श्लोक संग्रह और गाथा सप्तशती, आदि सभी ऐसे प्राचीन कथाग्रन्थ हैं जिनकी रचना पद्य रूप में ही उपलब्ध होती है । जैन कथा साहित्य के अनुशीलन से यह तथ्य अपने आप उभर कर सामने आता है कि इन कथाओं को लिपिबद्ध करने के पूर्व भी इनकी अक्षुण्ण परम्परा लोक जीवन में व्याप्त थी । जाति-पांति, भेदभाव, छुआछूत और ऊंचनीच की विषमताओं से लिप्त विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों और मत-मतान्तरों की लोकप्रियता दिनोदिन जाति
और समुदाय विशेष में सीमित होती जा रही थी तब जैन धर्म ने इन संकुचित विचारों की खाइयों को पाटकर समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अपने द्वार खोल दिये और वीतराग का वरदहस्त जैन और जैनेतर समाज के लिये समान रूप से छाया करने को अग्रसर हो उठा । जैन तीर्थंकरों और तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों का यही उद्देश्य भी था कि समग्र मानव समाज उनके धार्मिक विचारों को निर्द्वन्द्व होकर ग्रहण कर सकता है और आचारों को निस्संकोच जीवन में उतार कर अपना और मानव जाति का कल्याण कर सकता है । इसी का परिणाम था कि जैन धर्म जाति विशेष तक सीमित न रहकर अन्य जातियों में भी फैला और उसका साहित्य भी समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में व्यात हो गया । ऐसी अनेकों कथा-गाथाएं आज भी उपलब्ध होती हैं, जो लोक जीवन की कण्ठानुकण्ठ परम्परा में सदियों से विद्यमान है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जीवनयात्रा की नौका खेती हुई चली आ रही हैं । देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों, भाषा-भाषी क्षेत्रों, जाति वर्ग और समुदायों में इनका प्रवेश जब-जब हुआ, तब इन्होंने अपने आपको इस प्रकार बदल दिया और क्षेत्र विशेष में इस प्रकार घुलमिल गई कि कालान्तर में वे उनकी अपनी धरोहर मानी जाने लगी। प्रस्तुत तथ्य के निरूपण में हम दृढतापूर्वक यह कह सकते
(शेष पृष्ठ १११ पर)
१०४
राजेन्द्र ज्योति
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org