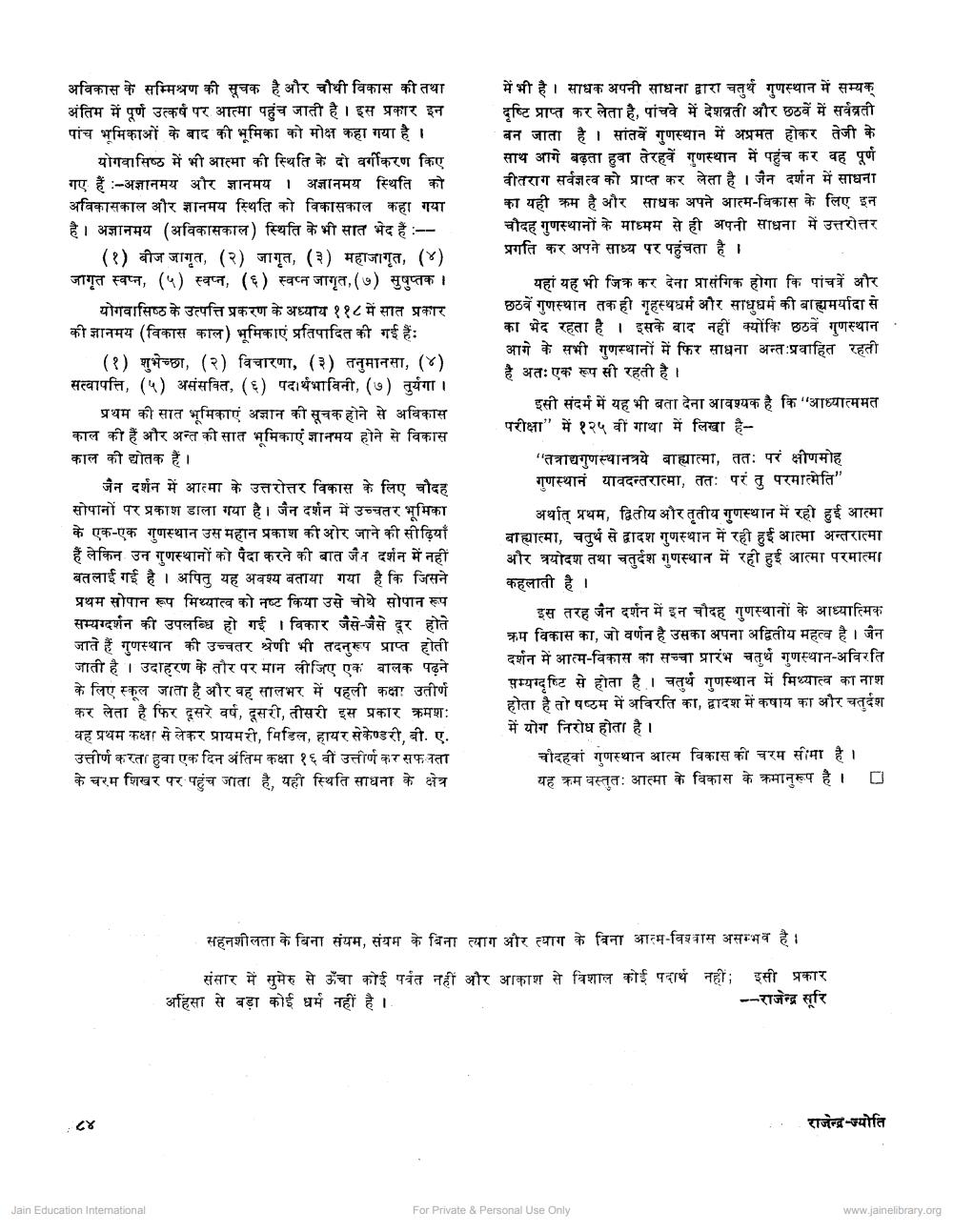________________
अविकास के सम्मिश्रण की सूचक है और चौथी विकास की तथा अंतिम में पूर्ण उत्कर्ष पर आत्मा पहुंच जाती है । इस प्रकार इन पांच भूमिकाओं के बाद की भूमिका को मोक्ष कहा गया है ।
योगवासिष्ठ में भी आत्मा की स्थिति के दो वर्गीकरण किए गए हैं :-अज्ञानमय और ज्ञानमय । अज्ञानमय स्थिति को अविकासकाल और ज्ञानमय स्थिति को विकासकाल कहा गया है। अज्ञानमय (अविकासकाल) स्थिति के भी सात भेद हैं :--
(१) बीज जागृत, (२) जागृत, (३) महाजागृत, (४) जागृत स्वप्न, (५) स्वप्न, (६) स्वप्न जागृत,(७) सुषुप्तक ।
योगवासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के अध्याय ११८ में सात प्रकार की ज्ञानमय (विकास काल) भूमिकाएं प्रतिपादित की गई हैं:
(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, (४) सत्वापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थभाविनी, (७) तुर्यगा।
प्रथम की सात भूमिकाएं अज्ञान की सूचक होने से अविकास काल की हैं और अन्त की सात भूमिकाएं ज्ञानमय होने से विकास काल की द्योतक हैं।
जैन दर्शन में आत्मा के उत्तरोत्तर विकास के लिए चौदह सोपानों पर प्रकाश डाला गया है। जैन दर्शन में उच्चतर भूमिका के एक-एक गुणस्थान उस महान प्रकाश की ओर जाने की सीढ़ियाँ हैं लेकिन उन गुणस्थानों को पैदा करने की बात जैन दर्शन में नहीं बतलाई गई है । अपितु यह अवश्य बताया गया है कि जिसने प्रथम सोपान रूप मिथ्यात्व को नष्ट किया उसे चोथे सोपान रूप सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो गई । विकार जैसे-जैसे दूर होते जाते हैं गुणस्थान की उच्चतर श्रेणी भी तदनुरूप प्राप्त होती जाती है । उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बालक पढ़ने के लिए स्कूल जाता है और वह सालभर में पहली कक्षा उतीर्ण कर लेता है फिर दूसरे वर्ष, दूसरी, तीसरी इस प्रकार क्रमश: वह प्रथम कक्षा से लेकर प्रायमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी, बी. ए. उत्तीर्ण करता हुवा एक दिन अंतिम कक्षा १६ वी उत्तीर्ण कर सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाता है, यही स्थिति साधना के क्षेत्र
में भी है। साधक अपनी साधना द्वारा चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक् दृष्टि प्राप्त कर लेता है, पांचवे में देशव्रती और छठवें में सर्वव्रती बन जाता है। सांतवें गुणस्थान में अप्रमत होकर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुवा तेरहवें गुणस्थान में पहुंच कर वह पूर्ण वीतराग सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लेता है । जैन दर्शन में साधना का यही क्रम है और साधक अपने आत्म-विकास के लिए इन चौदह गुणस्थानों के माध्मम से ही अपनी साधना में उत्तरोत्तर प्रगति कर अपने साध्य पर पहुंचता है ।
यहां यह भी जिक्र कर देना प्रासंगिक होगा कि पांचवें और छठवें गुणस्थान तक ही गृहस्थधर्म और साधुधर्म की बाह्यमर्यादा से का भेद रहता है । इसके बाद नहीं क्योंकि छठवें गुणस्थान आगे के सभी गुणस्थानों में फिर साधना अन्तःप्रवाहित रहती है अतः एक रूप सी रहती है।
इसी संदर्भ में यह भी बता देना आवश्यक है कि "आध्यात्ममत परीक्षा" में १२५ वी गाथा में लिखा है
"तत्राद्यगुणस्थानत्रये बाह्यात्मा, ततः परं क्षीणमोह गुणस्थानं यावदन्तरात्मा, ततः परं तु परमात्मेति"
अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान में रही हुई आत्मा बाह्यात्मा, चतुर्थ से द्वादश गुणस्थान में रही हुई आत्मा अन्तरात्मा
और त्रयोदश तथा चतुर्दश गुणस्थान में रही हुई आत्मा परमात्मा कहलाती है । _इस तरह जैन दर्शन में इन चौदह गुणस्थानों के आध्यात्मिक क्रम विकास का, जो वर्णन है उसका अपना अद्वितीय महत्व है। जैन दर्शन में आत्म-विकास का सच्चा प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान-अविरति सम्यग्दृष्टि से होता है । चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व का नाश होता है तो षष्टम में अविरति का, द्वादश में कषाय का और चतुर्दश में योग निरोध होता है।
चौदहवां गुणस्थान आत्म विकास की चरम सीमा है। यह कम वस्तुतः आत्मा के विकास के क्रमानुरूप है। "
सहनशीलता के बिना संयम, संयम के बिना त्याग और त्याग के बिना आत्म-विश्वास असम्भव है।
संसार में सुमेरु से ऊँचा कोई पर्वत नहीं और आकाश से विशाल कोई पदार्थ नहीं; इसी प्रकार अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
--राजेन्द्र सूरि
राजेन्द्र-ज्योति
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org