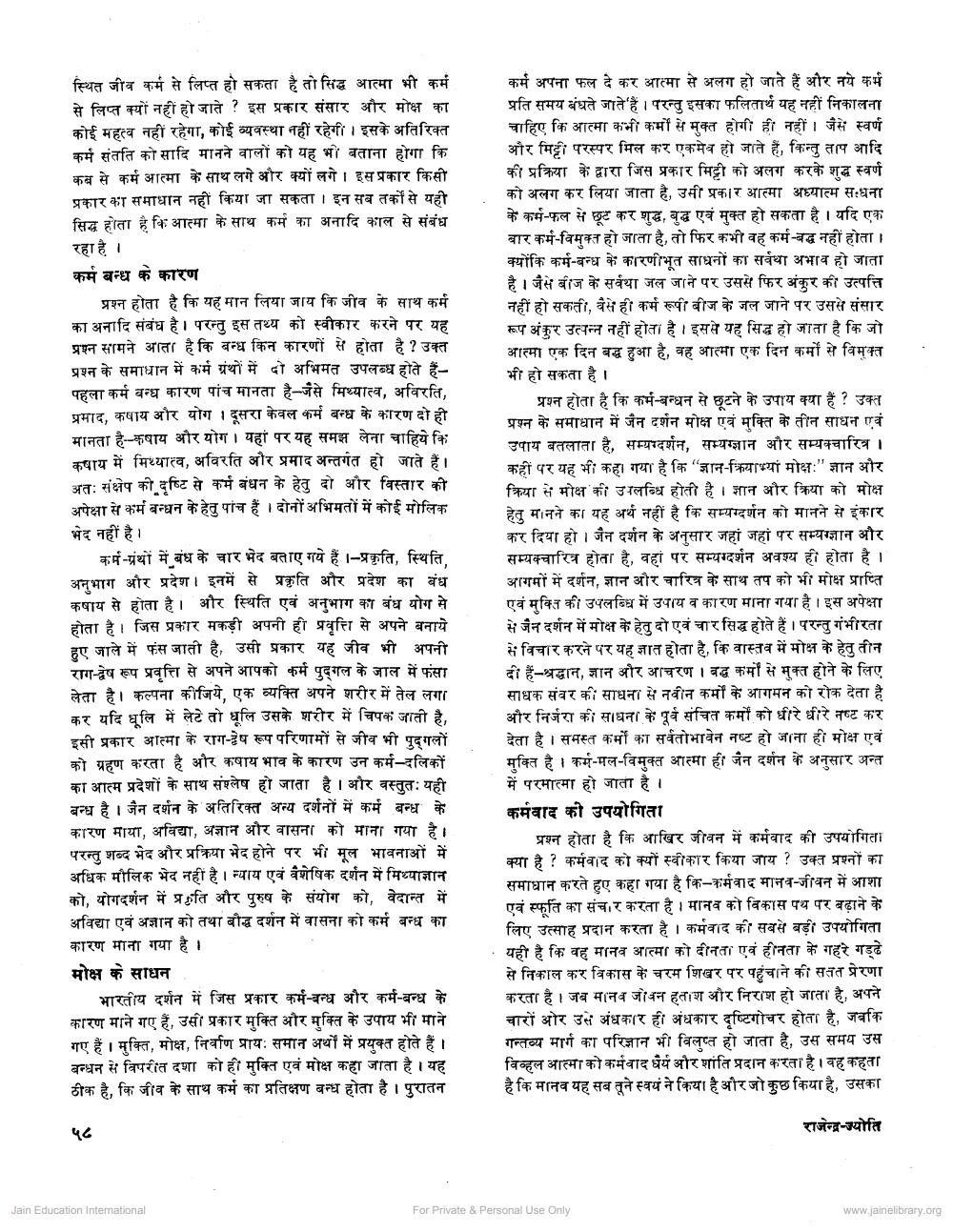________________
स्थित जीव कर्म से लिप्त हो सकता है तो सिद्ध आत्मा भी कर्म से लिप्त क्यों नहीं हो जाते ? इस प्रकार संसार और मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त कर्म संतति को सादि मानने वालों को यह भी बताना होगा कि कब से कर्म आत्मा के साथ लगे और क्यों लगे। इस प्रकार किसी प्रकार का समाधान नहीं किया जा सकता। इन सब तर्कों से यही सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ कर्म का अनादि काल से संबंध रहा है।
कर्म बन्ध के कारण
प्रश्न होता है कि यह मान लिया जाय कि जीव के साथ कर्म का अनादि संबंध है । परन्तु इस तथ्य को स्वीकार करने पर यह प्रश्न सामने आता है कि बन्ध किन कारणों से होता है ? उक्त प्रश्न के समाधान में कर्म ग्रंथों में दो अभिमत उपलब्ध होते हैंपहला कर्म बन्ध कारण पांच मानता है-जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । दूसरा केवल कर्म बन्ध के कारण दो ही मानता है-- कषाय और योग। यहां पर यह समझ लेना चाहिये कि कषाय में मिथ्यात्व अविरति और प्रमाद अन्तर्गत हो जाते हैं। अतः संक्षेप की दृष्टि से कर्मबंधन के हेतु दो और विस्तार की अपेक्षा से कर्म बन्धन के हेतु पांच हैं। दोनों अभिमतों में कोई मोलिक भेद नहीं है।
कर्म-ग्रंथों में बंध के चार भेद बताए गये हैं । - प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश । इनमें से प्रकृति और प्रदेश का बंध कषाय से होता है । और स्थिति एवं अनुभाग का बंध योग से होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने बनाये हुए जाले में फंस जाती है, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति से अपने आपको कर्म पुद्गल के जाल में फंसा लेता है। कल्पना कीजिये, एक व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा कर यदि धूलि में लेटे तो धूलि उसके शरीर में चिपक जाती है, इसी प्रकार आत्मा के राग-द्वेष रूप परिणामों से जीव भी पुद्गलों को ग्रहण करता है और कषाय भाव के कारण उन कर्म-दलिकों का आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष हो जाता है । और वस्तुतः यही बन्ध है । जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में कर्म बन्ध के कारण माया, अविद्या, अज्ञान और वासना को माना गया है। परन्तु शब्द भेद और प्रक्रिया भेद होने पर भी मूल भावनाओं में अधिक मौलिक भेद नहीं है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग को, वेदान्त में अविद्या एवं अज्ञान को तथा बौद्ध दर्शन में वासना को कर्म बन्ध का कारण माना गया है ।
मोक्ष के साधन
भारतीय दर्शन में जिस प्रकार कर्म-बन्ध और कर्म-बन्ध के कारण माने गए हैं, उसी प्रकार मुक्ति और मुक्ति के उपाय भी माने गए हैं। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राय: समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं । बन्धन से विपरीत दशा को ही मुक्ति एवं मोक्ष कहा जाता है। यह ठीक है, कि जीव के साथ कर्म का प्रतिक्षण बन्ध होता है । पुरातन
५८
Jain Education International
कर्म अपना फल दे कर आत्मा से अलग हो जाते हैं और नये कर्म प्रति समय बंधते जाते हैं। परन्तु इसका फलितार्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि आत्मा कभी कर्मों से मुक्त होगी ही नहीं। जैसे स्वर्ण और मिट्टी परस्पर मिल कर एकमेव हो जाते हैं, किन्तु ताप आदि की प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रकार मिट्टी को अलग करके स्वर्ण शुद्ध को अलग कर लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा अध्यात्म सधना के कर्म फल से छूट कर शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो सकता है। यदि एक बार कर्म-विमुक्त हो जाता है, तो फिर कभी वह कर्म - बद्ध नहीं होता । क्योंकि कर्म-बन्ध के कारणीभूत साधनों का सर्वथा अभाव हो जाता है । जैसे बीज के सर्वथा जल जाने पर उससे फिर अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही कर्म रूपी बीज के जल जाने पर उससे संसार रूप अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो आत्मा एक दिन बद्ध हुआ है, वह आत्मा एक दिन कर्मों से विमुक्त भी हो सकता है ।
प्रश्न होता है कि कर्म-बन्धन से छूटने के उपाय क्या हैं ? उक्त प्रश्न के समाधान में जैन दर्शन मोक्ष एवं मुक्ति के तीन साधन एवं उपाय बतलाता है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । कहीं पर यह भी कहा गया है कि "ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्षः" ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की उपलब्धि होती है। ज्ञान और क्रिया को मोक्ष हेतु मानने का यह अर्थ नहीं है कि सम्यग्दर्शन को मानने से इंकार कर दिया हो। जैन दर्शन के अनुसार जहां जहां पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होता है, वहां पर सम्यग्दर्शन अवश्य ही होता है । आगमों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ तप को भी मोक्ष प्राप्ति एवं मुक्ति की उपलब्धि में उपाय व कारण माना गया है। इस अपेक्षा से जैन दर्शन में मोक्ष के हेतु दो एवं चार सिद्ध होते हैं । परन्तु गंभीरता से विचार करने पर यह ज्ञात होता है, कि वास्तव में मोक्ष के हेतु तीन दी हैं - श्रद्धान, ज्ञान और आचरण । बद्ध कर्मों से मुक्त होने के लिए साधक संवर की साधना से नवीन कर्मों के आगमन को रोक देता है और निर्जरा की साधना के पूर्व संचित कर्मों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है । समस्त कर्मों का सर्वतोभावेन नष्ट हो जाना ही मोक्ष एवं मुक्तिकर्म-विमुक्त आत्मा ही जैन दर्शन के अनुसार जन्त में परमात्मा हो जाता है ।
कर्मवाद की उपयोगिता
प्रश्न होता है कि आखिर जीवन में कर्मवाद की उपयोगिता क्या है ? कर्मवाद को क्यों स्वीकार किया जाय ? उक्त प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा गया है कि- कर्मवाद मानव जीवन में आशा एवं स्फूर्ति का संचार करता है। मानव को विकास पथ पर बढ़ाने के लिए उत्साह प्रदान करता है। कर्मवाद की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि वह मानव आत्मा को दीनता एवं हीनता के गहरे गड्ढे से निकाल कर विकास के चरम शिखर पर पहुंचाने की सतत प्रेरणा करता है। जब मानव जोवन हताश और निराश हो जाता है, अपने चारों ओर उसे अंधकार ही अंधकार दृष्टिगोचर होता है, जबकि गन्तव्य मार्ग का परिज्ञान भी विलुप्त हो जाता है, उस समय उस विव्हल आत्मा को कर्मवाद धैर्य और शांति प्रदान करता है। वह कहता है कि मानव यह सब तूने स्वयं ने किया है और जो कुछ किया है, उसका
राजेन्द्र - ज्योति
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org