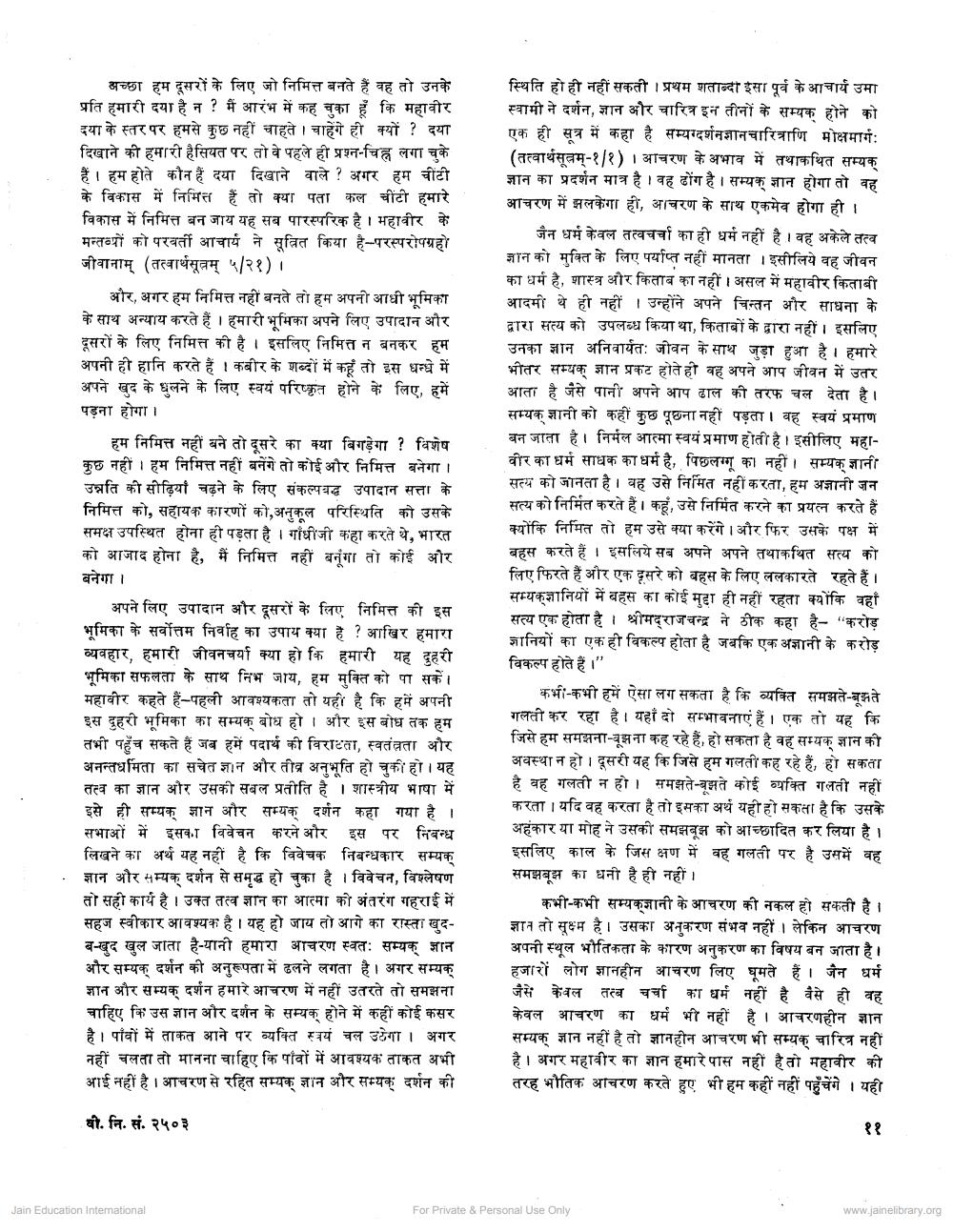________________
अच्छा हम दूसरों के लिए जो निमित्त बनते हैं वह तो उनके प्रति हमारी दया है न ? मैं आरंभ में कह चुका हूँ कि महावीर दया के स्तर पर हमसे कुछ नहीं चाहते । चाहेंगे ही क्यों ? दया दिखाने की हमारी हैसियत पर तो वे पहले ही प्रश्नचिह्न लगा चुके हैं। हम होते कौन हैं दया दिखाने वाले ? अगर हम चींटी के विकास में निमित्त हैं तो क्या पता कल चींटी हमारे विकास में निमित्त बन जाय यह सब पारस्परिक है। महावीर के मन्तव्यों को परवर्ती आचार्य ने सूचित किया है-परस्परोपग्रहो जीवानाम् (तस्थार्थमूलम् ५/२१) ।
"
और अगर हम निमित्त नहीं बनते तो हम अपनी आधी भूमिका के साथ अन्याय करते हैं। हमारी भूमिका अपने लिए उपादान और दूसरों के लिए निमित्त की है। इसलिए निमित्त न बनकर हम अपनी ही हानि करते हैं । कबीर के शब्दों में कहूँ तो इस धन्धे में अपने खुद के धुलने के लिए स्वयं परिष्कृत होने के लिए, हमें पड़ना होगा।
हम निमित्त नहीं बने तो दूसरे का क्या बिगड़ेगा ? विशेष कुछ नहीं। हम निमित्त नहीं बनेंगे तो कोई और निमित्त बनेगा । उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए संकल्पबद्ध उपादान सत्ता के निमित्त को, सहायक कारणों को, अनुकूल परिस्थिति को उसके समक्ष उपस्थित होना ही पड़ता है। गाँधीजी कहा करते थे, भारत को आजाद होना है, मैं निमित्त नहीं बनूंगा तो कोई और बनेगा ।
इस पर
अपने लिए उपादान और दूसरों के लिए निमित्त की इस भूमिका के सर्वोत्तम निर्वाह का उपाय क्या है ? आखिर हमारा व्यवहार, हमारी जीवनचर्या क्या हो कि हमारी यह दुहरी भूमिका सफलता के साथ निभ जाय, हम मुक्ति को पा सकें । महावीर कहते हैं- पहली आवश्यकता तो यहीं है कि हमें अपनी इस दुहरी भूमिका का सम्यक् बोध हो । और इस बोध तक हम तभी पहुँच सकते हैं जब हमें पदार्थ की विराटता स्वतंत्रता और अनन्तधर्मिता का सचेत ज्ञान और तीव्र अनुभूति हो चुकी हो। यह तत्व का ज्ञान और उसकी सबल प्रतीति है । शास्त्रीय भाषा में इसे ही सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन कहा गया है । सभाओं में इसका विवेचन करने और निबन्ध लिखने का अर्थ यह नहीं है कि विवेचक निबन्धकार सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन से समृद्ध हो चुका है। विवेचन, विश्लेषण तो सही कार्य है । उक्त तत्व ज्ञान का आत्मा को अंतरंग गहराई में सहज स्वीकार आवश्यक है। यह हो जाय तो आगे का रास्ता खुदब-खुद खुल जाता है- यानी हमारा आचरण स्वतः सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन की अनुरूपता में ढलने लगता है। अगर सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन हमारे आचरण में नहीं उतरते तो समझना चाहिए कि उस ज्ञान और दर्शन के सम्यक् होने में कहीं कोई कसर है । पाँवों में ताकत आने पर व्यक्ति स्वयं चल उठेगा। अगर नहीं चलता तो मानना चाहिए कि पाँवों में आवश्यक ताकत अभी आई नहीं है। आचरण से रहित सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन की
बी. नि. सं. २५०३
Jain Education International
स्थिति हो ही नहीं सकती । प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य उमा स्वामी ने दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों के सम्यक् होने को एक ही सूत्र में कहा है सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ( तत्वार्थ सूत्रम् - १ / १ ) । आचरण के अभाव में तथाकथित सम्यक् ज्ञान का प्रदर्शन मात्र है । वह ढोंग है। सम्यक् ज्ञान होगा तो वह आचरण में झलकेगा ही, आचरण के साथ एकमेव होगा ही ।
जैन धर्म केवल तत्वचर्चा का ही धर्म नहीं है। वह अकेले तत्व ज्ञान को मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं मानता । इसीलिये वह 'जीवन का धर्म है, शास्त्र और किताब का नहीं। असल में महावीर किताबी आदमी थे ही नहीं । उन्होंने अपने चिन्तन और साधना के द्वारा सत्य को उपलब्ध किया था, किताबों के द्वारा नहीं। इसलिए उनका ज्ञान अनिवार्यतः जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर सम्यक् ज्ञान प्रकट होते ही वह अपने आप जीवन में उतर आता है जैसे पानी अपने आप ढाल की तरफ चल देता है। सम्यक् ज्ञानी को कहीं कुछ पूछना नहीं पड़ता। वह स्वयं प्रमाण बन जाता है। निर्मल आत्मा स्वयं प्रमाण होती है। इसीलिए महावीर का धर्म साधक का धर्म है, पिछलग्गू का नहीं। सम्यक् ज्ञानी सत्य को जानता है । वह उसे निर्मित नहीं करता, हम अज्ञानी जन सत्य को निर्मित करते हैं। कहूँ, उसे निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि निर्मित तो हम उसे क्या करेंगे। और फिर उसके पक्ष में बहस करते हैं । इसलिये सब अपने अपने तथाकथित सत्य को लिए फिरते हैं और एक दूसरे को बहस के लिए ललकारते रहते हैं। सम्यक्ज्ञानियों में बहस का कोई मुद्दा ही नहीं रहता क्योंकि वहाँ सत्य एक होता है। श्रीमद्रराजचन्द्र ने ठीक कहा है- "करोड़ ज्ञानियों का एक ही विकल्प होता है जबकि एक अज्ञानी के करोड़ विकल्प होते हैं । "
कभी-कभी हमें ऐसा लग सकता है कि व्यक्ति समझते-बूझते गलती कर रहा है। यहाँ दो सम्भावनाएं हैं। एक तो यह कि जिसे हम समझना - बूझना कह रहे हैं, हो सकता है वह सम्यक् ज्ञान की अवस्था न हो। दूसरी यह कि जिसे हम गलती कह रहे हैं, हो सकता है वह गलती न हो समझते बूझते कोई व्यक्ति गलती नहीं करता। यदि वह करता है तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि उसके अहंकार या मोह ने उसकी समझबूझ को आच्छादित कर लिया है । इसलिए काल के जिस क्षण में वह गलती पर है उसमें वह समझबूझ का धनी है ही नहीं।
कभी-कभी सम्यक्ज्ञानी के आचरण की नकल हो सकती है। ज्ञान तो सूक्ष्म है। उसका अनुकरण संभव नहीं। लेकिन आचरण अपनी स्थूल भौतिकता के कारण अनुकरण का विषय बन जाता है। हजारों लोग ज्ञानहीन आचरण लिए घूमते हैं। जैन धर्म जैसे केवल तत्व चर्चा का धर्म नहीं है वैसे ही वह केवल आचरण का धर्म भी नहीं है । आचरणहीन ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं है तो ज्ञानहीन आचरण भी सम्यक् चारित्र नहीं है। अगर महावीर का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो महावीर की तरह भौतिक आचरण करते हुए भी हम कहीं नहीं पहुँचेंगे । यही
For Private & Personal Use Only
११
www.jainelibrary.org