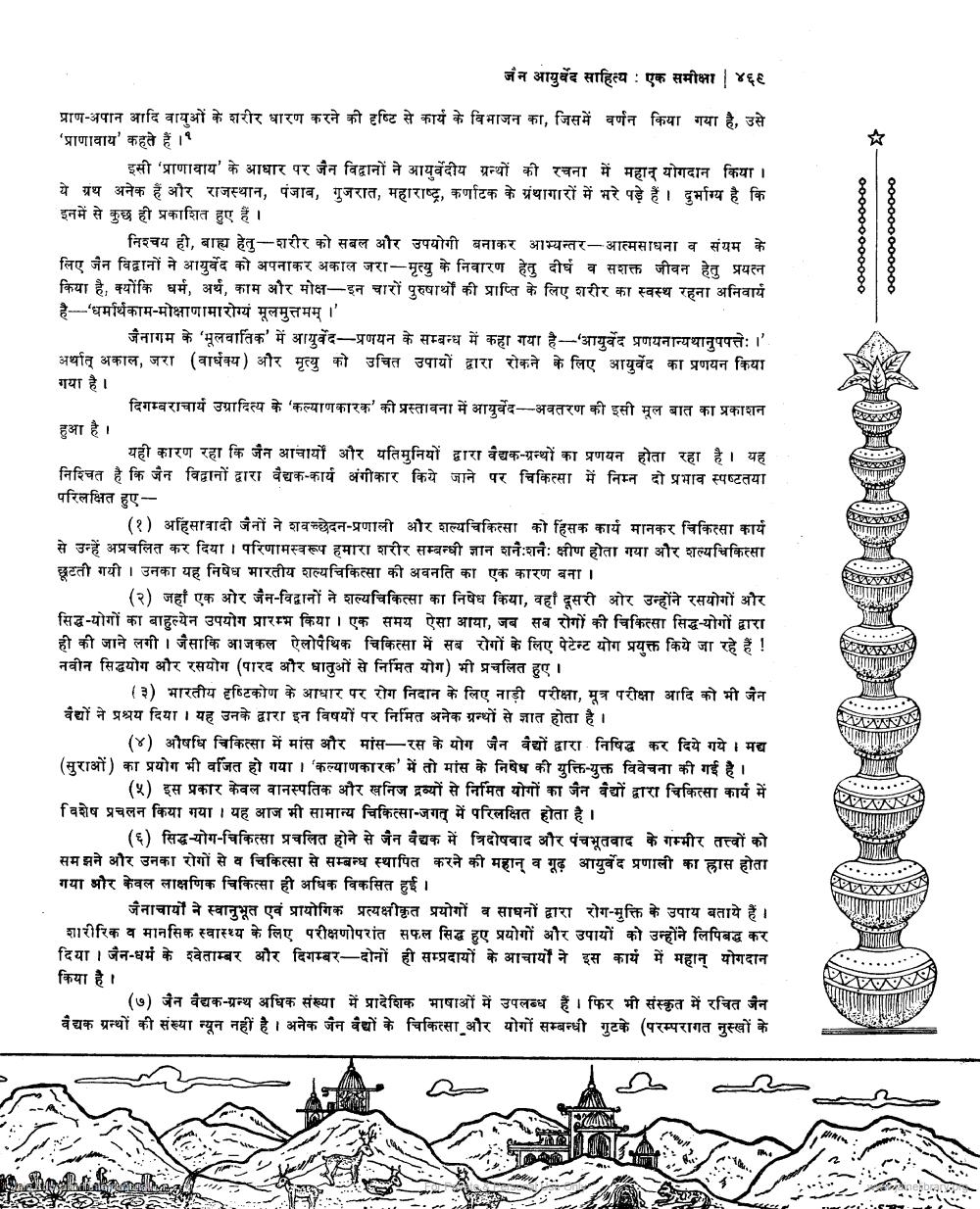________________
जैन आयुर्वेद साहित्य : एक समीक्षा | ४६६
००००००००००००
NEPA
CARDA
MAILY
ARRENA
Hary
प्राण-अपान आदि वायुओं के शरीर धारण करने की दृष्टि से कार्य के विभाजन का, जिसमें वर्णन किया गया है, उसे 'प्राणावाय' कहते हैं ।
इसी 'प्राणावाय' के आधार पर जैन विद्वानों ने आयुर्वेदीय ग्रन्थों की रचना में महान् योगदान किया। ये ग्रंथ अनेक हैं और राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक के ग्रंथागारों में भरे पड़े हैं। दुर्भाग्य है कि इनमें से कुछ ही प्रकाशित हुए हैं।
निश्चय ही, बाह्य हेतु-शरीर को सबल और उपयोगी बनाकर आभ्यन्तर-आत्मसाधना व संयम के लिए जैन विद्वानों ने आयुर्वेद को अपनाकर अकाल जरा-मृत्यु के निवारण हेतु दीर्घ व सशक्त जीवन हेतु प्रयत्न किया है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है-'धर्मार्थकाम-मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् ।'
जैनागम के 'मूलवार्तिक' में आयुर्वेद-प्रणयन के सम्बन्ध में कहा गया है-'आयुर्वेद प्रणयनान्यथानुपपत्तेः ।' अर्थात् अकाल, जरा (वार्धक्य) और मृत्यु को उचित उपायों द्वारा रोकने के लिए आयुर्वेद का प्रणयन किया गया है।
दिगम्बराचार्य उग्रादित्य के 'कल्याणकारक' की प्रस्तावना में आयुर्वेद-अवतरण की इसी मूल बात का प्रकाशन हुआ है।
__यही कारण रहा कि जैन आचार्यों और यतिमुनियों द्वारा वैद्यक-ग्रन्थों का प्रणयन होता रहा है। यह निश्चित है कि जैन विद्वानों द्वारा वैद्यक-कार्य अंगीकार किये जाने पर चिकित्सा में निम्न दो प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित हुए
(१) अहिंसावादी जैनों ने शवच्छेदन-प्रणाली और शल्यचिकित्सा को हिंसक कार्य मानकर चिकित्सा कार्य से उन्हें अप्रचलित कर दिया। परिणामस्वरूप हमारा शरीर सम्बन्धी ज्ञान शनैःशनैः क्षीण होता गया और शल्यचिकित्सा छूटती गयी। उनका यह निषेध भारतीय शल्यचिकित्सा की अवनति का एक कारण बना ।
(२) जहां एक ओर जैन-विद्वानों ने शल्यचिकित्सा का निषेध किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने रसयोगों और सिद्ध-योगों का बाहुल्येन उपयोग प्रारम्भ किया। एक समय ऐसा आया, जब सब रोगों की चिकित्सा सिद्ध-योगों द्वारा ही की जाने लगी। जैसाकि आजकल ऐलोपैथिक चिकित्सा में सब रोगों के लिए पेटेन्ट योग प्रयुक्त किये जा रहे हैं ! नवीन सिद्धयोग और रसयोग (पारद और धातुओं से निर्मित योग) भी प्रचलित हुए।
(३) भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर रोग निदान के लिए नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा आदि को भी जैन वैद्यों ने प्रश्रय दिया। यह उनके द्वारा इन विषयों पर निर्मित अनेक ग्रन्थों से ज्ञात होता है।
(४) औषधि चिकित्सा में मांस और मांस-रस के योग जैन वैद्यों द्वारा निषिद्ध कर दिये गये । मद्य (सुराओं) का प्रयोग भी वजित हो गया। 'कल्याणकारक' में तो मांस के निषेध की युक्ति-युक्त विवेचना की गई है।
(५) इस प्रकार केवल वानस्पतिक और खनिज द्रव्यों से निर्मित योगों का जैन वैद्यों द्वारा चिकित्सा कार्य में विशेष प्रचलन किया गया। यह आज भी सामान्य चिकित्सा-जगत् में परिलक्षित होता है ।
(६) सिद्ध-योग-चिकित्सा प्रचलित होने से जैन वैद्यक में त्रिदोषवाद और पंचभूतवाद के गम्भीर तत्त्वों को समझने और उनका रोगों से व चिकित्सा से सम्बन्ध स्थापित करने की महान व गूढ़ आयुर्वेद प्रणाली का ह्रास होता गया और केवल लाक्षणिक चिकित्सा ही अधिक विकसित हुई।
जैनाचार्यों ने स्वानुभूत एवं प्रायोगिक प्रत्यक्षीकृत प्रयोगों व साधनों द्वारा रोग-मुक्ति के उपाय बताये हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए परीक्षणोपरांत सफल सिद्ध हुए प्रयोगों और उपायों को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। जैन-धर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर–दोनों ही सम्प्रदायों के आचार्यों ने इस कार्य में महान् योगदान किया है।
(७) जैन वैद्यक-ग्रन्थ अधिक संख्या में प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हैं । फिर भी संस्कृत में रचित जैन वैद्यक ग्रन्थों की संख्या न्यून नहीं है । अनेक जैन वैद्यों के चिकित्सा और योगों सम्बन्धी गुटके (परम्परागत नुस्खों के