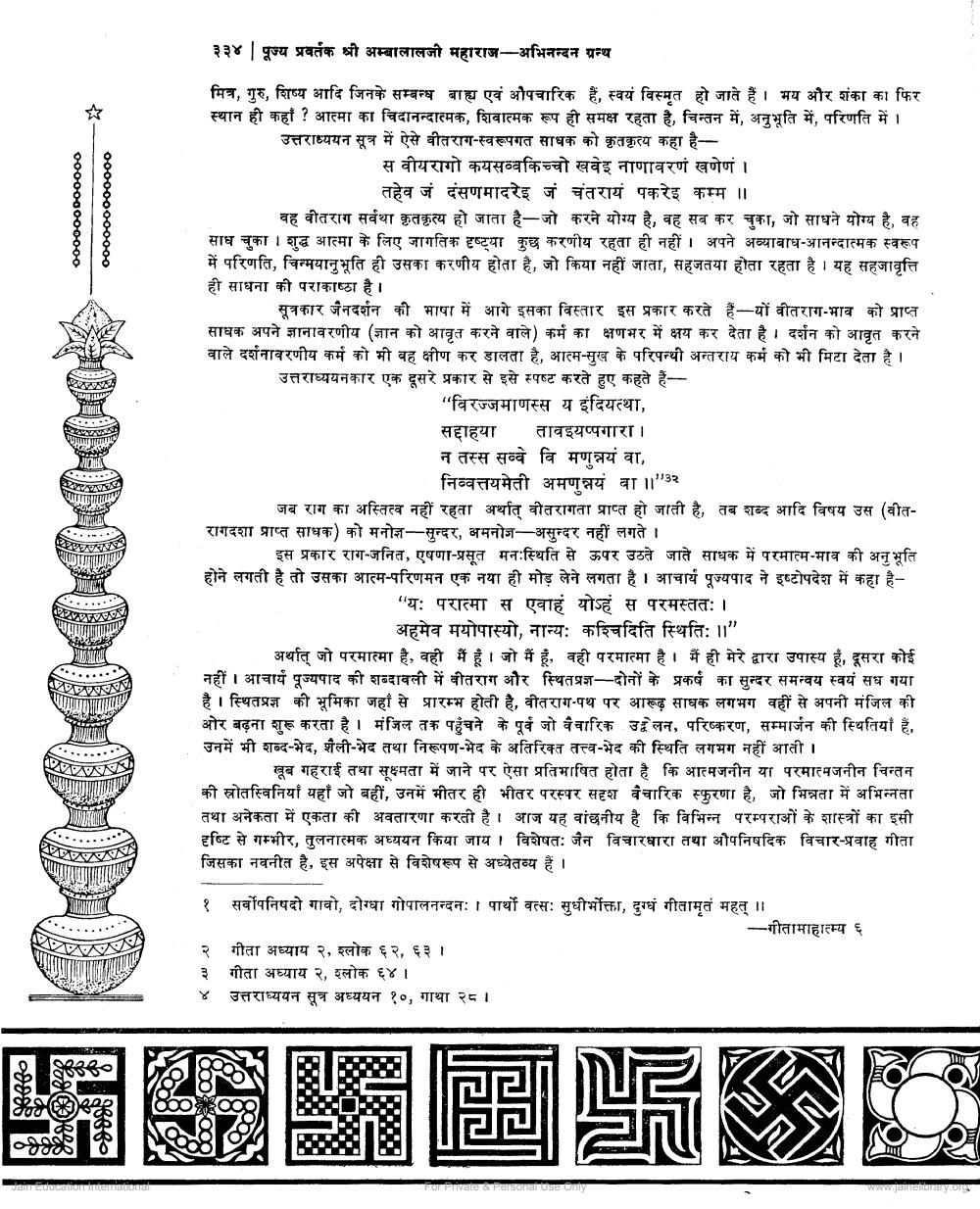________________
३३४ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
००००००००००००
००००००००००००
मित्र, गुरु, शिष्य आदि जिनके सम्बन्ध बाह्य एवं औपचारिक हैं, स्वयं विस्मृत हो जाते हैं। भय और शंका का फिर स्थान ही कहाँ ? आत्मा का चिदानन्दात्मक, शिवात्मक रूप ही समक्ष रहता है, चिन्तन में, अनुभूति में, परिणति में । उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसे वीतराग-स्वरूपगत साधक को कृतकृत्य कहा है
स वीयरागो कयसव्वकिच्चो खवेइ नाणावरणं खणेणं ।
तहेव जं दंसणमादरेइ जं चतरायं पकरेइ कम्म ।। वह वीतराग सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है जो करने योग्य है, वह सब कर चुका, जो साधने योग्य है, वह साध चुका । शुद्ध आत्मा के लिए जागतिक दृष्ट्या कुछ करणीय रहता ही नहीं। अपने अव्याबाध-आनन्दात्मक स्वरूप में परिणति, चिन्मयानुभूति ही उसका करणीय होता है, जो किया नहीं जाता, सहजतया होता रहता है । यह सहजावृत्ति ही साधना की पराकाष्ठा है।
सूत्रकार जनदर्शन की भाषा में आगे इसका विस्तार इस प्रकार करते हैं-यों वीतराग-भाव को प्राप्त साधक अपने ज्ञानावरणीय (ज्ञान को आवृत करने वाले) कर्म का क्षणभर में क्षय कर देता है। दर्शन को आवृत करने वाले दर्शनावरणीय कर्म को भी वह क्षीण कर डालता है, आत्म-सुख के परिपन्थी अन्तराय कर्म को भी मिटा देता है। उत्तराध्ययनकार एक दूसरे प्रकार से इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं
"विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सद्दाहया तावइयप्पगारा। न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा,
निव्वत्तयमेती अमणुन्नयं वा ॥"3२ जब राग का अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् वीतरागता प्राप्त हो जाती है, तब शब्द आदि विषय उस (वीतरागदशा प्राप्त साधक) को मनोज्ञ-सुन्दर, अमनोज-असुन्दर नहीं लगते ।
इस प्रकार राग-जनित, एषणा-प्रसूत मनःस्थिति से ऊपर उठते जाते साधक में परमात्म-माव की अनुभूति होने लगती है तो उसका आत्म-परिणमन एक नया ही मोड़ लेने लगता है । आचार्य पूज्यपाद ने इष्टोपदेश में कहा है
"यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः।
अहमेव मयोपास्यो, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ।।" अर्थात् जो परमात्मा है, वही मैं हूँ । जो मैं हूँ, वही परमात्मा है। मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, दूसरा कोई नहीं । आचार्य पूज्यपाद की शब्दावली में वीतराग और स्थितप्रज्ञ-दोनों के प्रकर्ष का सुन्दर समन्वय स्वयं सध गया है । स्थितप्रज्ञ की भूमिका जहाँ से प्रारम्भ होती है, वीतराग-पथ पर आरूढ़ साधक लगभग वहीं से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करता है। मंजिल तक पहुंचने के पूर्व जो वैचारिक उद्वेलन, परिष्करण, सम्मार्जन की स्थितियाँ हैं, उनमें भी शब्द-भेद, शैली-भेद तथा निरूपण-भेद के अतिरिक्त तत्त्व-भेद की स्थिति लगभग नहीं आती।
खूब गहराई तथा सूक्ष्मता में जाने पर ऐसा प्रतिभाषित होता है कि आत्मजनीन या परमात्मजनीन चिन्तन की स्रोतस्विनियाँ यहाँ जो बहीं, उनमें भीतर ही भीतर परस्पर सदृश वैचारिक स्फुरणा है, जो भिन्नता में अभिन्नता तथा अनेकता में एकता की अवतारणा करती है। आज यह वांछनीय है कि विभिन्न परम्पराओं के शास्त्रों का इसी दृष्टि से गम्भीर, तुलनात्मक अध्ययन किया जाय । विशेषतः जैन विचारधारा तथा औपनिषदिक विचार-प्रवाह गीता जिसका नवनीत है, इस अपेक्षा से विशेषरूप से अध्येतव्य हैं ।
UITAMILY
...
.-
A
१ सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत् ॥
-गीतामाहात्म्य ६ २ गीता अध्याय २, श्लोक ६२,६३ । ३ गीता अध्याय २, श्लोक ६४ । ४ उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १०, गाथा २८ ।
मना
SRAR0
O9000
du
JABAR
COOTROO
090018
1088
AVITA
FORPrivaterpersaroseroive
www.jainelibrary.org