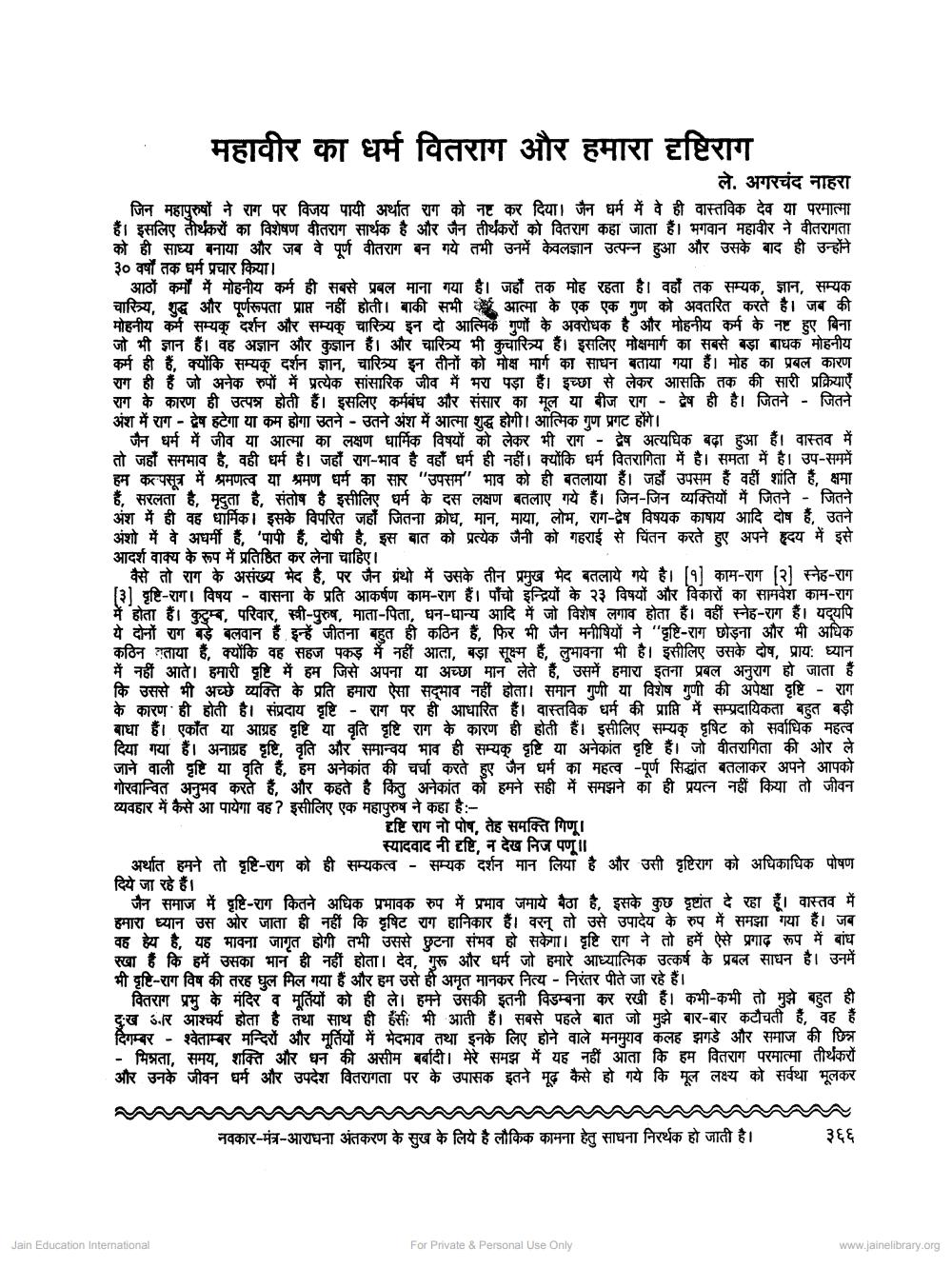________________
महावीर का धर्म वितराग और हमारा दृष्टिराग
ले. अगरचंद नाहरा जिन महापुरुषों ने राग पर विजय पायी अर्थात राग को नष्ट कर दिया। जैन धर्म में वे ही वास्तविक देव या परमात्मा हैं। इसलिए तीर्थकरों का विशेषण वीतराग सार्थक है और जैन तीर्थंकरों को वितराग कहा जाता हैं। भगवान महावीर ने वीतरागता को ही साध्य बनाया और जब वे पूर्ण वीतराग बन गये तभी उनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके बाद ही उन्होंने ३० वर्षों तक धर्म प्रचार किया।
आठों कर्मों में मोहनीय कर्म ही सबसे प्रबल माना गया है। जहाँ तक मोह रहता है। वहाँ तक सम्यक, ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, शुद्ध और पूर्णरूपता प्राप्त नहीं होती। बाकी सभी आत्मा के एक एक गुण को अवतरित करते है। जब की मोहनीय कर्म सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य इन दो आत्मिक गुणों के अवरोधक है और मोहनीय कर्म के नष्ट हुए बिना जो भी ज्ञान हैं। वह अज्ञान और कजान हैं। और चारित्र्य भी कुचारित्र्य हैं। इसलिए मोक्षमार्ग का सबसे बड़ा बाधक मोहनीय कर्म ही हैं, क्योंकि सम्यकू दर्शन ज्ञान, चारिख्य इन तीनों को मोक्ष मार्ग का साधन बताया गया हैं। मोह का प्रबल कारण राग ही हैं जो अनेक रूपों में प्रत्येक सांसारिक जीव में भरा पड़ा हैं। इच्छा से लेकर आसक्ति तक की सारी प्रक्रियाएँ राग के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए कर्मबंध और संसार का मूल या बीज राग - द्वेष ही है। जितने - जितने अंश में राग-द्वेष हटेगा या कम होगा उतने- उतने अंश में आत्मा शुद्ध होगी। आत्मिक गुण प्रगट होंगे।
जैन धर्म में जीव या आत्मा का लक्षण धार्मिक विषयों को लेकर भी राग - द्वेष अत्यधिक बढ़ा हुआ हैं। वास्तव में तो जहाँ समभाव है, वही धर्म है। जहाँ राग-भाव है वहाँ धर्म ही नहीं। क्योंकि धर्म वितरागिता में है। समता में है। उप-सममें हम कल्पसूत्र में श्रमणत्व या श्रमण धर्म का सार "उपसम" भाव को ही बतलाया हैं। जहाँ उपसम हैं वहीं शांति हैं, क्षमा हैं, सरलता है, मृदुता है, संतोष है इसीलिए धर्म के दस लक्षण बतलाए गये हैं। जिन-जिन व्यक्तियों में जितने - जितने अंश में ही वह धार्मिक। इसके विपरित जहाँ जितना क्रोध, मान, माया, लोम, राग-द्वेष विषयक काषाय आदि दोष हैं, उतने अंशो में वे अधर्मी हैं, 'पापी हैं, दोषी है, इस बात को प्रत्येक जैनी को गहराई से चिंतन करते हुए अपने हृदय में इसे आदर्श वाक्य के रूप में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए।
वैसे तो राग के असंख्य भेद है, पर जैन ग्रंथो में उसके तीन प्रमुख भेद बतलाये गये है। [9] काम-राग [२] स्नेह-राग [३] दृष्टि-राग। विषय - वासना के प्रति आकर्षण काम-राग हैं। पाँचो इन्द्रियों के २३ विषयों और विकारों का सामवेश काम-राग में होता हैं। कुटुम्ब, परिवार, स्त्री-पुरुष, माता-पिता, धन-धान्य आदि में जो विशेष लगाव होता हैं। वहीं स्नेह-राग हैं। यद्यपि ये दोनों राग बड़े बलवान हैं इन्हें जीतना बहुत ही कठिन हैं, फिर भी जैन मनीषियों ने "दृष्टि-राग छोड़ना और भी अधिक कठिन बताया हैं, क्योंकि वह सहज पकड़ में नहीं आता, बड़ा सूक्ष्म हैं, लुभावना भी है। इसीलिए उसके दोष, प्राय: ध्यान में नहीं आते। हमारी दृष्टि में हम जिसे अपना या अच्छा मान लेते हैं, उसमें हमारा इतना प्रबल अनुराग हो जाता हैं कि उससे भी अच्छे व्यक्ति के प्रति हमारा ऐसा सदभाव नहीं होता। समान गुणी या विशेष गुणी की अपेक्षा दृष्टि - राग के कारण ही होती है। संप्रदाय दृष्टि - राग पर ही आधारित हैं। वास्तविक धर्म की प्राप्ति में सम्प्रदायिकता बहुत बड़ी बाधा हैं। एकांत या आग्रह दृष्टि या वृति दृष्टि राग के कारण ही होती हैं। इसीलिए सम्यक् दृषिट को सर्वाधिक महत्व दिया गया हैं। अनाग्रह दृष्टि, वृति और समान्वय भाव ही सम्यक दृष्टि या अनेकांत दृष्टि हैं। जो वीतरागिता की ओर ले जाने वाली दृष्टि या वृति हैं, हम अनेकांत की चर्चा करते हुए जैन धर्म का महत्व -पूर्ण सिद्धांत बतलाकर अपने आपको गोरखान्वित अनुभव करते हैं, और कहते है किंतु अनेकांत को हमने सही में समझने का ही प्रयत्न नहीं किया तो जीवन व्यवहार में कैसे आ पायेगा वह? इसीलिए एक महापुरुष ने कहा है:
दृष्टि राग नो पोष, तेह समक्ति गिणू।
स्यादवाद नी दृष्टि, न देख निज पणू॥ अर्थात हमने तो दृष्टि-राग को ही सम्यकत्व - सम्यक दर्शन मान लिया है और उसी दृष्टिराग को अधिकाधिक पोषण दिये जा रहे हैं।
जैन समाज में दृष्टि-राग कितने अधिक प्रभावक रुप में प्रभाव जमाये बैठा है, इसके कुछ दृष्टांत दे रहा हूँ। वास्तव में हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं कि दृषिट राग हानिकार हैं। वरन् तो उसे उपादेय के रुप में समझा गया हैं। जब वह हेय है, यह भावना जागृत होगी तभी उससे छुटना संभव हो सकेगा। दृष्टि राग ने तो हमें ऐसे प्रगाढ़ रूप में बांध स्खा है कि हमें उसका भान ही नहीं होता। देव, गुरू और धर्म जो हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष के प्रबल साधन है। उनमें भी दृष्टि-राग विष की तरह घुल मिल गया हैं और हम उसे ही अमृत मानकर नित्य-निरंतर पीते जा रहे हैं।
वितराग प्रभु के मंदिर व मूर्तियों को ही ले। हमने उसकी इतनी विडम्बना कर रखी है। कभी-कभी तो मुझे बहुत ही दुःख र आश्चर्य होता है तथा साथ ही हसी भी आती हैं। सबसे पहले बात जो मुझे बार-बार कटौचती हैं, वह हैं दिगम्बर - श्वेताम्बर मन्दिरों और मूर्तियों में भेदभाव तथा इनके लिए होने वाले मनमुराव कलह झगडे और समाज की छिन - भिन्नता, समय, शक्ति और धन की असीम बर्बादी। मेरे समझ में यह नहीं आता कि हम वितराग परमात्मा तीर्थंकरों और उनके जीवन धर्म और उपदेश वितरागता पर के उपासक इतने मूढ़ कैसे हो गये कि मूल लक्ष्य को सर्वथा भूलकर
नवकार-मंत्र-आराधना अंतकरण के सुख के लिये है लौकिक कामना हेतु साधना निरर्थक हो जाती है।
३६६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org