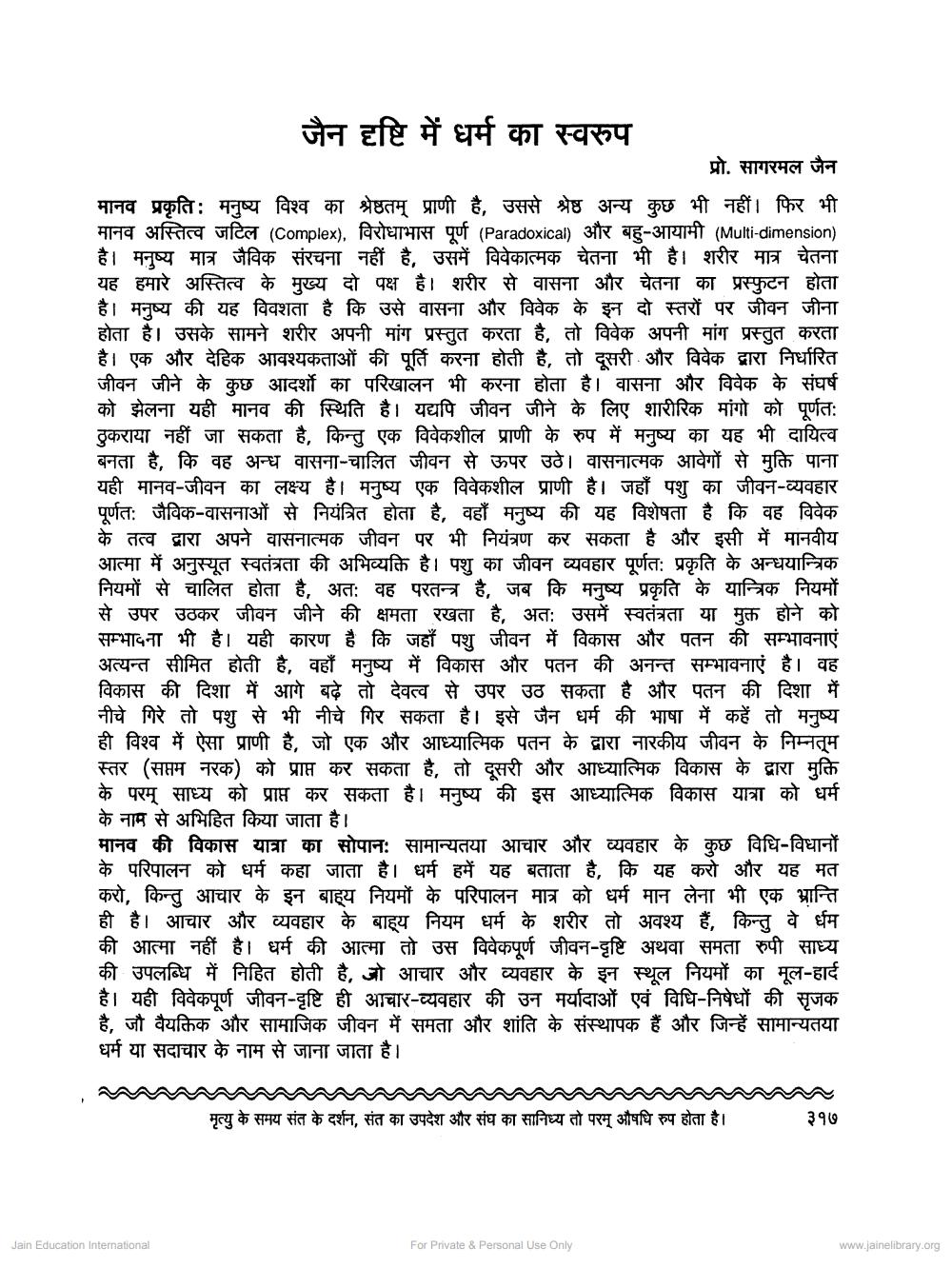________________
जैन दृष्टि में धर्म का स्वरुप
प्रो. सागरमल जैन मानव प्रकृति: मनुष्य विश्व का श्रेष्ठतम् प्राणी है, उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। फिर भी मानव अस्तित्व जटिल (Complex), विरोधाभास पूर्ण (Paradoxical) और बहु-आयामी (Multi-dimension) है। मनुष्य मात्र जैविक संरचना नहीं है, उसमें विवेकात्मक चेतना भी है। शरीर मात्र चेतना यह हमारे अस्तित्व के मुख्य दो पक्ष है। शरीर से वासना और चेतना का प्रस्फुटन होता है। मनुष्य की यह विवशता है कि उसे वासना और विवेक के इन दो स्तरों पर जीवन जीना होता है। उसके सामने शरीर अपनी मांग प्रस्तुत करता है, तो विवेक अपनी मांग प्रस्तुत करता है। एक और देहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होती है, तो दूसरी और विवेक द्वारा निर्धारित जीवन जीने के कुछ आदर्शों का परिखालन भी करना होता है। वासना और विवेक के संघर्ष को झेलना यही मानव की स्थिति है। यद्यपि जीवन जीने के लिए शारीरिक मांगो को पूर्णत: ठुकराया नहीं जा सकता है, किन्तु एक विवेकशील प्राणी के रुप में मनुष्य का यह भी दायित्व बनता है, कि वह अन्ध वासना-चालित जीवन से ऊपर उठे। वासनात्मक आवेगों से मुक्ति पाना यही मानव-जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। जहाँ पशु का जीवन-व्यवहार पूर्णत: जैविक-वासनाओं से नियंत्रित होता है, वहाँ मनुष्य की यह विशेषता है कि वह विवेक के तत्व द्वारा अपने वासनात्मक जीवन पर भी नियंत्रण कर सकता है और इसी में मानवीय आत्मा में अनुस्यूत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। पशु का जीवन व्यवहार पूर्णत: प्रकृति के अन्धयान्त्रिक नियमों से चालित होता है, अत: वह परतन्त्र है, जब कि मनुष्य प्रकृति के यान्त्रिक नियमों से उपर उठकर जीवन जीने की क्षमता रखता है, अत: उसमें स्वतंत्रता या मुक्त होने को सम्भावना भी है। यही कारण है कि जहाँ पशु जीवन में विकास और पतन की सम्भावनाएं अत्यन्त सीमित होती है, वहाँ मनुष्य में विकास और पतन की अनन्त सम्भावनाएं है। वह विकास की दिशा में आगे बढ़े तो देवत्व से उपर उठ सकता है और पतन की दिशा में नीचे गिरे तो पशु से भी नीचे गिर सकता है। इसे जैन धर्म की भाषा में कहें तो मनुष्य ही विश्व में ऐसा प्राणी है, जो एक और आध्यात्मिक पतन के द्वारा नारकीय जीवन के निम्नत्म स्तर (सप्तम नरक) को प्राप्त कर सकता है, तो दूसरी और आध्यात्मिक विकास के द्वारा मुक्ति के परम् साध्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की इस आध्यात्मिक विकास यात्रा को धर्म के नाम से अभिहित किया जाता है। मानव की विकास यात्रा का सोपान: सामान्यतया आचार और व्यवहार के कुछ विधि-विधानों के परिपालन को धर्म कहा जाता है। धर्म हमें यह बताता है, कि यह करो और यह मत करो, किन्तु आचार के इन बाह्य नियमों के परिपालन मात्र को धर्म मान लेना भी एक भ्रान्ति ही है। आचार और व्यवहार के बाह्य नियम धर्म के शरीर तो अवश्य हैं, किन्तु वे र्धम की आत्मा नहीं है। धर्म की आत्मा तो उस विवेकपूर्ण जीवन-दृष्टि अथवा समता रुपी साध्य की उपलब्धि में निहित होती है, जो आचार और व्यवहार के इन स्थूल नियमों का मूल-हार्द है। यही विवेकपूर्ण जीवन-दृष्टि ही आचार-व्यवहार की उन मर्यादाओं एवं विधि-निषेधों की सूजक है, जौ वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समता और शांति के संस्थापक हैं और जिन्हें सामान्यतया धर्म या सदाचार के नाम से जाना जाता है।
मृत्यु के समय संत के दर्शन, संत का उपदेश और संघ का सानिध्य तो परम् औषधि रुप होता है।
३१७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org